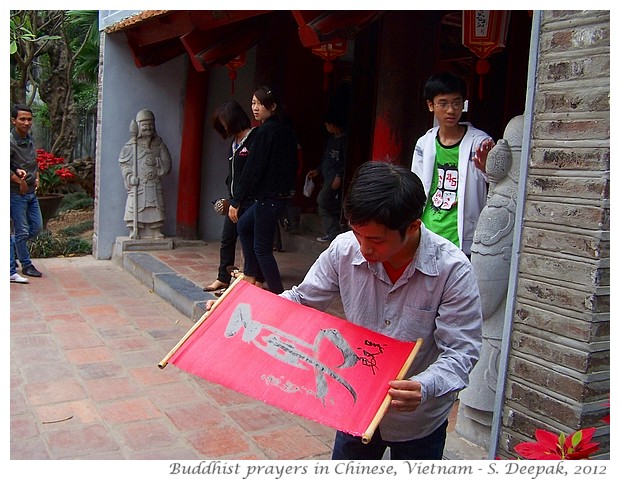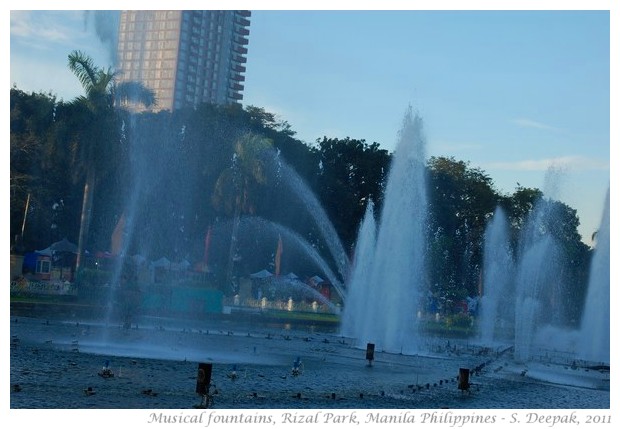प्रोफेसर अलेसाँद्रा कोनसोलारो उत्तरी इटली में तोरीनो (Turin) शहर में विश्वविद्यालय स्तर पर हिन्दी की प्रोफेसर हैं. उन्होंने बात उठायी मेरे एक 2007 में लिखे आलेख की जिसमें मैंने हिन्दी पत्रिका हँस में तीन हिस्सों में छपी हिन्दी के जाने माने लेखक पँकज बिष्ट की कहानी "पँखोंवाली नाव" की बात की थी. अलेसाँद्रा ने मुझसे पूछा कि क्या यह कहानी कहीं से मिल सकती है? इस कहानी में दो मित्र थे, जिनमें से एक समलैंगिक था. मैंने अपने आलेख में एक ओर तो बिष्ट जी द्वारा समलैंगिकता के विषय को छूने का साहस करने की सराहना की थी, वहीं मुझे यह भी लगा था कि इस कहानी में समलैंगिकता को "बाहर" या "विषमलैंगिक" दृष्टि से देखा सुनाया गया है, उसमें कथा के समलैंगिक पात्र के प्रति आत्मीयता कम है.
जहाँ तक मुझे मालूम है, बीच में कुछ समय तक हँस में छपी सामग्री इंटरनेट पर भी मिल जाती थी, लेकिन बहुत समय यह बन्द है. मेरे पास 2007 के हँस के कुछ अंक हैं लेकिन यह कहानी पूरी नहीं है, उसका बीच का भाग जो सितम्बर 2007 के हँस में छपा था, वह नहीं है. क्या आप में कोई सहायता कर सकता है या कोई तरीका है सितम्बर 2007 अंक से इस कहानी को पाने का? अगर किसी के पास हँस का वह अंक हो तो उसे स्कैन करके मुझे भेज सकता है.
अलेसाँद्रा के कुछ अन्य प्रश्न भी थे - हिन्दी में समलैंगिकता-अंतरलैंगिकता के विषय पर कौन सी महत्वपूर्ण कहानियाँ और उपन्यास हैं? हिन्दी में समलैंगिक या अंतरलैंगिक लेखक या लेखिकाएँ हैं? अगर हाँ तो वह इस विषय पर क्या लिख रहे हैं?
अलेसाँद्रा के इन प्रश्नों का मेरे पास कोई उत्तर नहीं. इंटरनेट पर खोजने से कुछ नहीं मिला. क्या आप में कोई इस विषय में हमारी सहायता कर सकता है यह जानकारी एकत्रित करने के लिए कि इस विषय पर किस तरह का लेखन हिन्दी में है और हो सके तो उनके लेखकों से सम्पर्क कराने के लिए?

पिछले दशकों में लेखन और साहित्य विधाओं में सच्चेपन (authenticity) और "जिसकी आपबीती हो वही अपने बारे में लिखे" की बातें उठी हैं. इस तरह से साहित्य में नारी लेखन, शोषित जनजातियों के लोगों के लेखन, दलित समाज के लोगों के लेखन, जैसी विधाएँ बन कर मज़बूत हुई हैं. इन्हीं दबे और हाशिये से बाहर किये गये जन समूहों में समलैंगिक तथा अंतरलैंगिक व्यक्ति समूह भी हैं, जिनके लेखन की अलग साहित्यिक विधा बनी गयी है जिसे अंग्रेज़ी में क्वीयर लेखन (Queer writings) कहते हैं. शब्दकोश के अनुसार "क्वीयर" का अर्थ है विचित्र, अनोखा, सनकी या भिन्न. यानि अगर बात लोगों के बारे में हो रहे हो तो इसका अर्थ हुआ आम लोगों से भिन्न. लेकिन अँग्रेज़ी में "क्वीयर" का आधुनिक उपयोग "यौनिक भिन्नता" की दृष्टि से किया जाता है. तो इस तरह के लेखन को बजाय "समलैंगिक-अंतरलैंगिक लेखन" कहने के बजाय हम "यौनिक भिन्न लेखन" भी कह सकते हैं. पश्चिमी देशों में विश्वविद्यालय स्तर पर जहाँ साहित्य की पढ़ायी होती है, तो उसमें साहित्य के साथ साथ, नारी लेखन, जनजाति लेखन, यौनिक भिन्न लेखन, विकलाँग लेखन, जैसे विषयों की पढ़ायी भी होती है.
नारी लेखन, दलित या जन जाति लेखन जैसे विषयों पर मैंने हँस जैसी पत्रिकाओं में या कुछ गिने चुने ब्लाग में पढ़ा है. लेकिन हिन्दी में विकलाँगता लेखन या समलैंगिक लेखन, इसके बारे में नहीं पढ़ा.
बहुत से लोग, लेखकों और लेखन को इस तरह हिस्सों में बाँटने से सहमत नहीं हैं. उनका कहना है कि लेखन केवल आपबीती नहीं होता, कल्पना भी होती है. अगर हम यह कहने लगें कि लेखक केवल अपनी आपबीती पर ही लिखे तो दुनिया के सभी प्रसिद्ध लेखकों का लिखना बन्द जाये. खुले समाज में जहाँ जन समान्य निर्धारित करे कि जो आप ने लिखा है वह पढ़ने लायक है या नहीं, उसे लोग खरीद कर पढ़ना चाहते हें या नहीं, यही लेखन की सार्थकता की सच्ची कसौटी है.
दूसरी ओर यह भी सच है कि समाज के हाशिये से बाहर किये और शोषित लोगों की आवाज़ों को शुरु से ही इतना दबाया जाता है कि वह आवाज़ें मन में ही घुट कर रह जाती हैं, कभी निकलती भी हैं तो इतनी हल्की कि कोई नहीं सुनता. आधा सच जैसे प्रयास भी अक्सर हर ओर से चारदीवारियों में घेर कर बाँध दिये जाते हैं जिन पर उन चारदीवारों से बाहर चर्चा न के बराबर होती है. इस स्थिति में यौनिक भिन्न लेखन की बात करके उन आवाज़ों को पनपने और बढ़ने का मौका देना आवश्यक है. जब उन आवाज़ों में आत्मविश्वास आ जाता है तो वह खुले समाज में अन्य लेखकों की तरह सबसे खुला मुकाबला कर सकती हैं.
रुथ वनिता तथा सलीम किदवाई द्वारा सम्पादित अँग्रेज़ी पुस्तक "भारत में समलैंगिक प्रेम - एक साहित्यिक इतिहास" ("Same sex love in India - a literary history" edited by Ruth Vanita and Saleem Kidwai, Penguin India, 2008) कुछ आधुनिक लेखकों की रचनाओं की बात करती है.
रुथ से मैंने पूछा कि अगर कोई लेखक जो स्वयं को समलैंगिक/द्विलैंगिक/अंतरलैंगिक न घोषित करते हुए भी यौनिक भिन्नता के बारे में लिखें तो क्या उसे "यौनिक भिन्न साहित्य" माना जायेगा?
तो रुथ ने कहा कि "यह इस बात पर भी निर्भर करेगा कि आप "क्वीयर" को किस तरह परिभाषित करते हैं? मेरे विचार में इस विषय पर कोई भी लिखे, चाहे वह स्वयं को यौनिक रूप से भिन्न परिभाषित करे या न करे, वह स्वीकृत होगा. किसकी यौनता क्या है, यह हम कैसे जान सकते हैं? इस विषय पर बहुत से हिन्दी लेखकों ने लिखा है जैसे कि राजेन्द्र यादव,निराला, उग्र तथा विषेशकर, विजयदान देथा जिन्होंने राजस्थानी में लिखा, उस सब को "समलैंगिक साहित्य" कह सकते हैं. चुगताई का लिखा जैसे कि "तेरही लकीर" के हिस्से और "लिहाफ़" भी इसी श्रेणी में आता है, हालाँकि यह उर्दू में लिखे गये. हरिवँश राय बच्चन की आत्मकथा, "क्या भूलूँ क्या याद करूँ" में वह भाग है जिसके बारे में नामवर सिंह ने कहा था कि वह एक पुरुष का दूसरे पुरुष के लिए प्रेम की स्पष्ट घोषणा थी."
यह जान कर अच्छा लगा कि हिन्दी-उर्दू जगत में जाने माने लेखकों ने इस विषय को छूने का साहस किया है, आज से नहीं, बल्कि कई दशकों से यह हो रहा है. लेकिन मैंने सोचा कि रूथ के दिये सभी उदाहरण कम से कम 1960-70 के दशक से पहले के हैं. जबकि मुझे अपने प्रश्न का उत्तर नहीं मिला कि, पिछले तीस चालिस सालों में यौनिक भिन्नता की दृष्टि से, पँकज बिष्ट की हँस में छपी कहानी "पँखवाली नाव" के अतिरिक्त क्या कुछ अन्य लिखा गया?
इस बहस में एक अन्य दिक्कत है जो कि साँस्कृतिक है और मूल सोच के अन्तरों से जुड़ी हुई है. पश्चिमी विचारक, कोई भी विषय हो, चाहे विज्ञान या दर्शन, वनस्पति या मानव यौन पहचान, वे हमेशा हर वस्तु, हर सोच को श्रेणियों में बाँटते हैं. जबकि भारतीय परम्परा के विचारक में हर वस्तु, हर सोच में समन्वय की दृष्टि देखते हैं. इस तरह से बहुत से यौनिक मानव व्यवहार हैं जिन्हें भारतीय समाज ने समलैंगिक-अंतरलैंगिक-द्वीलैंगिक श्रेणियों में नहीं बाँटा. जैसे कि महाभारत में चाहे वह शिखण्डी के लिँग बदलाव की कथा हो या अर्जुन का वर्ष भर नारी बन के जँगल घूमना हो, इन कथाओं में परम्परागत भारतीय विचारकों ने यौनिक भिन्नता की परिभाषाएँ नहीं खोजीं. तो सँशय उठता है कि हिन्दी में "क्वीयर साहित्य" की पहचान करना, भारतीय सोच और दर्शन को पश्चिमी सोच के आईने में टेढ़ा मेढ़ा करके बिगाड़ तो नहीं देगा?
इसी भारतीय तथा पश्चिमी सोच के अन्तर के विषय पर एक अन्य उदाहरण श्री अमिताव घोष की अंगरेज़ी में लिखी पुस्तक "सी आफ पोप्पीज़" (Sea of poppies) है जिसमें एक पात्र हैं बाबू नबोकृष्णो घोष जो तारोमयी माँ के भक्त हैं और इसी भक्ति में लीन हो कर स्वयं को माँ तारोमयी का रूप समझते हैं. इस पात्र की कहानी को केवल अंतरलैंगिकता या समलैंगिकता के रूप में देखना, उसकी साँस्कृतिक तथा आध्यात्मिक जटिलता का एकतरफ़ा सरलीकरण होगा जिससे पात्र को केरिकेचर सा बना दिया जायेगा. इसलिए भारतीय भाषाओं में "क्वीयर लेखन" की बहस में इस बात पर ध्यान रखना भी आवश्यक है.
जैसे रुथ ने कहा कि कोई भी इस विषय पर अच्छा लिखे, तो अच्छी बात है और उसे सराहना चाहिये. लेकिन मेरी नज़र में यह उतना ही महत्वपूर्ण कि स्वयं को "यौनिक भिन्न" स्वीकारने वाले लोग भी लिखें. भारतीय समाज ने अक्सर इस दिशा में बहुत संकीर्ण दृष्टिकोण लिया है. इस सारी बहस को अनैतिक, गैरकानूनी व अप्राकृतिक कह कर समाज ने लाखों व्यक्तियों को शर्म और छुप छुप कर जीने, अन्याय सहने, घुट घुट कर मरने के लिए विवश किया है. पिछले दशक में इस बारे में कुछ बात खुल कर होने लगी है. ओनीर की "माई ब्रदर निखिल" और "आई एम" जैसी फ़िल्मों ने इस बहस को अँधेरे से रोशनी में लाने की कोशिश की है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध लेखक विक्रम सेठ ने अपने द्विलैंगिक होने के बारे में लिखा है. इस तरह से अगर यौनिक भिन्न लोग अपनी भिन्नता को स्वीकारते हुए लिखेंगे तो इस विषय को शर्म और अँधेरे में छुपे रहने से बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा.
आज की दुनिया में अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए ब्लाग सबसे आसान माध्यम है. बड़े शहरों में और अंग्रेज़ी बोलने वाले युवक युवतियों ने ब्लाग की तकनीक का लाभ उठा कर "भिन्न यौनिक" ब्लाग बनाये हैं, जैसे कि आप इन तीन उदाहरणों में देख सकते हैं - एक, दो, तीन.
यह जान कर अच्छा लगा कि हिन्दी-उर्दू जगत में जाने माने लेखकों ने इस विषय को छूने का साहस किया है, आज से नहीं, बल्कि कई दशकों से यह हो रहा है. लेकिन मैंने सोचा कि रूथ के दिये सभी उदाहरण कम से कम 1960-70 के दशक से पहले के हैं. जबकि मुझे अपने प्रश्न का उत्तर नहीं मिला कि, पिछले तीस चालिस सालों में यौनिक भिन्नता की दृष्टि से, पँकज बिष्ट की हँस में छपी कहानी "पँखवाली नाव" के अतिरिक्त क्या कुछ अन्य लिखा गया?
इस बहस में एक अन्य दिक्कत है जो कि साँस्कृतिक है और मूल सोच के अन्तरों से जुड़ी हुई है. पश्चिमी विचारक, कोई भी विषय हो, चाहे विज्ञान या दर्शन, वनस्पति या मानव यौन पहचान, वे हमेशा हर वस्तु, हर सोच को श्रेणियों में बाँटते हैं. जबकि भारतीय परम्परा के विचारक में हर वस्तु, हर सोच में समन्वय की दृष्टि देखते हैं. इस तरह से बहुत से यौनिक मानव व्यवहार हैं जिन्हें भारतीय समाज ने समलैंगिक-अंतरलैंगिक-द्वीलैंगिक श्रेणियों में नहीं बाँटा. जैसे कि महाभारत में चाहे वह शिखण्डी के लिँग बदलाव की कथा हो या अर्जुन का वर्ष भर नारी बन के जँगल घूमना हो, इन कथाओं में परम्परागत भारतीय विचारकों ने यौनिक भिन्नता की परिभाषाएँ नहीं खोजीं. तो सँशय उठता है कि हिन्दी में "क्वीयर साहित्य" की पहचान करना, भारतीय सोच और दर्शन को पश्चिमी सोच के आईने में टेढ़ा मेढ़ा करके बिगाड़ तो नहीं देगा?
इसी भारतीय तथा पश्चिमी सोच के अन्तर के विषय पर एक अन्य उदाहरण श्री अमिताव घोष की अंगरेज़ी में लिखी पुस्तक "सी आफ पोप्पीज़" (Sea of poppies) है जिसमें एक पात्र हैं बाबू नबोकृष्णो घोष जो तारोमयी माँ के भक्त हैं और इसी भक्ति में लीन हो कर स्वयं को माँ तारोमयी का रूप समझते हैं. इस पात्र की कहानी को केवल अंतरलैंगिकता या समलैंगिकता के रूप में देखना, उसकी साँस्कृतिक तथा आध्यात्मिक जटिलता का एकतरफ़ा सरलीकरण होगा जिससे पात्र को केरिकेचर सा बना दिया जायेगा. इसलिए भारतीय भाषाओं में "क्वीयर लेखन" की बहस में इस बात पर ध्यान रखना भी आवश्यक है.
जैसे रुथ ने कहा कि कोई भी इस विषय पर अच्छा लिखे, तो अच्छी बात है और उसे सराहना चाहिये. लेकिन मेरी नज़र में यह उतना ही महत्वपूर्ण कि स्वयं को "यौनिक भिन्न" स्वीकारने वाले लोग भी लिखें. भारतीय समाज ने अक्सर इस दिशा में बहुत संकीर्ण दृष्टिकोण लिया है. इस सारी बहस को अनैतिक, गैरकानूनी व अप्राकृतिक कह कर समाज ने लाखों व्यक्तियों को शर्म और छुप छुप कर जीने, अन्याय सहने, घुट घुट कर मरने के लिए विवश किया है. पिछले दशक में इस बारे में कुछ बात खुल कर होने लगी है. ओनीर की "माई ब्रदर निखिल" और "आई एम" जैसी फ़िल्मों ने इस बहस को अँधेरे से रोशनी में लाने की कोशिश की है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध लेखक विक्रम सेठ ने अपने द्विलैंगिक होने के बारे में लिखा है. इस तरह से अगर यौनिक भिन्न लोग अपनी भिन्नता को स्वीकारते हुए लिखेंगे तो इस विषय को शर्म और अँधेरे में छुपे रहने से बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा.
आज की दुनिया में अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए ब्लाग सबसे आसान माध्यम है. बड़े शहरों में और अंग्रेज़ी बोलने वाले युवक युवतियों ने ब्लाग की तकनीक का लाभ उठा कर "भिन्न यौनिक" ब्लाग बनाये हैं, जैसे कि आप इन तीन उदाहरणों में देख सकते हैं - एक, दो, तीन.
जहाँ तक मुझे मालूम है, हिन्दी का केवल एक चिट्ठा है "आधा सच" जिसपर कुछ किन्नर या अंतरलैंगिक व्यक्ति अपनी बात कहते हैं. क्या इसके अतिरिक्त क्या कोई अन्य हिन्दी, मैथिली, भोजपुरी, अवधी, राजस्थानी आदि में इस तरह के अन्य चिट्ठे हैं? क्या स्थानीय स्तरों पर भारत के छोटे शहरों में, कस्बों में भी इस विषय पर लोगों ने कुछ लिखने की हिम्मत की है? क्या कुछ अंडरग्राइड पत्रिकाएँ या किताबें छपी हैं इस विषय पर?
यह नहीं कि चिट्ठों पर इस विषय पर लिखने मात्र से वह "यौनिक भिन्न" साहित्य हो जायेगा. साहित्य होने के लिए उसे साहित्य के मापदँडों पर भी खरा उतरना होगा, लेकिन शायद उन्हें शुरुआत की तरह से तरह से देखा जा सकता है जहाँ कल के "यौनिक भिन्न" साहित्य जन्म ले सकते हैं.
अगर आप के पास इस बारे में कोई जानकारी है तो कृपया मुझसे ईमेल से सम्पर्क कीजिये या नीचे टिप्पणीं छोड़िये. इस सहायता के लिए आप को पहले से ही मेरा धन्यवाद.
आप मुझसे ईमेल के माध्यम से सम्पर्क कर सकते हैं. मेरा ईमेल पता है sunil.deepak(at)gmail.com (ईमेल भेजते समय "(at)" को हटा कर उसकी जगह "@" को लगा दीजिये)
यह नहीं कि चिट्ठों पर इस विषय पर लिखने मात्र से वह "यौनिक भिन्न" साहित्य हो जायेगा. साहित्य होने के लिए उसे साहित्य के मापदँडों पर भी खरा उतरना होगा, लेकिन शायद उन्हें शुरुआत की तरह से तरह से देखा जा सकता है जहाँ कल के "यौनिक भिन्न" साहित्य जन्म ले सकते हैं.
अगर आप के पास इस बारे में कोई जानकारी है तो कृपया मुझसे ईमेल से सम्पर्क कीजिये या नीचे टिप्पणीं छोड़िये. इस सहायता के लिए आप को पहले से ही मेरा धन्यवाद.
आप मुझसे ईमेल के माध्यम से सम्पर्क कर सकते हैं. मेरा ईमेल पता है sunil.deepak(at)gmail.com (ईमेल भेजते समय "(at)" को हटा कर उसकी जगह "@" को लगा दीजिये)
***