आजकल वेनिस द्वीवार्षिकी कला प्रदर्शनी (Biennale) चल रही है। लेकिन चाह कर भी उसे देखने नहीं गया, क्योंकि प्रदर्शनी बहुत फ़ैले हुए क्षेत्र में लगती है जिससे वहाँ चलना बहुत पड़ता है और मेरे घुटने दुखने लगते हैं। लेकिन प्रमुख प्रदर्शनी के साथ-साथ वेनिस शहर में बहुत सी अन्य छोटी-बड़ी कला प्रदर्शनियाँ भी लगती हैं, जिन्हें देखना मेरे लिए अधिक आसान है। ऐसी ही एक कला प्रदर्शनी वेनिस के यूरोपी सांस्कृतिक केन्द्र में लगी तो कुछ दिन पहले मैं उसे देखने गया।
इस आलेख में मैंने आप के लिए अपनी पसंद की कुछ कलाकृतियाँ की लघु-प्रदर्शनी बनाई है।
यूरोपी सांस्कृतिक केन्द्र का भवन तीन
हिस्सों में बंटा है - पालात्ज़ो बैम्बो, पालात्ज़ो मोरो तथा मारिनारेस्सा के
बाग। इसमें कुल मिला कर करीब चालिस कक्ष हैं जिनमें विभिन्न देशों के करीब दो सौ कलाकारों की यह प्रदर्शनी लगी है। यह भवन वेनिस रेलवे स्टेशन से रिआल्तो पुल जाने वाले प्रमुख रास्ते पर है।
इस प्रदर्शनी में चैक रिपब्लिक की एक कलाकृति ने मुझे बहुत प्रभावित किया, देख कर ऐसा लगा मानो किसी ने छाती पर मुक्का मारा हो और साँस नहीं ली जा रही हो। इसलिए मेरे लिए यह इस प्रदर्शनी की सबसे महत्वपूर्ण कलाकृति थी। यह कलाकृति आप को नीचे मेरे आलेख के अंत में मिलेगी।
इस प्रदर्शनी को "व्यक्तिगत संरचनाएँ: सीमाओं से परे" का नाम दिया गया है और यह २४ नवम्बर २०२४ तक चलेगी। इसे देखने के लिए कोई टिकट नहीं चाहिये। अगर आप इन दिनों में वेनिस आ रहे हैं और आप को कला में रुचि है, तो इस प्रदर्शनी को अवश्य देखें।
नीचे की सभी कलाकृतियों की तस्वीरों पर क्लिक करके आप उन्हें बड़ा करके देख सकते हैं। तो आईये चलते हैं मेरी यह लघु कला प्रदर्शनी देखने।
ग्रीस के कोसतिस ज्योर्जो (Kostis Georgiou) की कलाकृतियाँ
यह पहली दो कलाकृतियाँ भवन में घुसने से पहले, उसके सामने वाले बाग में दिखती है। एलुमिनियम की बनी मानव मूर्तयों को उन्होंने लाल रंग से रंगा है। एक में दो आकृतियाँ एक चक्र के ऊपर हवा में टिकी हैं, दूसरी में एक सीढ़ी के आसपास चार आकृतियाँ ऊपर नीचे हैं। कुछ रंग की वजह से, कुछ आकृतियों का हवा में तैरना और खेलना, मुझे अच्छा लगा। अगर आप कोसतिस के वेब-स्थल वाली लिंक पर देखेंगे तो वहाँ लाल रंग से इस तरह की अन्य अनेक कलाकृतियाँ देख सकते हैं।
अमरीका की अलकनंदा मुखर्जी (Alakananda Mukerjin) की कला
अलकनंदा की जल-रंगों कि विभिन्न चित्रकला इस प्रदर्शनी में दिखी। मुझे यह विषेश नहीं भाईं, कुछ बेतरतीब सी लगीं, लेकिन साथ ही लगा कि उनकी आकृतियों में मकबूल फिदा हुसैन साहब की आकृतियों की प्रेरणा दिखती है। क्या आप को भी ऐसा लगता है?
आस्ट्रेलिया की एनेट्टे गोल्डन (Annette Golden) की चित्रकला
प्रदर्शनी में एनेट्ट की कलाकृतियों के लिए एक पूरा कमरा था जिसमें उनकी बीस-पच्चीस कलाकृतियाँ लगी थीं। वह एक्रेलिक, तेल-रंग और धातुओं की पत्तियाँ लगा कर केनवास पर कलाकृतियाँ बनाती हैं, जिनमें रंगबिरंगे विभिन्न नारी स्वरूप दिखते हैं। उन्हीं में से एक कलाकृति प्रस्तुत है जिसकी काली पृष्ठभूमि पर लाल और नीले रंगों से बनी युवती मुझे अच्छी लगी।
न्यूज़ीलैंड तथा भारत के अरीज़ कटकी (Areez Katki) का इस्टालेशन
अरीज़ पारसी हैं और उनके इंस्टालेशन में रुमालों में ज़राथुस्त्रा गाथा के सतरह हा (टुकड़े या हिस्से) दिखते हैं। रुमालों पर उन्होंने चित्र बना कर, उन्हें धागों से छत से लटकाया था। पीछे खिड़की से आती वेनिस की रोशनी और और वहाँ से दिखते भवनों के साथ उनके प्राचीन धर्म ग्रंथ का चित्रण मुझे अच्छा लगा हालाँकि उन चित्रों में कौन सी कहानी थी, यह समझ नहीं आया।
अमरीका के ब्रायन माक (Brian J. Mac) की वास्तुकला की कलाकृति
ब्रायन माक अमरीकी वास्तुकार हैं। अपने २७ सालों के वास्तुकार कार्य के हर साल उन्होंने एक डिब्बा बनाया जिसमें उनके रेखाचित्र, मॉडल, इत्यादि तोड़-मोड़ कर घुसा दिये। एक तरह से उनका पूरा कार्यजीवन इस तरह से उनकी कलाकृति में दिखता है। इसे देखते हुए मैं सोच रहा था कि हमारी हर चीज़ के साथ हमारी यादें जुड़ी होती हैं, कि इसे वहाँ से खरीदा था, इसे वैसे बनाया था, आदि, लेकिन हमारे बाद हमारी यादों की कोई कीमत नहीं रहती, उस सब सामान को कूड़े की तरह फ़ैंक देते हैं। इस दृष्टि से यह कलाकृति मुझे यादों का व्यक्तिगत स्मारक लगी।
रोमेनिया की कालिन टोपा (Calin Topa) और अदा गालेस (Ada Gales) की इन्स्टालेशन
कालिन स्वरों और ध्वनि की कलाकार है, उन्होंने इस प्रदर्शनी में एक लाल रोशनी वाला एक गलियारा बनाया, और जिसे स्वरों से भरा है। उस गलियारे की दीवारों पर अदा ने अपने शब्द लिखे हैं, और इस तरह से दोनों की कला-दृष्टि का संगम हुआ। मैं आप को कालिन की ध्वनि नहीं महसूस करा सकता लेकिन अदा के विभिन्न वाक्यों में से जो शब्द मैंने चुने हैं उनमें लिखा है, "मैं कभी कला बनाना चाहती हूँ और कभी थाई नूडल खाना चाहती हूँ"।
स्विटज़रलैंड की केरोल कोहलर (Carole Kohler) की लुकन-छिपाई
केरोल कोहलर ने कपड़े उतराते हुए व्यक्तियों की मूर्तियाँ बनायी थीं और कोलाज बनाये थे जिन्हें ३-डी चश्में से देखो तो उनके भीतर छुपी हुई आकृतियाँ दिखती थीं। मैं आप को वे छिपी हुई आकृतियाँ नहीं दिखा सकता लेकिन आप उनकी कपड़े उतारने वालों की मूर्तियों की एक झलक देख सकते हैं। सब मूर्तियों में बनियान या कमीज उतारने वालों के कपड़े से चेहरे छिप गये हैं, अवश्य इसका कोई प्रतीकात्मक अर्थ है, जैसे बच्चे अपना चेहरा ढक कर सोचते हैं कि उन्हें कोई नहीं देख सकता। या शायद, कलाकार कहना चाहता है कि हम कड़वी सच्चाई देखने से डरते हैं और उनसे अपना मुँह चुराते हैं।
स्विटज़रलैंड के क्रिस्टोफ स्टुकेलबर्गर (Christoph Stuckelberger) की जड़ें
स्टुकेलबर्गर हर वस्तु के नयी तरह से देखने के लिए कहते हैं। उनकी कलाकृतियों के लिए एक पूरा कक्ष था जिसमें वस्तुओ के भितर से बाहर, या नीचे से ऊपर, उल्टा दिखाया गया था। इस तस्वीर में आप उनकी "जड़ें" देख सकते हैं जो आपस में एक दूसरे के ऊपर-नीचे जा कर एक जाल बनाती हैं। जिस वस्तु को एक तरह से देखने की आदत हो, जब वह उससे भिन्न दिखे तो हमें रुकने और सोचने के लिए नया दृष्टिकोण देती है।
हंगरी के डेविड सज़ेंतग्रोती (David Szengroti) की अमूर्त चित्रकला
प्रदर्शनी में बहुत सी अमूर्त चित्रकला के नमूने थे जो मुझे अच्छे लगे। मैंने उनमें से इस लघु-प्रदर्शनी के लिए हंगरी के चित्रकार सज़ेंतग्रोती की तीन चित्रकलाओ को चुन कर उनकी एक मिली-जुली तस्वीर बनायी है। ऐसी कलाकृतियों के सामने मैं लम्बे समय तक खड़ा रह कर उन्हें देख सकता हूँ। इसमें रंगो का चुनाव, उनके आपस में सम्बंध, उनमें दिखती अमूर्त आकृतियाँ, सब का असर मिल जुल कर मुझे बहुत सुंदर लगा।
बेल्जियम की जाँन ओपगेन्होफ्फेन (Jeanne Opgenhoffen) की सिरामिक कला
ज़ाँन अपने सिरामिक के काम के लिए जानी जाती हैं। उनकी जिस कलाकृति को मैंने इस आलेख के लिए चुना है उसके लिए उन्होंने पहले महीन सेरामिक के चिप्स जैसे आकार के टुकड़े बनाये, फ़िर उन सबको जोड़ कर यह अमूर्त चित्र बनाये, जिनमें रंगों और अकृतियों का मेल मुझे बहुत अच्छा लगा। इसे देख कर सोचना कि इसे बनाने में उन्हें कितना समय और मेहनत लगी होगी, से इसकी सुंदरता और भी महत्वपूर्ण लगती है। इस तस्वीर पर क्लिक करके इसे बड़ा करके देखिये तब इसकी सुंदरता दिखेगी।
सीरिया-फिलिस्तीन के खैर अलाह सलीम (Khair Alah Salim) की चित्रकला
सलीम फिलिस्तीनी हैं और सीरिया में रहते हैं, उनकी केनवास पर एक्रेलिक से बनी इस तस्वीर की उदास मुस्कान वाली युवती मुझे बहुत अच्छी लगी। लगता है जैसे उसका चेहरा एक अंडे के छिलके के ऊपर बना है जिसमें दरारें पड़ रही हैं, जिनसे उसकी उदासी और भी गहरी हो जाती है।
फ्राँस के निकोलास लावारेन्न (Nicolas Lavarenne) और कोरीन फन्कन (Corin Funken) की कलाकृतियाँ
निकोलास ने रेज़िन से सोती हुई युवती की शिल्पकला बनाई है जिसकी बाजू नीचे, कोरीन की चित्रकला के सामने लडक रही है। निकोलास की मूर्ति छत पर लोहे के हैम्मोक पर झूल रही है, जबकि कोरीन की चित्रकला में वेनिस शहर के समुद्र से जुड़ी बातों-घटनाओं का चित्रण है जिसे उन्होंने "हमारा समुद्र" का नाम दिया है। मुझे कोरीन की चित्रकला कुछ विषेश नहीं लगी लेकिन निकोलास की मूर्ति के चेहरे का भाव और उनका कक्ष में छत पर तैरना बहुत अच्छे लगे।
नाईजीरिया की ओर्री शेनजोबी (Orry Shenjobi) की आ-वाम-बे पार्टी
ओर्री की कलाकृतियों का एक पूरा कक्ष है जिसमें दीवारों पर उन्होंने वहाँ की पाराम्परिक पार्टी जिसे आ-वाम-बे कहते हैं, में भाग लेने वालों की तस्वीरों के ऊपर से विभिन्न चीज़ो को जॊड़ कर कोलाज जैसे बनाये हैं। उनकी कलाकृति ऊर्जा, रंगों और आनंद लेते हुए लोगों से भरी हुई है। इस कक्ष में बहुत देर तक रुका। नीचे वाली तस्वीर में आप को उस कक्ष की दो दीवारों के हिस्से दिखेंगे। इस तस्वीर पर भी क्लिक करके उसे बड़ा करके देखिये, तब दिखेगा कि किस तरह उन्होंने तस्वीरों पर अन्य वस्तुओं को जोड़ कर कैसे कोलाज बनाये हैं।
चिल्ली की पेटरिशिया टोरो रिब्बेक (Patricia Toro Ribbeck) की मिठाईयाँ
दक्षिण अमरीका की इस कलाकार ने रंग-बिरंगी चमकती हुई सिरामिक से तरह-तरह के केक, पेस्ट्रियाँ और मिठाईयाँ बनाई हैं, जिन्हें देख कर भूख लग जाती है। मेरे विचार में यह कलाकृति जिस घर में रहेगी वहाँ रहने वाले लोग डाईटिन्ग नहीं कर सकते। वह कहती हैं कि इसे उन्हें कोविड के समय में घर में बन्द रहने के समय बनाया था क्योंकि उस समय वह सुंदर सपने देखना चाहती थीं।
फिलीपीनी कलाकारों का कक्ष
प्रदर्शनी में एक कक्ष में बहुत सारे फिलीपीनी कलाकारों की कलाकृतियाँ थीं। मुझे उनमें से कई कलाकृतियाँ अच्छी लगीं लेकिन उदाहरण के लिए मैंने उनमें से दो कलाकृतियाँ चुनी हैं। पहली चित्रकला डेमी पाडुवा की है और दूसरी चित्रकला सेड्रिक डेला पाज़ की है, दोनों कलाकृतियाँ केनवास पर एक्रेलिक रंगों से बनाई गई हैं।
प्रिन्सटन विश्वविद्यालय के फ़िल्म-शोध स्टूडियो की तस्वीरें
यह वाला कक्ष अमरीकी श्याम वर्ण के लोगों के संघर्ष के बारे में बना है। इसमें एक और हज़ारों छोटी-छोटी तस्वीरों को मिला कर कम्प्यूटर से चित्र बनाये थे जिनमें दूर से देखो तो उनमें जाने-पहचाने व्यक्तियों के चेहरे दिखतॆ थे। जैसे कि नीचे वाली तस्वीर अमरीकी अभिनेता जोर्डन पील की है, जिसे ध्यान से देखेंगे तो यह बहुत सी छोटी तस्वीरों को जोड़ कर बनाई गई है। इस तस्वीर पर क्लिक करके उसे बड़ा करके देखिये कि पील का चेहरा कैसे बनाया गया है।
सेशैल के रायन शैट्टी (Ryan Shetty) की तैरते हुए घर
रायन ने इस कक्ष में विभिन्न इस्टालेशन बनाई थीं। उनमें से मुझे यह तैरते घरों वाला हिस्सा अच्छा लगा। सफेद, चकोर, डिब्बे जैसे कमरों में खिड़कियाँ, सीढ़ियाँ और खम्बे बने हैं। नीचे से रोशनी से पीछे की दीवार पर प्रतिबिम्ब थे और साथ में एक वीडियो इंस्टालेशन भी था (यह सब इस तस्वीर में नहीं दिखते)।
भारत की सोनल अम्बानी (Sonal Ambani) का घायल बैल
सोनल के धातुओं के टुकड़ों को जोड़ कर बना यह बैल देख कर मुझे दिल्ली के चर्खा संग्रहालय में बने शेर की शिल्पकला याद आई जिसे भारत सरकार ने "भारत में बनाईये" कम्पेन के लिए लगाया था। बैल देख कर फाईनेन्शियल और शेयर बाज़ार मार्किट का ध्यान आता है, शायद इसलिए लाल तीरों से घायल यह बैल नहीं है, प्रतीमात्मक गाय है। यह शिल्प स्टील, पीतल और लकड़ी से बना है और उनके अनुसार, यह पुरुष तथा नारी को काम के लिए मिलने वाली पगार की विषमताओं को दर्शाता है। सोनल जी ने इस कलाकृति का नाम दिया है, "बड़े सौभाग्य के तीर और गुलेलें"।
दक्षिण कोरिया के याओ जुई छुंग (Yao Jui Chung) का झंडा
छुंग की इस कलाकृति के रंग यूक्रेन के झंडे के रंगों की याद दिलाते हैं और इस पर बनी दो आकृतियाँ ध्यान खींचती हैं। एक आकृती कुत्ते या सियार जैसी लगती है और दूसरी का चेहरा मानव सा है लेकिन उसके सींग हैं, यानि शैतान है। इसका अर्थ मुझे समझ नहीं आया लेकिन देख कर अच्छा लगा।
चीन के शांग मिंग शेंग (Chang Ming Sheng) की क्वान्टम भौतिकी कला
बाद में पता चला कि कलाकृति का नाम यी जिंग है और कलाकार का नाम शांग मिंग शेंग है। यह वैज्ञानिक तरीके से बालू के कणों को क्वांटम भौतिकी के माध्यम से घुमा कर अपनी कला बनाते हैं जो द्वीरूप और त्रीरूप के बीच में घूमती है। मुझे उनकी कोई बात समझ नहीं आई कि वह क्या करते हैं और क्यों करते हैं, इसलिए उनकी चित्रकला का एक नमूना यहाँ प्रस्तुत है ताकि आप में से बुद्धिमान व्यक्ति इसे समझ कर मुझे भी समझायें।
चेक गणतंत्र के डानिएल पेस्टा (Daniel Pesta) की चोटियाँ
मेरी इस लघु-प्रदर्शनी के अंत में वह कलाकृति प्रस्तुत है जिसने मेरे दिल को गहराई से छुआ। इसे देख कर मुझे बहुत धक्का लगा, मैं वहाँ खड़ा रह गया।
कलाकृति में युवतियों की तीन कटी हुई, खून से सनी हुई चोटियाँ हैं, जिनके नीचे लिखा है, "मेरा खून जंगली था", "मेरा खून गर्म था", और "मेरा खून स्वतंत्र था"। जब लड़की जंगली हो, काबू में न आये, स्वतंत्र जीना चाहे तो अक्सर समाज उन्हें दीवारों और पर्दों के पीछे छुपा देते हैं और फ़िर भी न माने, तो परिवार और धर्म की इज़्ज़त के नाम पर जान से मार देते हैं।
दुनिया भर में लड़कियों और औरतों पर धर्म, संस्कृति और परम्पराओं के नाम पर होने वाले अत्याचारों और बंधनों को दिखाती यह कलाकृति मेरे मन को छू गई। नीचे वाली तस्वीर में मैंने तीनो कलाकृतियों को एक तस्वीर में जोड़ दिया है। इस तस्वीर को क्लिक करके इसे बड़ा करके अवश्य देखें।
इसे देख कर पंजाबी गीत, "काली तेरी गुत ते परांदा तेरा लाल नी" का नया ही अर्थ दिखता है।
अंत में
पिछले दशक से कॉनसैप्ट आर्ट यानि किसी विचार पर आधारित कला का महत्व बढ़ता जा रहा है, जिसमें कलाकार अपनी कला का कौशल नहीं दिखाता बल्कि कला के माध्यम से एक विचार को अभिव्यक्ति देता है। डानियल पेस्टा की कला में लड़कियों की चोटियाँ बनाने का कौशल प्रभावित नहीं करता बल्कि उसके पीछे उनका विचार है कि जो लड़कियाँ हमारे समाज की बात नहीं मानती उनकी चोटियाँ काट कर उनके सिरों को लहु-लुहान कर दो।
कुछ कलाकार वैचारिक-कला के नाम पर आलसपन दिखाते हैं जैसे कि कोई कुछ टूटी ईंटों को रख कर, उसे "टूटे सपने" नाम की कलाकृति बताईये। लेकिन चेक कलाकार डानियल की इस कलाकृति को देख कर मुझे लगा कि वैचारिक कला भी बहुत सशक्त हो सकती है।
कहिये आप का क्या विचार है और मेरी इस लघु कला प्रदर्शनी में आप को कौन सी कलाकृति सबसे अधिक अच्छी लगी।
*****


























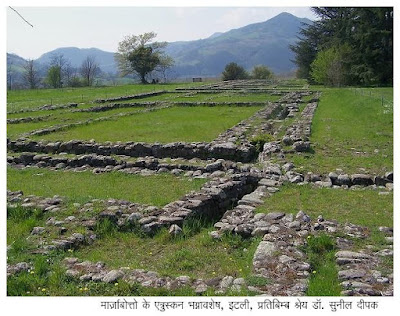


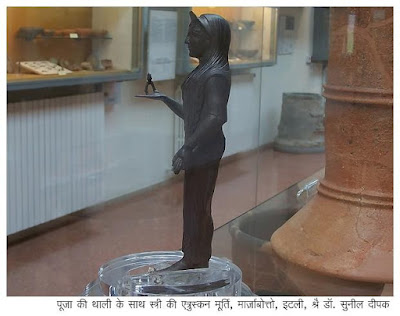







.jpg)
.jpg)

.jpg)











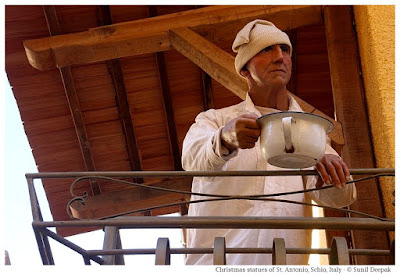




.JPG)