यह आलेख डॉ. सावित्री सिन्हा की लिखी और 1962 में नेशनल पब्लिशिन्ग हाउज़ द्वारा छापी पुस्तक "ब्रज भाषा के कृष्ण भक्ति काव्य में अभिव्यंजना शिल्प" की भूमिका का एक अंश है। आप चाहें तो इस पूरे आलेख को कल्पना पर पढ़ सकते हैं या पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं।
डॉ. सावित्री सिन्हा ने यह पुस्तक अपने माता-पिता (और मेरे दादा-दादी द्वारकाप्रसाद और जयदेवी) को इन शब्दों के साथ समर्पित की थी: "स्वर्गीय पिता जी की आंसूभरी, धूमिल बाल-स्मृतियों को तथा मां के असीम साहस, धैर्य, त्याग और वात्सल्य को"
***
सूरदास से पूर्व कृष्ण-भक्ति काव्य में अभिव्यंजना-शिल्प की स्थिति - एक विहंगावलोकन
डॉ. शिवप्रसाद सिंह के शोध के फलस्वरूप अभी हाल में ही सूरदास के समय से पहले का ब्रजभाषा काव्य प्रकाश में आया है। 'सूर-पूर्व ब्रजभाषा और उसका साहित्य' नामक उनके शोध-प्रबंध में उपलब्ध साहित्य के व्यख्यान के साथ ही कुछ अनुपलब्ध साहित्य भी प्रकाश में लाया गया है और सूरदास से पहले ब्रजभाषा कवियों के अस्तित्व को सिद्ध करने का प्रयास किया गया है। नामदेव, कबीर और रैदास की अनुभूतिपरक रचनाओं को लेखक ने कृष्ण-भक्ति काव्य के विकास का एक सोपान माना है। इस निर्णय को स्वीकार करने के पक्ष और विपक्ष दोनों ही ओर से अनेक तर्क दिये जा सकते हैं। परन्तु यह प्रश्न यहां पर अप्रासंगिक है।
संतमत के कवियों के अतिरिक्त उन्होंने कृष्ण-भक्ति काव्य के विकास में संगीतकार कवियों का महत्वपूर्ण योग स्वीकार किया है। उनके शब्दों में, “संगीतज्ञ कवियों ने न केवल अपनी स्वर-साधना से भाषा को परिष्कार और मधुर अभिव्यंजना प्रदान की, तथा अप्रतिम नाद-सौंदर्य से कविता को अधिक दीर्घयुगी बनाया परन्तु अपनी सम्पूर्ण संगीत-प्रतिभा को आराध्य कृष्ण के चरणों पर लुटा भी दिया। गोपाल नायक और बैजू बावरा के पदों में आत्मनिवेदन, गोपी-प्रेम और भक्ति के विविध पक्षों का बड़ा ही विशद और मार्मिक चित्रण हुआ है। गोपाल नायक के एक पद में रास का चित्रण इस प्रकार मिलता है -
कांधे कामरी गो आलाप के नाचे जमुना तीर, नाचे जमुना तीर
पीछे रे पांवरे लेती नाचि लोई मांगवा --
भुव आलि मृदंग बांसुरी बजावै गोपाल वैन वतरस ले आनन्द। (राग कल्पद्रुम)
बैजू बावरा का उल्लेख भी इस प्रसंग में किया गया है तथा राग कल्पद्रुम में संकलित उनके पदों के आधार पर उन्हें ब्रजभाषा का कवि सिद्ध किया गया है। राग कल्पद्रुम की यह रचनायें शुद्ध ब्रजभाषा में हैं -
आंगन भीर भई ब्रजपति के आज नन्द महोत्सव आनन्द भयो।
हरद दूब दधि अक्षत रोरी ले छिरकत परस्पर गावत मंगलचार नयो।
ब्रह्मा ईस नारद सुर नर मुनि हरषित विमानन पुष्प बरस रंग ठयो।
धन धन बैजू संतन हित प्रकट नन्द जसोदा ये सुख जो दयो। (राग कल्पद्रुम)
इन दोनों ही कवियों की रचनाओं में निहित संगीत तत्व परवर्ती कृष्ण-भक्त कवियों की संगीत-साधना की पृष्ठभूमि से जान पड़ते हैं, परन्तु जहां तक अभिव्यंजना शैली का प्रश्न है यह रचनायें परवर्ती रचनओं के सामने पासंग भर भी नहीं ठहरतीं।
इन रचनाओं के अतिरिक्त शोधकर्ता ने निम्नलिखित ७ अप्रकाशित पुस्तकों का परिचय-परीक्षण भी प्रस्तुत किया है - अग्रवाल कवि की प्रद्युमनचरित; विष्णुदास की महाभारत कथा, स्वर्गारोहड़, रुक्मिणी मंगल, स्वर्गारोहड़ पर्व और स्नेह लीला; थेघ नाथ की गीता भाषा।
कृष्णभक्ति सम्बंधी अप्रकाशित ग्रंथों को लेखक ने जिस रूप में हमारे सामने रखा है, उसे उसी रूप में स्वीकार कर लेने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं है। उनके मतों को उद्धृत करके विषय-विस्तार करने से कुछ लाभ नहीं होगा। जो कुछ भी सामग्री प्रकाश में आयी है उसके अध्ययन द्वारा ये निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं -
तत्कालीन ब्रजभाषा के दो रूप थे (१) अपभ्रंश मिश्रित ब्रजभाषा (२) तद्भव प्रधान ब्रजभाषा। संस्कृति के तत्सम शब्दों के प्रयोग द्वारा तत्कालीन ब्रजभाषा का रूप परिनिष्ठित नहीं हो पाया था। प्रथम कोटि की भाषा के उदाहरण के रूप में डूंगर कवि की एक रचना उद्धृत की जा रही है -
ऋतु बसंत उलहणी विविह वणराय फलह सहू।
कंटक विकट करीर पंत पिकखंत किंपि नहु।
धाराहर वर धवल बारि वरसंत घनघोर वन।
कुरलतंउ मूल मंत्री सर्प नहीम मानहिं दुर्जन।
***
औषधि मूल मंत्री सर्प नहिं मानहिं दुर्जन।
सर्प डसी वेदना एही दिट्ठइ हुई, गुंजन।
लागइ दोष अनन्त कियइ संसर्ग एनि परि।
तवडी जल हरइ घड़ी पीटियइ सुफल्लरि।
द्वितीय कोटि के उदाहरण के रूप में विष्णुदास रचित 'सनेह लीला' की ये पंक्तियां ली जा सकती हैं -
महलन मोहन करत विलास।
कहां मोहन कहां रमन रानी और कोऊ नहिं पास।
रुकमन चरन सिरावत पिय के पूजी मन की आस।
जो चाहे थी सो अब पायो हरि पति देवकी सास।
तुम बिन और कौन थो मेरौ धरति पताल आकास।
पल सुमिरन करत तिहारौ ससि पूस परगास।
इन कवियों की रचनाओं में प्रबुद्ध कला-चेतना का पूर्ण अभाव है। अभिव्यंजना-शैली की दृष्टि से ये अत्यंत साधारण कोटि की रचनायें हैं। उनकी शैली अधिकतर वर्णनात्मक और विवरणात्मक है। अप्रस्तुत योजना, लक्षित चित्र-योजना, वाग्वैदग्घय आदि तत्व बहुत ही कम हैं।
विषय-वस्तु के क्षेत्र में कुछ ऎसे तत्व अवश्य मिलते हैं जिन्हें परवर्ती कृष्ण-भक्ति काव्य का पूर्वाभास कहा जा सकता है। यह प्रभाव मुख्य रूप से दो क्षेत्रों में दिखाई पड़ता है: (१) लोक संस्कृति के चित्रण में (२) शास्त्रीय संगीत के समावेश में।
गोस्वामी विष्णुदास रचित रुक्मणि मंगल की ये पंक्तियां प्रथम वर्ग के उदाहरण के रूप में ली जा सकती हैं:
मोतियन चौक पुराय के कियौ आरती माय।
अति आनन्द भयौ है नगर में घर घर मंगल साजै।
मनमोहन प्रभु ब्याह कर आये पुरी द्वारका राजै।
अंगन तन में भूषन पहिने सब मिलि करत समाज।
बाजै बाजन कानन सुनियत, नौबत घन ज्यूं बाज।
नर नारिन मिलि देत बधाई सुख उपजै दुखभाज।
नाचत गावत मृदंग बाजत रंग बसावत आज।।
दूसरे वर्ग की रचनाओं के अन्तर्गत गोपाल नायक और बैजू बावरा की रचनायें रखी जा सकती हैं। डॉ. सिंह ने इन रचनाओं को काव्य-कल्पद्रुम से संकलित किया है। संगीत कला के क्षेत्र में इस ग्रंथ का महत्वपूर्ण स्थान है परन्तु भाषा और साहित्य की दृष्टि से उसमें संकलित पदों को प्रमाणिक माना जा सकता है या नहीं यह प्रश्न विवादरहित नहीं है। यदि उन्हें प्रमाणिक मान लिया जाये तो गोपाल नायक और बैजू बावरा के पदों को परवर्ती कृष्ण-भक्त कवियों के ध्रुपद शैली में रचित पदों का पूर्वरूप माना जा सकता है। शास्त्रीय संगीत के तत्वों का उल्लेख तथा ध्रुपद शैली के अनुकूल पद-योजना इन रचनाओं में प्राप्त होती है -
सप्त स्वर तीन ग्राम इकइस मूर्छन बाइस सुर्त
उनचास कोट ताल लाग डाट
गोपाल नायक हो सब लायक आहत अनाहत शब्द,
सो ध्यायो नाद ईश्वर बसे मो घाट
तथा
मार्ग देसी कर मूर्छना गुन उपजे मति सिद्ध गुरु साध चावै।
सो पंचम मघ दर पावै।
बैजू बावरा के पदों की योजना भी ध्रपुद शैली की श्वास-साधना के निमित्त की हुई जान पड़ती है:
बोलियो न डोलियो ले आऊं हूं प्यारी को,
सुन हौ सुघर वर अब हीं पै जाऊं हूं।
मानिनि मनाय के तिहारे पाय ल्याय के,
मधुर बुलाय के तो चरण गहाऊं हूं।
सुन री सुंदर नारि काहे करत एति रार,
मदन डारत पार चलत पल तुझाऊं हूं।
मेरी सीख मान कर मान न करो तुम,
हे जु प्रभु प्यारे सो बहियां गहाऊं हूं।
बधाई के लोक-गीत भी उनके नाम से प्राप्त होते हैं:
आंगन भीर भई ब्रजपति के आज नन्द महोत्वस आनन्द भयौ।
हरद दूब दघि अक्षत रोरी ले छिरकत परस्पर गावत मंगलचार नयो।
ब्रह्मा ईस नारद सुर नर मुनि हरषित विमानन पुष्प बरस रंग ठयो।
धन धन बैजू संतन हित प्रकट नन्द जसोदा ये सुख जो दयो।
अधिकतर कवियों ने दोहा, चोपाई और छप्पय का प्रयोग किया है। कुछ पदों के ऊपर गौरी, धनाश्री और पूर्वी रागों का उल्लेख भी हुआ है।
इस सामग्री के अध्ययन के उपरान्त सूरदास से पूर्व ब्रज-भाषा काव्य के अस्तित्व की स्वीकृति में आचार्य शुक्ल का अनुमान आंशिक रूप में ही सत्य माना जा सकता है। सूरदास के काव्य-सौष्ठव पर विचार करते हुए आचार्य शुक्ल ने कहा था, ‘इन पदों के सम्बंध में सबसे पहली बात ध्यान देने की यह है कि चलती हुई ब्रजभाषा में सबसे पहली साहित्यिक रचना होने पर भी ये इतनी सुडोल और परिमार्जित है, यह रचना इतनी प्रगल्भ और काव्यांग-पूर्ण है कि आगे होने वाले कवियों की उक्तियां सूर की जूठी सी जान पड़ती हैं। अत: सूर-सागर किसी चली आती हुई गीति काव्य परम्परा का - चाहे वह मौखिक ही रही हो - पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है।"
इन कृतियों के प्रकाश में आने पर भी कलाकार के रूप में सूर अपने पूर्व-स्थान पर ही शोभित हैं। इस काल के दर्जन कवियों में से एक भी ऎसा नहीं है जो अष्टछाप के अन्य कवियों के समकक्ष खड़ा रह सके, सूरदास तो दूर की बात है। जहां तक पूर्व-परम्परा की स्थापना का प्रश्न है यह तथ्य उसी रूप में स्वीकार किया जा सकता है जैसे हम यह कहें कि छायावादी कविता के बीज द्विवेदी-युग की रचनाओं में भी पाये जाते हैं।
सूर-पूर्व ब्रजभाषा काव्य में गीति-काव्य की मौखिक परम्परा भी स्थापित की जा सकती है, ब्रजभाषा का अस्तित्व भी माना जा सकता है पर उसमें कला-सौष्ठव का कोई ऎसा आधार नहीं मिलता जिसके कारण यह कहा जा सके कि सूरदास के पदों की प्रगल्भता और काव्यांगपूर्णता को कोई पूर्व आधार हिन्दी जगत् में विद्यमान था। कला के क्षेत्र में नये मार्गों का उद्घाटन सूरदास, नन्ददास और उनके समकालीन भक्तों ने ही किया। उनकी कला-चेतना का प्रादुर्भाव तत्कालीन परिस्थितियों के फलस्वरूप हुआ था। कला के पुनुर्त्थान युग में उनकी प्रतिभा प्रस्फुटित हो कर विकसित हुई। उत्तराधिकार रूप में उन्हें जो परम्परा प्राप्त हुई थी वह पूर्ण अविकसित थी, भाव, भाषा, शैली, किसी भी दृष्टि से मध्यकालीन कृष्ण-भक्त कवियों पर उनका ऋण नहीं स्वीकार किया जा सकता।
कृष्ण-काव्य परम्परा के विकास का संक्षिप्त परिचय
कृष्ण-काव्य परम्परा के विकास का प्रमुख श्रेय आचार्य वल्लभ और उनके पुत्र विट्ठलदास जी को है। आचार्य वल्लभ द्वारा प्रवर्तित 'पुष्टि मार्ग' को आधार बना कर श्री विट्ठलदास द्वारा स्थापित अष्टछाप के कवियों ने हिन्दी में अमर कृष्ण-भक्ति-काव्य की रचना की। पुष्टि मार्ग की अनुभूति मूलक साधना के कारण इन कवियों ने कृष्ण के व्यक्तित्व के लीला-प्रधान अंशों को ही ग्रहण किया है। राजनीतिज्ञ कृष्ण उनके आलम्बन नहीं हैं। कृष्ण के व्यक्तित्व में उन्होंने शक्ति के साथ माधुर्य और प्रेम का समन्वय कर दिया। अलौकिक आलम्बन में सहज और मधुर मानव का आरोपण उन्होंने जिस मनोवैज्ञानिक कौशल से किया है उसमें सार्वभौम उपादानों का समावेश हुआ है।
ऎतिहासिक क्रम से अष्टछाप के कवियों का उल्लेख इस प्रकार है - कुभंनदास, सूरदास, परमानन्ददास, कृष्णदास, नन्ददास, चतुर्भुजदास, छीतस्वामी और गोविन्दस्वामी। सूरदास प्रधान रूप से वात्सल्य और शृंगार रस के कवि हैं, परमानन्द जी के काव्य में वात्सल्य का अनुपात महत्वपूर्ण है। अन्य कवियों की रचनाओं में श्रंगार रस का ही प्राधान्य है, उसमें वात्सल्य तो है ही नहीं या अत्यंत गौणरूप में प्रयुक्त है। इन सभी के प्रतिपाद्य में साहित्यकता, पार्थिव अनुभूतियों और आध्यात्मिकता का सुंदर सामन्जस्य मिलता है। विभिन्न कवियों के व्यक्तित्व के अनुसार तीनों तत्वों का अनुपात उनकी रचनाओं में भिन्न-भिन्न है। साहित्यिक महत्व की दृष्टि से सूरदास के बाद नन्ददास का नाम आता है। उनकी अभिव्यंजना में सचेष्ट कलाकार का शिल्प है।
पूर्वमध्यकाल के इन पुष्टिमार्गी कवियों के बाद परिमाण और गुण दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण योग राधावल्लभ सम्प्रदाय के आचार्य हितहरिवंश तथा उनके शिष्यों और अनुयायियों ने दिया। राधावल्लभ सम्प्रदाय की उपासना पद्धति अन्य सम्प्रदायों से भिन्न थी। इस मत के सिद्धांतों के अनुसार राधा ही परम इष्ट हैं और कृष्ण की मान्यता इसीलिए है कि वह राधा के प्रियतम हैं। वे इष्ट नहीं हैं। भक्तजन राधा की सखी रूप में होते हैं। वे सखी रूप में उनके साथ परकीया गोपियों के समान स्वतंत्र रूप से सम्बंध स्थापित नहीं करते और न राधा के प्रति उनका सपत्नि भाव होता है। इस सम्प्रदाय में हितहरिवंश के अतिरिक्त ध्रुवदास की कला का महत्वपूर्ण स्थान है।
किसी विशिष्ठ सम्प्रदाय के बंधनों से मुक्त मतवाली मीरा और रसखान की रचनाओं का भी पूर्व-मध्यकालीन कृष्ण-भक्ति साहित्य में बड़ा महत्व है। मीराबाई द्वारा रचित कई ग्रंथों का उल्लेख प्राप्त होता है। नरसी का मायरा, गीत-गोविन्द की टीका, पद तथा गर्व गीत उनकी प्रमुख रचनायें मानी जाती हैं। उनका साहित्य और उसका स्वरूप दोनों ही संदिग्ध हैं। उनके काव्य में गिरधरगोपाल के प्रति उनकी आकुल भावनायें विर्बाध रूप से व्यक्त हुई हैं। जहां भावनायें उन्मुक्त हुईं, आकांक्षायें उच्छृंखल हो कर असंयत हो जाती हैं पर मीरा के काव्य की सबसे बड़ी सफलता यही है कि भावनाओं की निर्बाधता में असंयत और अनियंत्रित श्रृंगार की स्थूलताओं का समावेश नहीं होने पाया है। उनकी कला का एक अपूर्व ही सौंदर्य है जो कला सम्बंधी परिपक्वताओं से वंचित रहने पर भी पूर्ण है।
मुसलमान कृष्ण-भक्त कवि रसखान का नाम इस परम्परा में अमर है। उनके व्यक्तित्व में प्रधान प्रेम-तत्व ने लौकिक आलम्बन के अस्थायित्व के कारण अलौकिक कृष्ण का सहारा लिया और उनकी भावनायें भक्त हृदय के सुंदर उद्गारों के रूप में व्यक्त हो उठीं। भावानाओ की तीव्रता और उत्कटता के साथ ही साथ उनके काव्य का कलापक्ष भी प्रौढ़ और सबल है। 'प्रेम वाटिका' और 'सुजान रस सागर' उनके दो छोटे-छोटे ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं।
उत्तर-मध्य काल में भी कृष्ण-काव्य परम्परा विभिन्न सम्प्रदायों के संरक्षण में पल्लवित और पुष्पित होती रही। पूर्व-मध्य काल (भक्तिकाल) में कृष्ण-भक्ति-पद्धति में नैसर्गिक आलम्बन के प्रति मानवीय भावनाओं का जो उन्नयन हुआ उसमें राग और साधना का अपूर्व सामंजस्य था। इस परम्परा में रागतत्व के प्राधान्य के कारण ही १९वीं शती तक भक्ति-युग की परिष्कृत माधुर्य भावना लौकिकता में रंजित होने लगी। उत्तर-मध्य कालीन कृष्ण-काव्य परम्परा में आलम्बन और साधना दोनों पक्षों में अपार्थिव अंश केवल नाम-मात्र को ही शेष रह गया।
रीतिकालीन कृष्ण-भक्ति काव्य में श्रृंगारिक तत्वों का इतना प्राधान्य हो गया कि उसके फलस्वरूप ब्रह्मा की असीमता भी मानवीय क्रिया-कलापों में लिपट कर रह गई। साहित्य की रूढ़ परम्पराओं के अनुसार 'ब्रह्मा की प्रेमिकाओं' पर भी नायिका-भेद के विविध रूपों का आरोपण किया गया। हिन्दी काव्य जगत् में सतरहवीं शताब्दी के उपरान्त कृष्ण और गोपिकाओं के नाम पर श्रृंगारपरक ऎहिक भावनाओं की अभिव्यक्ति प्रधान हो उठी।
उत्तर-मध्य काल में वल्लभ सम्प्रदाय का कोई उल्लेखनीय कवि नहीं हुआ। केवल ब्रजवासीदास ने सूरसागर के आधार पर अपने ग्रंथ 'ब्रजविलास' की रचना की। राधावल्लभ सम्प्रदाय के हित वृंदावनदास ने 'लाड़ सागर' और 'ब्रज प्रेमानन्द सागर' ग्रंथों की रचना की। इसके अतिरिक्त निम्बार्क सम्प्रदाय के घनानन्द, नागरीदास, हठी जी, भगवत रसिक जी, रूप रसिक जी, सहचरिशरण ने कृष्ण-भक्ति सम्बन्धी रचनायें लिखीं, जिनमें उस युग की काव्य-चेतना की स्मस्त विशेषताओं का समावेश हो गया है।
प्रतिपाद्य के प्रति उनके दृष्टिकोण और उनकी अभिव्यंजना-कला का विवेचन आगामी अध्यायों में किया जायेगा।
आधुनिक काल नये संदेशों और नये जीवन-दर्शन से युक्त सामने आया। मध्यकालीन सामन्तीय व्यवस्था बीत चुकी थी। बौद्धिक जागरण और विज्ञान के इस युग में धार्मिकता और विशेषकर उपास्य के प्रति रागात्मक वृत्ति के उन्नयन को अंध-विश्वास और रूढ़िवादिता का नाम दिया गया। उत्तर-मध्य काल में कृष्ण-भक्ति में निहित श्रृंगार तत्व ने लौकिक श्रृंगार का रूप धारण कर लिया था, आधुनिक काल में केवल उसका अंधकार पक्ष ही अवशिष्ट रह गया। भक्ति के नाम पर भ्रष्टाचार, अंधविश्वास और पाखंड ने तत्कालीन सुधारवादी और बौद्धिक प्रवृत्तियों को अपने विरुद्ध आवाज़ उठाने की चुनौती दी। सूक्ष्म रागात्मक प्रवृत्तियों का आश्रित भक्ति बौद्धिक और ऎहिक जीवन-दर्शन के भार के नीचे दब गई। उसकी विकृति ही शेष रह गई।
मध्यकाल में भक्ति ने एक आंदोलन का रूप ग्रहण किया था। वह जनता के व्यक्तिगत और समष्टिगत संघर्षों और समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने आई थी। आधुनिक काल में उसका क्षेत्र 'व्यक्ति' की सीमा में ही संकीर्ण हो गया। परिवार के संसर्ग और वैयक्तिक संस्कार इत्यादि कारणों से 'धर्म' तत्व एक संकीर्ण दायरे में ही शेष रह गया। भारतेन्दु हरीशचन्द्र, जगन्नाथदास रत्नाकर, सत्यनारायण कविरत्न इत्यादि कवियों ने कृष्ण-भक्ति काव्य की रचना की जिसकी प्रेरणा स्थूल रूप में तीन प्रकार की मानी सकती है - (१) परम्परा-पालक (२) कृष्ण-चरित के गान द्वारा प्राचीन गौरव की स्थापना तथा (३) वैयक्तिक संस्कारजन्य आस्था। वल्लभाचार्य के शिष्यों द्वारा प्रवर्तित कृष्ण-काव्य परम्परा उत्थान और पतन के विविध सोपानों पर चढ़ती-गिरती आधुनिक काल तक चली आई। वल्लभ सम्प्रदाय के ही निष्ठावान भक्त भारतेन्दु हरीशचन्द्र ने उनमें पुन: माधुर्य-भक्ति की परिष्कृति और सूक्ष्मता के समावेश का प्रयत्न किया, परन्तु अब इस प्रकार की भक्ति का समय बीत चुका था, देश के सामने यथार्थ नग्न मुँह बाये खड़ा था, पाश्चात्य देशों का बुद्धिवाद भारत की आध्यात्मिकता को चुनौती दे रहा था, जिसके सूक्ष्म तन्तु बाह्य स्थूलताओं के सामने हार मान चुके थे। साहित्य में व्यवहारिक भाषा के अभाव के फलस्वरूप ब्रजभाषा का स्थान खड़ी-बोली ले रही थी, ऎसी स्थिति में ब्रजनायक से सम्बद्ध काव्य-परम्परा और ब्रजभाषा दोनों के विकास का मार्ग अवरुद्ध हो गया।



.JPG)
.JPG)






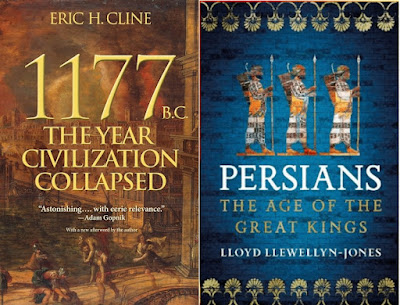
.jpg)
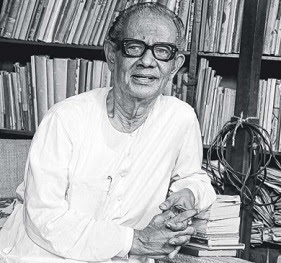

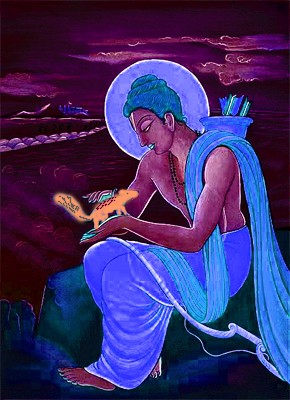
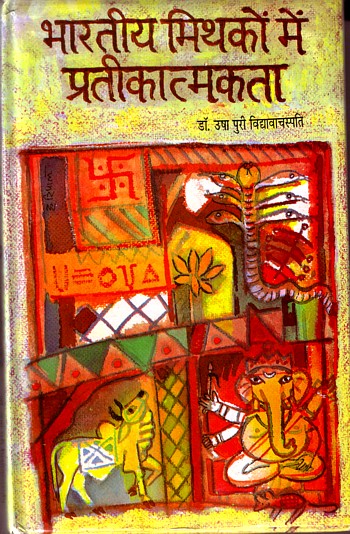
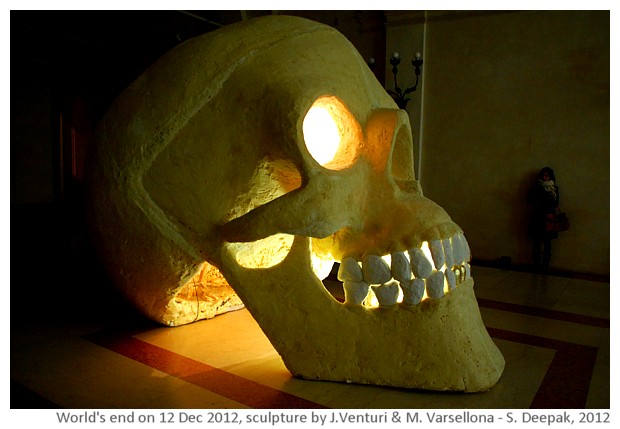
















.JPG)