अप्रैल 1967 में डा. राम मनोहर लोहिया और समाजवादी पार्टी से जुड़े बहुत से लेखकों तथा विचारकों ने मिल कर नियमित रूप से देश के विभिन्न प्रश्नों पर विचार विमर्श करने के लिए मासिक गोष्ठियों का आयोजन करने का निर्णय लिया था, और पहली गोष्ठी का विषय था हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं के भविष्य के बारे में. इस गोष्ठी के लिए श्री रघुवीर सहाय को आमान्त्रित किया गया था कि वह इस विषय पर लेख लिखें, जिस पर बहस की जाये. यह लेख और उस पर हुई बहस, मई 1967 की "जन" पत्रिका में छपे थे. वही विचारोत्तेजक लेख यहाँ प्रस्तुत है.
अपने पिता के पुराने साथियों में रघुवीर सहाय की याद मेरे मन में बहुत सालों बाद भी ताजा है. उनका सिगार पीना, उनकी मृदुल हँसी और उनका हम बच्चों से गम्भीरता से बात करना, सब याद है. उनके बच्चों में से, उनकी बड़ी बेटी मँजरी जो मेरी उम्र के कुछ करीब थी, की याद है, लेकिन छोटी बेटी और बेटे के नाम भी याद नहीं, पिता की अकस्मात मृत्यु के बाद उनसे सम्बंध नहीं रहे, लेकिन आज रघुवीर जी के इस लेख को प्रस्तुत करते समय सब याद आ गया.
भाषा की पूजा बन्द करो - रघुवीर सहाय
(यह लेख बहस के लिए लिखा गया है. इसमें लेखक ने अन्तिम विश्लेषण करके बहस खत्म कर देने का दावा नहीं किया है. पर वह यह मान कर चलता है कि भाषा पर बहस यह समझने के लिए की जा रही है कि भाषा के मामले में इस वक्त क्या करना है.)
भाषा के मामले पर पिछले 20 वर्षों में जो कुछ हुआ है, उसका जायज़ा एक वाक्य में लिया जा सकता हैः थोड़े से लोगों को, जो भाषा का इस्तेमाल करने की जरूरत से प्रतिश्रुत रहे हैं उन बहुत से लोगों के विरुद्ध संघर्ष करने को मजबूर किया गया है जो भाषा की पूजा करते रहे हैं. इस संघर्ष में वह लेखक - और इस लेखक की भी यही स्थिति है - जो थोड़े लोगों में शामिल रहा अब एक कोने में धकेल दिया गया है जहाँ उसे अपनी आखिरी जी तोड़ कोशिश के साथ छटपटाती हुई एक लड़ाई लड़नी है. बहस के लिए सच पूछिये तो उसके पास वक्त नहीं रह गया हैः बहस पुकार कर शायद कुछ एक अन्य लेखकों को पास बुला सकती है मगर पास खड़े हो जाने वाले अगर खुद छटपटा कर लड़ नहीं सकते तो बहस सिर्फ़ आततायी को और अधिक आक्रमण का मौका देने का साधन बनती है.
एक अच्छे योद्धा की तरह अपनी क्षति स्वीकार कर लेनी चाहिये - भाषा बुरी तरह टूट चुकी है. राजनीतिक दिमाग एक भाषा में वोट माँगता है, दूसरी में वक्तव्य देता है तीसरी में शपथ लेता है. कलाकार दिमाग़ एक भाषा में सोचता है, दूसरी में लिखता है और फ़िर पहली में यश प्राप्त करना चाहता है. बाकी लोग, किसी भाषा में सोच नहीं पाते, किसी भाषा में बोल नहीं पाते. उनके लिए दो व्यक्तियों के मध्य भाषा की एक बड़ी उपलब्धी - मतभेद संभव नहीं रह गया है, अधिक से अधिक वे एक अव्यक्त समझौता कर सकते हैं जो एक दूसरे के भ्रष्ट चरित्र के लिए चुपचाप हामी भरने का समझौता होता है. यह सब इतना जानते हुए कह रहा हूँ कि ये राजनीतिक, कलाकार और लोग कोई आदर्श नहीं हैं.
परन्तु कुछ आदर्श इन तीन वर्गों में कहीं न कहीं हैं. जो भी हैं वे भाषा को पूजा की नहीं इस्तेमाल की चीज़ बनाने के लिए लड़ते रहे हैं. इस लड़ाई में अब अंतिम दौर शुरु हो गया है. एक जगह हम देखते हैं कि सरिहन सरासर झूठ बोल कर अब उसे छिपाने की कोशिश चल भले ही कर जाये, सच्चाई को उजागर किया जा सकता है. दूसरी जगह विद्रोह को भटकाने में भाषा का सहारा लेने की चेष्टा, आकर्षण भले दिख ले, भले दिख ले, भाषा इसमें दग़ा जरूर दे जाती है, तीसरी जगह, कहने का कोई असर न हो और यहाँ तक न हो कि शब्द की जगह पत्थर ही एक रास्ता रह जाये, फिर भी विचार जनमत बन सकता है. ये सब मुक्ति के, विजय के लक्षण हैं. परन्तु लम्बी लड़ाई के दौरान पीछे हटते हुए प्रतिद्वन्द्वी ने इतनी बस्तियाँ उजाड़ दी हैं कि अब सारी दुनिया नये सिरे से बसानी होगी.
सबसे पहले तो राष्ट्रीय एकता को नये सिरे से समझना और बनाना पड़ेगा. यह एक चीज़ है जो सबसे ज़्यादा जलायी फ़ूँकी गयी है. एक से एक सूक्ष्म अस्त्र काम में लाये गये हैं जैसे यह कि सारे देश की एक राजभाषा जिस संविधान द्वारा स्थापित की गयी है उस सम्बन्ध में विहित समता के किसी भी आदेश का पालन नहीं किया गया है. जिस भाषा को राजभाषा बनाने का संकल्प किया गया है, उसके बहुमत का शोषण किया गया है, उसकी भाषा का नहीं. स्वामी शासक के जाने के बाद उसकी जगह उस बहुमत के समृद्ध प्रतिनिधियों ने ले ली है और शासक की भाषा के रूप में उस भाषा को बिठा दिया है जिसे आज़ादी भी नहीं मिल पायी थी. उसे स्वामिभाषा का स्थान दिलाने के लिए लालच दिया गया कि वह दासभाषा बन कर रहे और दासत्व का मुआवजा उपभोग करे. यदि वह भाषा आज़ाद होती तो काफ़ी बड़ा शासक वर्ग अपनी जगह से हटता. इसलिए उसे अधिक से अधिक समय तक मुआवज़ा देने की पेशकश की गयी. उसका विकास करने के लिए बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय धन का व्यय किया गया जिसमें हिस्सा बंटाने वह लोग आये जिन्होंने भाषा का विकास करते रहने का और उसे इस्तेमाल न होने देने का बीड़ा उठाया. राष्ट्रीय खर्च से एक भाषा को जो घूस दी गयी वह दूसरी राष्ट्रभाषाओं का पेट काट कर दी गयी. भाषाओं में एक भाषा के लिए घृणा फैलाने का काफ़ी इन्तज़ाम था. तब भाषा की दासता का मोर्चा यों बँधाः अंग्रेजी शासन की भाषा, हिन्दी प्रमुख दास भाषा और बाकी प्रतिद्वन्द्वी दासभाषाएँ.
यहाँ वह सम्पूर्ण कहानी दोहराना बहुत सी जानी मानी बातें दुहराना होगा जो हिन्दी के इस दास वैभव से उपजी विकृतियों की कहानी है. बहुत बड़े पैमाने पर हिन्दी क्षेत्र की प्रतिभा का विविध विद्याओं से, विविध भाषाओं और परम्पराओं से और अपने क्षेत्र के मनुष्य से अलगाव ही संक्षेप में वह कहानी है. एक प्रश्न अवश्य यहाँ अनुतरित नहीं छोड़ना चाहता हूँ. अक्सर कहा जाता है कि यदि स्वतंत्रता मिलते ही हिन्दी को सीधे राजभाषा घोषित करके स्थापित कर दिया होता तो अनन्तर जो कुछ हुआ, वह न होता - वैसा नहीं किया गया, यह बड़ी भूल हुई. पर ऐसा नहीं किया जा सका तो क्यों? क्यों कि जिन्होंने हिन्दी के नाम पर नेतृत्व सम्भाला था - सचमुच उन अल्प प्रतिशत लोगों के साथ थे जो बाद में अमीर से अमीर बने और इन नेताओं में स्वभावतः नैतिक शक्ति की कमी थी. और भी बहुत से काम हैं जो तब नहीं हुए और बाद में बहुत धीरे धीरे और तकलीफदेह तरीके से गलती सुधारने के प्रयत्न होते रहे. पर वे इतने दिखावटी थे कि उन्होंने न सिर्फ कोई परिवर्तन नहीं किया बल्कि हर बार समस्या को एक नयी उलझी हुई शक्ल दे डाली.
आज़ादी के बाद के पहले वर्षों में जब हिन्दी क्षेत्र में जन्म लेने के कारण हिन्दी भाषी को राजनीतिक सम्मान प्राप्त करने का निर्विवाद अधिकार दे दिया गया तभी उस क्षेत्र के असमपन्न हिन्दीभाषी को अपनी भाषा में अपना सामान्य सामाजिक अधिकार प्राप्त करने से निरन्तर वंचित रखा गया - उसे बताया गया कि कुछ लोग अभी उसकी हिन्दी का विकास करने के लिए अंग्रेज़ी से अनुवाद कर हैं और वह चाहे तो अपनी भाषा का इस्तमाल करने के खतरे और नुक़सान छोड़ कर अनुवाद के अनुष्ठान में शामिल हो सकता है. हिन्दी में अभिव्यक्ति की सामर्थ्य का जीवन में व्यवहार तब इस शकल में हुआ कि विद्याओं का, कौशल का और अन्ततः चरित्र का विकास नहीं, इन सबके अंग्रेज़ी नमूनों का भाषानुवाद ही हिन्दी भाषी का सामाजिक प्रतिष्ठा का माध्यम है. एक नतीजा इसका यह है कि हिन्दी में लिखने वाले लोग दिन ब दिन कम होते गये जो भाषा के अतिरिक्त किसी विद्या में पारंगत हों. सम्पूर्ण समाज रोक कर रखा गया, उस दिन की प्रतीक्षा में जब संविधान के अनुसार रातोंरात हिन्दी राजभाषा हो जायेगी और उस दिन भाषा का अधिकार हर एक को मिल जायेगा. यह दिन हिन्दीतर भाषाओं के सम्पन्न वर्ग को स्वभावतः खतरे का दिन दिखायी देने लगा क्योंकि यह प्रकट हो चुका था कि यह खुद हिन्दी भाषा के उतने ही सम्पन्न वर्ग के लिए खतरे का दिन है जिसे वे टालना चाहते हैं.
जब यह भय हिन्दीतर क्षेत्रों के सम्पन्न नेताओं ने प्रकट किया तो इसकी प्रतिक्रियाएँ हिन्दी क्षेत्र में और हिन्दीतर क्षेत्रों में प्रायः एक सी हुईं. हिन्दी नेताओं ने इसे हिन्दी विरोध का नाम दिया जबकि यह हिन्दी नेताओं का ही समधर्मी अंग्रेज़ी समर्थन था. हिन्दीतर क्षेत्र के वंचित पिछड़े वर्ग को भी अपने नेताओं का यह अंग्रेज़ी समर्थन मातृभाषा की रक्षा के साधन के रूप में दिखायी दिया, या कम से कम दिखाया गया और बहुत समय तक एक झूठी बहस हिन्दी और हिन्दीतर दोनो पक्षों के स्वार्थी नेताओं में चली जिससे वास्तव में दोनो अपने अपने क्षेत्र की भाषा शक्ति को आगे बढ़ने से रोकने के मामले में सहमत थे. हिन्दी नेताओं ने अपनी जनताओं से कहा, चूँकि सरकार और हिन्दीतर भाषी हिन्दी का विरोध कर रहे हैं इसलिए हम हिन्दी में हस्ताक्षर करने, हिन्दी में नामपट लिखवाने और हिन्दी में पुरस्कार दिलाने के कार्यक्रम और आंदोलन चला रहे हैं. हिन्दीतर क्षेत्र की जनता से इन्होंने कहा - हम दूसरी भाषाओँ हम दूसरी भाषाओं के विरोधी नहीं हैं, दूसरी भाषाओं का भी वैसा ही विकास होना चाहिये जैसा हम अपनी भाषा का कर रहे हैं, अर्थात उनके इस्तमाल को रोक रखने वाला विकास. फलतः केन्द्र ने सब भाषाओं के विकास का नारा उठाया, क्योंकि सत्ताधारी नेतृत्व इन दोनो क्षेत्रों के सम्पन्न नेतावर्ग को अपने साथ रखना चाहता था. हिन्दी के इस वर्ग की जो राजनीतिक शक्ति इस बीच बढ़ गयी थी. उसका पलड़ा दूसरी भाषाओं के समानधर्मी वर्ग की राजनीतिक शक्ति के बराबर लाने के लिए बन्दर बाँट का रास्ता केन्द्रीय नेतृत्व ने अपनाया, हिन्दीवालों का घमण्ड चूर करने के लिए सरल और सर्वसुगम हिन्दी का डँडा श्री नेहरू जब तब चलाते रहे. इस दौर की एक छोटी सी घटना का उल्लेख यहाँ किया जा सकता है जो दिखाती है कि हिन्दी का नेता इस काण्ड में किस तरह शामिल था. जब नये रेडियोमंत्री गोपाल रेड्डी से हिन्दी वालों की अक्ल दुरुस्त करने को नेहरू ने कहा तो मंत्री के स्वागत में सेठ गोविनददास के घर पर प्रीतिगोष्ठी का आयोजन हुआ. उसमें सेठ जी ने हिन्दी विरोधी रेड्डी की खूब खबर ली. मंत्री इस सत्कार के लिए तैयार न थे. बहुत नाराज हुए. डा. नगेन्द्र ने उन्हें शान्त होने में सहायता दी. उन्होंने बड़े अबदकायदे से कुछ बहस भी चलायी, पर उन्होंने या किसी बड़े आदमी ने मंत्री से एक बार भी नहीं कहा कि आप अंग्रेज़ी से अनुवाद बंद करा दें और मौलिक हिन्दी में लिखाना शुरु करें तो भाषा सरल हो सकती है. आखिरकार नेताओं और मंत्री के बीच तयतोड़ अनुवाद की जाँच कराने पर हुआ, मौलिक लेखन पर नहीं. भाषा की आज़ादी की बात नहीं उठी, भाषा की गुलामी का फायदा नयी अनुवाद जाँच समिति के रूप में उठाया गया. बन्दर बाँट ने जो टुकड़ा भाषा में से काटा वह भाषा के इस्तेमाल का टुकड़ा था.
फ़िर 1963 में अंग्रेज़ी को सहभाषा के रूप में बनाये रखने का कानून पास होते ही, विकास का ढोंग खत्म हो कर, एक नया ढोंग, पूजा का ढोंग शुरु हुआ, जिसके बीज विकास के ढोंग में पहले से ही थे. अब द्वार पर नामपट पर हिन्दी में नाम लिखाना भी भगवान को दरदर भटकाने का पाप समझा जाने लगा और हिन्दी सम्बंधी छोटे बड़े सराकारी कार्यलय शुद्ध रूप से मन्दिर बन गये जिनमें पूजा पाठ की विधियों पर शास्त्रीय उपदेश करते हुए छोटे बड़े पुजारी आज जय हिन्दी, जय नागरी कर रहे हैं. हिन्दी के विकास के काम में कभी मजबूरन कुछ गतिशीलता का जो बन्धन था वह भी अब आत्महत्या, न्यस्त स्वार्थ की हत्या, माना जाने लगा है. भाषा को कमरे में बैठ कर गढ़ने का काम दिन प्रतिदिन कम होने वाला काम हो तभी वह गतिशील कहला सकता है, पर अब तो प्रश्न उसे अनन्त बनाने का रह गया है, क्योंकि संविधान में हिन्दी के प्रकरण से हिन्दी भाषी को यह जो सामाजिक प्रतिष्ठा उपलब्ध हुई है अब कम से कम इसे बचाये रखने का सवाल हिन्दी नेता के लिए हिन्दी के नाम पर सबसे महत्वपूर्ण सवाल है.
तो भी कुछ अपनी नेतागिरी जताने के लिए और कुछ सचमुच पदहानि के दुख से हिन्दी नेता जनता के सामने आ कर "हा हिन्दी का दुर्भाग्य" कह कर रोया था. साथ ही उसने कहना शुरु किया था कि दूसरी भारतीय भाषाओं की मदद के बिना हम अंग्रेजी को नहीं हटा सकते. सुनने में यह हृदय परिवर्तन जैसा लगता है पर है यह केवल वेश परिवर्तन. वह अभी भी "अंग्रेजी को हटा नहीं सकते" के बाद "और हिन्दी को नहीं स्थापित कर सकते" जोड़ देता है और अभी भी समझौता उस हिन्दीतर भाषी से करना चाहता है जो अपने क्षेत्र में अपनी भाषा का इस्तेमाल रोक कर उसके विकास के लिए मोहलत और पैसा माँग रहा है और कहता है कि अंग्रेज़ी तभी हटे जब मेरी भाषा भी हिन्दी जितनी रिश्वत खा ले.
यह सब केन्द्रीय नेतृत्व के हित में है. प्रदेशों में वास्तविक जनमत को भटकाने दबाने नहीं तो भटकाने का कितना सीधा नुस्खा है. अंग्रेज़ी और हिन्दी को एक ही कोटि की भाषाएँ बताते रहना और देशी भाषाओं का अंग्रेज़ी विरोध, हिन्दी विरोध की तरफ़ भटकाते रहना. इस सिलसिले की अब वह घड़ी आ गयी है जब पीछे को जाने वाले दो गलत रास्ते बहुत आकर्षक हो उठे हैं. एक यह है कि अंग्रेज़ी को - दो प्रतिशत भारतीयों की जानी भाषा को जिसमें वह किसी तरह लड़खड़ाते हुए ही चल सकते हैं - सत्ता की, सामाजिक प्रतिष्ठा की भाषा हमेशा के लिए बनाये रखा जाये, और इसकी सिद्धी के लिए जो ढोंग, पाखण्ड और चरित्रपतन ज़रूरी हो वह मातृभाषाओं में प्रोतसाहित किया जाये. दूसरा रास्ता है, प्रदेशों को करने दो जो करते हैं, अपनी मातृभाषाओं में पढ़ायें, लिखायें, सरकार चलायें, केन्द्र में हमें अंग्रेज़ी के साथ हिन्दी को ही लगाये रखने दो फ़िर चाहे प्रदेश में आपस में कितनी भी दूरी बढ़े. "सम्पर्क भाषा ही राष्ट्र एकता है, प्रदेशों की परस्पर दूरी कम करने की, सम्पर्क बढ़ाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि उससे विदेशी सम्पर्क भाषा की ज़रूरत कम होती है.
परन्तु मेरे विचार में आगे जाने वाले रास्तों की संख्या दो से भी कम है, एक ही रास्ता है और वह भी ऊबड़ खाबड़ ज़मीन पर से हो कर जाता है. वह भाषा की पूजा तुरंत बंद करके उसके इस्तेमाल का रास्ता है. अंग्रेज़ी का इस्तेमाल करने को संविधान बाध्य नहीं करता, हिन्दी का इस्तेमाल करने की इज़ाज़त देता है. परन्तु सरकारी काम में भी हिन्दी नेता हिन्दी न खुद इस्तेमाल करते हैं न दूसरों को करने देते हैं, क्योंकि उनका तर्क है कि जो हिन्दी नहीं चाहते वे भी केन्द्र की प्रजा हैं और उनके लिए अंग्रेज़ी इस्तेमाल करनी पड़ेगी. इस तरह बिल्कुल स्पष्ट है कि संघ भारतीय भाषाओं को दबाये और 2 प्रतिशत अंग्रेज़ी को बनाये रखने के लिए ही यह किया जा रहा है. अब प्रश्न यह है कि यह सब देखते हुए जो अंग्रेज़ी हटाना चाहते हैं वे लोग क्या पहले आपस में लड़ कर यह बात तय करेंगे कि कौन सी भाषा अंग्रेज़ी की जगह ले तब अंग्रेज़ी जायेगी? अंग्रेज़ों को हटाने के पहले यह निणर्य करने की ज़रूरत बहुत से भारतीय बताते थे और वे वही थे जो अंग्रेज़ों के जाने से सबसे अधिक दुखी होने वाले थे. भारतीय एकता की जो परिकल्पना हमनें अंग्रेज़ी शासनकाल में की थी उसमें भाषा की स्वतंत्रता का मुख्य स्थान था, परन्तु भाषा के प्राधान्य की कल्पना नहीं थी. सब भाषाओं के बोलनेवालों को एक सूत्र में बाँधने के लिए गाँधी ने एक राजनीतिक कार्यक्रम को साधन बनाया था, हिन्दी नामक भाषा के तंत्र मंत्र को नहीं. बाकी उन्होंने कई प्रकार से बार बार कहा था कि मातृभाषा में शिक्षा देना ही स्वाधीन व्यक्ति बनाने का उपाय है और अगर यह काम आज शुरु कर दिया जाये तो पाठ्यपुस्तकें झक मार के बन जायेंगी. भाषावार राज्यों का सिद्धांत भी इसी भावना के अंतर्गत माना गया था. परंतु स्वतंत्रता के बाद भारतीय एकता के सभी प्रतिमान सत्ताधारी पार्टी की एकता के प्रतिमान के साथ जोड़ दिये गये और हम लोगों को कुछ समय के लिए ऐसा समझाया गया कि भाषावार राज्यों में बाँटना तो बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि उससे देश की विविधता को समृद्धि मिलती है और जन समुदाय भावाभिव्यक्ति पाते हैं, परन्तु यदि यह सब भाषाएँ एक जगह एकत्र हो जायें तो देश टूटने लगता है. दरअसल देश नहीं सत्ताधारी दल टूटने लगता है क्योंकि विचार और कर्म के एक होने की प्रक्रिया और तेजी से चलने लगती है.
प्रश्न यह था कि अंग्रेज़ी हटाने के लिए हम ठीक इसी समय क्या करेंगे? जो 1951 में नहीं किया गया, वह क्या था, हिन्दी को निर्णयपूर्वक रातोंरात राजभाषा बना देना या सब भाषाओं को साथ मिला कर प्रयोग करना कि देश अपने लिए रास्ता निकाले. तब सरकार को काम करना था. वह सरकार प्रयोग नहीं कर सकती थी, पर वह सरकार तो निर्णय भी नहीं ले सकी. जो राजनीतिक शक्तियाँ अब देश में उभर रहीं हैं तथा जो परिवर्तन की प्रक्रिया चल रही है उनके सन्दर्भ में अब क्या किया जाना चाहिये जिससे 28 वर्ष की गलतियाँ दूर हों सकें?
ऊबड़खाबड़ रास्ते पर चलने के लिए तैयार होना ही एक उपाय है. रास्ता बनाने की ज़िम्मेदारी जिन पर है उनको भारतीय एकता की एक कहीं अधिक जीवित और स्पंदित परिकल्पना करनी होगी. छत्र के नीचे एक भारत की कल्पना जिसमें न यह भय रहता है कि केन्द्र में सिर्फ़ अंग्रेज़ी या हिन्दी रहने से ही एकता सम्भव है, न यह भ्रम कि दोनो रहने से अंग्रेज़ी जायेगी. आज भाषा के अन्दर के उस खोखल को जो पुजारियों ने उसका ढोल बजाने के लिए किया था, अस्वीकार करने वाली शक्तियाँ उदित हो रहीं हैं. शब्द में सत्य की अवधारण करने के लिए भाषा ने कोई दीप नैवद्य नहीं बरता, उसने असत्य को तोड़ा और वहीं सत्य स्थापित हुआ. 14 भाषाओं के एकत्र इस्तेमाल से देश की एकता टूटेगी इस असत्य को हम तोड़ें तो वास्तविक एकता का सत्य स्थापित होता है. इस सत्य में कोई शास्त्रीयता नहीं है. जीवन की शक्तियों के परस्पर टकराव से एक या दो या तीन बहुमान्य रास्ते निकालना ही इस सत्य की खोज है. भाषाओं की आंतरिक एकता, शब्दों की समानता और संस्कृतियों की समान धर्मिता के बहुत गुणगान करने वाले अंग्रेज़ी समर्थकों को संविधान सम्मत भाषाओं के टकराव से घबराना नहीं चाहिये. यदि प्रत्येक प्रदेश में ऊपर से नीचे तक मातृभाषा और केन्द्र में सभी भाषाओं के इस्तेमाल की व्यवस्था तुरंत की जाये तभी पिछले वर्षों से स्वार्थी नेताओं के हाथों नष्ट हुई राष्ट्रीयता आज सही रास्ते पर चल कर अपनी भारतीयता खोज सकती है, अन्यथा वह अंग्रेज़ी की खिड़की खोल कर बाहर का विश्वदृश्य निहारती रहेगी और भीतर भाषायिक भुखमरी और "श्टारवेशन डेथ" में अर्थभेद करते रहेंगे और शब्दकोश की पूजा होती रहेगी. जो लोग भाषा को मथ कर, कूट कर उसमें से बरतने योग्य कुछ गढ़ते रहे हैं, वे लोग ही आज मातृभाषाओं के इस्तेमाल का मामला आगे बढ़ा सकते हैं. उनकी छटपटाती हुई लड़ाई का यह आखिरी दौर होगा.
***
शनिवार, नवंबर 27, 2010
रविवार, नवंबर 07, 2010
गिरगिट
सुबह तौलिये से सिर पौँछ रहा था तो अचानक हाथ में कुछ लिजलिजा सा लगा. घबरा कर देखा तो छोटा सा हरे रंग कर गिरगिट नीचे गिरा. डरा हुआ था बेचारा. जाने कैसे हमारी तीसरी मंजि़ल तक पहुँच गया था. सोचा कि उसे उठा कर बाहर छोड़ा जाये. उसे पकड़ा तो पहले तो उसने भागने की कोशिश नहीं की, पर थोड़ी देर में ही बचने की कोशिश में कसमसाने लगा. मैने पत्नी से कहा कि उसे उँगली से पकड़ कर रखे तो जल्दी से उसकी एक तस्वीर खींची जाये.

यहाँ के गिरगिट भारतीय गिरगिटों से भिन्न लगते हैं. इनसे मिलता जुलता एक छोटा सा जन्तु दिल्ली में भी दिखता था जिसे हम लोग साँप की नानी कहते थे, जो एक जगह रुकता नहीं था, बहुत तेज़ी से निकल जाता था. यहाँ के यह हरे चितकबरे से गिरगिट बाहर बाग में बहुत बार देखे थे पर उनकी तस्वीरे लेने का मौका पहले नहीं मिला था.
गिरगिट की बात से मन में बचपन की एक भूली बिसरी याद उभर आयी. शायद पाँच या छः साल का था, कमरे में चारपाई पर लेटा था कि छत से एक छिपकली मेरे पेट पर गिरी. मैं डर के मारे उठा और काँपता हुआ माँ से लिपट गया था. फ़िर याद आयी बचपन में स्कूल में खेले जाने वाले खेल लँगड़ी टाँग की जिसमें मैं एक टाँग से बहुत तेज़ी से भागता था और लोग मुझे छिपकली कहते थे. तब था भी बहुत दुबला पतला, हड्डियाँ बाहर निकली हुई, छिपकली जैसा.
तब लोगों का मुझे छिपकली कहना अच्छा नहीं लगता था. अब मोटापे को कम करने की चिंता लगी रहती है और लगता है कि अगर पहले जैसा पतला हो सकूँ तो कितना अच्छा हो!
बचपन में मेरा एक और सपना था, पालतू गिरगिट पालने का. एक दो बार गिरगिट को पकड़ कर उसे धागे से बाँध कर पालतू बनाने की कोशिश भी की थी, लेकिन उसे खिलाने के लिए मक्खियाँ या कीड़े पकड़ना बहुत कठिन लगता था. बेचारा मुझे काटने की कोशिश करता, लेकिन छोटे गिरगिट के दाँत इतने तेज़ नहीं होते थे कि ठीक से काट सके. एक दो बार की कोशिश में ही, कुछ घँटों में गिरगिट को पालतू बनाने का भूत सर से उतर गया. लेकिन तब से गिरगिट का डर मन से निकल सा गया.
खैर आज छोटे गिरगिट से मुलाकात की खुशी में विभिन्न देशों से खींची गिरगिटों की कुछ तस्वीरें प्रस्तुत हैं -
यह पहली तस्वीर कुछ दिन पहले की है, नाईजीरिया की राजधानी अबूजा में जहाँ के गिरगिट, का सिर तो मुझे गिरगिट जैसा लगता है, पर नीचे वाला हिस्सा भारतीय छिपकली जैसा.

यह दूसरी तस्वीर, दिल्ली के महरौली पुरात्तव बाग से एक गिरगिट की है.

तीसरी तस्वीर में ब्राज़ील के पोर्तो नेस्योनाल शहर में बड़े गिरगिट जैसे गोह की है.

यह आखिरी तस्वीर है इतली के एक चिड़ियाघर में रँग बदलने वाले गिरगिट की जो हरी दीवार पर बिल्कुल हरा हो गया है.

क्या आप को गिरगिट अच्छे लगते हैं? क्या कभी आप ने किसी पालतू गिरगिट को देखा है? आप को मौका मिले तो क्या आप पालतू गिरगिट रखना चाहेंगे?
***

यहाँ के गिरगिट भारतीय गिरगिटों से भिन्न लगते हैं. इनसे मिलता जुलता एक छोटा सा जन्तु दिल्ली में भी दिखता था जिसे हम लोग साँप की नानी कहते थे, जो एक जगह रुकता नहीं था, बहुत तेज़ी से निकल जाता था. यहाँ के यह हरे चितकबरे से गिरगिट बाहर बाग में बहुत बार देखे थे पर उनकी तस्वीरे लेने का मौका पहले नहीं मिला था.
गिरगिट की बात से मन में बचपन की एक भूली बिसरी याद उभर आयी. शायद पाँच या छः साल का था, कमरे में चारपाई पर लेटा था कि छत से एक छिपकली मेरे पेट पर गिरी. मैं डर के मारे उठा और काँपता हुआ माँ से लिपट गया था. फ़िर याद आयी बचपन में स्कूल में खेले जाने वाले खेल लँगड़ी टाँग की जिसमें मैं एक टाँग से बहुत तेज़ी से भागता था और लोग मुझे छिपकली कहते थे. तब था भी बहुत दुबला पतला, हड्डियाँ बाहर निकली हुई, छिपकली जैसा.
तब लोगों का मुझे छिपकली कहना अच्छा नहीं लगता था. अब मोटापे को कम करने की चिंता लगी रहती है और लगता है कि अगर पहले जैसा पतला हो सकूँ तो कितना अच्छा हो!
बचपन में मेरा एक और सपना था, पालतू गिरगिट पालने का. एक दो बार गिरगिट को पकड़ कर उसे धागे से बाँध कर पालतू बनाने की कोशिश भी की थी, लेकिन उसे खिलाने के लिए मक्खियाँ या कीड़े पकड़ना बहुत कठिन लगता था. बेचारा मुझे काटने की कोशिश करता, लेकिन छोटे गिरगिट के दाँत इतने तेज़ नहीं होते थे कि ठीक से काट सके. एक दो बार की कोशिश में ही, कुछ घँटों में गिरगिट को पालतू बनाने का भूत सर से उतर गया. लेकिन तब से गिरगिट का डर मन से निकल सा गया.
खैर आज छोटे गिरगिट से मुलाकात की खुशी में विभिन्न देशों से खींची गिरगिटों की कुछ तस्वीरें प्रस्तुत हैं -
यह पहली तस्वीर कुछ दिन पहले की है, नाईजीरिया की राजधानी अबूजा में जहाँ के गिरगिट, का सिर तो मुझे गिरगिट जैसा लगता है, पर नीचे वाला हिस्सा भारतीय छिपकली जैसा.

यह दूसरी तस्वीर, दिल्ली के महरौली पुरात्तव बाग से एक गिरगिट की है.

तीसरी तस्वीर में ब्राज़ील के पोर्तो नेस्योनाल शहर में बड़े गिरगिट जैसे गोह की है.

यह आखिरी तस्वीर है इतली के एक चिड़ियाघर में रँग बदलने वाले गिरगिट की जो हरी दीवार पर बिल्कुल हरा हो गया है.

क्या आप को गिरगिट अच्छे लगते हैं? क्या कभी आप ने किसी पालतू गिरगिट को देखा है? आप को मौका मिले तो क्या आप पालतू गिरगिट रखना चाहेंगे?
***
मंगलवार, नवंबर 02, 2010
हिंदी राष्ट्रवाद का इतिहास
हिन्दी पत्रिका हँस के अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के अंकों में, तीन हिस्सों में "राष्ट्रवाद और हिन्दी समाज" के शीर्षक से प्रसन्न कुमार चौधरी का लम्बा आलेख छपा है जिसे इन दिनों बहुत रुची से पढ़ा. हिन्दी लेखन और विमर्श जगत की सीमाएँ अक्सर अपनी घरेलू बातों तक ही रुक जाती हैं, या बहुत अधिक हो तो, अंग्रेज़ी बोलने वाले विश्व की कुछ बात कर लेती हैं.
उन घरेलू बातों की भी सीमाएँ संकरी हैं, अधिकतर साहित्य, कविता तक के विषयों पर रुकी हुई, ऐसा कुछ विमर्श मौहल्ला लाईव पर हो रहा है जहाँ पर इन्हीं दिनों में अविनाश ने "भारतीयता" पर ओम थानवी, पवन कुमार वर्मा आदि की बहस के बारे में लिखा, फ़िर उस पर विजय शर्मा का एक आलेख भी निकला.
प्रसन्न चौधरी का आलेख सभ्यता, संस्कृति, भाषा के विषयों पर विहंगम दृष्टि है जिसमें सारे विश्व के विभिन्न क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक युगों के अनेक उदाहरण हैं. यह आलेख उन्होंने सुधीर रंजन सिंह की पुस्तक "हिंदी समुदाय और राष्ट्रवाद" की आलोचना के रूप में लिखना शुरु किया था, लेकिन पुस्तक की आलोचना आलेख का छोटा सा हिस्सा है.
वह लेख का प्रारम्भ राष्ट्र, राष्ट्र राज्य और राष्ट्रवाद के आधुनिक यूरोप के देशों के बनने से जुड़े अर्थों के विवेचन से करते हैं, कैसे राष्ट्रवाद के सिद्धांतों को विख्यातित किया गया, इन सिद्धांतों की क्या आलोचनाएँ हुईं, आदि. इस हिस्से में उनका विमर्श कि किस तरह यूरोप ने अपने नागरिकों के लिए सदियों से चले आ रहे शोषण को बदल कर नये आधुनिक समतावादी समाज की संरचना की और साथ ही, उपनिवेशवाद द्वारा, अपने देशों की सीमाओं के बाहर शोषण के नये रास्ते खोले, बहुत अच्छी तरह से किया गया है. इस विमर्श में वह पूर्व में रूस से ले कर पश्चिमी यूरोप तक की बात करते हैं, और साथ साथ, भारत तथा अन्य उपनिवेशित देशों में होने वाले विमर्श की परम्परा का ज़िक्र भी.
आलेख के दूसरे हिस्से में बात है भारत में प्रभाव डालने वाली पश्चिमी विचार परम्परा की और दूसरी ओर, भारत के अपने इतिहास, धर्म और दर्शन से जुड़ी सोच की, और किस तरह से यह दो दृष्टियाँ कभी एक दूसरे से मिलती हैं, और कभी एक दूसरे से अलग हो कर प्रतिद्वंदी बन जाती हैं. इस दूसरी दृष्टि को वह भारत से बाहर के भी विचारकों में खोजते हैं. आलेख का तीसरा भाग, हिंदी समुदाय और आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास से ले कर, हिंदी समुदाय के राष्ट्रवाद का विश्लेषण करता है.
आलेख का पूरा अर्थ समझने के लिए उसे दो बार पढ़ा. उनकी हर बात से सहमत होना संभव नहीं, लेकिन यह मानना पड़ेगा कि उन्होंने अपनी बात को उसके ऐतिहासिक संदर्भ से ले कर, आज तक के विकास तक, बहुत खूबी से व्यक्त किया है. लेख पढ़ते हुए कई बार मन में आया कि काश वह यहीं कहीं आसपास रहते तो उनके साथ बहस करने में कितना आनंद आता!
हँस को इस लम्बे आलेख को पूरा छापने की लिए धन्यवाद.
उन घरेलू बातों की भी सीमाएँ संकरी हैं, अधिकतर साहित्य, कविता तक के विषयों पर रुकी हुई, ऐसा कुछ विमर्श मौहल्ला लाईव पर हो रहा है जहाँ पर इन्हीं दिनों में अविनाश ने "भारतीयता" पर ओम थानवी, पवन कुमार वर्मा आदि की बहस के बारे में लिखा, फ़िर उस पर विजय शर्मा का एक आलेख भी निकला.
प्रसन्न चौधरी का आलेख सभ्यता, संस्कृति, भाषा के विषयों पर विहंगम दृष्टि है जिसमें सारे विश्व के विभिन्न क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक युगों के अनेक उदाहरण हैं. यह आलेख उन्होंने सुधीर रंजन सिंह की पुस्तक "हिंदी समुदाय और राष्ट्रवाद" की आलोचना के रूप में लिखना शुरु किया था, लेकिन पुस्तक की आलोचना आलेख का छोटा सा हिस्सा है.
वह लेख का प्रारम्भ राष्ट्र, राष्ट्र राज्य और राष्ट्रवाद के आधुनिक यूरोप के देशों के बनने से जुड़े अर्थों के विवेचन से करते हैं, कैसे राष्ट्रवाद के सिद्धांतों को विख्यातित किया गया, इन सिद्धांतों की क्या आलोचनाएँ हुईं, आदि. इस हिस्से में उनका विमर्श कि किस तरह यूरोप ने अपने नागरिकों के लिए सदियों से चले आ रहे शोषण को बदल कर नये आधुनिक समतावादी समाज की संरचना की और साथ ही, उपनिवेशवाद द्वारा, अपने देशों की सीमाओं के बाहर शोषण के नये रास्ते खोले, बहुत अच्छी तरह से किया गया है. इस विमर्श में वह पूर्व में रूस से ले कर पश्चिमी यूरोप तक की बात करते हैं, और साथ साथ, भारत तथा अन्य उपनिवेशित देशों में होने वाले विमर्श की परम्परा का ज़िक्र भी.
आलेख के दूसरे हिस्से में बात है भारत में प्रभाव डालने वाली पश्चिमी विचार परम्परा की और दूसरी ओर, भारत के अपने इतिहास, धर्म और दर्शन से जुड़ी सोच की, और किस तरह से यह दो दृष्टियाँ कभी एक दूसरे से मिलती हैं, और कभी एक दूसरे से अलग हो कर प्रतिद्वंदी बन जाती हैं. इस दूसरी दृष्टि को वह भारत से बाहर के भी विचारकों में खोजते हैं. आलेख का तीसरा भाग, हिंदी समुदाय और आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास से ले कर, हिंदी समुदाय के राष्ट्रवाद का विश्लेषण करता है.
आलेख का पूरा अर्थ समझने के लिए उसे दो बार पढ़ा. उनकी हर बात से सहमत होना संभव नहीं, लेकिन यह मानना पड़ेगा कि उन्होंने अपनी बात को उसके ऐतिहासिक संदर्भ से ले कर, आज तक के विकास तक, बहुत खूबी से व्यक्त किया है. लेख पढ़ते हुए कई बार मन में आया कि काश वह यहीं कहीं आसपास रहते तो उनके साथ बहस करने में कितना आनंद आता!
हँस को इस लम्बे आलेख को पूरा छापने की लिए धन्यवाद.
सोमवार, नवंबर 01, 2010
शाह रुख और महाश्वेता देवी
रोम फ़िल्म फेस्टीवल में कल रात को एक ओर थे कर्ण जौहर और शाहरुख खान, "माई नेम इज़ खान" के साथ. दूसरी ओर थी महाश्वेता देवी जिनकी कहानी पर इतालवी निर्देशक इतालो स्वीनेल्ली (Italo Spinelli) ने फ़िल्म बनायी है, "गँगोर" (Gangor).
शाहरुख रोम आने वाले हैं इसका हल्ला तो इटली के बोलीवुड प्रेमियों में कई हफ्तों से चल रहा था. पहले यही बहस थी कि आयेंगे या नहीं? रोम में बोलीवुड के नृत्य करने वाली लड़कियों से जब पूछा गया कि क्या वह शाहरुख की फ़िल्म से पहले वहाँ रेड कार्पट पर नृत्य करेंगी तो उनके हर्ष की सीमा नहीं थी. उनमें से एक युवती कुछ महीने पहले जब मुंबई में जोन एब्राहम से मिल कर आयी थी, तो फेसबुक पर कई महीनों तक उस एक मिलन की गाथा के किस्से सुने थे. अब जिन युवतियों को शाहरुख के सामने नृत्य दिखाने का मौका मिलेगा, तो उसके किस्से तो अगले बारह महीने तक सुनने को मिलेंगे!
खैर आज सुबह के अखबारों में "माई नेम इज़ खान" की आलोचना ठीक ठाक ही है. सबसे अधिक बिकने वाले अखबार "कोरिएरे देल्ला सेरा" (Corriere della Sera) ने शाहरुख को भारत का टाम क्रूज़ कहा है.
स्पीनेल्ली की फ़िल्म "गँगोर" की आलोचना अधिक दिलचस्प है. फ़िल्म की मुख्य अभिनेत्री प्रियँका बोस की बहुत प्रशँसा की गयी है. फ़िल्म की कहानी है, बच्चे को दूध पिलाती युवती गँगोर की, जिसके नँगे वक्ष की तस्वीर पर हल्ला मच जाता है और पुलिस अत्याचार जिसे शरीर बेचने वाली बना देता है.
"माई नेम इज़ खान" इतालवी सिनेमा हालों में 26 नवम्बर को प्रदर्शित होगी, गँगोर को सिनेमा में निकलने का मौका मिलेगा या नहीं, यह नहीं पता.
शाहरुख रोम आने वाले हैं इसका हल्ला तो इटली के बोलीवुड प्रेमियों में कई हफ्तों से चल रहा था. पहले यही बहस थी कि आयेंगे या नहीं? रोम में बोलीवुड के नृत्य करने वाली लड़कियों से जब पूछा गया कि क्या वह शाहरुख की फ़िल्म से पहले वहाँ रेड कार्पट पर नृत्य करेंगी तो उनके हर्ष की सीमा नहीं थी. उनमें से एक युवती कुछ महीने पहले जब मुंबई में जोन एब्राहम से मिल कर आयी थी, तो फेसबुक पर कई महीनों तक उस एक मिलन की गाथा के किस्से सुने थे. अब जिन युवतियों को शाहरुख के सामने नृत्य दिखाने का मौका मिलेगा, तो उसके किस्से तो अगले बारह महीने तक सुनने को मिलेंगे!
स्पीनेल्ली की फ़िल्म "गँगोर" की आलोचना अधिक दिलचस्प है. फ़िल्म की मुख्य अभिनेत्री प्रियँका बोस की बहुत प्रशँसा की गयी है. फ़िल्म की कहानी है, बच्चे को दूध पिलाती युवती गँगोर की, जिसके नँगे वक्ष की तस्वीर पर हल्ला मच जाता है और पुलिस अत्याचार जिसे शरीर बेचने वाली बना देता है.
"माई नेम इज़ खान" इतालवी सिनेमा हालों में 26 नवम्बर को प्रदर्शित होगी, गँगोर को सिनेमा में निकलने का मौका मिलेगा या नहीं, यह नहीं पता.
शुक्रवार, अक्तूबर 01, 2010
अयोध्या के राम
आज आखिरकार अयोध्या के मुकदमें का फैसला हो ही गया. पिछले कई दिनों से चिन्ता हो रही थी कि क्या होगा, फ़िर से दंगे, मार पीट तो नहीं शुरु हो जायेंगे!
जब बबरी मस्जिद को ढाया गया था तब 1992 में इंटरनेट आदि कुछ नहीं था, इटली में उसका समाचार तक मुझे बहुत दिन के बाद मिला था, लेकिन उसके कुछ वर्ष बाद मैंने उसके कुछ परिणाम बम्बई में देखे थे, जब भिवँडी की झोपड़पट्टी में दंगों में हिंसा के शिकार परिवारों से मिला था. धर्म के नाम पर मासूमों की जान लेना, इससे बड़ा धर्म का अपमान क्या हो सकता है?
अयोध्या में राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के विवाद का क्या निवारण हो, इसमें मुझे उन सुझावों से कभी सहमति नहीं हुई जो वहाँ अस्पताल या विद्यालय बनाने की बात करते थे. इसलिए नहीं कि मुझे अस्पतालों या विद्यालयों की उपयोगिता की समझ नहीं. बात मेरे धार्मिक विचारों की भी नहीं है.
भारत के अन्य करोड़ों हिंदूओं की तरह, मेरे लिए भगवान का स्वरूप वो है जो गायत्री मंत्र में व्याख्यित किया जाता है, यानि भगवान जिसका न कोई आदि है न अंत, जो सर्वव्यापा, सर्वज्ञानी है, जिसका कोई रूप या आकार नहीं. इसलिए मेरी समझ उस भगवान को राम, कृष्ण या शिव के रूप में चिन्ह की तरह स्वीकार करती है, पर उसकी प्रार्थना के लिए मुझे किसी मंदिर या मूर्ति की आवश्यकता नहीं. हर धर्म में, चाहे वह ईसाई हो या मुसलमान, सिख या पारसी या बहायी, अंत में मुझे यही आध्यात्मिक सच दिखता है.
लेकिन मेरे विचार में भारत में मुझ जैसे आध्यात्मिक हिंदूओं से कहीं गुणा अधिक वह लोग हैं जिनके लिए राम ही भगवान का रूप हैं, उन्हीं में उनकी आस्था और विश्वास हैं. इस आस्था में सच क्या या झूठ क्या, इतिहास क्या कहता है या पुरातत्व क्या कहता है, उस सबका कुछ अर्थ नहीं. सभी धर्मों को मानने वाले अधिकतर ऐसे ही होते हैं. लोगों को इस बात का कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं चाहिये कि जीसस ने सचमुच समुद्र को चीरा था या नहीं, या फ़िर पैगम्बर मुहम्मद ने सचमुच अल्ला की आवाज़ सुनी थी या नहीं, यह विज्ञान या तर्क का सवाल नहीं, आस्था का है, उनके लिए तो उनका पैगम्बर ही ईश्वर का दूत और पुत्र है.
करोड़ों लोगों के इसी विश्वास के बारे में सोच कर मेरे विचार में अयोध्या में उस जगह पर राम का मन्दिर बनाने देना चाहिये, क्योंकि अगर सोचूँ कि ईसाई जिस जगह पर मानते हैं कि येसू का जन्म हुआ था, या मसलमान मक्का और मदीना में जिन जगहों को अपने पैगम्बर से जुड़ा मानते हैं, उनसे उनके विश्वास को छीन कर, उस पर कुछ बनाने की बात कभी कोई नहीं कर सकता. तो राम को मानने वालों के साथ ही तर्क या विज्ञान और सबूत की बात क्यों की जाये?
बचपन में अपनी दादी से रामायण की बहुत कहानियाँ सुनता था. उन कहानियों के नायक राम न शबरी से भेदभाव करते थे न सरयू पार कराने वाले केवट से, उनके सबसे बड़े भक्त और स्वयं पूजे जाने वाले हनुमान तो वानर जाति के थे. उन कथाओं के राम क्या धर्मी, विधर्मी का भेद करेंगे? मेरे विचार में नहीं, वह तो सबको अपनायेंगे. इसलिए मेरा बस चलेगा तो उस राम के मन्दिर को सब धर्मों को लोग मिल कर बनवायेंगे और विश्व हिंदू परिषद, हिंदू महासभा, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आदि सब राम मन्दिर बनवाना चाहने वाले दल मिल कर उस मन्दिर में बाबरी मस्जिद का कमरा भी बनायेगे, यूसू का गिरजा भी, नानक का गुरुद्वारा भी, यहूदियों का सिनागोग भी. घृणा और भेद भाव के बदले अगर अयोध्या के राम सब धर्मों को मान देंगे तभी सचमुच अयोध्या में वापस आयेंगे.
जब बबरी मस्जिद को ढाया गया था तब 1992 में इंटरनेट आदि कुछ नहीं था, इटली में उसका समाचार तक मुझे बहुत दिन के बाद मिला था, लेकिन उसके कुछ वर्ष बाद मैंने उसके कुछ परिणाम बम्बई में देखे थे, जब भिवँडी की झोपड़पट्टी में दंगों में हिंसा के शिकार परिवारों से मिला था. धर्म के नाम पर मासूमों की जान लेना, इससे बड़ा धर्म का अपमान क्या हो सकता है?
अयोध्या में राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के विवाद का क्या निवारण हो, इसमें मुझे उन सुझावों से कभी सहमति नहीं हुई जो वहाँ अस्पताल या विद्यालय बनाने की बात करते थे. इसलिए नहीं कि मुझे अस्पतालों या विद्यालयों की उपयोगिता की समझ नहीं. बात मेरे धार्मिक विचारों की भी नहीं है.
भारत के अन्य करोड़ों हिंदूओं की तरह, मेरे लिए भगवान का स्वरूप वो है जो गायत्री मंत्र में व्याख्यित किया जाता है, यानि भगवान जिसका न कोई आदि है न अंत, जो सर्वव्यापा, सर्वज्ञानी है, जिसका कोई रूप या आकार नहीं. इसलिए मेरी समझ उस भगवान को राम, कृष्ण या शिव के रूप में चिन्ह की तरह स्वीकार करती है, पर उसकी प्रार्थना के लिए मुझे किसी मंदिर या मूर्ति की आवश्यकता नहीं. हर धर्म में, चाहे वह ईसाई हो या मुसलमान, सिख या पारसी या बहायी, अंत में मुझे यही आध्यात्मिक सच दिखता है.
लेकिन मेरे विचार में भारत में मुझ जैसे आध्यात्मिक हिंदूओं से कहीं गुणा अधिक वह लोग हैं जिनके लिए राम ही भगवान का रूप हैं, उन्हीं में उनकी आस्था और विश्वास हैं. इस आस्था में सच क्या या झूठ क्या, इतिहास क्या कहता है या पुरातत्व क्या कहता है, उस सबका कुछ अर्थ नहीं. सभी धर्मों को मानने वाले अधिकतर ऐसे ही होते हैं. लोगों को इस बात का कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं चाहिये कि जीसस ने सचमुच समुद्र को चीरा था या नहीं, या फ़िर पैगम्बर मुहम्मद ने सचमुच अल्ला की आवाज़ सुनी थी या नहीं, यह विज्ञान या तर्क का सवाल नहीं, आस्था का है, उनके लिए तो उनका पैगम्बर ही ईश्वर का दूत और पुत्र है.
करोड़ों लोगों के इसी विश्वास के बारे में सोच कर मेरे विचार में अयोध्या में उस जगह पर राम का मन्दिर बनाने देना चाहिये, क्योंकि अगर सोचूँ कि ईसाई जिस जगह पर मानते हैं कि येसू का जन्म हुआ था, या मसलमान मक्का और मदीना में जिन जगहों को अपने पैगम्बर से जुड़ा मानते हैं, उनसे उनके विश्वास को छीन कर, उस पर कुछ बनाने की बात कभी कोई नहीं कर सकता. तो राम को मानने वालों के साथ ही तर्क या विज्ञान और सबूत की बात क्यों की जाये?
बचपन में अपनी दादी से रामायण की बहुत कहानियाँ सुनता था. उन कहानियों के नायक राम न शबरी से भेदभाव करते थे न सरयू पार कराने वाले केवट से, उनके सबसे बड़े भक्त और स्वयं पूजे जाने वाले हनुमान तो वानर जाति के थे. उन कथाओं के राम क्या धर्मी, विधर्मी का भेद करेंगे? मेरे विचार में नहीं, वह तो सबको अपनायेंगे. इसलिए मेरा बस चलेगा तो उस राम के मन्दिर को सब धर्मों को लोग मिल कर बनवायेंगे और विश्व हिंदू परिषद, हिंदू महासभा, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आदि सब राम मन्दिर बनवाना चाहने वाले दल मिल कर उस मन्दिर में बाबरी मस्जिद का कमरा भी बनायेगे, यूसू का गिरजा भी, नानक का गुरुद्वारा भी, यहूदियों का सिनागोग भी. घृणा और भेद भाव के बदले अगर अयोध्या के राम सब धर्मों को मान देंगे तभी सचमुच अयोध्या में वापस आयेंगे.
सोमवार, सितंबर 20, 2010
ज़ंग लगे गुलाब
हल्की हल्की बारिश आ रही है. हवा की ठंडक से झुरझुरी सी आ रही है. ग्रीष्म ऋतु कब गयी और शिशर कब आया, पता ही नहीं चला. पेड़ों के कथ्थई, भूरे, पीले पत्तों की चादर बिछी है बाग में, उन पर चलो तो छपक छपक की गीली आवाज़ आती है और जूतों पर चिपक जाते हैं. लगता है कि बस पलक झपकूँगा तो वर्ष बीत जायेगा, समय इतनी तेज़ी से निकल रहा है. विश्वास नहीं होता कि कल लगभग इसी समय मैं मापूतो शहर में था.
चमकती हरी घास पर पानी की बूँदें. तम्बारा के बूढ़े नवयुवकों के चेहरे सामने आ जाते हैं. बालों में, आँखों में, नाक में धूल भर गयी थी. सात घँटों तक कच्ची सड़क पर जीप के धक्के खाने से कमर दर्द कर रही थी, सुबह सुबह चाय के साथ बस एक केला खाया था, भूख भी लगी थी. वे सब हमारे इन्तज़ार में स्वयंसेवकों की संस्था के दफ़्तर में बैठे थे. आसपास कोई और पक्का घर नहीं था, केवल झोपड़ियाँ. "स्वास्थ्य के अतिरिक्त और क्या समस्याएँ हैं यहाँ की?" मैंने टीबी, कुष्ठ रोग और एड्स की रिपोर्ट पढ़ने वाले नवयुवक से पूछा था. मुझे कुछ देर तक देखता रहा था, फ़िर धीरे से बोला था, "भूख, भूख है हमारी सबसे बड़ी समस्या, कुछ खाने को नहीं मिलता." उसके पिचके गाल और निराश आँखों में दबे गुस्से से हतप्रभ रह गया था, अपने आप पर बहुत शर्म आयी थी.
दस साल बीत गये लड़ाई को खत्म हुए, अब जगह जगह दबे बम जिससे बच्चों की टाँगें उड़ जाती है, बहुत कम हैं. लेकिन बीहड़ जंगल में अब भी कोई चिड़िया पशु आसानी से नहीं दिखते, लड़ाई में सब खत्म हो गया. थोड़ी दूर ही बहती है जम्बेज़ी नदी, जिसका पाट इतना चौड़ा है कि दूसरा सिरा नहीं दिखता, पर गाँव वाले बारिश के पानी के लिए तरस रहे हैं. हथियार मिल जाते हैं इस दुनिया में, बम मिल जाते हैं, सड़क, पानी नहीं मिलते.
"मेरा एक साल का बेटा मरा, पेट खराब हुआ था उसका", "मेरी छः महीने की बेटी मरी, मीसल्स से", "मेरा तीन महीने का बच्चा मरा मलेरिया से", मेरे एक अन्य प्रश्न के उत्तर में उनके मरे हुए छोटे बच्चों की सूची खत्म होने को नहीं आती थी.
"यह सब सोचने से क्या फ़ायदा", मैं स्वयं से कहता हूँ. यहाँ हरे भरे बाग में कुत्ते को सैर कराते समय, अफ्रीकी गाँव की धूल मिट्टी सपना सा लगती है.
छप छप करते हैं जूते पानी पर. क्यारी में लगे पीले गुलाब को देख कर पोलैंड के कवियत्री मारिया पाउलीकोव्सका की कविता की पंक्तियाँ याद आती हैं
चमकती हरी घास पर पानी की बूँदें. तम्बारा के बूढ़े नवयुवकों के चेहरे सामने आ जाते हैं. बालों में, आँखों में, नाक में धूल भर गयी थी. सात घँटों तक कच्ची सड़क पर जीप के धक्के खाने से कमर दर्द कर रही थी, सुबह सुबह चाय के साथ बस एक केला खाया था, भूख भी लगी थी. वे सब हमारे इन्तज़ार में स्वयंसेवकों की संस्था के दफ़्तर में बैठे थे. आसपास कोई और पक्का घर नहीं था, केवल झोपड़ियाँ. "स्वास्थ्य के अतिरिक्त और क्या समस्याएँ हैं यहाँ की?" मैंने टीबी, कुष्ठ रोग और एड्स की रिपोर्ट पढ़ने वाले नवयुवक से पूछा था. मुझे कुछ देर तक देखता रहा था, फ़िर धीरे से बोला था, "भूख, भूख है हमारी सबसे बड़ी समस्या, कुछ खाने को नहीं मिलता." उसके पिचके गाल और निराश आँखों में दबे गुस्से से हतप्रभ रह गया था, अपने आप पर बहुत शर्म आयी थी.
दस साल बीत गये लड़ाई को खत्म हुए, अब जगह जगह दबे बम जिससे बच्चों की टाँगें उड़ जाती है, बहुत कम हैं. लेकिन बीहड़ जंगल में अब भी कोई चिड़िया पशु आसानी से नहीं दिखते, लड़ाई में सब खत्म हो गया. थोड़ी दूर ही बहती है जम्बेज़ी नदी, जिसका पाट इतना चौड़ा है कि दूसरा सिरा नहीं दिखता, पर गाँव वाले बारिश के पानी के लिए तरस रहे हैं. हथियार मिल जाते हैं इस दुनिया में, बम मिल जाते हैं, सड़क, पानी नहीं मिलते.
"मेरा एक साल का बेटा मरा, पेट खराब हुआ था उसका", "मेरी छः महीने की बेटी मरी, मीसल्स से", "मेरा तीन महीने का बच्चा मरा मलेरिया से", मेरे एक अन्य प्रश्न के उत्तर में उनके मरे हुए छोटे बच्चों की सूची खत्म होने को नहीं आती थी.
"यह सब सोचने से क्या फ़ायदा", मैं स्वयं से कहता हूँ. यहाँ हरे भरे बाग में कुत्ते को सैर कराते समय, अफ्रीकी गाँव की धूल मिट्टी सपना सा लगती है.
छप छप करते हैं जूते पानी पर. क्यारी में लगे पीले गुलाब को देख कर पोलैंड के कवियत्री मारिया पाउलीकोव्सका की कविता की पंक्तियाँ याद आती हैं
पतझड़ के जंग लगे गुलाबकश्मीर में भी गुलाबों को जंग लगा होगा. पत्थर फैंकने वाले किशोरों की लाशों का. उनकी माँओं के आँसुओं से अब तक झील में बाढ़ नहीं आयी क्या?
बारिश के सफेद हाशिये को देखते हैं - बारिश आसमान को धरती से सिल रही है
झुरझुरियों और टाँकों के साथ
शनिवार, अगस्त 21, 2010
अंतिम श्रद्धाँजलि - राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त
टिप्पणीः यह आलेख स्व. डा. सावित्री सिन्हा के आलेख संग्रह "तुला और तारे", (नेशनल पब्लिशिंग हाउस दिल्ली, 1966) से है. दद्दा (राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त) का देहांत 12 दिसंबर 1964 में हुआ.
***
 उस दिन दद्दा की विदा के बाद हम सबका मन भारी हो रहा था. स्टेशन के वेटिंग रूम में थोड़ी देर के लिए उनके गले में जलन सी होने लगी थी, इसलिए हमारी चिन्ता और भी बढ़ गयी थी. रात में दो तीन बार आँखें खुल गयीं. सुबह तड़के ही मुझसे रहा न गया और झाँसी के लिए ट्रंककाल बुक करवायी, न जाने मन में कैसी कैसी दुश्चिताएँ उठती रहीं, परन्तु टेलीफोन एक्सचेंज की कृपा से काल झाँसी नहीं, राँची की मिली, वह भी ग्यारह बजे दिन को. मेरे क्लास का समय हो रहा था इसलिए विवश हो कर उसे कैंसल करवाना पड़ा. पत्र लिखने की सोच रही थी कि ज्वरग्रस्त हो गयी और फ़िर उसी ज्वर में खबर मिली कि दद्दा नहीं रहे. जीवन की कुछ अमूल्य निधियों में मेरे लिए सबसे गौरवपूर्ण निधि दद्दा का अकारण स्नेह था. कहाँ मैं, एक अकिंचन, महत्वहीन तुच्छ व्यक्ति, और कहाँ भारत के महान राष्ट्रकवि के वात्सल्य का अगाध समुद्र. आज लग रहा है जैसे मेरी अपात्रता और अकिंचता ने ही मुझे उस अपार वैभव से वंचित कर दिया है. न जाने कौन सा सूत्र पिछले तीन दिनों से दद्दा के लिए बैचेन कर रहा था. निधन का समाचार कान में पड़ते ही मैं भरे बुखार में रजाई छोड़ कर उठ खड़ी हुई, डा. नगेन्द्र के घर फोन किया, मालूम पड़ा कि जब से चिरगाँव से ट्रंककाल आयी है, डा. साहब कमरा बन्द किये बैठे हैं. डा. विजयेनद्र स्नातक जी के यहाँ फोन किया तो मालूम हुआ उन्हें यह सन्देश डा. साहब के यहाँ से ही मिला था. मेरी अस्वस्थता और रुग्णता के कारण मुझे खबर नहीं दी गयी. मन किया किसी तरह चिरगाँव उड़ जाऊँ. दद्दा के अन्तिम दर्शन तो मिल जायेंगे, परन्तु फोन से पता चला कि उनकी अन्त्येष्टि क्रिया के लिए निर्धारित समय तक पहुंचना सम्भव नहीं है. और फ़िर दद्दा की बातें, उनकी हँसी, उनके लाड़ दुलार, कानों में गूँजते रहे, उनकी तस्वीर आँखों के आँसुओं के साथ उभरती रही.
उस दिन दद्दा की विदा के बाद हम सबका मन भारी हो रहा था. स्टेशन के वेटिंग रूम में थोड़ी देर के लिए उनके गले में जलन सी होने लगी थी, इसलिए हमारी चिन्ता और भी बढ़ गयी थी. रात में दो तीन बार आँखें खुल गयीं. सुबह तड़के ही मुझसे रहा न गया और झाँसी के लिए ट्रंककाल बुक करवायी, न जाने मन में कैसी कैसी दुश्चिताएँ उठती रहीं, परन्तु टेलीफोन एक्सचेंज की कृपा से काल झाँसी नहीं, राँची की मिली, वह भी ग्यारह बजे दिन को. मेरे क्लास का समय हो रहा था इसलिए विवश हो कर उसे कैंसल करवाना पड़ा. पत्र लिखने की सोच रही थी कि ज्वरग्रस्त हो गयी और फ़िर उसी ज्वर में खबर मिली कि दद्दा नहीं रहे. जीवन की कुछ अमूल्य निधियों में मेरे लिए सबसे गौरवपूर्ण निधि दद्दा का अकारण स्नेह था. कहाँ मैं, एक अकिंचन, महत्वहीन तुच्छ व्यक्ति, और कहाँ भारत के महान राष्ट्रकवि के वात्सल्य का अगाध समुद्र. आज लग रहा है जैसे मेरी अपात्रता और अकिंचता ने ही मुझे उस अपार वैभव से वंचित कर दिया है. न जाने कौन सा सूत्र पिछले तीन दिनों से दद्दा के लिए बैचेन कर रहा था. निधन का समाचार कान में पड़ते ही मैं भरे बुखार में रजाई छोड़ कर उठ खड़ी हुई, डा. नगेन्द्र के घर फोन किया, मालूम पड़ा कि जब से चिरगाँव से ट्रंककाल आयी है, डा. साहब कमरा बन्द किये बैठे हैं. डा. विजयेनद्र स्नातक जी के यहाँ फोन किया तो मालूम हुआ उन्हें यह सन्देश डा. साहब के यहाँ से ही मिला था. मेरी अस्वस्थता और रुग्णता के कारण मुझे खबर नहीं दी गयी. मन किया किसी तरह चिरगाँव उड़ जाऊँ. दद्दा के अन्तिम दर्शन तो मिल जायेंगे, परन्तु फोन से पता चला कि उनकी अन्त्येष्टि क्रिया के लिए निर्धारित समय तक पहुंचना सम्भव नहीं है. और फ़िर दद्दा की बातें, उनकी हँसी, उनके लाड़ दुलार, कानों में गूँजते रहे, उनकी तस्वीर आँखों के आँसुओं के साथ उभरती रही.
दद्दा की त्रयोदशी में सम्मिलित होने के लिए दिल्ली से एक स्पेशल बोगी का प्रबन्ध हो गया था. यात्रियों में से अधिक ऐसे थे जिन्हें दद्दा चिरगाँव आने का निमन्त्रण दे गये थे, पर अपने अतिथियों को हाथों हाथ लेने वाला अतिथेय, अपने स्वभाव और संस्कार के विरुद्ध सबको अपने घर बुला कर स्वयं अदृष्य हो गया था. रात को लगभग डेढ़ बजे गाड़ी झाँसी पहुँच गयी, और वहीं हमारा डिब्बा कट गया. झाँसी का स्टेशन फ़िर अपने साथ अनेक स्मृतियाँ ले कर सामने खड़ा हो गया. पिछली दो बार जब हम आये थे, दद्दा स्टेशन पर आतुरता से हमारा इन्तजार करते हुए मिले थे, उनके चेहरे पर उमड़ता हुआ वह आह्लाद, वह स्फटिक सा व्यवहार आज इस लेखनी में कैसे बाँधू -
हिन्दी के प्रसिद्ध उपन्यासकार श्रद्धेय वृन्दावनलाल वर्मा के प्रेस में हमारे भोजन की व्यवस्था थी. निःशब्द भोजन चल रहा था जैसे यह कोई यांत्रिक काम था जिसे किसी तरह पूरा करना था. ग्रास थाली से हाथ में आ कर मुँह में जा रहे थे और पिछली बार झाँसी की हवेली में भोजन करते हुए दद्दा के स्नेहपूर्ण आग्रह कान में गूँज रहे थे. श्रुतिपुट से आयी दद्दा की स्मृतियाँ पलकों में न समा सकने के कारण आँसू बन कर बिखर रही थीं.
भोजनोपरान्त, हम बस में बैठ कर चिरगाँव चले. चारों ओर की हरियाली भरी पहाड़ियों का हमारे लिए कोई अर्थ नहीं था, अतीत के मौन ताने बाने में बस की घरघराहट और आसपास का शोर गुल जैसे लुप्त हो गया था और फ़िर उसके बाद हम बेतवा के बाँध पर आये. यह स्थान दद्दा को बहुत प्रिय था, मेरे मानस चक्षु के सामने दद्दा बोल रहे थे, "पंडित जी (पं. जवाहरलाल नेहरू) को यह स्थान बहुत अच्छा लगा था, वे इसे देख कर भाव विभोर काफ़ी देर तक खड़े रहे, हमारे मना करते करते भागते दौड़ते वहाँ .. वहाँ.. दूर तक पहुँच गये थे." उस दिन दद्दा बेतवा के किनारे खड़े हो कर दिवंगत राष्ट्रनायक को भरे गले से याद कर रहे थे और आज राष्ट्रकवि के अभाव में बेतवा की पछाड़ खाती लहरों के निकट ठहरने का हमें साहस नहीं हुआ. उदास और क्लांत हृदय यात्री बस से उतर पैदल मौन गुप्त बंधुओं की प्रसिद्ध बखरी की ओर चले, "चिरगाँव की शोभा" को झुक झुक प्रणाम करने वाली, हाट की जनता हमारी ओर उदास नेत्रों और म्लान मुख से देख रही थी, जैसे उन्हें यह पूछने की आवश्यकता ही नहीं थी कि हम वहाँ किस उद्देश्य से गये हैं. बखरी के फाटक पर गम्भीर विषाद से युक्त गिरधारी ने मौन विनयाचार में हाथ जोड़े, उसके होंठ सिहरे और आँखें आँसुओं से भर आयीं. गुप्त बंधुओं की पुश्तैनी बखरी मौन साधे सविषाद पाषाण बनी खड़ी थी, हमारे पहुँचते ही प्रस्तर मूर्तियों की तरह निश्चल खड़े दद्दा के स्वजन यन्त्रवत चल कर निकट आये और फ़िर बखरी में कुहराम मच गया, दद्दा के पुत्र उर्मिल जी डा. नगेन्द्र के अंक में मुँह छिपा कर क्रन्दन कर उठे और फ़िर सारी बखरी में रुदन और विलाप का स्वर छा गया.
हिम्मत नहीं होती थी अंदर जाने की. "गौरवमंण्डित सुहागनी" के करुण वैधव्य का सामना करने का साहस मुझे नहीं हो रहा था, मैं बड़ी हिम्मत करके अन्दर गयी और जिया के वलयशून्य हाथों ने मुझे लपेट लिया, उनकी आँखों से निरन्तर आँसू बहते रहे, साकेत की "मूर्तिमति ममता माया" आज अपना मुँह अवगुण्ठन में लपेटे वटवृक्ष की छाया से छिन्न लता सी क्लांत, शिथिल हो रही थी. शान्ति, दद्दा की पुत्रवधू अपनी गोद में नन्ही सी बिटिया को लिए बिलख रही थी.
श्राद्ध पूरा हुआ. होम का धूँआ सारी बखरी पर छा गया, जिया ने लाल जोड़ा उतार कर श्वेत वस्त्र धारण किया और गु्प्त कुल की बखरी की दीवारें जैसे सिर धुन धुन कर रोने लगीं. उसके इतिहास का उज्जवलतम अध्याय अब नये चरण में प्रवेश कर रहा था, वह माई का लाल जिसने पितृव्यों को भौतिक ऋण से मुक्त किया था, अपने कुल के उपास्यदेव राम की नयी प्रतिष्ठा द्वारा उनका आध्यात्मिक ऋण चुकाया. जिसकी वाणी से सारा राष्ट्र प्रेरणा स्फूर्त हो उठा आज इस बखरी से सदा के लिए विदा ले चुका था. शेष रह गयी थी मस्तिष्क में एक दूसरे को ढकेलती हुई उसकी असंख्य स्मृतियाँ, उसकी दिव्य साधना के भौतिक अवशेष.
दर्शक उनके शयन कक्ष, अध्ययन कक्ष और बैठक के सामने सिर नवा कर अपनी श्रद्धा अर्पित कर रहे थे और मेरे मानस चक्षु के सामने दद्दा बोल रहे थे, "यह देखिए सावित्री जी, इसी कमरे में दोपहरी बिताता हूँ, पीछे का दरवाजा खोल देता हूँ, खूब अच्छी हवा आती है. यह ऊपर वाला कमरा मैंने जब विनोबा जी आने वाले थे तब बनवाया था ..बहुत दिल्ली देखी है, जरा गवंई गाँव भी देखिए."
और फ़िर चिरगाँव की शोकसभा का अविस्मरणीय दृश्य, बूढ़े बच्चे, चिरगाँव की अवगुण्ठनवती स्त्रियाँ और झाँसी की जाग्रत महिलाएँ सब आँसू बरसाते, श्रद्धा के सुमन चढ़ाते हुए. वहाँ का दृश्य देख कर साहित्यिक मनीषियों और कवियों के शब्द चुक गये. सर्वेश्वर दयाल की कविता के पाठ पर बूढ़ों की पुरानी पीढ़ी करुण आर्द्रता से सिर हिलाती रही, अज्ञेय का वक्तव्य भीड़ पर छा गया. एक युग समाप्त हुआ, इतिहास का एक पृष्ठ पलट गया, हिन्दी का सबसे बड़ा स्तम्भ गिर गया. नये और पुराने, बूढ़े और जवान, कृषक और कवि, स्त्री और पुरुष, एक भाव, एक रस में निमग्न हो गये, सब करुणा प्लावित, सब असहाय.
***
मैथिलीशरण गुप्त की मूल तस्वीर कविताकोष के साभार
***

दद्दा की त्रयोदशी में सम्मिलित होने के लिए दिल्ली से एक स्पेशल बोगी का प्रबन्ध हो गया था. यात्रियों में से अधिक ऐसे थे जिन्हें दद्दा चिरगाँव आने का निमन्त्रण दे गये थे, पर अपने अतिथियों को हाथों हाथ लेने वाला अतिथेय, अपने स्वभाव और संस्कार के विरुद्ध सबको अपने घर बुला कर स्वयं अदृष्य हो गया था. रात को लगभग डेढ़ बजे गाड़ी झाँसी पहुँच गयी, और वहीं हमारा डिब्बा कट गया. झाँसी का स्टेशन फ़िर अपने साथ अनेक स्मृतियाँ ले कर सामने खड़ा हो गया. पिछली दो बार जब हम आये थे, दद्दा स्टेशन पर आतुरता से हमारा इन्तजार करते हुए मिले थे, उनके चेहरे पर उमड़ता हुआ वह आह्लाद, वह स्फटिक सा व्यवहार आज इस लेखनी में कैसे बाँधू -
"छिन्न भी है, भिन्न भी है हाय,जितनी देर हमारे सामान इत्यादि की व्यवस्था होती रही, दद्दा वहीं प्लेटफार्म पर पड़ी हुई लकड़ी की बैंच पर बैठे रहे, और आते जाते लोग उनके सामने सिर झुका झुका कर जाते रहे. जनता का यह नमन किसी खद्दरधारी राजनीतिज्ञ के प्रति नहीं था, उनकी श्रद्धामयी आँखों में और मुग्ध भावाभिव्यक्ति में भक्ति का आह्लाद ही था आतंकजन्य विनय नहीं. एक जीर्ण शीर्ण वस्त्रधारी भिखारी दद्दा के चरणों के पास आ कर साष्टांग प्रणाम करके लेट गया, उनकी दयार्द्र आँखों ने उसे कुछ दिलवा कर विदा किया, एक अर्ध विक्षिप्त सा व्यक्ति बाल बिखराये उनके निकट आ कर प्रलाप करता रहा, और दद्दा बड़ी सहिष्णुता और सुहानुभूति के साथ उसे देखते और उसकी बात सुनते रहे. मैंने कई बार बड़े बड़े मठाधिकारियों और धर्म के संरक्षकों का व्यवहार इस वर्ग के प्रति देख रखा था. पीड़ित दुखी जनता के प्रति उनकी दुरदुराहट की तीव्र प्रतिक्रिया के फ़लस्वरूप ही मेरा मन मिशनों, धर्म संस्थाओं और आध्यात्मिक व्यक्तित्वों से विमुख हो गया है, पर उस दिन स्वच्छता और छूत पाक के वैष्णव विधान पर पूर्ण विश्वास करने वाले दद्दा का वैष्णव नहीं केवल मानव रूप देखा. आज झाँसी के उसी महामानव और हिन्दी संसार के दद्दा के स्नेहपूर्ण स्वागत के बिना स्टेशन भाँय भाँय कर रहा था.
क्यों न रोवे लेखनी निरुपाय?"
हिन्दी के प्रसिद्ध उपन्यासकार श्रद्धेय वृन्दावनलाल वर्मा के प्रेस में हमारे भोजन की व्यवस्था थी. निःशब्द भोजन चल रहा था जैसे यह कोई यांत्रिक काम था जिसे किसी तरह पूरा करना था. ग्रास थाली से हाथ में आ कर मुँह में जा रहे थे और पिछली बार झाँसी की हवेली में भोजन करते हुए दद्दा के स्नेहपूर्ण आग्रह कान में गूँज रहे थे. श्रुतिपुट से आयी दद्दा की स्मृतियाँ पलकों में न समा सकने के कारण आँसू बन कर बिखर रही थीं.
भोजनोपरान्त, हम बस में बैठ कर चिरगाँव चले. चारों ओर की हरियाली भरी पहाड़ियों का हमारे लिए कोई अर्थ नहीं था, अतीत के मौन ताने बाने में बस की घरघराहट और आसपास का शोर गुल जैसे लुप्त हो गया था और फ़िर उसके बाद हम बेतवा के बाँध पर आये. यह स्थान दद्दा को बहुत प्रिय था, मेरे मानस चक्षु के सामने दद्दा बोल रहे थे, "पंडित जी (पं. जवाहरलाल नेहरू) को यह स्थान बहुत अच्छा लगा था, वे इसे देख कर भाव विभोर काफ़ी देर तक खड़े रहे, हमारे मना करते करते भागते दौड़ते वहाँ .. वहाँ.. दूर तक पहुँच गये थे." उस दिन दद्दा बेतवा के किनारे खड़े हो कर दिवंगत राष्ट्रनायक को भरे गले से याद कर रहे थे और आज राष्ट्रकवि के अभाव में बेतवा की पछाड़ खाती लहरों के निकट ठहरने का हमें साहस नहीं हुआ. उदास और क्लांत हृदय यात्री बस से उतर पैदल मौन गुप्त बंधुओं की प्रसिद्ध बखरी की ओर चले, "चिरगाँव की शोभा" को झुक झुक प्रणाम करने वाली, हाट की जनता हमारी ओर उदास नेत्रों और म्लान मुख से देख रही थी, जैसे उन्हें यह पूछने की आवश्यकता ही नहीं थी कि हम वहाँ किस उद्देश्य से गये हैं. बखरी के फाटक पर गम्भीर विषाद से युक्त गिरधारी ने मौन विनयाचार में हाथ जोड़े, उसके होंठ सिहरे और आँखें आँसुओं से भर आयीं. गुप्त बंधुओं की पुश्तैनी बखरी मौन साधे सविषाद पाषाण बनी खड़ी थी, हमारे पहुँचते ही प्रस्तर मूर्तियों की तरह निश्चल खड़े दद्दा के स्वजन यन्त्रवत चल कर निकट आये और फ़िर बखरी में कुहराम मच गया, दद्दा के पुत्र उर्मिल जी डा. नगेन्द्र के अंक में मुँह छिपा कर क्रन्दन कर उठे और फ़िर सारी बखरी में रुदन और विलाप का स्वर छा गया.
हिम्मत नहीं होती थी अंदर जाने की. "गौरवमंण्डित सुहागनी" के करुण वैधव्य का सामना करने का साहस मुझे नहीं हो रहा था, मैं बड़ी हिम्मत करके अन्दर गयी और जिया के वलयशून्य हाथों ने मुझे लपेट लिया, उनकी आँखों से निरन्तर आँसू बहते रहे, साकेत की "मूर्तिमति ममता माया" आज अपना मुँह अवगुण्ठन में लपेटे वटवृक्ष की छाया से छिन्न लता सी क्लांत, शिथिल हो रही थी. शान्ति, दद्दा की पुत्रवधू अपनी गोद में नन्ही सी बिटिया को लिए बिलख रही थी.
श्राद्ध पूरा हुआ. होम का धूँआ सारी बखरी पर छा गया, जिया ने लाल जोड़ा उतार कर श्वेत वस्त्र धारण किया और गु्प्त कुल की बखरी की दीवारें जैसे सिर धुन धुन कर रोने लगीं. उसके इतिहास का उज्जवलतम अध्याय अब नये चरण में प्रवेश कर रहा था, वह माई का लाल जिसने पितृव्यों को भौतिक ऋण से मुक्त किया था, अपने कुल के उपास्यदेव राम की नयी प्रतिष्ठा द्वारा उनका आध्यात्मिक ऋण चुकाया. जिसकी वाणी से सारा राष्ट्र प्रेरणा स्फूर्त हो उठा आज इस बखरी से सदा के लिए विदा ले चुका था. शेष रह गयी थी मस्तिष्क में एक दूसरे को ढकेलती हुई उसकी असंख्य स्मृतियाँ, उसकी दिव्य साधना के भौतिक अवशेष.
दर्शक उनके शयन कक्ष, अध्ययन कक्ष और बैठक के सामने सिर नवा कर अपनी श्रद्धा अर्पित कर रहे थे और मेरे मानस चक्षु के सामने दद्दा बोल रहे थे, "यह देखिए सावित्री जी, इसी कमरे में दोपहरी बिताता हूँ, पीछे का दरवाजा खोल देता हूँ, खूब अच्छी हवा आती है. यह ऊपर वाला कमरा मैंने जब विनोबा जी आने वाले थे तब बनवाया था ..बहुत दिल्ली देखी है, जरा गवंई गाँव भी देखिए."
और फ़िर चिरगाँव की शोकसभा का अविस्मरणीय दृश्य, बूढ़े बच्चे, चिरगाँव की अवगुण्ठनवती स्त्रियाँ और झाँसी की जाग्रत महिलाएँ सब आँसू बरसाते, श्रद्धा के सुमन चढ़ाते हुए. वहाँ का दृश्य देख कर साहित्यिक मनीषियों और कवियों के शब्द चुक गये. सर्वेश्वर दयाल की कविता के पाठ पर बूढ़ों की पुरानी पीढ़ी करुण आर्द्रता से सिर हिलाती रही, अज्ञेय का वक्तव्य भीड़ पर छा गया. एक युग समाप्त हुआ, इतिहास का एक पृष्ठ पलट गया, हिन्दी का सबसे बड़ा स्तम्भ गिर गया. नये और पुराने, बूढ़े और जवान, कृषक और कवि, स्त्री और पुरुष, एक भाव, एक रस में निमग्न हो गये, सब करुणा प्लावित, सब असहाय.
***
मैथिलीशरण गुप्त की मूल तस्वीर कविताकोष के साभार
रविवार, अगस्त 15, 2010
पूज्य दद्दा अंतिम बार
भारत के राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त की, उनके अवसान से कुछ दिन पहले की, अंतिम दिल्ली यात्रा का संस्मरण स्व. डा. सावित्री सिन्हा की कलम से
जिसकी मुक्त आत्मीयता हर व्यक्ति के लिए एक खुली पुस्तक हो, उस व्यक्ति के अन्तरंग क्षणों का वैशिष्ट्य व्याख्या विश्लेषण की अपेक्षा नहीं रखता. परन्तु इस बार दद्दा के दिल्ली प्रवास की संक्षिप्त अविधि में कई बार ऐसा भास हुआ जैसे उनकी स्निग्ध आत्मीयता और कातर आर्द्रता जाने अनजाने ही बहुत बार हृदय के किसी बड़े ही अन्तरंग अंश को छू जाती है, सामान्य सहज से अधिक वह विशिष्ट आर्द्र हो उठती है.
 दिल्ली में दद्दा का निवास स्थान, 35 मीना बाग, इधर बहुत दिनों से वह संगम स्थल बन गया था, जहाँ दिल्ली की भागदौड़ में महीनों और बरसों एक दूसरे से न मिलने वाले व्यक्ति बरबस ही मिल जाते थे. साहित्य अकादमी, विश्व विद्यालय, आकाशवाणी, सरकारी दफ्तर और प्राईमरी स्कूल तक के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े प्रतिनिधि वहाँ एक धरातल , एक स्तर पर मिलते थे. इस बार दद्दा के आने के साथ ही दिल्ली के इन सभी वर्गों के व्यक्ति इस संगम की ओर दूने उत्साह और वेग से आने जाने लगे थे, क्योंकि इस बार दद्दा संसद सदस्य के नहीं दिल्ली के अतिथि के रूप में आये थे. ऐसे अतिथि के रूप में, जिससे मिलने को उत्सुक श्रद्धालुओं के स्वागत में एलेक्ट्रिक मिक्सर में बनी हुई काफ़ी, बीकानेरी भुजिया और मिठाई का सतत दौर चलता रहता था. जिया के हाथों की बनी हुई मट्ठी और लड्डू के स्थान पर राजस्थानी अतिथेय श्री रामेश्वर टाँटिया द्वारा निर्धारित मीनू के इस परिवर्तन पर ध्यान सबका गया परन्तु डा. नगेंद्र का पाँच वर्षीय दौहित्र वर्तमान में अतीत को नहीं भुला सका. उसे तो दद्दा के घर में हर रोज लड्डू ले कर तोड़ फोड़ कर खाने खी आदत पड़ी हुई थी. उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरु कर दिया, "लड्डू चाहिए, लड्डू चाहिए". दद्दा सामान्यतः इस प्रकार की ज़िद्द के प्रति थोड़े सहिष्णु हो उठते थे, पर उस दिन उसे बड़ी देर तक बहलाते फुसलाते रहे. उनके स्वर की आर्द्रता और नेत्रों के वात्सल्य से ऐसा लग रहा था जैसे बच्चों को बहलाने के लिए दद्दा स्वयं बच्चा बन गये हों. मैं मौन, मुग्ध नेत्रों से वयोवृद्ध राष्ट्रकवि का बाल रूप देखती रही.
दिल्ली में दद्दा का निवास स्थान, 35 मीना बाग, इधर बहुत दिनों से वह संगम स्थल बन गया था, जहाँ दिल्ली की भागदौड़ में महीनों और बरसों एक दूसरे से न मिलने वाले व्यक्ति बरबस ही मिल जाते थे. साहित्य अकादमी, विश्व विद्यालय, आकाशवाणी, सरकारी दफ्तर और प्राईमरी स्कूल तक के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े प्रतिनिधि वहाँ एक धरातल , एक स्तर पर मिलते थे. इस बार दद्दा के आने के साथ ही दिल्ली के इन सभी वर्गों के व्यक्ति इस संगम की ओर दूने उत्साह और वेग से आने जाने लगे थे, क्योंकि इस बार दद्दा संसद सदस्य के नहीं दिल्ली के अतिथि के रूप में आये थे. ऐसे अतिथि के रूप में, जिससे मिलने को उत्सुक श्रद्धालुओं के स्वागत में एलेक्ट्रिक मिक्सर में बनी हुई काफ़ी, बीकानेरी भुजिया और मिठाई का सतत दौर चलता रहता था. जिया के हाथों की बनी हुई मट्ठी और लड्डू के स्थान पर राजस्थानी अतिथेय श्री रामेश्वर टाँटिया द्वारा निर्धारित मीनू के इस परिवर्तन पर ध्यान सबका गया परन्तु डा. नगेंद्र का पाँच वर्षीय दौहित्र वर्तमान में अतीत को नहीं भुला सका. उसे तो दद्दा के घर में हर रोज लड्डू ले कर तोड़ फोड़ कर खाने खी आदत पड़ी हुई थी. उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरु कर दिया, "लड्डू चाहिए, लड्डू चाहिए". दद्दा सामान्यतः इस प्रकार की ज़िद्द के प्रति थोड़े सहिष्णु हो उठते थे, पर उस दिन उसे बड़ी देर तक बहलाते फुसलाते रहे. उनके स्वर की आर्द्रता और नेत्रों के वात्सल्य से ऐसा लग रहा था जैसे बच्चों को बहलाने के लिए दद्दा स्वयं बच्चा बन गये हों. मैं मौन, मुग्ध नेत्रों से वयोवृद्ध राष्ट्रकवि का बाल रूप देखती रही.
एक दिन जब हम उनके यहाँ पहुँचे दद्दा वात्स्यायन जी के यहाँ जाने को व्यग्र थे. बाबू गंगाशरण सिंह जी के साथ उन्हें जाना था जो किसी मीटिंग में व्यस्त हो जाने के कारण समय पर नहीं आ पाये थे. गंगा बाबू के आते ही उनके मुख पर ऐसी सहज प्रसन्नता दौड़ गयी जैसे किसी बालक को मिठाई मिल गयी हो. हर्षातुर हो कर उन्होंने मुझसे फ़ोन द्वारा कपिला से उनके घर का पता और उसका रास्ता पुछवाया. चलने से पहले मैंने खूब अच्छी तरह से उन्हें रास्ता समझा दिया, पर सत्य मार्ग के आसपास 45 मिनट तक चक्कर लगा कर वे लौट आये. उनके मुँह पर ऐसी कातरता थी जैसे मिठाई हाथ से छिनने पर कोई बालक रुँआसा हो गया हो. मुझे उलाहना सा देते हुए बोले, "मैं कह रहा था सावित्री जी आप चलिए हमारे साथ, आप नहीं गयी इसीलिए हमें रास्ता नहीं मिला." उस शाम को काफ़ी देर तक वे अपनी सहज प्रफुल्ल मनःस्थिति में नहीं आ सके.
दद्दा जैसे इस बार दिल्ली में हर परिचित व्यक्ति से मिल कर जाने का निश्चय करके आये थे. "अमुक का कोई कार्य अड़ा हुआ है, वो आ जाता तो शायद मैं कुछ कर सकता", न जाने कितने फ़ोन कराये. अमुक बड़ा दुखी है उससे मिलना चाहता हूँ, अमुक का पत्र मेरे पास चिरगाँव गया था, वह मिल जाता तो अच्छा था, अमुक को मेरे आने का पता नहीं है, अमुक दिल्ली से बाहर है उससे नहीं मिल सका, इत्यादि, इत्यादि. अतिशय भावनामयता की इन घड़ियों के अतिरिक्त दद्दा खूभ प्रसन्न और स्वस्थ रहे. वही खुली हुई हँसी, विनोद हास्य, छेड़ छाड़, चुभते हुए संस्मरण, हँसाने वाले चुटकले, जो छोटो को विश्वास और साहस देते थे, और उनके मित्रों को मनोरंजन की सामग्री. उस दिन डा. नगेन्द्र के रस सिद्धांत ग्रन्थ के विमोचन समारोह के बाद दद्दा बहुत प्रसन्न थे. सेठ गोविन्ददास और श्री नरेंद्र शर्मा समारोह से लौटते समय उन्हीं के साथ कार में आये. रास्ते भर दद्दा अपने सरल आर्द्र शब्दों में सेठ जी को सान्तवना देने का प्रयास करते रहे. कई सन्तानों को अपने हाथ से पृथ्वी में सुला देने वाले पिता के हृदय का मौन क्रन्दन जैसे स्वतः ही उनके कण्ठ में हिल हिल उठता था, उधर जवान पुत्र की मौट से विषण्ण पिता के मुख पर करुणा साकार हो रही थी. अन्ततः दद्दा बोले, "तुम मेरी कविता 'सान्त्वना' पढ़ो उससे तुम्हारा मन अवश्य स्थिर होगा, सावित्री जी, उच्छवास (जिसमें सान्त्वना कविता छपी है) की अपनी कापी इनके पास भिजवा दें, मैं आप को और भेज दूँगा." "तुम" सम्बोधन उस व्यस्क मित्र के लिए था जिसके करुणा विगलित हृदय की द्रवित व्यथा को दद्दा बाँट लेना चाहते थे और "आप" सम्बोधन उस व्यक्ति के प्रति जिसे उन्होंने पिता का सा वात्सल्य और स्नेह दे कर कृतकृत्य कर दिया था. शायद दद्दा की सामन्तीय कुलीनता, वैष्णव शील और मर्यादा के संस्कार का आग्रह नारी के प्रति "आप" सम्बोधन का स्थान "तुम" को नहीं लेने देता था. सेठ जी को उनके निवास स्थान पर छोड़ कर हम मीना बाग़ आये. घर आते आते दद्दा स्वस्थ और प्रकृतिस्थ हो चुके थे जैसे जानबूझ कर वे हमारे मन पर छा गये अवसाद को दूर करने का प्रयास करते रहे.
विविध प्रसंगों पर चर्चा होते होते बात कविता में प्रयुक्त लय और छन्द विधान पर पहुँची. मैंने नरेन्द्र जी से एक प्रश्न पूछ लिया, "गीतों की रचना करते समय आप का ध्यान लय की गेयता पर रहता है या मात्राओं की संख्या पर?" इसी प्रसंग को स्पष्ट करने के लिए दद्दा ने दर्जनों संस्कृत के श्लोक सुनाये, हिन्दी में उनका अनुवाद किया, उनमें निहित सौष्ठव और लय तथा छन्द के अन्योन्याश्रित सम्बन्धों को स्पष्ट किया. घण्टे डेढ़ घण्टे हम उनकी बातों में विभोर, तन्मय मुग्ध रहे. इस आयु में यह स्मरण शक्ति! लड़ी में पिरोई हुई मुक्ताओं के समान श्लोक उनके मुख से निकलते रहे और कक्षा के लिए आवश्यक उद्धरणों को भी याद कर सकने में असमर्थ मैं उनकी स्मरण शक्ति पर अवाक् आश्चर्यान्वित होती रही.
जिस दिन दद्दा को जाना था उसके एक दिन पहले कुछ परिस्थितियोंवश मैं मीना बाग नहीं पहुँच पायी. दूसरे दिन जब हम पहुँचे दद्दा का सामान बँध चुका था. उनकी गाड़ी यद्यपि साढ़े नौ के लगभग छूटती थी, परन्तु शीत का आधिक्य और कुछ दूसरे कारणों से उन्होंने जल्दी स्टेशन पहुँचने का निर्णय कर लिया था. मुझे देखते ही बोले, "कल मैं आप के लिए बड़ा दुखी रहा. कई बार फ़ोन किया पर वह भी न मिला." मैं भावविमूढ़, ठगी सी उनका मुँह देखती रह गयी. आज दद्दा होते तो यह वाक्य अपने मित्रों के बीच दुहरा कर मैं कितनी बार गौरावान्वित होती, पर अब तो वह हृदय में एक फाँस बन कर समाया हुआ है जिसकी चुभन जिन्दगी भर न मिट सकेगी.
नयी दिल्ली स्टेशन पर हम उन्हें पहुँचाने गये. पटना विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग के अध्यक्ष डा. देवेन्द्र शर्मा, डा. दशरथ ओझा, डा. नगेन्द्र और कई व्यक्ति साथ थे. स्टेशन पहुँचते ही मुझे अलग बुला कर धीरे कहा, "मेरे पास रुपये काफी हैं, इसलिए सामान पर ध्यान रखियेगा." डा. साहब के पास जा कर उनके कान में भी यही बात कही. पर उसकी हमें अधिक चिन्ता नहीं थी, क्योंकि गिरधारी जैसा स्वामीभक्त और सतर्क परिचारक और सजग प्रहरी उनके साथ था. वेटंग रूम में काफी देर तक मैं उनके साथ अकेली रही. अभिनव कुर्सियाँ खीचता, शोर मचाता, और मुँह से सीटी बजा कर रेलगाड़ी चलाता रहा, दद्दा उसको देखते रहे और बोले, "बड़ा ही चंचल है यह." फ़िर न जाने कैसे उन्हें मेरे पुत्र अन्नु की याद आ गयी. बड़ी कोमलता से कहा उन्होंने, "अन्नु तो अब बड़ा हो गया है, अब वह हम लोगों की परवाह नहीं करता. वह भी छोटेपन में बड़े हज़रत थे. इस बार उसको नहीं देख सका." दद्दा के मन में पौत्र देखने की साध छिपी हुई थी. बातों ही बातों में कहने लगे, "मेरे सामने उर्मिल जी का एक भी लड़का हो जाता तो अच्छा था, पर मेरे यहाँ तो एक और देवी अवतरित हुई है." मैंने कहा "दद्दा! चार पौत्रियाँ पा कर तो आप अब पूरी तरह से विदेह हो गये हैं." दद्दा के ठहाके से सारा वेटिंग रूम गूँज उठा. आज सोचती हूँ न जाने किस मनहूस घड़ी में मेरे मुँह से यह शब्द निकला था. मेरे होठों में मन्थरा बैठ गयी थी क्या! विभिन्न शब्द शक्तियों की अर्थवत्ता के वैपरीत्य की इतनी कठोर, यथार्थ और तीक्ष्ण अनुभूति शायद ही कभी किसी को हुई होगी. श्लेष का इतना क्रूर मजाक शायद ही किसी ने झेला होगा.
थोड़ी देर में फ़िर बोले, "सावित्री जी! अब की दिसम्बर की छुट्टियों में आप चिरगाँव आइये, चार पाँच दिन रहिये निश्चिंत हो कर, कार मे सारा बुन्देलखण्ड घूमेंगे." कुछ देर रुक कर बोले, "आप को विश्वास नहीं आयेगा, मुझे आप की चिरगाँव में बहुत बार याद आती है, कुछ संस्कार होंगे हमारे आप के", और उनकी आँखों से आँसू टप टप गिरने लगे, मैं कृतकृत्य, अभिभूत भावावेश को गले और आँखों में सम्हाले मौन सिर झुकाये रही, आँख उठा कर उनकी ओर देखने का साहस भी नहीं हुआ. वात्सल्य का अपार समुद्र मेरी झोली में भरकर दद्दा संयत हो गये, मैं उसी में अवगाहन करती डूबती उतरती रही. गाड़ी चलने का समय हुआ, डा. नगेन्द्र को उन्होंने मोहाकुल आलिंगन में बाँध लिया, अभिनव को प्यार किया, सबसे विदा ली और मेरे भर्राये हुए चेहरे को देख सिर पर हाथ रख कर मौन आशीर्वाद दिया, बोले, "अब आप लोग जाइये, बहुत देर हो गयी है, सर्दी भी बहुत हो रही है. हमारे चलने का भी समय हो गया है." एक स्निग्ध दृष्टि उन्होंने हम सब पर डाली और कम्पार्टमेण्ट का दरवाजा खींच दिया. हमें क्या मालूम था कि वह हमारे लिए उस महानायक के जीवन नाटक का अन्तिम पटाक्षेप था.
***
टिप्पणीः यह आलेख डा. सावित्री सिन्हा के आलेख संग्रह "तुला और तारे", (नेशनल पब्लिशिंग हाउस दिल्ली, 1966) से है. दद्दा (राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त) का देहांत 12 दिसंबर 1964 में हुआ.
मैथिलीशरण गुप्त की मूल तस्वीर कविताकोष के साभार
जिसकी मुक्त आत्मीयता हर व्यक्ति के लिए एक खुली पुस्तक हो, उस व्यक्ति के अन्तरंग क्षणों का वैशिष्ट्य व्याख्या विश्लेषण की अपेक्षा नहीं रखता. परन्तु इस बार दद्दा के दिल्ली प्रवास की संक्षिप्त अविधि में कई बार ऐसा भास हुआ जैसे उनकी स्निग्ध आत्मीयता और कातर आर्द्रता जाने अनजाने ही बहुत बार हृदय के किसी बड़े ही अन्तरंग अंश को छू जाती है, सामान्य सहज से अधिक वह विशिष्ट आर्द्र हो उठती है.

एक दिन जब हम उनके यहाँ पहुँचे दद्दा वात्स्यायन जी के यहाँ जाने को व्यग्र थे. बाबू गंगाशरण सिंह जी के साथ उन्हें जाना था जो किसी मीटिंग में व्यस्त हो जाने के कारण समय पर नहीं आ पाये थे. गंगा बाबू के आते ही उनके मुख पर ऐसी सहज प्रसन्नता दौड़ गयी जैसे किसी बालक को मिठाई मिल गयी हो. हर्षातुर हो कर उन्होंने मुझसे फ़ोन द्वारा कपिला से उनके घर का पता और उसका रास्ता पुछवाया. चलने से पहले मैंने खूब अच्छी तरह से उन्हें रास्ता समझा दिया, पर सत्य मार्ग के आसपास 45 मिनट तक चक्कर लगा कर वे लौट आये. उनके मुँह पर ऐसी कातरता थी जैसे मिठाई हाथ से छिनने पर कोई बालक रुँआसा हो गया हो. मुझे उलाहना सा देते हुए बोले, "मैं कह रहा था सावित्री जी आप चलिए हमारे साथ, आप नहीं गयी इसीलिए हमें रास्ता नहीं मिला." उस शाम को काफ़ी देर तक वे अपनी सहज प्रफुल्ल मनःस्थिति में नहीं आ सके.
दद्दा जैसे इस बार दिल्ली में हर परिचित व्यक्ति से मिल कर जाने का निश्चय करके आये थे. "अमुक का कोई कार्य अड़ा हुआ है, वो आ जाता तो शायद मैं कुछ कर सकता", न जाने कितने फ़ोन कराये. अमुक बड़ा दुखी है उससे मिलना चाहता हूँ, अमुक का पत्र मेरे पास चिरगाँव गया था, वह मिल जाता तो अच्छा था, अमुक को मेरे आने का पता नहीं है, अमुक दिल्ली से बाहर है उससे नहीं मिल सका, इत्यादि, इत्यादि. अतिशय भावनामयता की इन घड़ियों के अतिरिक्त दद्दा खूभ प्रसन्न और स्वस्थ रहे. वही खुली हुई हँसी, विनोद हास्य, छेड़ छाड़, चुभते हुए संस्मरण, हँसाने वाले चुटकले, जो छोटो को विश्वास और साहस देते थे, और उनके मित्रों को मनोरंजन की सामग्री. उस दिन डा. नगेन्द्र के रस सिद्धांत ग्रन्थ के विमोचन समारोह के बाद दद्दा बहुत प्रसन्न थे. सेठ गोविन्ददास और श्री नरेंद्र शर्मा समारोह से लौटते समय उन्हीं के साथ कार में आये. रास्ते भर दद्दा अपने सरल आर्द्र शब्दों में सेठ जी को सान्तवना देने का प्रयास करते रहे. कई सन्तानों को अपने हाथ से पृथ्वी में सुला देने वाले पिता के हृदय का मौन क्रन्दन जैसे स्वतः ही उनके कण्ठ में हिल हिल उठता था, उधर जवान पुत्र की मौट से विषण्ण पिता के मुख पर करुणा साकार हो रही थी. अन्ततः दद्दा बोले, "तुम मेरी कविता 'सान्त्वना' पढ़ो उससे तुम्हारा मन अवश्य स्थिर होगा, सावित्री जी, उच्छवास (जिसमें सान्त्वना कविता छपी है) की अपनी कापी इनके पास भिजवा दें, मैं आप को और भेज दूँगा." "तुम" सम्बोधन उस व्यस्क मित्र के लिए था जिसके करुणा विगलित हृदय की द्रवित व्यथा को दद्दा बाँट लेना चाहते थे और "आप" सम्बोधन उस व्यक्ति के प्रति जिसे उन्होंने पिता का सा वात्सल्य और स्नेह दे कर कृतकृत्य कर दिया था. शायद दद्दा की सामन्तीय कुलीनता, वैष्णव शील और मर्यादा के संस्कार का आग्रह नारी के प्रति "आप" सम्बोधन का स्थान "तुम" को नहीं लेने देता था. सेठ जी को उनके निवास स्थान पर छोड़ कर हम मीना बाग़ आये. घर आते आते दद्दा स्वस्थ और प्रकृतिस्थ हो चुके थे जैसे जानबूझ कर वे हमारे मन पर छा गये अवसाद को दूर करने का प्रयास करते रहे.
विविध प्रसंगों पर चर्चा होते होते बात कविता में प्रयुक्त लय और छन्द विधान पर पहुँची. मैंने नरेन्द्र जी से एक प्रश्न पूछ लिया, "गीतों की रचना करते समय आप का ध्यान लय की गेयता पर रहता है या मात्राओं की संख्या पर?" इसी प्रसंग को स्पष्ट करने के लिए दद्दा ने दर्जनों संस्कृत के श्लोक सुनाये, हिन्दी में उनका अनुवाद किया, उनमें निहित सौष्ठव और लय तथा छन्द के अन्योन्याश्रित सम्बन्धों को स्पष्ट किया. घण्टे डेढ़ घण्टे हम उनकी बातों में विभोर, तन्मय मुग्ध रहे. इस आयु में यह स्मरण शक्ति! लड़ी में पिरोई हुई मुक्ताओं के समान श्लोक उनके मुख से निकलते रहे और कक्षा के लिए आवश्यक उद्धरणों को भी याद कर सकने में असमर्थ मैं उनकी स्मरण शक्ति पर अवाक् आश्चर्यान्वित होती रही.
जिस दिन दद्दा को जाना था उसके एक दिन पहले कुछ परिस्थितियोंवश मैं मीना बाग नहीं पहुँच पायी. दूसरे दिन जब हम पहुँचे दद्दा का सामान बँध चुका था. उनकी गाड़ी यद्यपि साढ़े नौ के लगभग छूटती थी, परन्तु शीत का आधिक्य और कुछ दूसरे कारणों से उन्होंने जल्दी स्टेशन पहुँचने का निर्णय कर लिया था. मुझे देखते ही बोले, "कल मैं आप के लिए बड़ा दुखी रहा. कई बार फ़ोन किया पर वह भी न मिला." मैं भावविमूढ़, ठगी सी उनका मुँह देखती रह गयी. आज दद्दा होते तो यह वाक्य अपने मित्रों के बीच दुहरा कर मैं कितनी बार गौरावान्वित होती, पर अब तो वह हृदय में एक फाँस बन कर समाया हुआ है जिसकी चुभन जिन्दगी भर न मिट सकेगी.
नयी दिल्ली स्टेशन पर हम उन्हें पहुँचाने गये. पटना विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग के अध्यक्ष डा. देवेन्द्र शर्मा, डा. दशरथ ओझा, डा. नगेन्द्र और कई व्यक्ति साथ थे. स्टेशन पहुँचते ही मुझे अलग बुला कर धीरे कहा, "मेरे पास रुपये काफी हैं, इसलिए सामान पर ध्यान रखियेगा." डा. साहब के पास जा कर उनके कान में भी यही बात कही. पर उसकी हमें अधिक चिन्ता नहीं थी, क्योंकि गिरधारी जैसा स्वामीभक्त और सतर्क परिचारक और सजग प्रहरी उनके साथ था. वेटंग रूम में काफी देर तक मैं उनके साथ अकेली रही. अभिनव कुर्सियाँ खीचता, शोर मचाता, और मुँह से सीटी बजा कर रेलगाड़ी चलाता रहा, दद्दा उसको देखते रहे और बोले, "बड़ा ही चंचल है यह." फ़िर न जाने कैसे उन्हें मेरे पुत्र अन्नु की याद आ गयी. बड़ी कोमलता से कहा उन्होंने, "अन्नु तो अब बड़ा हो गया है, अब वह हम लोगों की परवाह नहीं करता. वह भी छोटेपन में बड़े हज़रत थे. इस बार उसको नहीं देख सका." दद्दा के मन में पौत्र देखने की साध छिपी हुई थी. बातों ही बातों में कहने लगे, "मेरे सामने उर्मिल जी का एक भी लड़का हो जाता तो अच्छा था, पर मेरे यहाँ तो एक और देवी अवतरित हुई है." मैंने कहा "दद्दा! चार पौत्रियाँ पा कर तो आप अब पूरी तरह से विदेह हो गये हैं." दद्दा के ठहाके से सारा वेटिंग रूम गूँज उठा. आज सोचती हूँ न जाने किस मनहूस घड़ी में मेरे मुँह से यह शब्द निकला था. मेरे होठों में मन्थरा बैठ गयी थी क्या! विभिन्न शब्द शक्तियों की अर्थवत्ता के वैपरीत्य की इतनी कठोर, यथार्थ और तीक्ष्ण अनुभूति शायद ही कभी किसी को हुई होगी. श्लेष का इतना क्रूर मजाक शायद ही किसी ने झेला होगा.
थोड़ी देर में फ़िर बोले, "सावित्री जी! अब की दिसम्बर की छुट्टियों में आप चिरगाँव आइये, चार पाँच दिन रहिये निश्चिंत हो कर, कार मे सारा बुन्देलखण्ड घूमेंगे." कुछ देर रुक कर बोले, "आप को विश्वास नहीं आयेगा, मुझे आप की चिरगाँव में बहुत बार याद आती है, कुछ संस्कार होंगे हमारे आप के", और उनकी आँखों से आँसू टप टप गिरने लगे, मैं कृतकृत्य, अभिभूत भावावेश को गले और आँखों में सम्हाले मौन सिर झुकाये रही, आँख उठा कर उनकी ओर देखने का साहस भी नहीं हुआ. वात्सल्य का अपार समुद्र मेरी झोली में भरकर दद्दा संयत हो गये, मैं उसी में अवगाहन करती डूबती उतरती रही. गाड़ी चलने का समय हुआ, डा. नगेन्द्र को उन्होंने मोहाकुल आलिंगन में बाँध लिया, अभिनव को प्यार किया, सबसे विदा ली और मेरे भर्राये हुए चेहरे को देख सिर पर हाथ रख कर मौन आशीर्वाद दिया, बोले, "अब आप लोग जाइये, बहुत देर हो गयी है, सर्दी भी बहुत हो रही है. हमारे चलने का भी समय हो गया है." एक स्निग्ध दृष्टि उन्होंने हम सब पर डाली और कम्पार्टमेण्ट का दरवाजा खींच दिया. हमें क्या मालूम था कि वह हमारे लिए उस महानायक के जीवन नाटक का अन्तिम पटाक्षेप था.
***
टिप्पणीः यह आलेख डा. सावित्री सिन्हा के आलेख संग्रह "तुला और तारे", (नेशनल पब्लिशिंग हाउस दिल्ली, 1966) से है. दद्दा (राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त) का देहांत 12 दिसंबर 1964 में हुआ.
मैथिलीशरण गुप्त की मूल तस्वीर कविताकोष के साभार
शनिवार, अगस्त 14, 2010
जिया, राष्ट्रकवि की प्रेरणा
टिप्पणीः यह आलेख मेरी बड़ी बुआ स्व. डा. सावित्री सिन्हा की पुस्तक तुला और तारे से है जो 1966 में नेश्नल प्रिन्टिंग प्रेस द्वारा छपी थी, जब वह दिल्ली विश्वविद्यलय के हिन्दी विभाग की रीडर थीं. मेरे विचार में यह आलेख 1963 तथा 1964 के बीच में लिखा गया, क्योंकि इसको लिखते समय मैथिलीशरण गुप्त के अनुज सियाराम शरण गुप्त की मृत्यु हो चुकी थी जो 1963 में हुई.
राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त के बारे में कुछ जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध है, जिनमें उनके माता पिता के नाम तो हैं तो लेकिन उनकी पत्नी, यानि इस आलेख की नायिका "जिया" का नाम नहीं मिला मुझे. गुप्त जी के काव्य में उपेक्षित उर्मिला की बात तो होती है, लेकिन उनकी अपनी उर्मिला को भूलने वाली भी क्या वही बात नहीं?
जिया
लगभग दस वर्ष पूर्व छः, नार्थ एवेन्यू की बैठक में घुसते ही स्क्रीन की आड़ में खड़ी एक नारी मूर्ती की ओर अनायास ही मेरी आँखें उठ गयीं, और मैं अपने आप ही समझ गयी कि यह "जिया" हैं. ग्रामवधु की सहज मुस्कान, स्निग्ध आर्द्र वात्सल्यमयी आँखें, गौरवान्वित भावाभिव्यक्ति, पर अभिमान और दम्भ का स्पर्श नहीं - साकेत की "मूर्तिमती ममता माया" ही जैसे मेरे सामने खड़ी थी. मुझे देखते ही मुस्कान का स्थान, मृदुल हास्य ने ले लिया और फ़िर हँसते हुए हाथ जोड़ कर उन्होंने मुझे नमस्ते किया - सब कुछ एक क्षण में हो गया और मैं स्तम्भित खड़ी रह गयी. क्या कहूँ, क्या करूँ ? संकोशवश बिना कुछ बोले केवल नमस्कार कर सकी. उनके प्रथम दर्शन की वह झलक मेरे मानस पर जैसे स्थायी हो गयी है. शुद्ध खद्दर की केसरिया साड़ी उनके त्यागपूर्ण गौरव भरे सुहाग की कहानी कह रही थी. गले में पड़ी हुई सोने की जंजीर के साथ तुलसी की कण्ठी में, मानो उच्चकुल वधू का गरिमापूर्ण पत्नित्व और यशोधरा की वैष्णव भावना एक दूसरे को बल देते हुए साकार थी. माथे पर लगी चमकती हुई बिंदिया पर सुनहले अक्षरों
 में अंकित "सीताराम" शब्द बार बार चमक कर यह घोषित करना चाहता था कि "पति का इष्ट ही उनका इष्ट है, उनके गौरव से ही उनका सुहाग मण्डित है." पैरों में पड़ी हुई हल्की सी चाँदी की पायल, पैर की उँगली में सुहाग चिन्ह बिछुये, हाथों की लाल काँच की चूड़ियाँ और लाल सिन्दूर से भरी माँग को देख कर साकेत की "सुहागनियों" और यशोधरा के व्यक्तित्व के सभी अंश आँखों में उमड़ आये जिन्हें दद्दा ने बार बार दोहराया है और महत्ता दी है. मुझे ऐसा लगा जैसे मैं दद्दा द्वारा निर्मित त्यागमयी नारियों को उनकी प्रौढ़ावस्था में देख रही हूँ, जिनके त्याग, समर्पण, सेवा और आत्मदान की परिणति कुण्ठा, हीनभाव और स्नायविक विकृतियों में नहीं, आनन्द और सुख में होती है.
में अंकित "सीताराम" शब्द बार बार चमक कर यह घोषित करना चाहता था कि "पति का इष्ट ही उनका इष्ट है, उनके गौरव से ही उनका सुहाग मण्डित है." पैरों में पड़ी हुई हल्की सी चाँदी की पायल, पैर की उँगली में सुहाग चिन्ह बिछुये, हाथों की लाल काँच की चूड़ियाँ और लाल सिन्दूर से भरी माँग को देख कर साकेत की "सुहागनियों" और यशोधरा के व्यक्तित्व के सभी अंश आँखों में उमड़ आये जिन्हें दद्दा ने बार बार दोहराया है और महत्ता दी है. मुझे ऐसा लगा जैसे मैं दद्दा द्वारा निर्मित त्यागमयी नारियों को उनकी प्रौढ़ावस्था में देख रही हूँ, जिनके त्याग, समर्पण, सेवा और आत्मदान की परिणति कुण्ठा, हीनभाव और स्नायविक विकृतियों में नहीं, आनन्द और सुख में होती है.
यदि मैं यह कहूँ तो अतिशयोक्ति न होगी कि दद्दा की नारी भावना का व्यवहारिक मूल्य मैंने जिया के सम्पर्क में आ कर ही जाना. हो सकता है इसका कारण यह भी हो कि समय के साथ साथ प्रौढ़ता प्राप्त करने के कारण भी नारी के जीवन मूल्यों के सम्बन्ध में मेरी धारणाओं में परिवर्तन आया हो. नारी सम्स्याओं के विषय में जब कुछ सोचने समझने की बुद्धि आयी उसी समय मैंने महादेवी जी की "श्रृंखला की कड़ियाँ" नामक पुस्तक पढ़ी थी. पुरुष जाति की नृशंसता, कठोरता, शोषण प्रवृति, दमन नीति इत्यादि के विरुद्ध मेरी प्रतिक्रियाएँ बड़ी विद्रोहात्मक हुआ करती थीं, और वादविवाद प्रतियोगिताओं और बहसों में भी नारी की ओर से पुरुषों के "जिहाद" का झण्डा उठा कर चलना चाहती थी (पर समय के साथ ही साथ अकल ठिकाने आ गयी) ऐसी स्थिति में गुप्त जी नारियों को आदर्श रूप में स्वीकार करना मेरे वश की बात नहीं थी. मुझे बराबर यही लगता था कि काव्य की उपेक्षिताओं का जो "उद्धार" गुप्त जी ने किया है वह अव्यावहारिक, काल्पनिक और यथार्थ से परे है, उनके व्यक्तित्वों में जो आदर्शोन्मुख है उसी के कारण नारी जाति पतन के गर्त में गिरी है, उनके मानसिक व्यक्तित्व की शक्ति भौतिक शक्ति और शारीरिक क्षमता के अभाव में अर्थहीन है.
जिया के दीर्घकालीन सम्पर्क में आने के बाद, जैसे धीरे धीरे मेरी आँखौं के सामने से भ्रम का उठता हुआ परदा, एक वेग से उठ गया, और मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि "नारी" के इस उद्धार में दद्दा की प्रेरणा अतीतोन्मुखी नहीं थी, परम्परा और भारतीय संस्कारों की लीक में बँध कर उसके व्यक्तित्व का निर्माण नहीं किया गया था, बल्कि भारतीय वांग्मय के इतिहास में शायद पहली बार दद्दा ने अपने युग की भारतीय संस्कारों में पली नारी की गरिमा और त्याग को महत्ता और अभिव्यक्ति दी थी. और इनके पीछे वह निरक्षर नारी थी जो अपने त्याग और आदर्श को जाने बिना ही अपने देवता की भावनाओं को इन गुणों के रस से सिक्त कर रही थी. गुप्त जी की चलाई हुई इस परम्परा का विकास "उर्वशी" की औशीनरी, "सुहाग के नूपुर" की कन्नगी तथा "बूँद और समुद्र" की वनकन्या में हुआ है, जहाँ उस पीढ़ी और वर्ग की भारतीय नारी के व्यक्तित्व में निहित धरती की सी शक्ति और महिमा को पहिचाना गया है. दद्दा ने जिस "प्रपत्ति" का चिंतन किया है, जिया ने उसे झेला है, अगर दद्दा ने उसका अनुभव किया है जो जिया के माध्यम से, ऐसा मैं विनयपूर्ण, पर निःसंकोच कह सकती हूँ.
दद्दा के दरबार में जब कभी तीन चार दरबारियों से अधिक भीड़ आ जाती, मैं जिया की रसोई में आश्रय लेती. वे दद्दा की बैठक के प्रसिद्ध लड्डू, मट्ठी और चटनी का प्रबंध करवातीं और मेरे लिए कुर्सी मंगा देतीं, परन्तु मुझे तो उनके पास पट्टे पर बैठना ही अच्छा लगता था. उनके पास बैठ कर इधर उधर की, खासकर दद्दा और बापू के विषय में बात करने में मुझे बड़ा आनन्द आता. मैं एक प्रसंग छेड़ देती और उससे सम्बद्ध छोटी छोटी कई घटनाएँ वह मुझे सुना देती. एक दिन मैंने उनसे पूछ लिया, "जिया, आप अपनी शादी में कितनी बड़ी थीं?" प्रश्न शायद अप्रत्याशित था, उनकी आँखें संकोच और शील मिश्रित स्निग्धता से भर उठीं. अपनी हँसी को रोकने के लिए उन्होंने आंचल का पल्ला मुख पर रख लिया और फ़िर संयत हो कर बुंदेलखँडी में अपने विवाह के समय की तीन चार घटनाएँ सुनायीं. अच्छा होता मैं उसे जिया की भाषा में ही सुना सकती, पर बुंदेलखँडी लिखने में मैं गलती अवश्य कर जाऊँगी, इसलिए स्मृतियों को अपनी भाषा में ही व्यक्त कर रही हूँ. इस प्रसंग से सम्बन्धित एक रोचक चित्र है, एक चौदह वर्षीय किशोरी, नववधु के रूप में, चिरगाँव के प्रसिद्ध श्रेष्ठीकुल की भारी गृहस्थी और वंशविस्तार के दायित्व का बोझ अपने कन्धों पर झेलने के लिए, गुप्त परिवार में प्रवेश करती है, पति गृह में होने वाली सब परिक्षाओं के लिए तैयार है. पर उससे यह कैसा प्रश्न पूछा जाता है. "तुम्हें पढ़ना लिखना आता है?" अवगुण्ठनवती बहु उत्तर में सिर हिला कर कहती है, "नहीं". प्रश्नकर्ता समझते हैं उसका उत्तर स्वीकारात्मक है. बहु असमंजस में पड़ जाती है और पढ़ने लिखने की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाती है.
इसी प्रकार एक दिन "नारी के कवि" की पत्नी कि प्रतिक्रियाओं से अवगत होने की सहज इच्छा से प्रेरित हो कर मैंने पूछा, "जिया जब दद्दा अपनी किताबें लिखते थे तो आप को पता रहता था कि वह क्या लिखते हैं?" जिया अपनी सहज मुस्कान के साथ बोलीं, "मुझे तो इतना ही पता है कि जब ये छोटे थे तभी कवित्त बनाने लगे थे. सात आठ साल की उमर में ही इन्होंने कवित्त बना दिये तो मेरे ससुर बहुत खुश हुए थे, तभी लोग समझ गये थे कि आगे चलकर ये बहुत अच्छी कविता बनायेंगे. फ़िर तो इनने बहुतेरी किताबें बनायीं. एक में तो मेरे ससुर जी की फोटो भी लगी थी." मैंने पूछा, "अच्छा जिया, जब दद्दा कविता लिखते हैं तब आप को पता चल जाता है?" और उनका उत्तर तत्पर था, "हाँ घँटों बैठे सोचते रहते हैं, इधर उधर टहलते हैं, बार बार स्लेट पर लिख कर बार बार मिटाते हैं, ठीक करते हैं, देर देर तक काम करते रहते हैं." मैं जिया की ओर मुग्ध तन्मयता के साथ देखती हुई सोचती रही, क्या वन में सीता का सफ़ल गार्हस्थ, दद्दा जिया के योग के बिना जगा सकते थे? क्या परिवार के लिए सतत कार्यरत, जिया की विश्रामरहित दिनचर्या की प्रेरणा के बिना दद्दा की सीता "श्रमवारिबिन्दु फ़ल स्वास्थ्य शुक्ति फ़ल" बन सकती थी? क्या सीता का "अंचल व्यजन" का चित्रण करते समय जिया का "अंचल व्यजन" दद्दा के समाने नहीं होगा? मेरे ध्यान योग में उस समय दद्दा अकेले नहीं रह गये थे. शिरिष कुसुम से सूक्ष्म और कोमल पर रेशम के से दृढ़ सूत्रों में बँधा दद्दा का कवि व्यक्तित्व जिया के साथ मेरी आँखों में साकार हो उठा.
12 डी, फ़िरोज़शाह रोड, सीतानवमी का दिन. अन्नपूर्णा की रसोई से उठी हुई विविध प्रकार के व्यंजनों की सुगन्ध सारे घर में फ़ैल रही थी. पता नहीं किस प्रेरणा से उस दिन मैं सीधे जिया के कमरे की ओर ही चली गयी. जिया उस समय सद्य स्नान किये हुए पीताम्बर परिधान में पवित्रता में पगी हुई देवार्चन में लीन थीं. सामने देव सिंहासन पर सीताराम की युगल मूर्ती विराजमान थी. तुलसी का गमला साथ रखा हुआ था, और मूर्ति के निकट ही रामचरितमानस की प्रति फ़ूलों से ढकी हुई रखी थी. धूप, दीप, आरती और पूजा के अन्य उपकरणों के साथ वातावरण बड़ा शुभ्र और पवित्र हो रहा था, पास ही शान्ति, जिया की पुत्रवधु, मैना के साथ उमा सी खड़ी थी. पूजा में बाधा न पड़े, यह सोच कर मैं पैरों की आहट दिये बिना, पीछे ही दीवार से टिकी, अभिभूत हो कर जिया की पूजाविधि देखती रही. रामभक्त वैष्णव महाकवि की निरक्षर पत्नि जब रामचरित मानस पर सिर टेक कर ध्यान में लीन थी, मुझे आज की नारी की सारी साक्षरता और विद्वता तुच्छ जान पड़ रही थी. श्रद्धा, आस्था और विश्वास की गरिमा से वंचित हो कर रामचरितमानस की पंक्तियों का अर्थ निकालने और व्याख्या करने वाली नारी का ज्ञान मुझे इस आस्था के सामने सिर झुकाता जान पड़ा. इड़ा की हार और श्रद्धा का विजय जैसे अनायास ही आँखों के सामने घटित हो गयी. मेरे मन में आया, काश! पुरुष ने इस श्रद्धा और समर्पण का दुरुपयोग न किया होता.
एक दिन मन बहुत संतप्त था. मेरी एक शिष्या का छः वर्षीय पुत्र कई दिनों से अस्पताल में था. अस्पताल में ही उसने मुझसे काले शीशे की ऐनक की माँग की थी. ऐनक मेरे बैग में ही रखी थी और मुझे सूचना मिली कि उसकी मृत्यु हो गयी. मन और मस्तिष्क पर मृत्यु का अवसाद और उदासी छायी हुई थी. जिया ने मुझे देखते ही पूछा, "तबियत ठीक नहीं है क्या?" मैंने उन्हें बच्चे की बीमारी और मृत्यु का हाल सुना दिया. जिया के मुख पर जैसे छाया और अन्धकार की कुछ रेखाएँ उभर आयीं. अपनी दिवंगत सन्तानों की बीमारी और मृत्यु की स्मृतियाँ उनके मस्तिष्क में भी ताज़ी हो गयीं. एक पुत्र सुदर्शन की बातें करते करते उनका गला भर आया. वह कह रही थीं, "तुम्हारे दद्दा उसे बहुत प्यार करते थे. चौबीस घँटे अपने पास ही रखते थे. जब वह मरा तो बहुत देर तक उसके मुँह पर मुँह रख कर रोते रहे. फ़िर मैंने धीर बाँध कर अजमेरी जी पास संदेश भिजवाया (दद्दा के कुल की मर्यादा के अनुसार पत्नी सब के सामने पति से बात नहीं कर सकती थी) कि उनसे कह दें कि वे मरे मुरे के मुँह में मुँह न लगायें. मैं धीर धर रही हूँ तो वे भी धरें." जिया का यह वाक्य जैसे मेरे हृदय को बेध गया. मेरी दृष्टि जैसे चमक गयी. "राहुल" का दान देती यशोधरा में क्या जिया की यह शक्ति नहीं बोल रही थी?
जिया के प्रति बापू (स्व. सिया राम शरण गुप्त) का मर्यादापूर्ण व्यवहार देख और सम्मान का भाव देख कर उस देवर की याद आ जाती थी, जो अपनी भाभी के आभूषण ही पहचान सकता था. यह "लक्ष्मण" तो शायद अपनी अन्नपूर्णा भाभी के हाथों की चूड़ियाँ ही पहचान सकता, जो भोजन की थाली सामने रखते हुए अपने आप ही दिखाई पड़ जाती रही होंगी.
राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त के बारे में कुछ जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध है, जिनमें उनके माता पिता के नाम तो हैं तो लेकिन उनकी पत्नी, यानि इस आलेख की नायिका "जिया" का नाम नहीं मिला मुझे. गुप्त जी के काव्य में उपेक्षित उर्मिला की बात तो होती है, लेकिन उनकी अपनी उर्मिला को भूलने वाली भी क्या वही बात नहीं?
जिया
लगभग दस वर्ष पूर्व छः, नार्थ एवेन्यू की बैठक में घुसते ही स्क्रीन की आड़ में खड़ी एक नारी मूर्ती की ओर अनायास ही मेरी आँखें उठ गयीं, और मैं अपने आप ही समझ गयी कि यह "जिया" हैं. ग्रामवधु की सहज मुस्कान, स्निग्ध आर्द्र वात्सल्यमयी आँखें, गौरवान्वित भावाभिव्यक्ति, पर अभिमान और दम्भ का स्पर्श नहीं - साकेत की "मूर्तिमती ममता माया" ही जैसे मेरे सामने खड़ी थी. मुझे देखते ही मुस्कान का स्थान, मृदुल हास्य ने ले लिया और फ़िर हँसते हुए हाथ जोड़ कर उन्होंने मुझे नमस्ते किया - सब कुछ एक क्षण में हो गया और मैं स्तम्भित खड़ी रह गयी. क्या कहूँ, क्या करूँ ? संकोशवश बिना कुछ बोले केवल नमस्कार कर सकी. उनके प्रथम दर्शन की वह झलक मेरे मानस पर जैसे स्थायी हो गयी है. शुद्ध खद्दर की केसरिया साड़ी उनके त्यागपूर्ण गौरव भरे सुहाग की कहानी कह रही थी. गले में पड़ी हुई सोने की जंजीर के साथ तुलसी की कण्ठी में, मानो उच्चकुल वधू का गरिमापूर्ण पत्नित्व और यशोधरा की वैष्णव भावना एक दूसरे को बल देते हुए साकार थी. माथे पर लगी चमकती हुई बिंदिया पर सुनहले अक्षरों

यदि मैं यह कहूँ तो अतिशयोक्ति न होगी कि दद्दा की नारी भावना का व्यवहारिक मूल्य मैंने जिया के सम्पर्क में आ कर ही जाना. हो सकता है इसका कारण यह भी हो कि समय के साथ साथ प्रौढ़ता प्राप्त करने के कारण भी नारी के जीवन मूल्यों के सम्बन्ध में मेरी धारणाओं में परिवर्तन आया हो. नारी सम्स्याओं के विषय में जब कुछ सोचने समझने की बुद्धि आयी उसी समय मैंने महादेवी जी की "श्रृंखला की कड़ियाँ" नामक पुस्तक पढ़ी थी. पुरुष जाति की नृशंसता, कठोरता, शोषण प्रवृति, दमन नीति इत्यादि के विरुद्ध मेरी प्रतिक्रियाएँ बड़ी विद्रोहात्मक हुआ करती थीं, और वादविवाद प्रतियोगिताओं और बहसों में भी नारी की ओर से पुरुषों के "जिहाद" का झण्डा उठा कर चलना चाहती थी (पर समय के साथ ही साथ अकल ठिकाने आ गयी) ऐसी स्थिति में गुप्त जी नारियों को आदर्श रूप में स्वीकार करना मेरे वश की बात नहीं थी. मुझे बराबर यही लगता था कि काव्य की उपेक्षिताओं का जो "उद्धार" गुप्त जी ने किया है वह अव्यावहारिक, काल्पनिक और यथार्थ से परे है, उनके व्यक्तित्वों में जो आदर्शोन्मुख है उसी के कारण नारी जाति पतन के गर्त में गिरी है, उनके मानसिक व्यक्तित्व की शक्ति भौतिक शक्ति और शारीरिक क्षमता के अभाव में अर्थहीन है.
जिया के दीर्घकालीन सम्पर्क में आने के बाद, जैसे धीरे धीरे मेरी आँखौं के सामने से भ्रम का उठता हुआ परदा, एक वेग से उठ गया, और मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि "नारी" के इस उद्धार में दद्दा की प्रेरणा अतीतोन्मुखी नहीं थी, परम्परा और भारतीय संस्कारों की लीक में बँध कर उसके व्यक्तित्व का निर्माण नहीं किया गया था, बल्कि भारतीय वांग्मय के इतिहास में शायद पहली बार दद्दा ने अपने युग की भारतीय संस्कारों में पली नारी की गरिमा और त्याग को महत्ता और अभिव्यक्ति दी थी. और इनके पीछे वह निरक्षर नारी थी जो अपने त्याग और आदर्श को जाने बिना ही अपने देवता की भावनाओं को इन गुणों के रस से सिक्त कर रही थी. गुप्त जी की चलाई हुई इस परम्परा का विकास "उर्वशी" की औशीनरी, "सुहाग के नूपुर" की कन्नगी तथा "बूँद और समुद्र" की वनकन्या में हुआ है, जहाँ उस पीढ़ी और वर्ग की भारतीय नारी के व्यक्तित्व में निहित धरती की सी शक्ति और महिमा को पहिचाना गया है. दद्दा ने जिस "प्रपत्ति" का चिंतन किया है, जिया ने उसे झेला है, अगर दद्दा ने उसका अनुभव किया है जो जिया के माध्यम से, ऐसा मैं विनयपूर्ण, पर निःसंकोच कह सकती हूँ.
दद्दा के दरबार में जब कभी तीन चार दरबारियों से अधिक भीड़ आ जाती, मैं जिया की रसोई में आश्रय लेती. वे दद्दा की बैठक के प्रसिद्ध लड्डू, मट्ठी और चटनी का प्रबंध करवातीं और मेरे लिए कुर्सी मंगा देतीं, परन्तु मुझे तो उनके पास पट्टे पर बैठना ही अच्छा लगता था. उनके पास बैठ कर इधर उधर की, खासकर दद्दा और बापू के विषय में बात करने में मुझे बड़ा आनन्द आता. मैं एक प्रसंग छेड़ देती और उससे सम्बद्ध छोटी छोटी कई घटनाएँ वह मुझे सुना देती. एक दिन मैंने उनसे पूछ लिया, "जिया, आप अपनी शादी में कितनी बड़ी थीं?" प्रश्न शायद अप्रत्याशित था, उनकी आँखें संकोच और शील मिश्रित स्निग्धता से भर उठीं. अपनी हँसी को रोकने के लिए उन्होंने आंचल का पल्ला मुख पर रख लिया और फ़िर संयत हो कर बुंदेलखँडी में अपने विवाह के समय की तीन चार घटनाएँ सुनायीं. अच्छा होता मैं उसे जिया की भाषा में ही सुना सकती, पर बुंदेलखँडी लिखने में मैं गलती अवश्य कर जाऊँगी, इसलिए स्मृतियों को अपनी भाषा में ही व्यक्त कर रही हूँ. इस प्रसंग से सम्बन्धित एक रोचक चित्र है, एक चौदह वर्षीय किशोरी, नववधु के रूप में, चिरगाँव के प्रसिद्ध श्रेष्ठीकुल की भारी गृहस्थी और वंशविस्तार के दायित्व का बोझ अपने कन्धों पर झेलने के लिए, गुप्त परिवार में प्रवेश करती है, पति गृह में होने वाली सब परिक्षाओं के लिए तैयार है. पर उससे यह कैसा प्रश्न पूछा जाता है. "तुम्हें पढ़ना लिखना आता है?" अवगुण्ठनवती बहु उत्तर में सिर हिला कर कहती है, "नहीं". प्रश्नकर्ता समझते हैं उसका उत्तर स्वीकारात्मक है. बहु असमंजस में पड़ जाती है और पढ़ने लिखने की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाती है.
इसी प्रकार एक दिन "नारी के कवि" की पत्नी कि प्रतिक्रियाओं से अवगत होने की सहज इच्छा से प्रेरित हो कर मैंने पूछा, "जिया जब दद्दा अपनी किताबें लिखते थे तो आप को पता रहता था कि वह क्या लिखते हैं?" जिया अपनी सहज मुस्कान के साथ बोलीं, "मुझे तो इतना ही पता है कि जब ये छोटे थे तभी कवित्त बनाने लगे थे. सात आठ साल की उमर में ही इन्होंने कवित्त बना दिये तो मेरे ससुर बहुत खुश हुए थे, तभी लोग समझ गये थे कि आगे चलकर ये बहुत अच्छी कविता बनायेंगे. फ़िर तो इनने बहुतेरी किताबें बनायीं. एक में तो मेरे ससुर जी की फोटो भी लगी थी." मैंने पूछा, "अच्छा जिया, जब दद्दा कविता लिखते हैं तब आप को पता चल जाता है?" और उनका उत्तर तत्पर था, "हाँ घँटों बैठे सोचते रहते हैं, इधर उधर टहलते हैं, बार बार स्लेट पर लिख कर बार बार मिटाते हैं, ठीक करते हैं, देर देर तक काम करते रहते हैं." मैं जिया की ओर मुग्ध तन्मयता के साथ देखती हुई सोचती रही, क्या वन में सीता का सफ़ल गार्हस्थ, दद्दा जिया के योग के बिना जगा सकते थे? क्या परिवार के लिए सतत कार्यरत, जिया की विश्रामरहित दिनचर्या की प्रेरणा के बिना दद्दा की सीता "श्रमवारिबिन्दु फ़ल स्वास्थ्य शुक्ति फ़ल" बन सकती थी? क्या सीता का "अंचल व्यजन" का चित्रण करते समय जिया का "अंचल व्यजन" दद्दा के समाने नहीं होगा? मेरे ध्यान योग में उस समय दद्दा अकेले नहीं रह गये थे. शिरिष कुसुम से सूक्ष्म और कोमल पर रेशम के से दृढ़ सूत्रों में बँधा दद्दा का कवि व्यक्तित्व जिया के साथ मेरी आँखों में साकार हो उठा.
12 डी, फ़िरोज़शाह रोड, सीतानवमी का दिन. अन्नपूर्णा की रसोई से उठी हुई विविध प्रकार के व्यंजनों की सुगन्ध सारे घर में फ़ैल रही थी. पता नहीं किस प्रेरणा से उस दिन मैं सीधे जिया के कमरे की ओर ही चली गयी. जिया उस समय सद्य स्नान किये हुए पीताम्बर परिधान में पवित्रता में पगी हुई देवार्चन में लीन थीं. सामने देव सिंहासन पर सीताराम की युगल मूर्ती विराजमान थी. तुलसी का गमला साथ रखा हुआ था, और मूर्ति के निकट ही रामचरितमानस की प्रति फ़ूलों से ढकी हुई रखी थी. धूप, दीप, आरती और पूजा के अन्य उपकरणों के साथ वातावरण बड़ा शुभ्र और पवित्र हो रहा था, पास ही शान्ति, जिया की पुत्रवधु, मैना के साथ उमा सी खड़ी थी. पूजा में बाधा न पड़े, यह सोच कर मैं पैरों की आहट दिये बिना, पीछे ही दीवार से टिकी, अभिभूत हो कर जिया की पूजाविधि देखती रही. रामभक्त वैष्णव महाकवि की निरक्षर पत्नि जब रामचरित मानस पर सिर टेक कर ध्यान में लीन थी, मुझे आज की नारी की सारी साक्षरता और विद्वता तुच्छ जान पड़ रही थी. श्रद्धा, आस्था और विश्वास की गरिमा से वंचित हो कर रामचरितमानस की पंक्तियों का अर्थ निकालने और व्याख्या करने वाली नारी का ज्ञान मुझे इस आस्था के सामने सिर झुकाता जान पड़ा. इड़ा की हार और श्रद्धा का विजय जैसे अनायास ही आँखों के सामने घटित हो गयी. मेरे मन में आया, काश! पुरुष ने इस श्रद्धा और समर्पण का दुरुपयोग न किया होता.
एक दिन मन बहुत संतप्त था. मेरी एक शिष्या का छः वर्षीय पुत्र कई दिनों से अस्पताल में था. अस्पताल में ही उसने मुझसे काले शीशे की ऐनक की माँग की थी. ऐनक मेरे बैग में ही रखी थी और मुझे सूचना मिली कि उसकी मृत्यु हो गयी. मन और मस्तिष्क पर मृत्यु का अवसाद और उदासी छायी हुई थी. जिया ने मुझे देखते ही पूछा, "तबियत ठीक नहीं है क्या?" मैंने उन्हें बच्चे की बीमारी और मृत्यु का हाल सुना दिया. जिया के मुख पर जैसे छाया और अन्धकार की कुछ रेखाएँ उभर आयीं. अपनी दिवंगत सन्तानों की बीमारी और मृत्यु की स्मृतियाँ उनके मस्तिष्क में भी ताज़ी हो गयीं. एक पुत्र सुदर्शन की बातें करते करते उनका गला भर आया. वह कह रही थीं, "तुम्हारे दद्दा उसे बहुत प्यार करते थे. चौबीस घँटे अपने पास ही रखते थे. जब वह मरा तो बहुत देर तक उसके मुँह पर मुँह रख कर रोते रहे. फ़िर मैंने धीर बाँध कर अजमेरी जी पास संदेश भिजवाया (दद्दा के कुल की मर्यादा के अनुसार पत्नी सब के सामने पति से बात नहीं कर सकती थी) कि उनसे कह दें कि वे मरे मुरे के मुँह में मुँह न लगायें. मैं धीर धर रही हूँ तो वे भी धरें." जिया का यह वाक्य जैसे मेरे हृदय को बेध गया. मेरी दृष्टि जैसे चमक गयी. "राहुल" का दान देती यशोधरा में क्या जिया की यह शक्ति नहीं बोल रही थी?
जिया के प्रति बापू (स्व. सिया राम शरण गुप्त) का मर्यादापूर्ण व्यवहार देख और सम्मान का भाव देख कर उस देवर की याद आ जाती थी, जो अपनी भाभी के आभूषण ही पहचान सकता था. यह "लक्ष्मण" तो शायद अपनी अन्नपूर्णा भाभी के हाथों की चूड़ियाँ ही पहचान सकता, जो भोजन की थाली सामने रखते हुए अपने आप ही दिखाई पड़ जाती रही होंगी.
शुक्रवार, अगस्त 13, 2010
वैज्ञानिक की परीक्षा
जाने क्यों बचपन से ही मेरे मन में बात घुस गयी कि गणित बहुत कठिन है और मेरे बस की बात नहीं. जब हाई स्कूल पास किया तो गणित में अच्छे नम्बर आये थे लेकिन उससे भी मेरे मन की यह सोच नहीं बदली. तब से गणित के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए सम्मान और उत्सुकता महसूस होती है कि जाने कैसे यह लोग इस विषय में दिलचस्पी रखते हैं और इसे समझ पाते हैं. उनके बारे में कुछ नया सुनता हूँ तो अवश्य पढ़ता हूँ और समझने की कोशिश करता हूँ. इसीलिए जब भारतीय अंग्रेज़ी दैनिक टेलीग्राफ़ में शीर्षक पढ़ा "भारतीय इंजीनियर विनय देवलालिकर ने गणित की जटिल समस्या का हल किया" तो तुरंत उस समाचार को पढ़ा.
इस समाचार में जिस जटिल समस्या की बात की गयी है, उसे कहते हैं, "पी बनाम एनपी" समस्या, लेकिन इसका क्या अर्थ है, यह मेरी समझ से बाहर है. तीस साल से इस समस्या का समाधान खोजने वालों ने घोषणा की हुई है कि इस समस्या को सुलझाने वाले को दस लाख डालर का पुरस्कार मिलेगा. समाचार में यह भी बताया गया कि दुनिया के बहुत से अन्य गणितविज्ञों ने संदेह प्रकट किया है कि सचमुच विनय देवलालिकर ने इस समस्या का समाधान खोज निकाला है, या यह झूठ है. एक महोदय ने तो अपनी तरफ़ दावा किया है कि अगर देवलालिकर जी ने सचमुच इस समस्या का हल निकाला हो तो वह अपनी ओर से अन्य दो लाख डालर का पुरस्कार देंगे.
देवलालिकर के दावे और उस पर होती बहस की बात से कुछ दिन पढ़ी एक अन्य बात याद आ गयी. इस वर्ष मानव कोष के डीएनए (DNA) में छुपे जीन (Gene) का नक्शा समझने की दसवीं वर्षगाँठ मनायी जा रही है. इसी जीन के माध्यम से सभी पेड़, जीव जन्तु अपनी संतान को अपने गुण देते हैं और इस मानव जीन के नक्शे से भविष्य की वैज्ञानिक तरक्कियों की बहुत सी उम्मीदें जुड़ी हैं. इसकी वजह से आज कई तरह के कैंसर तथा अन्य बीमारियों की समझ बढ़ी है और नयी दवाईयों की खोज हो सकी है, कई जन्मजात बीमारियों यानि माँ के गर्भ में ही पनपी बीमारियों के इलाज की आशा बँधी है. आने वालों दशकों में इस खोज से मानव जीवन कितना बदल जायेगा, इसका आज अनुमान लगाना आसान नहीं, लेकिन इसमें किसी को शक नहीं इस खोज से दुनिया बदल जायेगी.
 छोटे से बैक्टीरिया यानि सूक्ष्म एक कोषरुपी किटाणुओं से ले कर मानव जैसे विकसित जन्तुओं के जीन करोड़ों छोटे कणों से बने होते हैं जिन्हें जीनोम (Genome) कहते हैं, और जीन का नक्शा बनाने का अर्थ है कि यह बताया जाये कि उन करोड़ों कणों में से कौन सा कण कहाँ पर है.
छोटे से बैक्टीरिया यानि सूक्ष्म एक कोषरुपी किटाणुओं से ले कर मानव जैसे विकसित जन्तुओं के जीन करोड़ों छोटे कणों से बने होते हैं जिन्हें जीनोम (Genome) कहते हैं, और जीन का नक्शा बनाने का अर्थ है कि यह बताया जाये कि उन करोड़ों कणों में से कौन सा कण कहाँ पर है.
आज से करीब बीस साल पहले, 1989 में सिस्टिक फाईब्रोसिस नाम की बीमारी के जीन का नक्शा बनाने वाली एक कम्पनी ने इस खोज पर कई सालों तक काम किया था और इसमें खर्चा पड़ा था करीब 5 करोड़ डालर. आज कुछ हज़ार डालर में पूरे मानव डीएनए के सभी जीनों का पूरा नक्शा बनाया जा सकता है. कहते हैं कि अगले कुछ वर्षों में इसकी कीमत एक हज़ार डालर से भी कम हो जायेगी. जीन शौध के साथ एक अन्य महत्वपूर्ण बात जुड़ी है कि इस वैज्ञानिक खोज की सभी जानकारी किसी एक व्यक्ति या एक कम्पनी के हाथ में नहीं है बल्कि खुले रूप में दुनिया के सभी वैज्ञानिकों के लिए उपलब्ध है. इस वर्ष मार्च में भारत ने भी घोषणा की कि दिल्ली की जेनोमिक्स संस्थान ने एक मानव जीन का नक्शा पूरा किया.
इस जीन के नक्शे बनाने की खोज में एक वैज्ञानिक ने बहुत महत्वपूर्ण काम किया था जिनका नाम है जीन मेयरस (Gene Myers).
मेयरस ने एक नये तरीके से जीन की जाँच की खोज की थी. इस तरीके में पूरे डीएनए को सूक्ष्म कोष स्तर पर बम विस्फोट जैसा करके छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है फ़िर उन टुकड़ों की जाँच की जाती है. 1998-99 जब उन्होंने अपना यह नया तरीका अन्य वैज्ञानिकों के सामने पेश किया तो उस समय अन्य वैज्ञानिकों ने उनके तरीके की बहुत आलोचना की थी. अन्य वैज्ञानिकों का कहना था कि इससे बहुत गलतियाँ होंगी और यह ठीक तरीका नहीं. आज भी मेयरस के मन में गुस्सा है कि शुरु में उनके काम को सराहना नहीं मिली. उनका एक साक्षात्कार पढ़ा जिसमें वह कह रहे थे कि प्रारम्भ में उनके तरीके को जो उपेक्षा मिली, उसकी चोट उनके दिल में आज भी है, जबकि आज जीनोम शौध में उनका तरीका ही अच्छा माना जाता है.
मेरा विचार है कि किसी भी नयी बात का आविष्कार जो उस समय होने वाले तरीकों से बिल्कुल भिन्न हो या उल्टा लगे, उस पर संदेह करना आवश्यक है. इसी में विज्ञान की प्रगति छुपी है. सच्चा वैज्ञानिक वही है जो अपने काम पर संदेह करने वालों से निर्भय बात, बहस कर सके और अपने विचारों की सच्चाई को साबित कर सके.
कई बार सब लोग सोचते हैं कि हाँ बहुत अच्छा और बढ़िया आविष्कार है लेकिन समय ही बताता है कि वह सचमुच का नया आविष्कार था या केवल मन का धोखा. दुनिया में नीम हकीम और लोगों के विश्वासों का फायदा उठाने वाले लोग कम नहीं हैं, उनकी बात नहीं कर रहा मैं. जिसने सच में पूरी वैज्ञानिक सोच के साथ कुछ नया खोजा हो, उस पर भी संदेह करना, उसमें नुक्स निकालना, उसकी कमियों की बात करना, यही वैज्ञानिक प्रगति का रास्ता है. शायद इसीलिए अधिकतर आविष्कारक बिना प्रसिद्धि और पैसे के ही जीवन गुज़ारते हैं और यह प्रसिद्धि उनके मरने के बाद ही आती है.
इस समाचार में जिस जटिल समस्या की बात की गयी है, उसे कहते हैं, "पी बनाम एनपी" समस्या, लेकिन इसका क्या अर्थ है, यह मेरी समझ से बाहर है. तीस साल से इस समस्या का समाधान खोजने वालों ने घोषणा की हुई है कि इस समस्या को सुलझाने वाले को दस लाख डालर का पुरस्कार मिलेगा. समाचार में यह भी बताया गया कि दुनिया के बहुत से अन्य गणितविज्ञों ने संदेह प्रकट किया है कि सचमुच विनय देवलालिकर ने इस समस्या का समाधान खोज निकाला है, या यह झूठ है. एक महोदय ने तो अपनी तरफ़ दावा किया है कि अगर देवलालिकर जी ने सचमुच इस समस्या का हल निकाला हो तो वह अपनी ओर से अन्य दो लाख डालर का पुरस्कार देंगे.
देवलालिकर के दावे और उस पर होती बहस की बात से कुछ दिन पढ़ी एक अन्य बात याद आ गयी. इस वर्ष मानव कोष के डीएनए (DNA) में छुपे जीन (Gene) का नक्शा समझने की दसवीं वर्षगाँठ मनायी जा रही है. इसी जीन के माध्यम से सभी पेड़, जीव जन्तु अपनी संतान को अपने गुण देते हैं और इस मानव जीन के नक्शे से भविष्य की वैज्ञानिक तरक्कियों की बहुत सी उम्मीदें जुड़ी हैं. इसकी वजह से आज कई तरह के कैंसर तथा अन्य बीमारियों की समझ बढ़ी है और नयी दवाईयों की खोज हो सकी है, कई जन्मजात बीमारियों यानि माँ के गर्भ में ही पनपी बीमारियों के इलाज की आशा बँधी है. आने वालों दशकों में इस खोज से मानव जीवन कितना बदल जायेगा, इसका आज अनुमान लगाना आसान नहीं, लेकिन इसमें किसी को शक नहीं इस खोज से दुनिया बदल जायेगी.

आज से करीब बीस साल पहले, 1989 में सिस्टिक फाईब्रोसिस नाम की बीमारी के जीन का नक्शा बनाने वाली एक कम्पनी ने इस खोज पर कई सालों तक काम किया था और इसमें खर्चा पड़ा था करीब 5 करोड़ डालर. आज कुछ हज़ार डालर में पूरे मानव डीएनए के सभी जीनों का पूरा नक्शा बनाया जा सकता है. कहते हैं कि अगले कुछ वर्षों में इसकी कीमत एक हज़ार डालर से भी कम हो जायेगी. जीन शौध के साथ एक अन्य महत्वपूर्ण बात जुड़ी है कि इस वैज्ञानिक खोज की सभी जानकारी किसी एक व्यक्ति या एक कम्पनी के हाथ में नहीं है बल्कि खुले रूप में दुनिया के सभी वैज्ञानिकों के लिए उपलब्ध है. इस वर्ष मार्च में भारत ने भी घोषणा की कि दिल्ली की जेनोमिक्स संस्थान ने एक मानव जीन का नक्शा पूरा किया.
इस जीन के नक्शे बनाने की खोज में एक वैज्ञानिक ने बहुत महत्वपूर्ण काम किया था जिनका नाम है जीन मेयरस (Gene Myers).
मेयरस ने एक नये तरीके से जीन की जाँच की खोज की थी. इस तरीके में पूरे डीएनए को सूक्ष्म कोष स्तर पर बम विस्फोट जैसा करके छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है फ़िर उन टुकड़ों की जाँच की जाती है. 1998-99 जब उन्होंने अपना यह नया तरीका अन्य वैज्ञानिकों के सामने पेश किया तो उस समय अन्य वैज्ञानिकों ने उनके तरीके की बहुत आलोचना की थी. अन्य वैज्ञानिकों का कहना था कि इससे बहुत गलतियाँ होंगी और यह ठीक तरीका नहीं. आज भी मेयरस के मन में गुस्सा है कि शुरु में उनके काम को सराहना नहीं मिली. उनका एक साक्षात्कार पढ़ा जिसमें वह कह रहे थे कि प्रारम्भ में उनके तरीके को जो उपेक्षा मिली, उसकी चोट उनके दिल में आज भी है, जबकि आज जीनोम शौध में उनका तरीका ही अच्छा माना जाता है.
मेरा विचार है कि किसी भी नयी बात का आविष्कार जो उस समय होने वाले तरीकों से बिल्कुल भिन्न हो या उल्टा लगे, उस पर संदेह करना आवश्यक है. इसी में विज्ञान की प्रगति छुपी है. सच्चा वैज्ञानिक वही है जो अपने काम पर संदेह करने वालों से निर्भय बात, बहस कर सके और अपने विचारों की सच्चाई को साबित कर सके.
कई बार सब लोग सोचते हैं कि हाँ बहुत अच्छा और बढ़िया आविष्कार है लेकिन समय ही बताता है कि वह सचमुच का नया आविष्कार था या केवल मन का धोखा. दुनिया में नीम हकीम और लोगों के विश्वासों का फायदा उठाने वाले लोग कम नहीं हैं, उनकी बात नहीं कर रहा मैं. जिसने सच में पूरी वैज्ञानिक सोच के साथ कुछ नया खोजा हो, उस पर भी संदेह करना, उसमें नुक्स निकालना, उसकी कमियों की बात करना, यही वैज्ञानिक प्रगति का रास्ता है. शायद इसीलिए अधिकतर आविष्कारक बिना प्रसिद्धि और पैसे के ही जीवन गुज़ारते हैं और यह प्रसिद्धि उनके मरने के बाद ही आती है.
शनिवार, जुलाई 31, 2010
भाषा, लिपि और लेखनी
आजकल अक्सर हिंदी के शब्द अँग्रेज़ी यानि रोमन लिपि में लिखे हुए दिखने लगे हैं. ईमेल से या मोबाईल पर एस.एम.एस से या फ़िर गूगल टाक या फैसबुक पर चेट, बहुत सी बातें होती तो हिंदी में हैं लेकिन सहूलियत के लिए लिखी रोमन लिपि में जाती है. भारतीय नामों को अगर रोमन लिपि में देखा जाये तो अक्सर पता नहीं चलता कि उनका सही उच्चारण क्या है, क्योंकि अँग्रेज़ी भाषा तथा रोमन लिपि में बहुत से स्वर होते ही नहीं.
 कुछ साल पहले जर्मनी में रहने वाले एक भारतीय डाक्टर हमारे यहाँ बोलोनिया आये, नाम था गोपाल दाबड़े. तब वह यही कह रहे थे कि यहाँ यूरोप के लोग उनके नाम को कितनी अलग अलग तरह से कहते हैं. यानि अँग्रेज़ी भाषा के अलावा अन्य यूरोपीय भाषाओं को देखें तो दिक्कतें और भी बढ़ जाती हैं, क्योंकि बहुत सी भाषाओं में रोमन लिपि का ही प्रयोग होता है पर उनका उच्चारण अलग अलग है, जिससे दाबड़े का डाबड, डाबडे, दाबदे, दबदे, कुछ भी बन सकता है.
कुछ साल पहले जर्मनी में रहने वाले एक भारतीय डाक्टर हमारे यहाँ बोलोनिया आये, नाम था गोपाल दाबड़े. तब वह यही कह रहे थे कि यहाँ यूरोप के लोग उनके नाम को कितनी अलग अलग तरह से कहते हैं. यानि अँग्रेज़ी भाषा के अलावा अन्य यूरोपीय भाषाओं को देखें तो दिक्कतें और भी बढ़ जाती हैं, क्योंकि बहुत सी भाषाओं में रोमन लिपि का ही प्रयोग होता है पर उनका उच्चारण अलग अलग है, जिससे दाबड़े का डाबड, डाबडे, दाबदे, दबदे, कुछ भी बन सकता है.
इन्हीं बातों के अनुभव से सोच रहा था कि क्या धीरे धीरे हमारी हिंदी के कुछ स्वर जो अन्य भाषाओं में नहीं होते, लुप्त हो जायेंगे?
वैसे तो एशिया में अन्य कई देश हैं, जैसे इंदोनेशिया, फिलिपीन, वियतनाम, जहाँ पर उनकी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है, पर इससे उनकी भाषा ने अपने विषेश स्वर नहीं खोये. इसका एक कारण यह है कि इन देशों में आम जनता में अँग्रेज़ी बोलने वाले बहुत कम हैं, और वर्षों पहले जब इन्होंने रोमन लिपि को अपनाने का निश्चय किया तो उस समय रोमन लिपि की वर्णमाला की कमियों को पूरा करने के लिए एक्सेंट वाले वर्णों को लेटिन वर्णमाला से ले कर जोड़ लिया जिनका प्रयोग अन्य यूरोपीय भाषाओं में होता है जैसे कि à á â ã ä å. इस तरह उन्हें अपनी भाषा के विषेश स्वरों को लिखने के अन्य वर्ण मिल गये.
उदाहरण के लिए D Ð Ď d जैसे वर्णों से आप वियतनामी भाषा में द, ड, ड़, ध जैसे विभिन्न स्वरों को अलग अलग वर्ण दे सकते हैं, इसलिए जब वह रोमन लिपि में लिखते हैं तो भी अपनी भाषाओं के विषेश स्वरों के उच्चारण को संभाल कर रखते हैं. पर हिंदी या अन्य भारतीय भाषाओं के साथ ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे उनकी बोली और विषेश स्वरों का रोमनीकरण न हो?
भाषा एक जैसी नहीं रहती, समय के साथ बदलती रहती है. वेदों, पुराणों, बाइबल, कुरान और अन्य प्राचीन ग्रंथों को भाषाविज्ञानी जाँच कर बता सकते हें कि कौन सा हिस्सा पहले लिखा गया, कौन सा बाद में जोड़ा गया.
भाषा समय के साथ क्यों बदलती है? इसकी एक वजह तो नये आविष्कार है, जिनके लिए नये शब्दों की ज़रूरत पड़ती है. जैसे कम्प्यूटर, ईमेल, इंटरनेट जो पहले नहीं थे, और इनसे जुड़ी बहुत से बातों के शब्द नये बने हैं. समय के साथ कुछ वस्तुओं का उपयोग कम या बंद हो जाता है, जैसे लालटेन, बैलगाड़ी आदि और इनके शब्द धीरे धीरे समय के साथ खो जाते हैं. जब छोटा था तो गुसलखाने में झाँवा होता था पाँव साफ़ करने के लिए लेकिन जब पिछली बार दिल्ली गया और छोटी बहन से पूछा कि क्या उसके घर में झाँवा मिलेगा तो वह हँसने लगी, बोली कितने सालों के बाद यह शब्द सुना है.
विद्वानों का कहना है कि भाषा के विकास का सम्बंध उसकी लिखायी से भी हैं.
बोलने वाली भाषा और लिखने वाली भाषा के बीच में क्या सम्बंध होता है इस विषय पर वाल्टर जे ओंग (Walter J. Ong) ने बहुत शौध किया है और लिखा है. उनकी 1982 की किताब ओराल्टी एँड लिट्रेसी (Orality and Literacy) जो इसी विषय पर है, मुझे बहुत अच्छी लगी. उनका कहना है कि मानव बोली का विकास तीस से पचास हज़ार साल पहले हुआ जबकि लिखाई का आविष्कार केवल छः हज़ार साल पहले हुआ. इस तरह से मानव भाषाएँ बोली के साथ विकसित हुईं. दुनिया की हज़ारों भाषाओं में से केवल 106 में लिखित साहित्य की रचना हुई. आज भी कई सौ ऐसी बोली जाने वाली भाषाएँ हैं जिनकी कोई लिपि नहीं है.
ओंग कहते हैं कि लिखने से मानव के सोचने का तरीका बदल जाता है. शब्दों के जो आज अर्थ हैं, पहले कुछ और अर्थ थे. बोले जाने वाली भाषा में जब नये अर्थ बनते थे, तो पुराने अर्थ धीरे धीरे गुम हो जाते थे. लेकिन जब से लिखाई का आविष्कार हुआ, शब्दों के पुराने अर्थ गुम नहीं होते, उन्हें खोजा जा सकता है. इसीलिए उनका कहना है कि पुरानी किताबों को पढ़ें तो उनका अर्थ समझने के लिए आज की भाषा का प्रयोग करना उचित नहीं. मैंने भी एक बार पढ़ा था कि ऋगवेद में वर्णित अश्वमेध, घोड़ों के वध की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि उस समय अश्व का अर्थ कुछ और भी था.
ओंग कहते हैं कि बोलने वाली भाषा में रची कविताओ़, कथाओं, काव्यों में एक ही बात को कई बार दोहराया जाता है, विभिन्न तरीके से कहा जाता है, मुहावरों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इससे सुनने वालों को समझने में और याद रखने में आसानी होती है. इसी तरह से बोलने वाली भाषा के बारे में ही प्राचीन ग्रीस में भाषण देने की कला के नियम बनाये गये थे. बोलने वाले को इतना कुछ याद रखना होता है, जिससे उसकी सोच और तर्क का विकास भी सीमित रहता है. गीत, कविता में बार बार कुछ पंक्तियों को दोहराना, शब्दों की ताल, धुन खोजना, यह बोलने वाली भाषा के लिए ज़रूरी है. बोलने वाली भाषा में अमूर्त विचारों और तर्कों का गहन विशलेषण करना कठिन है, बात गहरी या जटिल भी हों तो उन्हे सरलता से ही कहना होता है, वरना लोग समझ नहीं पाते.
जबकि लिखने से मानव सोच को याद रखने की आवश्यकता नहीं, जरुरत पढ़ने पर दोबारा पढ़ा जा सकता है. इससे दिमाग को स्मृति पर ज़ोर नहीं देना पड़ता और वह अन्य दिशाओं मे विकसित हो सकता है. इसलिए विचार और तर्क अधिक जटिल तरीके से विकसित किये जा सकते हैं, कविताओं, कहानियों को भी दोहराव नहीं चाहिये, जिस दिशा में चाहे, विकसित हो सकती हैं और लेखक के लिखने का तरीका बदल जाता है. ओंग के अनुसार, इसी वजह से लिखने पढ़ने वाला मानव दिमाग विज्ञान और तकनीकी तरक्की कर पाया.
मेरे विचार में प्राचीन भारत में संस्कृत लिखी जाने वाली भाषा थी, हालाँकि अधिकाँश जनता संस्कृत लिखना, पढ़ना, बोलना नहीं जानती थी. दूसरी ओर हिंदी भाषा का विकास बोलने वाली भाषा की तरह हुआ. पिछले कुछ सौ सालों को छोड़ दिया जाये तो भारत के अधिकाँश लोगों के लिए हिंदी केवल बोलने वाली बोली थी, लिखने वाली नहीं. जब भारत स्वतंत्र हुआ तब भी पढ़ने लिखने वाले लोग भारत की जनसंख्या का छोटा सा हिस्सा थे. जब उसे लिखने लगे तो उससे उसके स्वरों तथा शब्दों में कुछ बदलाव आये. भाषा के लिखने से आने वाले अधिकतर बदलाव पिछले कुछ दशकों में ही आये हैं, जब भारत की अधिकाँश जनसंख्या शिक्षित होने लगी है, और लोग किताब पत्रिका पढ़ने लगे हैं. लेकिन क्या इस वजह से भारत के अधिकाँश लोगों के सोचने का तरीका अभी भी बोलने वाली भाषा पर टिका है, लिखी भाषा पर नहीं? और समय के साथ जैसे जैसे साक्षरता बढ़ेगी, भारतीय मानस के सोचने का तरीका इस बात से बदल जायेगा?
पिछले कुछ समय में, टीवी और टेलीफ़ोन के विकास से, बोलने और सुनने की संस्कृति बढ़ रही है, पढ़ने की कम हो रही है. दूसरी ओर, अवधी, मैथिली, भोजपुरी, जैसी भाषाएँ जो भूली जा रहीं थीं, लेकिन इंटरनेट की वजह से आज उन्हें भी नया जीवन मिल सकता है.
इन सब बदलावों के क्या अर्थ हैं, क्या प्रभाव पड़ेगा हमारी भाषा पर, उसके विकास पर? क्या रोमन लिपि में लिखी हिंदी कमज़ोर हो कर मर जायेगी, या रूप बदल लेगी? आप का क्या विचार है?

इन्हीं बातों के अनुभव से सोच रहा था कि क्या धीरे धीरे हमारी हिंदी के कुछ स्वर जो अन्य भाषाओं में नहीं होते, लुप्त हो जायेंगे?
वैसे तो एशिया में अन्य कई देश हैं, जैसे इंदोनेशिया, फिलिपीन, वियतनाम, जहाँ पर उनकी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है, पर इससे उनकी भाषा ने अपने विषेश स्वर नहीं खोये. इसका एक कारण यह है कि इन देशों में आम जनता में अँग्रेज़ी बोलने वाले बहुत कम हैं, और वर्षों पहले जब इन्होंने रोमन लिपि को अपनाने का निश्चय किया तो उस समय रोमन लिपि की वर्णमाला की कमियों को पूरा करने के लिए एक्सेंट वाले वर्णों को लेटिन वर्णमाला से ले कर जोड़ लिया जिनका प्रयोग अन्य यूरोपीय भाषाओं में होता है जैसे कि à á â ã ä å. इस तरह उन्हें अपनी भाषा के विषेश स्वरों को लिखने के अन्य वर्ण मिल गये.
उदाहरण के लिए D Ð Ď d जैसे वर्णों से आप वियतनामी भाषा में द, ड, ड़, ध जैसे विभिन्न स्वरों को अलग अलग वर्ण दे सकते हैं, इसलिए जब वह रोमन लिपि में लिखते हैं तो भी अपनी भाषाओं के विषेश स्वरों के उच्चारण को संभाल कर रखते हैं. पर हिंदी या अन्य भारतीय भाषाओं के साथ ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे उनकी बोली और विषेश स्वरों का रोमनीकरण न हो?
भाषा एक जैसी नहीं रहती, समय के साथ बदलती रहती है. वेदों, पुराणों, बाइबल, कुरान और अन्य प्राचीन ग्रंथों को भाषाविज्ञानी जाँच कर बता सकते हें कि कौन सा हिस्सा पहले लिखा गया, कौन सा बाद में जोड़ा गया.
भाषा समय के साथ क्यों बदलती है? इसकी एक वजह तो नये आविष्कार है, जिनके लिए नये शब्दों की ज़रूरत पड़ती है. जैसे कम्प्यूटर, ईमेल, इंटरनेट जो पहले नहीं थे, और इनसे जुड़ी बहुत से बातों के शब्द नये बने हैं. समय के साथ कुछ वस्तुओं का उपयोग कम या बंद हो जाता है, जैसे लालटेन, बैलगाड़ी आदि और इनके शब्द धीरे धीरे समय के साथ खो जाते हैं. जब छोटा था तो गुसलखाने में झाँवा होता था पाँव साफ़ करने के लिए लेकिन जब पिछली बार दिल्ली गया और छोटी बहन से पूछा कि क्या उसके घर में झाँवा मिलेगा तो वह हँसने लगी, बोली कितने सालों के बाद यह शब्द सुना है.
विद्वानों का कहना है कि भाषा के विकास का सम्बंध उसकी लिखायी से भी हैं.
बोलने वाली भाषा और लिखने वाली भाषा के बीच में क्या सम्बंध होता है इस विषय पर वाल्टर जे ओंग (Walter J. Ong) ने बहुत शौध किया है और लिखा है. उनकी 1982 की किताब ओराल्टी एँड लिट्रेसी (Orality and Literacy) जो इसी विषय पर है, मुझे बहुत अच्छी लगी. उनका कहना है कि मानव बोली का विकास तीस से पचास हज़ार साल पहले हुआ जबकि लिखाई का आविष्कार केवल छः हज़ार साल पहले हुआ. इस तरह से मानव भाषाएँ बोली के साथ विकसित हुईं. दुनिया की हज़ारों भाषाओं में से केवल 106 में लिखित साहित्य की रचना हुई. आज भी कई सौ ऐसी बोली जाने वाली भाषाएँ हैं जिनकी कोई लिपि नहीं है.
ओंग कहते हैं कि लिखने से मानव के सोचने का तरीका बदल जाता है. शब्दों के जो आज अर्थ हैं, पहले कुछ और अर्थ थे. बोले जाने वाली भाषा में जब नये अर्थ बनते थे, तो पुराने अर्थ धीरे धीरे गुम हो जाते थे. लेकिन जब से लिखाई का आविष्कार हुआ, शब्दों के पुराने अर्थ गुम नहीं होते, उन्हें खोजा जा सकता है. इसीलिए उनका कहना है कि पुरानी किताबों को पढ़ें तो उनका अर्थ समझने के लिए आज की भाषा का प्रयोग करना उचित नहीं. मैंने भी एक बार पढ़ा था कि ऋगवेद में वर्णित अश्वमेध, घोड़ों के वध की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि उस समय अश्व का अर्थ कुछ और भी था.
ओंग कहते हैं कि बोलने वाली भाषा में रची कविताओ़, कथाओं, काव्यों में एक ही बात को कई बार दोहराया जाता है, विभिन्न तरीके से कहा जाता है, मुहावरों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इससे सुनने वालों को समझने में और याद रखने में आसानी होती है. इसी तरह से बोलने वाली भाषा के बारे में ही प्राचीन ग्रीस में भाषण देने की कला के नियम बनाये गये थे. बोलने वाले को इतना कुछ याद रखना होता है, जिससे उसकी सोच और तर्क का विकास भी सीमित रहता है. गीत, कविता में बार बार कुछ पंक्तियों को दोहराना, शब्दों की ताल, धुन खोजना, यह बोलने वाली भाषा के लिए ज़रूरी है. बोलने वाली भाषा में अमूर्त विचारों और तर्कों का गहन विशलेषण करना कठिन है, बात गहरी या जटिल भी हों तो उन्हे सरलता से ही कहना होता है, वरना लोग समझ नहीं पाते.
जबकि लिखने से मानव सोच को याद रखने की आवश्यकता नहीं, जरुरत पढ़ने पर दोबारा पढ़ा जा सकता है. इससे दिमाग को स्मृति पर ज़ोर नहीं देना पड़ता और वह अन्य दिशाओं मे विकसित हो सकता है. इसलिए विचार और तर्क अधिक जटिल तरीके से विकसित किये जा सकते हैं, कविताओं, कहानियों को भी दोहराव नहीं चाहिये, जिस दिशा में चाहे, विकसित हो सकती हैं और लेखक के लिखने का तरीका बदल जाता है. ओंग के अनुसार, इसी वजह से लिखने पढ़ने वाला मानव दिमाग विज्ञान और तकनीकी तरक्की कर पाया.
मेरे विचार में प्राचीन भारत में संस्कृत लिखी जाने वाली भाषा थी, हालाँकि अधिकाँश जनता संस्कृत लिखना, पढ़ना, बोलना नहीं जानती थी. दूसरी ओर हिंदी भाषा का विकास बोलने वाली भाषा की तरह हुआ. पिछले कुछ सौ सालों को छोड़ दिया जाये तो भारत के अधिकाँश लोगों के लिए हिंदी केवल बोलने वाली बोली थी, लिखने वाली नहीं. जब भारत स्वतंत्र हुआ तब भी पढ़ने लिखने वाले लोग भारत की जनसंख्या का छोटा सा हिस्सा थे. जब उसे लिखने लगे तो उससे उसके स्वरों तथा शब्दों में कुछ बदलाव आये. भाषा के लिखने से आने वाले अधिकतर बदलाव पिछले कुछ दशकों में ही आये हैं, जब भारत की अधिकाँश जनसंख्या शिक्षित होने लगी है, और लोग किताब पत्रिका पढ़ने लगे हैं. लेकिन क्या इस वजह से भारत के अधिकाँश लोगों के सोचने का तरीका अभी भी बोलने वाली भाषा पर टिका है, लिखी भाषा पर नहीं? और समय के साथ जैसे जैसे साक्षरता बढ़ेगी, भारतीय मानस के सोचने का तरीका इस बात से बदल जायेगा?
पिछले कुछ समय में, टीवी और टेलीफ़ोन के विकास से, बोलने और सुनने की संस्कृति बढ़ रही है, पढ़ने की कम हो रही है. दूसरी ओर, अवधी, मैथिली, भोजपुरी, जैसी भाषाएँ जो भूली जा रहीं थीं, लेकिन इंटरनेट की वजह से आज उन्हें भी नया जीवन मिल सकता है.
इन सब बदलावों के क्या अर्थ हैं, क्या प्रभाव पड़ेगा हमारी भाषा पर, उसके विकास पर? क्या रोमन लिपि में लिखी हिंदी कमज़ोर हो कर मर जायेगी, या रूप बदल लेगी? आप का क्या विचार है?
शनिवार, जुलाई 17, 2010
कोमिक्स साहित्य
बचपन में बेताल की कोम्किस पढ़ना मुझे वहुत अच्छा लगता था. तब इंद्रजाल कोमिक्स के नाम से यह पत्रिकाएँ आती थीं. कुछ साल बाद जब अंग्रेज़ी बोलने समझने की क्षमता बढ़ी तो आर्ची, जगहेड, सुपरमैन, स्पाईडरमैन जैसी कोमिक्स कुछ दिन पढ़ीं पर उनमें मेरी कोई विषेश दिलचस्पी नहीं बनी, और धीरे धीरे मेरा कोमिक्स पढ़ना बंद हो गया. तब लगता कि इस तरह की कोमिक्स की किताबें या पत्रिकाएँ केवल बच्चों के पढ़ने के लिए होती हैं.
इटली में आये तो पहले जापानी चित्रकथाओं से परिचय हुआ, जब मेरा बेटा इनका दीवाना था. उस समय जापानी कामिक्स "मैंगा" (Manga) और जापानी कार्टून फिल्मों "एनीम" (Anime) से परिचय हुआ. बहुत साल के बाद अमर चित्र कथा का नाम सुनाई देने लगा, जिसमें पंचतंत्र, रामायण और महाभारत की कहानियाँ प्रस्तुत की जाती थीं. उस समय विदेशों में इनका प्रसार करते समय कहा जाता कि वे भारत से दूर पैदा हुए भारतीय मूल के बच्चों को भारत की संस्कृति के बारे में बताने का यह अच्छा तरीका है, कि चित्रकथाओं के माध्यम से बच्चे धर्म, परम्पराओं के बारे में भी जानेंगे और साथ ही हिंदी का अभ्यास भी हो जायेगा.
तभी यह बात भी मन में आयी कि शायद इन्हें कामिक्स कहना ठीक नहीं था, क्योंकि कामिक्स का अर्थ है "हँसी मज़ाक", जबकि इनमें तो रहस्य, रोमांच से ले कर प्रेम कथा तक विभिन्न तरह की पत्रिकाए मिलती हैं. इसी तरह से कार्टून शब्द का अर्थ शुरु में तो शायद हाथ से बनी आकृतियों से जुड़ा था लेकिन आज यह भी "हँसी मज़ाक" या "व्यंग" से जुड़ा है, जबकि इस तरह की फ़िल्मों में खेल कूद, प्रेम कथा, एक्शन, सभी कुछ होता है. ओस्कर पुरस्कार पाने वाली फ़िल्म "डांस विद बशीर" (Dance with Bashir), जिसमें फिलिस्तीनियों के शरणार्थी कैंम्प में नरसंहार की कहानी है, या फ़िर ईरानी लेखिका मरजान की "पेरसोपोलिस" (Persepolis), उन्हें कार्टून फ़िल्म कहना अज़ीब सा लगता है, और "एनिमेटिड फ़िल्म" (animated film) कहना अधिक ठीक लगता है, "एनिमेटिड" यानि यानि "कत्रिम जान डाले हुए पात्र".
जैसे जैसे इस दुनिया से अधिक जानकारी हुई, तो अपनी इस सोच को बदलना पड़ा पड़ा कि इस तरह की चित्रकथाएँ केवल बच्चों के लिए होती हैं. बल्कि कुछ चित्रकथाएँ तो केवल व्यस्कों के लिए बनायी जाती हैं. जिन्होंने इंटरनेट पर "सविता भाभी" की चित्रकथाएँ देखी हैं वह यह जानते हैं कि इस तरह की सेक्स से जुड़ी चित्रकथाएँ हिंदी में भी उपलब्ध हैं. मुझे नहीं मालूम कि हिंदी में सेक्स की बात न भी की जाये, तो क्या बड़े लोगों के लिए विषेश रूप से कहानियाँ या किताबें बनती हैं? शायद "ग्राफ़िक उपन्यास" के रूप में बनती हैं? यह तो भारत में रहने वाला कोई जागरूक पाठक ही बता सकता है.
हमारे शहर बोलोनिया में हर वर्ष बिलबोलबुल नाम से चित्रकथा लिखने, बनाने वालों की प्रदर्शनी और ट्रेडफेयर लगते हैं जो यूरोप में इस तरह का सबसे बड़ा मेला है. पिछले वर्ष, इस प्रदर्शनी में बहुत से अफ़्रीकी कलाकार और लेखक आये थे. युद्ध में बच्चों को सैनिक बनाने से ले कर औरतों पर होने वाले अत्याचारों की बातें थीं, विषयों की विविधता थी. कला की दृष्टि से, ग्रफ़िक्स की दृष्टि से, विषय और लेखन की दृष्टि से, हर तरह से लगा कि यह सचमुच साहित्य की विधा है, इसे केवल बच्चों की कहानियाँ सोचना ठीक नहीं. (नीचे की तस्वीर में शराब के नशे में हिंसा और बलात्कार की बात करने वाली एक अफ्रीकी चित्रकथा)
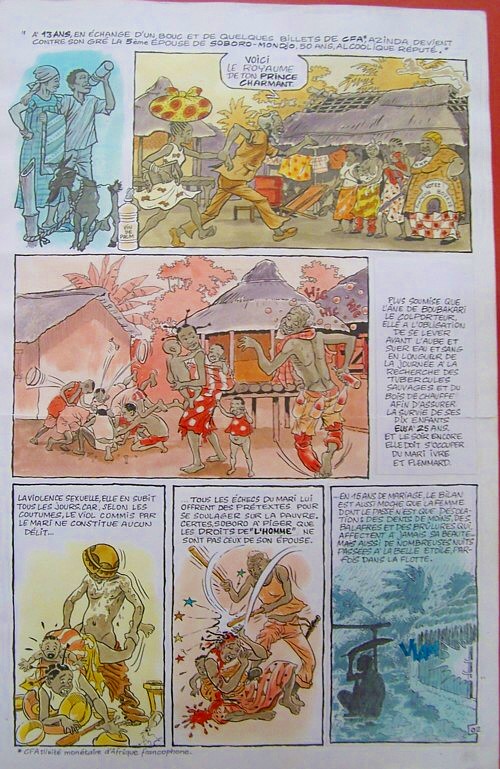
इटली में सभी पुस्कालयों और किताबों की दुकानों में चित्रकथाओं की किताबों का अलग से हिस्सा होता है. इतालवी भाषा में इन्हें फूमेत्तो कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है, छोटा सा धूँए का बादल और इस शब्द का मूल उन बादल जैसे बुलबुलों में है जिनमें इन किताबों के पात्रों की बातें लिखी होती हैं. फूमेत्तो के कलाकारों और लेखकों को इतालवी साहित्य जगत में बहुत मान मिलता है, शायद इसलिए भी कि इन किताबों की बिक्री बहुत है और इन्हें लिखने बनाने वालों को पैसा अच्छा मिलता है. इन पर फ़िल्में भी बनती हैं. कुछ लोग अपनी किताबों की कहानी भी लिखते हैं और वही उनके साथ के चित्र भी बनाते हैं, लेकिन अधिकतर, लेखक और चित्र बनाने वाले लोग भिन्न होते हैं.
चित्रकथाओं की दुनिया में जापान का स्थान सबसे आगे है, जहाँ पर मैंगा और एनीम के दीवानों की संख्या लाखों में है, और जहाँ लिखी छपी किताबें विभिन्न भाषाओं में अनुवादित होती हैं, हालाँकि मुझे नहीं मालूम कि यह किताबें हिंदी में भी उपलब्ध हैं या नहीं. मैंगा बनाने और लिखने वाली एक सुप्रसिद्ध जापानी लेखिका कलाकार यहीं बोलोनिया में रहती हैं जिनका नाम है केईको इछिगूचि (Keiko Ichiguchi) जिनसे एक बार मिलने का मौखा मिला था.
जापानी चित्रकाथाओं से एक अन्य नया खेल ने जन्म लिया है जिसका नाम है कोसूपूरे (Kosupure) या कोज़प्ले (Cosplay) जिसमें नवयुवक और नवयुवतियाँ प्रसिद्ध चित्रकाथाओं तथा वीदियोंगेम के पात्रों जैसे वस्त्र पहनते हैं, मेकअप करते हैं जैसे कि आप नीचे की तस्वीर में देख सकते हैं. कोज़प्ले के दीवाने प्रतियोगिताओं का आयाजोन करते हैं, अपने मनचाहे पात्रों जैसा बनने के लिए पैसा और समय दोनो ही लगाते हैं.

अगर आप को मौका मिले अपने मनपसंद कोमिक हीरो या हीरोईन के भेस बनाने का, तो आप क्या बनना चाहेंगे? अमरीकी कोमिक वाले सुपरमैन या वंडरवूमन? अमर चित्रकथा से राम या कृष्ण? किसी जापानी मैंगा पर आधारित पात्र? मुझे स्वयं जापानी मैंगा की तरह रंगबिरंगे बालों वाला हीरो बनना अच्छा लगेगा, लेकिन शीशे में अपने शरीर का आकार देखूँ तो लगता है कि सूमों की कुश्ती वाला रोल ही मेरे लिए ठीक रहेगा
इटली में आये तो पहले जापानी चित्रकथाओं से परिचय हुआ, जब मेरा बेटा इनका दीवाना था. उस समय जापानी कामिक्स "मैंगा" (Manga) और जापानी कार्टून फिल्मों "एनीम" (Anime) से परिचय हुआ. बहुत साल के बाद अमर चित्र कथा का नाम सुनाई देने लगा, जिसमें पंचतंत्र, रामायण और महाभारत की कहानियाँ प्रस्तुत की जाती थीं. उस समय विदेशों में इनका प्रसार करते समय कहा जाता कि वे भारत से दूर पैदा हुए भारतीय मूल के बच्चों को भारत की संस्कृति के बारे में बताने का यह अच्छा तरीका है, कि चित्रकथाओं के माध्यम से बच्चे धर्म, परम्पराओं के बारे में भी जानेंगे और साथ ही हिंदी का अभ्यास भी हो जायेगा.
तभी यह बात भी मन में आयी कि शायद इन्हें कामिक्स कहना ठीक नहीं था, क्योंकि कामिक्स का अर्थ है "हँसी मज़ाक", जबकि इनमें तो रहस्य, रोमांच से ले कर प्रेम कथा तक विभिन्न तरह की पत्रिकाए मिलती हैं. इसी तरह से कार्टून शब्द का अर्थ शुरु में तो शायद हाथ से बनी आकृतियों से जुड़ा था लेकिन आज यह भी "हँसी मज़ाक" या "व्यंग" से जुड़ा है, जबकि इस तरह की फ़िल्मों में खेल कूद, प्रेम कथा, एक्शन, सभी कुछ होता है. ओस्कर पुरस्कार पाने वाली फ़िल्म "डांस विद बशीर" (Dance with Bashir), जिसमें फिलिस्तीनियों के शरणार्थी कैंम्प में नरसंहार की कहानी है, या फ़िर ईरानी लेखिका मरजान की "पेरसोपोलिस" (Persepolis), उन्हें कार्टून फ़िल्म कहना अज़ीब सा लगता है, और "एनिमेटिड फ़िल्म" (animated film) कहना अधिक ठीक लगता है, "एनिमेटिड" यानि यानि "कत्रिम जान डाले हुए पात्र".
जैसे जैसे इस दुनिया से अधिक जानकारी हुई, तो अपनी इस सोच को बदलना पड़ा पड़ा कि इस तरह की चित्रकथाएँ केवल बच्चों के लिए होती हैं. बल्कि कुछ चित्रकथाएँ तो केवल व्यस्कों के लिए बनायी जाती हैं. जिन्होंने इंटरनेट पर "सविता भाभी" की चित्रकथाएँ देखी हैं वह यह जानते हैं कि इस तरह की सेक्स से जुड़ी चित्रकथाएँ हिंदी में भी उपलब्ध हैं. मुझे नहीं मालूम कि हिंदी में सेक्स की बात न भी की जाये, तो क्या बड़े लोगों के लिए विषेश रूप से कहानियाँ या किताबें बनती हैं? शायद "ग्राफ़िक उपन्यास" के रूप में बनती हैं? यह तो भारत में रहने वाला कोई जागरूक पाठक ही बता सकता है.
हमारे शहर बोलोनिया में हर वर्ष बिलबोलबुल नाम से चित्रकथा लिखने, बनाने वालों की प्रदर्शनी और ट्रेडफेयर लगते हैं जो यूरोप में इस तरह का सबसे बड़ा मेला है. पिछले वर्ष, इस प्रदर्शनी में बहुत से अफ़्रीकी कलाकार और लेखक आये थे. युद्ध में बच्चों को सैनिक बनाने से ले कर औरतों पर होने वाले अत्याचारों की बातें थीं, विषयों की विविधता थी. कला की दृष्टि से, ग्रफ़िक्स की दृष्टि से, विषय और लेखन की दृष्टि से, हर तरह से लगा कि यह सचमुच साहित्य की विधा है, इसे केवल बच्चों की कहानियाँ सोचना ठीक नहीं. (नीचे की तस्वीर में शराब के नशे में हिंसा और बलात्कार की बात करने वाली एक अफ्रीकी चित्रकथा)
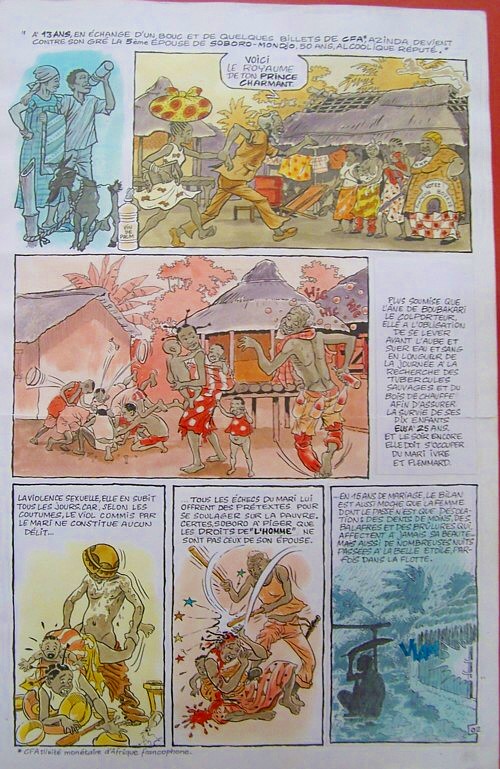
इटली में सभी पुस्कालयों और किताबों की दुकानों में चित्रकथाओं की किताबों का अलग से हिस्सा होता है. इतालवी भाषा में इन्हें फूमेत्तो कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है, छोटा सा धूँए का बादल और इस शब्द का मूल उन बादल जैसे बुलबुलों में है जिनमें इन किताबों के पात्रों की बातें लिखी होती हैं. फूमेत्तो के कलाकारों और लेखकों को इतालवी साहित्य जगत में बहुत मान मिलता है, शायद इसलिए भी कि इन किताबों की बिक्री बहुत है और इन्हें लिखने बनाने वालों को पैसा अच्छा मिलता है. इन पर फ़िल्में भी बनती हैं. कुछ लोग अपनी किताबों की कहानी भी लिखते हैं और वही उनके साथ के चित्र भी बनाते हैं, लेकिन अधिकतर, लेखक और चित्र बनाने वाले लोग भिन्न होते हैं.
चित्रकथाओं की दुनिया में जापान का स्थान सबसे आगे है, जहाँ पर मैंगा और एनीम के दीवानों की संख्या लाखों में है, और जहाँ लिखी छपी किताबें विभिन्न भाषाओं में अनुवादित होती हैं, हालाँकि मुझे नहीं मालूम कि यह किताबें हिंदी में भी उपलब्ध हैं या नहीं. मैंगा बनाने और लिखने वाली एक सुप्रसिद्ध जापानी लेखिका कलाकार यहीं बोलोनिया में रहती हैं जिनका नाम है केईको इछिगूचि (Keiko Ichiguchi) जिनसे एक बार मिलने का मौखा मिला था.
जापानी चित्रकाथाओं से एक अन्य नया खेल ने जन्म लिया है जिसका नाम है कोसूपूरे (Kosupure) या कोज़प्ले (Cosplay) जिसमें नवयुवक और नवयुवतियाँ प्रसिद्ध चित्रकाथाओं तथा वीदियोंगेम के पात्रों जैसे वस्त्र पहनते हैं, मेकअप करते हैं जैसे कि आप नीचे की तस्वीर में देख सकते हैं. कोज़प्ले के दीवाने प्रतियोगिताओं का आयाजोन करते हैं, अपने मनचाहे पात्रों जैसा बनने के लिए पैसा और समय दोनो ही लगाते हैं.

(यह तस्वीर feer.wsj.com से)
अगर आप को मौका मिले अपने मनपसंद कोमिक हीरो या हीरोईन के भेस बनाने का, तो आप क्या बनना चाहेंगे? अमरीकी कोमिक वाले सुपरमैन या वंडरवूमन? अमर चित्रकथा से राम या कृष्ण? किसी जापानी मैंगा पर आधारित पात्र? मुझे स्वयं जापानी मैंगा की तरह रंगबिरंगे बालों वाला हीरो बनना अच्छा लगेगा, लेकिन शीशे में अपने शरीर का आकार देखूँ तो लगता है कि सूमों की कुश्ती वाला रोल ही मेरे लिए ठीक रहेगा
शुक्रवार, जुलाई 09, 2010
पिँजरे के पंछी
अमरीकी महाद्वीप के बहुत से हिस्सों में इतिहास बस कुछ सौ साल पुराना ही दिखता है, उससे पहले का इतिहास, कोलोम्बस के बाद आये यूरोपीय उपनिपेश से मिट कर, दब कर, कहीं गुम हो चुका है.
"यह भवन शहर के सबसे प्राचीन भवनों में से है", हमारी साथी और गाईड तानिया ने बताया था. ऊँची दीवारें और काले रंग से पुते ऊँचे गेट के पीछे से भवन दिख नहीं रहा था. गेट पर बड़ा भारी सा ताला लगा था. उसे खोला गया और गाड़ी भीतर गयी, तो सामने वैसा ही एक अन्य गेट था, जिसे खोलने से पहले, पहले वाला गेट बंद किया गया, उस पर ताला लगाया गया.
"मिल्ट्री वालों की बटालियन वहाँ तैनात रहती है, उन्हें अस्पताल में अंदर आना मना है", तानिया ने एक कोने में बंदूक ले कर खड़े सिपाहियों की ओर इशारा कर के कहा. हरी भरी घास से घिरा, वह पुराना भवन सुंदर लग रहा था. घास पर इधर उधर पीले वस्त्रों में बहुत से पुरुष थे, एक ओर पीले रंग की मेज़ और कुर्सियाँ थीं, जिन पर और पीले वस्त्र पहने पुरुष बैठे थे. लगा कि कोई बसंत मेला लगा हो. "यहाँ किसी व्यक्ति की तस्वीर नहीं खींच सकते", तानिया ने मुझे कैमरा बाहर निकालते देख कर कहा तो मैंने कैमरा वापस बैग में रख लिया. हर तरफ़ तो आदमी थे, बिना उनके कैसे तस्वीर खींचता?
"स्वागत है, आईये" कहते कहते, अस्पताल के अध्यक्ष डा. पाउलो हमें लेने आ गये. उन्होंने ही अस्पताल के बारे में बताया कि यह मानसिक रोग वाले अपराधियों के लिए अस्पताल भी है और जेल भी, जहाँ सौ से कुछ अधिक मानसिक रोगी रहते हैं जिनमे से अधिकतर पुरुष हैं. डा. पाउलो के साथ अस्पताल के विभिन्न भागों में निरीक्षण के लिए गये. जैसे मानसिक रोग के अस्पतालों में अक्सर होता है, हर तरफ़ गेट और ताले लगे थे, कहीं से भी घुसते या निकलते तो गार्ड हमारे लिए ताला खोलता और पीछे से तुरंत ही बंद कर देता. अस्पताल के वार्डों में हर जगह, नर्स और डाक्टर भी, तालों के पीछे अपने कमरों में जेल की तरह ही बंद थे, तभी बाहर आते थे, जब कुछ काम हो.
मैं कहीं कुछ रुक कर देखने लगा तो घबरायी हुई तानिया मेरे पास आयी, बोली "तुम सब लोगों के साथ झुँड में ही रहो, पीछे रुक कर अकेले पड़ने में खतरा है." तो मुझे कुछ हँसी आयी. मैंने पहले भी बहुत से मानसिक रोग के अस्पताल देखें हैं, जहाँ असमान्य व्यवहार करने वाले लोग अक्सर दिखते हैं लेकिन वे लोग किसी तरह से खतरनाक नहीं होते. भारत में तो कई बार बेघर लोगों को, मानसिक रोगियों तथा कुष्ठ रोगियों को भी इसी तरह जेल में बंद कर देते हैं, और गरीब अनपढ़ लोग बिना किसी जुर्म के सुनवाई के इंतज़ार में जेल काट देते हैं. वह बोली कि यह विचार आम मानसिक अस्पतालों के बारे में सही था लेकिन इस अस्पताल+जेल में रहने वाले केवल रोगी ही नहीं अपराधी भी हैं और आम मानसिक रोगियों से भिन्न हैं, अधिक खतरनाक हैं.
वहाँ पर जहाँ एक ओर सचमुच के अपराधी थे, कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका यही अपराध था कि वह मानसिक रोगी थे. डा. पाउलो ने बताया कि जब इस तरह के व्यक्ति को पुलिस वहाँ ले आती है, तो भी उस व्यक्ति को छोड़ नहीं सकते, उसे पहली सुनवाई का इंतज़ार करना पड़ता है जब मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को निर्दोष कह कर जेल से जाने की अनुमति दे सकता है, और इसमें कुछ महीने लग जाते हैं. अन्य देशों के मुकाबले में मुझे लगा कि ब्राज़ील की इस जेल+अस्पताल में डाक्टरों और नर्सों का व्यवहार अच्छा है, काम करने में मानसिक रोगियों के मानव अधिकारों की भी कुछ संचेतना है.
अस्पताल में घूमते हुए अंत में महिला विभाग में पहुँचे. गेट के पास ही एक गर्भवती महिला खड़ी थी. पाउलो ने बताया कि वह सुनवाई का इंतज़ार कर रही थी, उसने कोई अपराध नहीं किया था, और शायद उसका गर्भ भी बलात्कार का नतीजा था. मानसिक रोग वाली युवतियों के साथ अक्सर बलात्कार होते हैं, कई बार तो अस्पतालों में भी और जेलों में भी.
पीछे एक कोने में बाल बिखेरे उदास मुख वाली एक वृद्ध सी महिला बैठी थीं. इन्होंने क्या किया, मैंने जिज्ञासा से पूछा. "दो सप्ताह पहले आयी थी, तो इनकी बीमारी दूसरे चर्म पर थी", पाउलो ने बताया, "ज़ोर ज़ोर से गाना गा रही थी, चिल्ला रही थी, हँस रही थी. इसने अपने पति को उसका गला दबा कर उसे मार डाला और फ़िर घर को आग लगाने की कोशिश की."
"क्या मालूम बेचारी पर क्या बीती होगी, शायद इसका पति शराबी था, या घर में मारपीट करता था?", मैंने उस वृद्ध महिला के भोले भाले उदास चेहरे को देख कर कहा, तो पाउलो ने मुस्करा कर सिर हिला दिया, "नहीं सब कहते हैं कि वह बहुत अच्छा था, कई सालों से यह बीमार चल रही थी और वह पत्नी की देखभाल करता था. यह बात तो है कि अगर पुरुष हिंसा करता है तो सब लोग उसे तुरंत दोषी मान लेते हैं, स्त्री करती है तो पहला विचार यही आता है कि मजबूर हो कर किया होगा. पर यह बात भी है कि यहाँ हिंसा का अपराध करने वाले करीब पचास पुरुष कैदी हैं, जबकि हिंसा करने वाली स्त्री यहाँ बस एक ही है."
जनाना वार्ड में खिड़की के बाहर सलेटी और काले रंग की चिरईया को देखा तो मन में बिमल राय की फ़िल्म बंदिनी की याद आ गयी. फ़िल्म में जेल में बंद कैदी स्त्रियाँ पिंजरे में बंद पक्षी को देख कर गाना गाती हैं, "ओ पंछी प्यारे, सांझ सखारे, बोले तो कौन सी बोली बता रे, बोले तू कौन सी बोली".

निरीक्षण स्माप्त हुआ और बाहर आने लगे तो पाउलो ने कहा, "आज मानसिक रोगो का इलाज करना बहुत सरल हो गया है, नयी दवाएँ असरकारी होती हैं, पुराने इलाज जैसे बिजली के शाक देना आदि को अब ठीक नहीं माना जाता. पर आम लोगों में इन रोगियों के बारे में बहुत डर भी होते हैं और अंधविश्वास भी. यहाँ लाये जाने वाले लोगों में से करीब बीस पच्चीस प्रतिशत लोगों ने कोई अपराध नहीं किया होता, अन्य कई छोटे मोटे अपराध करने वाले भी इसी लिए यहाँ ले आते हें कि वह रोगी हैं."
उस अस्पताल के बारे में सोचूँ तो मन में खुशनुमा पीले कपड़े पहने हुए उदास चेहरे वाले कैदी याद आते हैं. और उस वृद्धा का उदास चेहरा दिखता है, जाने क्या सोच रही थी वह?
"यह भवन शहर के सबसे प्राचीन भवनों में से है", हमारी साथी और गाईड तानिया ने बताया था. ऊँची दीवारें और काले रंग से पुते ऊँचे गेट के पीछे से भवन दिख नहीं रहा था. गेट पर बड़ा भारी सा ताला लगा था. उसे खोला गया और गाड़ी भीतर गयी, तो सामने वैसा ही एक अन्य गेट था, जिसे खोलने से पहले, पहले वाला गेट बंद किया गया, उस पर ताला लगाया गया.
"मिल्ट्री वालों की बटालियन वहाँ तैनात रहती है, उन्हें अस्पताल में अंदर आना मना है", तानिया ने एक कोने में बंदूक ले कर खड़े सिपाहियों की ओर इशारा कर के कहा. हरी भरी घास से घिरा, वह पुराना भवन सुंदर लग रहा था. घास पर इधर उधर पीले वस्त्रों में बहुत से पुरुष थे, एक ओर पीले रंग की मेज़ और कुर्सियाँ थीं, जिन पर और पीले वस्त्र पहने पुरुष बैठे थे. लगा कि कोई बसंत मेला लगा हो. "यहाँ किसी व्यक्ति की तस्वीर नहीं खींच सकते", तानिया ने मुझे कैमरा बाहर निकालते देख कर कहा तो मैंने कैमरा वापस बैग में रख लिया. हर तरफ़ तो आदमी थे, बिना उनके कैसे तस्वीर खींचता?
"स्वागत है, आईये" कहते कहते, अस्पताल के अध्यक्ष डा. पाउलो हमें लेने आ गये. उन्होंने ही अस्पताल के बारे में बताया कि यह मानसिक रोग वाले अपराधियों के लिए अस्पताल भी है और जेल भी, जहाँ सौ से कुछ अधिक मानसिक रोगी रहते हैं जिनमे से अधिकतर पुरुष हैं. डा. पाउलो के साथ अस्पताल के विभिन्न भागों में निरीक्षण के लिए गये. जैसे मानसिक रोग के अस्पतालों में अक्सर होता है, हर तरफ़ गेट और ताले लगे थे, कहीं से भी घुसते या निकलते तो गार्ड हमारे लिए ताला खोलता और पीछे से तुरंत ही बंद कर देता. अस्पताल के वार्डों में हर जगह, नर्स और डाक्टर भी, तालों के पीछे अपने कमरों में जेल की तरह ही बंद थे, तभी बाहर आते थे, जब कुछ काम हो.
मैं कहीं कुछ रुक कर देखने लगा तो घबरायी हुई तानिया मेरे पास आयी, बोली "तुम सब लोगों के साथ झुँड में ही रहो, पीछे रुक कर अकेले पड़ने में खतरा है." तो मुझे कुछ हँसी आयी. मैंने पहले भी बहुत से मानसिक रोग के अस्पताल देखें हैं, जहाँ असमान्य व्यवहार करने वाले लोग अक्सर दिखते हैं लेकिन वे लोग किसी तरह से खतरनाक नहीं होते. भारत में तो कई बार बेघर लोगों को, मानसिक रोगियों तथा कुष्ठ रोगियों को भी इसी तरह जेल में बंद कर देते हैं, और गरीब अनपढ़ लोग बिना किसी जुर्म के सुनवाई के इंतज़ार में जेल काट देते हैं. वह बोली कि यह विचार आम मानसिक अस्पतालों के बारे में सही था लेकिन इस अस्पताल+जेल में रहने वाले केवल रोगी ही नहीं अपराधी भी हैं और आम मानसिक रोगियों से भिन्न हैं, अधिक खतरनाक हैं.
वहाँ पर जहाँ एक ओर सचमुच के अपराधी थे, कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका यही अपराध था कि वह मानसिक रोगी थे. डा. पाउलो ने बताया कि जब इस तरह के व्यक्ति को पुलिस वहाँ ले आती है, तो भी उस व्यक्ति को छोड़ नहीं सकते, उसे पहली सुनवाई का इंतज़ार करना पड़ता है जब मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को निर्दोष कह कर जेल से जाने की अनुमति दे सकता है, और इसमें कुछ महीने लग जाते हैं. अन्य देशों के मुकाबले में मुझे लगा कि ब्राज़ील की इस जेल+अस्पताल में डाक्टरों और नर्सों का व्यवहार अच्छा है, काम करने में मानसिक रोगियों के मानव अधिकारों की भी कुछ संचेतना है.
अस्पताल में घूमते हुए अंत में महिला विभाग में पहुँचे. गेट के पास ही एक गर्भवती महिला खड़ी थी. पाउलो ने बताया कि वह सुनवाई का इंतज़ार कर रही थी, उसने कोई अपराध नहीं किया था, और शायद उसका गर्भ भी बलात्कार का नतीजा था. मानसिक रोग वाली युवतियों के साथ अक्सर बलात्कार होते हैं, कई बार तो अस्पतालों में भी और जेलों में भी.
पीछे एक कोने में बाल बिखेरे उदास मुख वाली एक वृद्ध सी महिला बैठी थीं. इन्होंने क्या किया, मैंने जिज्ञासा से पूछा. "दो सप्ताह पहले आयी थी, तो इनकी बीमारी दूसरे चर्म पर थी", पाउलो ने बताया, "ज़ोर ज़ोर से गाना गा रही थी, चिल्ला रही थी, हँस रही थी. इसने अपने पति को उसका गला दबा कर उसे मार डाला और फ़िर घर को आग लगाने की कोशिश की."
"क्या मालूम बेचारी पर क्या बीती होगी, शायद इसका पति शराबी था, या घर में मारपीट करता था?", मैंने उस वृद्ध महिला के भोले भाले उदास चेहरे को देख कर कहा, तो पाउलो ने मुस्करा कर सिर हिला दिया, "नहीं सब कहते हैं कि वह बहुत अच्छा था, कई सालों से यह बीमार चल रही थी और वह पत्नी की देखभाल करता था. यह बात तो है कि अगर पुरुष हिंसा करता है तो सब लोग उसे तुरंत दोषी मान लेते हैं, स्त्री करती है तो पहला विचार यही आता है कि मजबूर हो कर किया होगा. पर यह बात भी है कि यहाँ हिंसा का अपराध करने वाले करीब पचास पुरुष कैदी हैं, जबकि हिंसा करने वाली स्त्री यहाँ बस एक ही है."
जनाना वार्ड में खिड़की के बाहर सलेटी और काले रंग की चिरईया को देखा तो मन में बिमल राय की फ़िल्म बंदिनी की याद आ गयी. फ़िल्म में जेल में बंद कैदी स्त्रियाँ पिंजरे में बंद पक्षी को देख कर गाना गाती हैं, "ओ पंछी प्यारे, सांझ सखारे, बोले तो कौन सी बोली बता रे, बोले तू कौन सी बोली".

निरीक्षण स्माप्त हुआ और बाहर आने लगे तो पाउलो ने कहा, "आज मानसिक रोगो का इलाज करना बहुत सरल हो गया है, नयी दवाएँ असरकारी होती हैं, पुराने इलाज जैसे बिजली के शाक देना आदि को अब ठीक नहीं माना जाता. पर आम लोगों में इन रोगियों के बारे में बहुत डर भी होते हैं और अंधविश्वास भी. यहाँ लाये जाने वाले लोगों में से करीब बीस पच्चीस प्रतिशत लोगों ने कोई अपराध नहीं किया होता, अन्य कई छोटे मोटे अपराध करने वाले भी इसी लिए यहाँ ले आते हें कि वह रोगी हैं."
उस अस्पताल के बारे में सोचूँ तो मन में खुशनुमा पीले कपड़े पहने हुए उदास चेहरे वाले कैदी याद आते हैं. और उस वृद्धा का उदास चेहरा दिखता है, जाने क्या सोच रही थी वह?
शुक्रवार, जून 18, 2010
फ़लों से झुका पेड़
बचपन में यह कहावत सुनी थी कि जिस पेड़ पर जितना फ़ल अधिक लगता है, वह उतना ही झुक जाता है. इस कहावत से यह शिक्षा दी जाती थी कि जीवन में जितना ऊपर उठो, उतने ही विनम्र बनो. लेकिन बहुत से बड़े लोगों को देख कर लग कि असल में तो ऊल्टा ही होता है, जो जितना ऊँचा चढ़ता है, उसके उतने ही नखरे, मानो भगवान ने उन्हें अलग बनाया हो और उनका होना भर ही सारी मानवता पर उपकार है.
लेकिन कुछ दिन पहले सचमुच ऐसे व्यक्ति से मिलने का मौका मिला जिसने इस कहावत को आत्मसार किया था, हालाँकि शायद उन्हें इस कहावत के बारे में कुछ मालूम न हो.
अमरीका से सम्बंधी आये थे, उन्हें शहर घुमा रहा था. हम लोग शहर के पुराने भाग में थे, अचानक मुझे अपने सामने से आते हुए इटली के पूर्व प्रधान मंत्री दिखे, श्री रोमानो प्रोदी. वह दो बार इटली के प्रधान मंत्री बने, 1996 से 1998 और फ़िर, 2006 से 2008 तक.
इटली के दूसरी बार प्रधान मंत्री होने से पहले, बीच में 1999 से 2004 तक वह यूरोप संसद के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं. बहुत वर्ष पहले वह प्रधान मंत्री बनने से पहले, हमारे शहर में ही अर्थशास्त्र पढ़ाते थे. मैंने अखबार में पढ़ा तो था कि वह बिना सुरक्षा दल आदि के सामान्य रूप से घूमते हैं, लेकिन उन्हें इस तरह सामने देख कर मैं एक क्षण को हकबका गया. बिना कुछ सोचे तुरंत उनके सामने हाथ मिलाने के लिए बढ़ा दिया. उनके आस पास के लोग कुछ कहते उससे पहले ही, वह तुरंत मेरे पास आये, बड़ी आत्मीयता से मिले, बात की मानो पुराने मित्र हों. साथ तस्वीर भी खिंचवायी.
मेरे अमरीकी सम्बंधी भी दंग रह गये कि इतनी सरलता से वह सड़क के बीच में खड़े हमसे बात करते रहे. बोले ऐसा तो यहीं हो सकता है, भारत या अमरीका में नहीं. पर मेरे मन में भारतीय प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह की भी कुछ इसी तरह की तस्वीर है, लगता है कि सामान्य जीवन वह भी इसी तरह के होंगे. प्रोदी जी की तरह वह भी अर्थशास्त्री रहे हैं.
लेकिन कुछ दिन पहले सचमुच ऐसे व्यक्ति से मिलने का मौका मिला जिसने इस कहावत को आत्मसार किया था, हालाँकि शायद उन्हें इस कहावत के बारे में कुछ मालूम न हो.
अमरीका से सम्बंधी आये थे, उन्हें शहर घुमा रहा था. हम लोग शहर के पुराने भाग में थे, अचानक मुझे अपने सामने से आते हुए इटली के पूर्व प्रधान मंत्री दिखे, श्री रोमानो प्रोदी. वह दो बार इटली के प्रधान मंत्री बने, 1996 से 1998 और फ़िर, 2006 से 2008 तक.
इटली के दूसरी बार प्रधान मंत्री होने से पहले, बीच में 1999 से 2004 तक वह यूरोप संसद के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं. बहुत वर्ष पहले वह प्रधान मंत्री बनने से पहले, हमारे शहर में ही अर्थशास्त्र पढ़ाते थे. मैंने अखबार में पढ़ा तो था कि वह बिना सुरक्षा दल आदि के सामान्य रूप से घूमते हैं, लेकिन उन्हें इस तरह सामने देख कर मैं एक क्षण को हकबका गया. बिना कुछ सोचे तुरंत उनके सामने हाथ मिलाने के लिए बढ़ा दिया. उनके आस पास के लोग कुछ कहते उससे पहले ही, वह तुरंत मेरे पास आये, बड़ी आत्मीयता से मिले, बात की मानो पुराने मित्र हों. साथ तस्वीर भी खिंचवायी.
***
अगर फ़िर से शुरु होता?
कल सुबह कार पार्क कर रहा था तो अचानक मन में विचार आया, अगर यह जीवन फ़िर से शुरु करने का मौका मिले, एक बार फ़िर से बच्चा बन जाऊँ, तो क्या कौन सी बातें अपने इस जीवन की बदलना चाहूँगा? हरी भरी पहाड़ी के नीचे, सुंदर शांत जगह पर है यह कार पार्क, शायद इसीलिए वहाँ पर सुबह सुबह इस तरह के गम्भीर और महत्वपूर्ण विचार मन में आते हैं?
पिछले कुछ दिनों से मैं अमरीकी प्रोफेसर रेंडी पाउश (Randy Pausch) की किताब "द लास्ट लेक्चर" (The last lecture) पढ़ रहा था. शायद यह दोबारा जीवन शुरु करने वाली बात मन में अचानक उनकी किताब पढ़ने की वजह से ही आयी थी. उनके अमरीकी विश्वविद्यालय में इस तरह के भाषण देने का प्रचलन था कि प्रोफेसर से कहिये कि अगर आप को एक अंतिम बार विद्यार्थियों से बोलने का मौका मिले तो आप कौन सी बात कहना चाहेंगे? इन भाषणों को "अंतिम भाषण" कहा जाता है.
2007 में जब रेंडी से इस तरह का भाषण देने के लिए कहा गया था तो उनकी स्थिति कुछ भिन्न थी. कुछ ही महीने पहले उन्हें अपने शरीर में पनपते लाइलाज कैंसर होने की बात का पता चला था. डाक्टरों का कहना था कि उनके जीवन के कुछ महीने ही शेष बचे थे. पत्नी और तीन छोटे बच्चों का क्या होगा, इसकी चिंता भी थी उनके मन में.
फ़िर भी रेंडी ने इस भाषण को देना स्वीकार किया. उनका यह भाषण, इंटरनेट पर एक दूसरे से सुन कर, हज़ारों लोगों ने देखा, सुना और सराहा. इतना प्रसिद्ध हुआ उनका यह भाषण कि उसे किताब के रूप में भी छापा गया, जिसे मैंने भी पिछली भारत यात्रा में बँगलौर की एक दुकान में खरीदा था. रेंडी तो चले गये, लेकिन उनके इस भाषण की किताब ने उनकी पत्नी और तीन बच्चों को कुछ आमदनी भी दी. अगर आप चाहें तो रेंडी के इस भाषण को आप इंटरनेट पर भी सुन सकते हैं.
जो प्रश्न सुबह मेरे मन में उठा था, उस पर दिन में कई बार सोचा. बचपन से मुझे साहित्य, इतिहास, जैसे आर्ट विषयों में बहुत रुची थी, लेकिन जब विद्यालय में विषय चुनने का समय आया था तो मैंने विज्ञान के विषय चुने थे, जिसका प्रमुख कारण था कि उस समय मुझे लगता था कि इस रास्ते से अच्छी नौकरी मिलने और ठीक पैसा कमाने का मौका मिलेगा, साथ ही डाक्टरी से लोगों के काम भी आ सकूँगा. उस समय आज जैसी बात नहीं थी, तब इंजीनियर, डाक्टर या आई.ए.एस जैसे दो तीन काम छोड़ कर लगता था कि और कोई ढंग का काम नहीं होगा. जीवन में कई बार मन में आता रहा है कि अगर डाक्टरी न कर के कुछ साहित्य संम्बधी किया होता तो शायद मन को अधिक संतोष मिलता. तो क्या अगर जीवन दोबारा से शुरु किया जा सके तो इस बार साहित्य को चुनूँगा, इस बात पर देर तक सोचता रहा.
बहुत सोच कर इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि नहीं मैं इस तरह की कोई बात अपने जीवन में नहीं बदलना चाहूँगा, अगर जीवन दोबारा शुरु करने का मौका मिले, तो सब कुछ फ़िर से वैसा ही करूँगा जैसा इस बार किया था.
हाँ कुछ बातें हैं जिन्हें अगर मौका मिल पाता तो अवश्य बदलता. तीस साल पहले मेरे एक प्रिय मित्र ने आत्महत्या की थी. उसने मुझे बहुत संकेत दिये थे, लेकिन मैं उन्हें समझ नहीं पाया था, उसकी बात को गम्भीरता से नहीं लिया था. दोबारा मौका मिले तो उसे अकेला नहीं छोड़ूँगा, उसे रोक लूँगा.
कितनी बार छोटी छोटी बातों पर गुस्सा किया है, अपनों के मन को दुखाया है. दोबारा मौका मिले तो यह मागूँगा कि भगवान मुझे इतनी समझ दे कि उनका मन न दुखाऊँ. बस इसी तरह की बातें मन में आयीं, लेकिन अपने जीवन के किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को बदलने का बात मुझे ठीक नहीं लगी.
कुछ कुछ रेंडी जैसी बात एडम सेवेज (Adam Savage) ने भी की है, अपने आलेख "फूड फार द ईगल" (Food for the eagle) में. धर्म में या ईश्वर में वह विश्वास नहीं करते. कहते हैं कि अगर विश्वास ही करना हो तो कार्लस कास्टानेडा जैसे लेखकों के बनाये मिथकों में किया जा सकता है. वह बात करते हैं कास्टानेडा (Carlos Castaneda) की किताब "द ईगल्स गिफ्ट" (The eagle's gift) की, जिसमें आध्यात्मिक गुरु दान जुआन (Don Juan) अंत में अपने शिष्य को बताते हैं कि जीवन का और कुछ ध्येय नहीं, जितने साल का भी जीवन मिलेगा, उसके बाद गरुड़ आप की संज्ञा को ले कर खा जायेगा, आत्मसात कर लेगा. इस लिए जीवन में अपनी संज्ञा को जितना ज्ञान और अनुभव दे कर उसे बढ़ा सको उतना ही अच्छा ताकि अंत में तब आप की संज्ञा गरुण से मिले तो उसे भी आनंद मिले.
शायद हम सब को जीवन क्या है और क्यों है इसका कोई उत्तर चाहिये होता है, विषेशकर जब अपने किसी प्रियजनों को खो बैठते हैं. बहुत सालों से मेरी प्रिय पुस्तक है कठोपानिषद, जिसमें कहानी है नचिकेता की, जो पिता की आज्ञा को मान कर यम के पास चले जाते हैं और यम से जीवन और मृत्यु के बारे में समझाने के लिए कहते हैं. मेरा विश्वास इसी पुस्तक से बना है, कठोपानिषद से. मुझे जैसा समझ आया वह कास्तानेदा के गुरु वाली बात ही है. यानि, मुझे भी यही विश्वास है कि जो संज्ञा संसार के कण कण में बसी है, वही भगवान है, और जीवन का ध्येय जितने अनुभव, जितना ज्ञान पा सकें, उसे प्राप्त करना ही है, जीवन समाप्त होगा तो इसी सर्वव्याप्त संज्ञा में हम घुलमिल जायेंगे.
कभी कभी इस तरह की किताब या आलेख पढ़ते रहना अच्छा लगता है ताकि जीवन में क्या आवश्यक है, क्या महत्वपूर्ण है उसका ध्यान बना रहे, छोटी मोटी बातों की चिंता में जीवन को व्यर्थ न करें. आप क्या सोचते हैं कि जीवन का ध्येय क्या है? आप को अपना जीवन फ़िर से जीने को मिले तो क्या बदलना चाहेंगे? और कोई आप से कहे कि आप अपना अंतिम भाषण दीजिये तो आप क्या कहना चाहेंगे?
पिछले कुछ दिनों से मैं अमरीकी प्रोफेसर रेंडी पाउश (Randy Pausch) की किताब "द लास्ट लेक्चर" (The last lecture) पढ़ रहा था. शायद यह दोबारा जीवन शुरु करने वाली बात मन में अचानक उनकी किताब पढ़ने की वजह से ही आयी थी. उनके अमरीकी विश्वविद्यालय में इस तरह के भाषण देने का प्रचलन था कि प्रोफेसर से कहिये कि अगर आप को एक अंतिम बार विद्यार्थियों से बोलने का मौका मिले तो आप कौन सी बात कहना चाहेंगे? इन भाषणों को "अंतिम भाषण" कहा जाता है.
2007 में जब रेंडी से इस तरह का भाषण देने के लिए कहा गया था तो उनकी स्थिति कुछ भिन्न थी. कुछ ही महीने पहले उन्हें अपने शरीर में पनपते लाइलाज कैंसर होने की बात का पता चला था. डाक्टरों का कहना था कि उनके जीवन के कुछ महीने ही शेष बचे थे. पत्नी और तीन छोटे बच्चों का क्या होगा, इसकी चिंता भी थी उनके मन में.
फ़िर भी रेंडी ने इस भाषण को देना स्वीकार किया. उनका यह भाषण, इंटरनेट पर एक दूसरे से सुन कर, हज़ारों लोगों ने देखा, सुना और सराहा. इतना प्रसिद्ध हुआ उनका यह भाषण कि उसे किताब के रूप में भी छापा गया, जिसे मैंने भी पिछली भारत यात्रा में बँगलौर की एक दुकान में खरीदा था. रेंडी तो चले गये, लेकिन उनके इस भाषण की किताब ने उनकी पत्नी और तीन बच्चों को कुछ आमदनी भी दी. अगर आप चाहें तो रेंडी के इस भाषण को आप इंटरनेट पर भी सुन सकते हैं.
जो प्रश्न सुबह मेरे मन में उठा था, उस पर दिन में कई बार सोचा. बचपन से मुझे साहित्य, इतिहास, जैसे आर्ट विषयों में बहुत रुची थी, लेकिन जब विद्यालय में विषय चुनने का समय आया था तो मैंने विज्ञान के विषय चुने थे, जिसका प्रमुख कारण था कि उस समय मुझे लगता था कि इस रास्ते से अच्छी नौकरी मिलने और ठीक पैसा कमाने का मौका मिलेगा, साथ ही डाक्टरी से लोगों के काम भी आ सकूँगा. उस समय आज जैसी बात नहीं थी, तब इंजीनियर, डाक्टर या आई.ए.एस जैसे दो तीन काम छोड़ कर लगता था कि और कोई ढंग का काम नहीं होगा. जीवन में कई बार मन में आता रहा है कि अगर डाक्टरी न कर के कुछ साहित्य संम्बधी किया होता तो शायद मन को अधिक संतोष मिलता. तो क्या अगर जीवन दोबारा से शुरु किया जा सके तो इस बार साहित्य को चुनूँगा, इस बात पर देर तक सोचता रहा.
बहुत सोच कर इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि नहीं मैं इस तरह की कोई बात अपने जीवन में नहीं बदलना चाहूँगा, अगर जीवन दोबारा शुरु करने का मौका मिले, तो सब कुछ फ़िर से वैसा ही करूँगा जैसा इस बार किया था.
हाँ कुछ बातें हैं जिन्हें अगर मौका मिल पाता तो अवश्य बदलता. तीस साल पहले मेरे एक प्रिय मित्र ने आत्महत्या की थी. उसने मुझे बहुत संकेत दिये थे, लेकिन मैं उन्हें समझ नहीं पाया था, उसकी बात को गम्भीरता से नहीं लिया था. दोबारा मौका मिले तो उसे अकेला नहीं छोड़ूँगा, उसे रोक लूँगा.
कितनी बार छोटी छोटी बातों पर गुस्सा किया है, अपनों के मन को दुखाया है. दोबारा मौका मिले तो यह मागूँगा कि भगवान मुझे इतनी समझ दे कि उनका मन न दुखाऊँ. बस इसी तरह की बातें मन में आयीं, लेकिन अपने जीवन के किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को बदलने का बात मुझे ठीक नहीं लगी.
कुछ कुछ रेंडी जैसी बात एडम सेवेज (Adam Savage) ने भी की है, अपने आलेख "फूड फार द ईगल" (Food for the eagle) में. धर्म में या ईश्वर में वह विश्वास नहीं करते. कहते हैं कि अगर विश्वास ही करना हो तो कार्लस कास्टानेडा जैसे लेखकों के बनाये मिथकों में किया जा सकता है. वह बात करते हैं कास्टानेडा (Carlos Castaneda) की किताब "द ईगल्स गिफ्ट" (The eagle's gift) की, जिसमें आध्यात्मिक गुरु दान जुआन (Don Juan) अंत में अपने शिष्य को बताते हैं कि जीवन का और कुछ ध्येय नहीं, जितने साल का भी जीवन मिलेगा, उसके बाद गरुड़ आप की संज्ञा को ले कर खा जायेगा, आत्मसात कर लेगा. इस लिए जीवन में अपनी संज्ञा को जितना ज्ञान और अनुभव दे कर उसे बढ़ा सको उतना ही अच्छा ताकि अंत में तब आप की संज्ञा गरुण से मिले तो उसे भी आनंद मिले.
शायद हम सब को जीवन क्या है और क्यों है इसका कोई उत्तर चाहिये होता है, विषेशकर जब अपने किसी प्रियजनों को खो बैठते हैं. बहुत सालों से मेरी प्रिय पुस्तक है कठोपानिषद, जिसमें कहानी है नचिकेता की, जो पिता की आज्ञा को मान कर यम के पास चले जाते हैं और यम से जीवन और मृत्यु के बारे में समझाने के लिए कहते हैं. मेरा विश्वास इसी पुस्तक से बना है, कठोपानिषद से. मुझे जैसा समझ आया वह कास्तानेदा के गुरु वाली बात ही है. यानि, मुझे भी यही विश्वास है कि जो संज्ञा संसार के कण कण में बसी है, वही भगवान है, और जीवन का ध्येय जितने अनुभव, जितना ज्ञान पा सकें, उसे प्राप्त करना ही है, जीवन समाप्त होगा तो इसी सर्वव्याप्त संज्ञा में हम घुलमिल जायेंगे.
कभी कभी इस तरह की किताब या आलेख पढ़ते रहना अच्छा लगता है ताकि जीवन में क्या आवश्यक है, क्या महत्वपूर्ण है उसका ध्यान बना रहे, छोटी मोटी बातों की चिंता में जीवन को व्यर्थ न करें. आप क्या सोचते हैं कि जीवन का ध्येय क्या है? आप को अपना जीवन फ़िर से जीने को मिले तो क्या बदलना चाहेंगे? और कोई आप से कहे कि आप अपना अंतिम भाषण दीजिये तो आप क्या कहना चाहेंगे?
गुरुवार, जून 17, 2010
बॉली या पॉउली ?
बम्बई के फ़िल्म जगत को बॉलीवुड का नाम कब मिला यह तो कोई ठीक से नहीं कह सकता, विकीपीडिया भी नहीं. मुझे लगता है कि 1970 के दशक में बम्बई से निकलने वाली स्टारडस्ट, सिने ब्लिट्ज़ जैसी फ़िल्मी पत्रिकाओं में तब भी बॉलीवुड शब्द का प्रयोग होता था.
इधर पिछले कुछ सालों में कई बार पढ़ा कि बम्बई के कुछ प्रसिद्ध सितारे अभिनेता, इस नाम से खुश नहीं, वे अपनी पहचान को हॉलीवुड के नकलची छोटा भाई के रुप में नहीं करवाना चाहते, अपने आत्मसम्मान का सोचते हैं. लेकिन यहाँ यूरोप में तो धीरे धीरे बॉलीवुड शब्द की पहचान ही हर तरफ़ बढ़ती जा रही है, और इसका प्रयोग केवल बम्बई में बनने वाली हिंदी फ़िल्मों के लिए ही नहीं बल्कि भारत में बनी सभी फ़िल्मों के लिए किया जाने लगा है, चाहे वे तमिल में हों या बंगला में.
कुछ दिन पहले, इटली के एक लेखक जो कि आजकल बम्बई की पृष्ठभूमि पर एक उपन्यास लिख रहे हैं, उनसे बात हो रही थी, तो वे कहने लगे कि बॉलीवुड शब्द को केवल बम्बई में बनने वाली मसाला फ़िल्मों के लिए प्रयोग करना चाहिये, कला फ़िल्मों, समानांतर सिनेमा, कलकत्ता या केरल में बनने वाली फ़िल्में, इन सब को बॉलीवुड कहना गलत है.
मुझे भारत के अलग अलग हिस्सों में बनने वाली फ़िल्मों तथा कला फ़िल्मों और फार्मूला फ़िल्मों का अंतर समझ में आता है, लेकिन यह भी लगता है कि यूरोप में भारतीय फ़िल्मों के बढ़ते प्रशंसकों को इन अंतरों को समझने में कोई दिलचस्पी नहीं है. इटली में भारतीय फ़िल्मों की जानकारी पिछले दो वर्षों में अचानक तेज़ी से बढ़ी है जबसे यहाँ की एक प्रमुख टीवी चेनल ने बहुत सारी बम्बई की मसाला फ़िल्में, "हम तुम" और "नमस्ते इंडिया" से ले कर "जब वी मेट" को दिखाया है. इससे पहले, भारतीय फ़िल्मों को कुछ थोड़े बहुत लोग ही जानते थे. हालाँकि टीवी पर जब यह फ़िल्में दिखायी गयीं तब इनमें से अधिकतर गाने व नृत्य काट दिये गये थे, लेकिन फ़िर भी लोगों में गानों और नत्यों के प्रति उत्सुकता जागी और लोग यूट्यूब जैसे वेब पन्नों पर भारतीय फ़िल्मों को खोजने लगे हैं.
आज इटली के बहुत से शहरों में बौलीवुड क्ल्ब बने हैं, इन फ़िल्मों के दीवाने, शाहरुख खान, आमीर खान और अक्षय कुमार जैसे अभिनेताओं की प्रशंसा में पत्र लिखते हैं, उनकी तस्वीरें सहेजते हैं. फेसबुक पर पृष्ठ बनाते हैं, बॉलीवुड नृत्यों के स्कूल खोलते हैं. उन्हें फ़िल्म की मूल भाषा क्या है, हिंदी या बंगला या तमिल, इसमें दिलचस्पी नहीं, सबटाईटल हैं या नहीं, बस यह जानना होता है. फेसबुक पर बने इतालवी बॉलीवुड पृष्ठ के एक हज़ार से अधिक सदस्य हैं. कुछ दिन पहले एक इतालवी युवती का ईमेल मिला कि क्यों न सब लोग मिल कर ए. आर रहमान को इटली में आ कर संगीत कार्यक्रम करने को कहें?
बॉलीवुड से मिलती जुलती बात का एक समाचार ब्राज़ील से मिला.
कुछ दिनों के लिए मुझे ब्राज़ील जाना है, उसकी तैयारी के लिए खोज कर रहा था तो ब्राज़ील के पॉउलीवुड के बारे में एक लेख दिखा, जिसमें लिखा है कि ब्राज़ील के सनपाउलो राज्य में एक छोटे से शहर ने, जिसका नाम पाउलीनिया है, फ़िल्म शहर बनने का निश्चय किया है. इस शहर में ब्राज़ील की सबसे बड़ी पेट्रोल रिफाईनरी फैक्ट्री है जिस पर टेक्स लगाने की वजह से शहर की नगरपालिका की बहुत आय होती है, और नगरपालिका ने निर्णय लया कि वे इस आय से वे लोग फ़िल्म बनाने वालों को सहारा देंगे, उन्हें सब सुविधाएँ देंगे, पैसे देंगे, इत्यादि. इस नीति की वजह से कुछ ही वर्षों में पाउलीनिया का छोटा सा, अनजाना शहर, अचानक प्रसिद्ध होने लगा है और पिछले वर्ष, ब्राज़ील में बनने वाली एक तिहायी फ़िल्मों की शूटिंग यहीं हुई है. वह चाहते हैं कि शहर का नाम अब लोग पाउलीनिया के जगह, बॉलीवुड की प्रसिद्धी से प्रेरणा पा कर, पॉउलीवुड कहा जाये.
आज के भूमँडलिकरण के जगत का नियम है कि आत्मसम्मान और अपने नाम या पहचान के अलग होने की चिंता न करके, कैसे ब्रैंडनेम बनाया जाये, जिसे दुनिया में प्रसिद्धी मिले, धँधा बढ़े, पैसा आये, कमाई हो, इसको सोचना चाहिये. जब गाँधी जी के नाम को ब्रैँड बना कर बेचा जा सकता है तो बॉलीवुड की ब्रैंड को बेचने में दुविधा क्यों? तो बॉलीवुड के बने बनाये नाम का फ़ायदा पाना ही बेहतर है या फ़िर अपने आत्म सम्मान के लिए सबसे यह कहना कि भारतीय सिनेमा को बॉलीवुड कह कर उसकी तौहीन न करें?
***
इधर पिछले कुछ सालों में कई बार पढ़ा कि बम्बई के कुछ प्रसिद्ध सितारे अभिनेता, इस नाम से खुश नहीं, वे अपनी पहचान को हॉलीवुड के नकलची छोटा भाई के रुप में नहीं करवाना चाहते, अपने आत्मसम्मान का सोचते हैं. लेकिन यहाँ यूरोप में तो धीरे धीरे बॉलीवुड शब्द की पहचान ही हर तरफ़ बढ़ती जा रही है, और इसका प्रयोग केवल बम्बई में बनने वाली हिंदी फ़िल्मों के लिए ही नहीं बल्कि भारत में बनी सभी फ़िल्मों के लिए किया जाने लगा है, चाहे वे तमिल में हों या बंगला में.
कुछ दिन पहले, इटली के एक लेखक जो कि आजकल बम्बई की पृष्ठभूमि पर एक उपन्यास लिख रहे हैं, उनसे बात हो रही थी, तो वे कहने लगे कि बॉलीवुड शब्द को केवल बम्बई में बनने वाली मसाला फ़िल्मों के लिए प्रयोग करना चाहिये, कला फ़िल्मों, समानांतर सिनेमा, कलकत्ता या केरल में बनने वाली फ़िल्में, इन सब को बॉलीवुड कहना गलत है.
मुझे भारत के अलग अलग हिस्सों में बनने वाली फ़िल्मों तथा कला फ़िल्मों और फार्मूला फ़िल्मों का अंतर समझ में आता है, लेकिन यह भी लगता है कि यूरोप में भारतीय फ़िल्मों के बढ़ते प्रशंसकों को इन अंतरों को समझने में कोई दिलचस्पी नहीं है. इटली में भारतीय फ़िल्मों की जानकारी पिछले दो वर्षों में अचानक तेज़ी से बढ़ी है जबसे यहाँ की एक प्रमुख टीवी चेनल ने बहुत सारी बम्बई की मसाला फ़िल्में, "हम तुम" और "नमस्ते इंडिया" से ले कर "जब वी मेट" को दिखाया है. इससे पहले, भारतीय फ़िल्मों को कुछ थोड़े बहुत लोग ही जानते थे. हालाँकि टीवी पर जब यह फ़िल्में दिखायी गयीं तब इनमें से अधिकतर गाने व नृत्य काट दिये गये थे, लेकिन फ़िर भी लोगों में गानों और नत्यों के प्रति उत्सुकता जागी और लोग यूट्यूब जैसे वेब पन्नों पर भारतीय फ़िल्मों को खोजने लगे हैं.
आज इटली के बहुत से शहरों में बौलीवुड क्ल्ब बने हैं, इन फ़िल्मों के दीवाने, शाहरुख खान, आमीर खान और अक्षय कुमार जैसे अभिनेताओं की प्रशंसा में पत्र लिखते हैं, उनकी तस्वीरें सहेजते हैं. फेसबुक पर पृष्ठ बनाते हैं, बॉलीवुड नृत्यों के स्कूल खोलते हैं. उन्हें फ़िल्म की मूल भाषा क्या है, हिंदी या बंगला या तमिल, इसमें दिलचस्पी नहीं, सबटाईटल हैं या नहीं, बस यह जानना होता है. फेसबुक पर बने इतालवी बॉलीवुड पृष्ठ के एक हज़ार से अधिक सदस्य हैं. कुछ दिन पहले एक इतालवी युवती का ईमेल मिला कि क्यों न सब लोग मिल कर ए. आर रहमान को इटली में आ कर संगीत कार्यक्रम करने को कहें?
बॉलीवुड से मिलती जुलती बात का एक समाचार ब्राज़ील से मिला.
कुछ दिनों के लिए मुझे ब्राज़ील जाना है, उसकी तैयारी के लिए खोज कर रहा था तो ब्राज़ील के पॉउलीवुड के बारे में एक लेख दिखा, जिसमें लिखा है कि ब्राज़ील के सनपाउलो राज्य में एक छोटे से शहर ने, जिसका नाम पाउलीनिया है, फ़िल्म शहर बनने का निश्चय किया है. इस शहर में ब्राज़ील की सबसे बड़ी पेट्रोल रिफाईनरी फैक्ट्री है जिस पर टेक्स लगाने की वजह से शहर की नगरपालिका की बहुत आय होती है, और नगरपालिका ने निर्णय लया कि वे इस आय से वे लोग फ़िल्म बनाने वालों को सहारा देंगे, उन्हें सब सुविधाएँ देंगे, पैसे देंगे, इत्यादि. इस नीति की वजह से कुछ ही वर्षों में पाउलीनिया का छोटा सा, अनजाना शहर, अचानक प्रसिद्ध होने लगा है और पिछले वर्ष, ब्राज़ील में बनने वाली एक तिहायी फ़िल्मों की शूटिंग यहीं हुई है. वह चाहते हैं कि शहर का नाम अब लोग पाउलीनिया के जगह, बॉलीवुड की प्रसिद्धी से प्रेरणा पा कर, पॉउलीवुड कहा जाये.
आज के भूमँडलिकरण के जगत का नियम है कि आत्मसम्मान और अपने नाम या पहचान के अलग होने की चिंता न करके, कैसे ब्रैंडनेम बनाया जाये, जिसे दुनिया में प्रसिद्धी मिले, धँधा बढ़े, पैसा आये, कमाई हो, इसको सोचना चाहिये. जब गाँधी जी के नाम को ब्रैँड बना कर बेचा जा सकता है तो बॉलीवुड की ब्रैंड को बेचने में दुविधा क्यों? तो बॉलीवुड के बने बनाये नाम का फ़ायदा पाना ही बेहतर है या फ़िर अपने आत्म सम्मान के लिए सबसे यह कहना कि भारतीय सिनेमा को बॉलीवुड कह कर उसकी तौहीन न करें?
***
शुक्रवार, मई 28, 2010
कविता के शब्द
कुछ दिन पहले लाल्टू की कविताओं की नयी किताब मिली. कविताएँ मुझे धीरे धीरे पढ़ना अच्छा लगता है, जैसे शाम को सैर से पहले दो एक कविता पढ़ कर जाओ तो सैर के दौरान उन पर सोचने का समय मिल जाता है और इस तरह से यह भी समझ में आता है कि कविता में दम था या नहीं. अगर थोड़ी देर में ही कविता भूल जाये तो लगता है कि कुछ विषेश दम नहीं था. कभी किसी कविता से कुछ और याद आ जाता है.
लाल्टू की किताब का शीर्षक है "लोग ही चुनेंगे रंग", और शीर्षक वाली कविता बहुत सुंदर हैः
चुप्पी के खिलाफ़
किसी विषेश रंग का झंडा नहीं चाहिए
खड़े या बैठे भीड़ में जब कोई हाथ लहराता है
लाल या सफ़ेद
आँखें ढूँढ़ती हैं रंगो के अर्थ
लगातार खुलना चाहते बन्द दरवाज़े
कि थरथराने लगे चुप्पी
फ़िर रंगों की धक्कलपेल में
अचानक ही खुले दरवाज़े वापस बंद होने लगते हैं
कुछ ऐसी ही बात स्पेनी गीतकार और गायक मिगेल बोज़े (Miguel Bosé) ने अपने एक गीत में कही थी जिसमें वह ऐसे रंग के सपने की बात करते थे जो किसी झँडे में न हो. राष्ट्रीयता के नाम पर होने वाले भूतपूर्व युगोस्लोविया में होने वाले युद्ध के बारे में लिखा यह गीत मेरे पसंदीदा गीतों में से है.
कुछ दिन पहले सुप्रसिद्ध ईज़राइली कवि येहुदा अमिछाई (Yehuda Amichai), जिन्हें ईज़राइल के सर्वश्रेष्ठ आधुनिक कवियों में गिना जाता है, की एक कविता भी पढ़ीः
तुम्हारे मुझे छोड़ने के बाद
गंध को परखने वाले कुत्ते से मैंने सुंघवाया
अपनी छाती, अपने पेट को, भर ले
नाक में गंध, और तुम्हे खोजने जाये
आशा है कि तुम्हें खोज ले, और उखाड़ ले
तुम्हारे प्रेमी की गोलियाँ और काट ले
उसका लिंग, या कम से कम
अपने दाँतों में तुम्हारी एक जुराब ले आये
पढ़ कर पहला विचार आया कि यह कविता है कि विशाल भारद्वाज की किसी फ़िल्म का डायलाग? ऐसी बातें सोच तो सकते हैं लेकिन कविता में कहना क्या साहित्य है? आप का क्या विचार है?
फ़िर कल एक अन्य अच्छी कविता पढ़ी, यह कविता बच्चों के लिए है और एक विज्ञान सम्बंधित चिट्ठे पर लिखी है, कविता का विषय है एक गायिका की छोटी उँगली. हिंदी में लिखने से उसमें वह बात नहीं आ रही जो कविता में है, इसे मूल अंग्रेज़ी में ही पढ़िये.
लाल्टू की किताब का शीर्षक है "लोग ही चुनेंगे रंग", और शीर्षक वाली कविता बहुत सुंदर हैः
चुप्पी के खिलाफ़
किसी विषेश रंग का झंडा नहीं चाहिए
खड़े या बैठे भीड़ में जब कोई हाथ लहराता है
लाल या सफ़ेद
आँखें ढूँढ़ती हैं रंगो के अर्थ
लगातार खुलना चाहते बन्द दरवाज़े
कि थरथराने लगे चुप्पी
फ़िर रंगों की धक्कलपेल में
अचानक ही खुले दरवाज़े वापस बंद होने लगते हैं
कुछ ऐसी ही बात स्पेनी गीतकार और गायक मिगेल बोज़े (Miguel Bosé) ने अपने एक गीत में कही थी जिसमें वह ऐसे रंग के सपने की बात करते थे जो किसी झँडे में न हो. राष्ट्रीयता के नाम पर होने वाले भूतपूर्व युगोस्लोविया में होने वाले युद्ध के बारे में लिखा यह गीत मेरे पसंदीदा गीतों में से है.
कुछ दिन पहले सुप्रसिद्ध ईज़राइली कवि येहुदा अमिछाई (Yehuda Amichai), जिन्हें ईज़राइल के सर्वश्रेष्ठ आधुनिक कवियों में गिना जाता है, की एक कविता भी पढ़ीः
तुम्हारे मुझे छोड़ने के बाद
गंध को परखने वाले कुत्ते से मैंने सुंघवाया
अपनी छाती, अपने पेट को, भर ले
नाक में गंध, और तुम्हे खोजने जाये
आशा है कि तुम्हें खोज ले, और उखाड़ ले
तुम्हारे प्रेमी की गोलियाँ और काट ले
उसका लिंग, या कम से कम
अपने दाँतों में तुम्हारी एक जुराब ले आये
पढ़ कर पहला विचार आया कि यह कविता है कि विशाल भारद्वाज की किसी फ़िल्म का डायलाग? ऐसी बातें सोच तो सकते हैं लेकिन कविता में कहना क्या साहित्य है? आप का क्या विचार है?
फ़िर कल एक अन्य अच्छी कविता पढ़ी, यह कविता बच्चों के लिए है और एक विज्ञान सम्बंधित चिट्ठे पर लिखी है, कविता का विषय है एक गायिका की छोटी उँगली. हिंदी में लिखने से उसमें वह बात नहीं आ रही जो कविता में है, इसे मूल अंग्रेज़ी में ही पढ़िये.
मंगलवार, अप्रैल 20, 2010
वेदों की मूल दुनिया
हर नयी यात्रा में मेरा प्रयत्न होता है कि कुछ नया पढ़ा जाये जिसे पढ़ने का घर पर आम व्यस्तता में समय नहीं मिलता. इस बार बँगलौर गया तो पढ़ने के लिए श्री राजेश कोच्चड़ की लिखी पुस्तक "वेदिक पीपल", यानि "वेदों के समय के लोग" पढ़ी. चूँकि आईसलैंड के ज्वालामुखी की वजह से अभी बँगलौर में रुका हुआ हूँ तो इस पुस्तक के बारे में लिखने का समय भी मिल गया. दरअस्ल, यह पुस्तक सभी वेदों को लिखने वाले लोगों की बात नहीं करती, इसका मुख्य ध्येय सबसे पहले वेद, ऋगवेद को लिखने वाले लोगों के बारे में है. साथ ही, यह पुस्तक रामायण तथा महाभारत की कुछ मुख्य घटनाओं की इतिहासिक जाँच करती है. (The vedic people - Their history and geography, by Rajesh Kocchar, Orient Blackswan 2009 - first ediation, 2000 by Orient Longman).
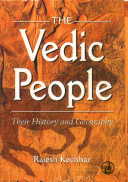 राजेश जी सामान्य व्यक्ति नहीं, नक्षत्रशा्स्त्र से जुड़ी भौतिकी के विषेशज्ञ हैं, बँगलौर में स्थित भारतीय नक्षत्रीय भौतिकी राष्ट्रीय संस्थान के डायरेक्टर रह चुके हैं तथा तथा आजकल दिल्ली में भारतीय विज्ञान, तकनीकी तथा विकास राष्ट्रीय संस्थान के डायरेक्टर हैं.
राजेश जी सामान्य व्यक्ति नहीं, नक्षत्रशा्स्त्र से जुड़ी भौतिकी के विषेशज्ञ हैं, बँगलौर में स्थित भारतीय नक्षत्रीय भौतिकी राष्ट्रीय संस्थान के डायरेक्टर रह चुके हैं तथा तथा आजकल दिल्ली में भारतीय विज्ञान, तकनीकी तथा विकास राष्ट्रीय संस्थान के डायरेक्टर हैं.
वेदों को लिखने वाले कौन लोग थे, वह कहाँ से आये थे, उनका क्या इतिहास था, इस सबके बारे में लिखने के लिए राजेश जी भाषा विज्ञान, साहित्य, प्राकृतिक इतिहास, पुरात्तवशास्त्र, नक्षत्रशास्त्र आदि विभिन्न दृष्टिकोणों से इस विषय की छानबीन करते हैं. उनके शौध के निष्कर्श चौंका देते हैं लेकिन उनके तर्क को नकारना कठिन है. जिस वैज्ञानिक तरीके से विभिन्न दृष्टिकोणों से उपलब्ध जानकारी को वह प्रस्तुत करते हैं, उससे यह लगता है कि किसी अन्य निष्कर्श पर पहुँचना संभव भी नहीं. इस पुस्तक को पढ़ कर, भारत की प्रचीन संस्कृति और धर्म के बारे में जो धारणाएँ थी, उनको नये सिरे से सोचने का अँकुश सा चुभता है.
पुस्तक का प्रमुख निष्कर्श है कि इंडोयूरोपी मूल के लोग एशिया के मध्य भाग में बसे थे, जहाँ इन्होंने घोड़े को पालतु बनाया, पहिये, रथों तथा घोड़ेगाड़ियों का आविष्कार किया. इन्हीं का एक गुट, पश्चिम की ओर निकला जिससे यूरोप के विभिन्न लोग बने. इन लोगों का फिनलैंड और हँगरी के मूल लोगों से सम्पर्क था जिससे दोनों की भाषाओं में आपसी प्रभाव पड़ा, जिसकी वजह से फिनिश तथा हँगेरियन इंडोयूरोपी भाषाएँ न होते हुए भी, इन भाषाओं के कुछ शब्द मिलते हैं. इन लोगों के दल विभिन्न समय पर जहाँ आज अफगानिस्तान है उस तरफ़ से हो कर ईरान भी गये और भारत की ओर भी बढ़े, जहाँ वह लोग हड़प्पा के जनगुटों से मिलजुल गये. इसी वजह से प्राचीन ईरानी धर्म जोरस्थत्रा के धर्मग्रंथ अवेस्ता में कुछ वही देवता मिलते हैं जो कि ऋगवेद में मिलते हैं जैसे कि इंद्र, मित्र, वरुण आदि. अग्नि पूजा का मूल भी दोनों लोगों को मिला.
राजेश जी के अनुसार ईसा से 1400 वर्ष पहले वहीं दक्षिण अफगानिस्तान में इसी भारतीय ईरानी मूल के कुछ लोगों ने ऋगवेद के श्लोक लिखना प्रारम्भ किया. यह श्लोक लिखने का कार्य करीब पाँच सौ वर्ष तक चला इसलिए ऋगवेद का मूल प्राचीन भाग ईसा से 900 वर्ष पहले के आसपास पूर्ण हुआ, तब तक यह लोग भारत के पश्चिमी भाग में पहुँच चुके थे. उनका कहना है कि जिस सरस्वती नदी जिसे "नदियों की माँ" कहा गया, वह दक्षिण अफगानिस्तान में बहने वाली नदी थी. उनके अनुसार रामायण की घटनाओं का समय भी ईसा से 1480 वर्ष पूर्व का है, वह सब दक्षिण अफगानिस्तान में ही घटित हुआ. महाभारत का युद्ध जो ईसा से करीब 900 वर्ष पहले हुआ, उसकी कर्मभूमि भी पश्चिम का वह हिस्सा है जहाँ आज पाकिस्तान है.
उनका कहना है पूर्व को बढ़ते यह मानव गुट, हड़प्पा के लोगों से मिल कर यायावर जीवन छोड़ कर कृषि में लगे. यह लोग अपने साथ साथ नदियों तथा जगहों के पुराने नाम भी ले कर आये और नये देश में कुछ जगहों तथा नदियों को यह पुराने नाम दिये, कुछ वैसे ही जैसे इटली, फ्राँस, ईग्लैंड से अमरीका जाने वाले प्रवासी अपने साथ अपने शहरों के नाम ले गये और नये अमरीकी शहरों को न्यू योर्क, न्यू ओरलियोन, रोम, वेनिस जैसे नाम दिये. यानि कुरुक्षेत्र, अयोध्या आदि मूल जगह दक्षिण अफगानिस्तान में थीं जिनके नामों को भारत में लाया गया. इसी वजह से ऋगवेद में गँगा नदी का नाम नहीं मिलता.
इन सब बातों के बारे में वह साहित्य, भाषाविज्ञान, पुरात्तव, गणिकी, नक्षत्रज्ञान आदि विभिन्न सूत्रों से जानकारी देते हैं, और उनके तर्कों के सामने अचरज सा होता है और लगता है कि हाँ यह हो सकता है.
किताब को पढ़ने के बाद सोच रहा था कि अगर अफगानिस्तान में पुरात्तव की खुदाई हो सके और राजेश जी कि विचारों को पक्का करने के लिए अन्य सबूत मिलने लगें तो इसका क्या असर पड़ेगा? शायद इस तरह की बातें भारत विभाजन के समय अगर मालूम होतीं तो क्या असर पड़ता?
मन में यह बात भी उठी कि पश्चिम से आने वाले यह लोग, अपने पहले आ कर बस जाने वाले लोगों से किस तरह मिले, किस तरह उनके धर्मों का समन्वय हुआ? जैसे कि हिंदू धर्म के तीन सबसे अधिक पूजे जाने वाले भगवान, राम, कृष्ण तथा शिव, तीनों ही श्याम वर्ण के कैसे हुए जबकि ऋगवेद को लिखने वाले तो गोरे रंग के थे? कैसे भारत के एक हिस्से में महोबा का पूजा होती है, दूसरे हिस्से में उसे महिषासुर कह कर मारा जाता है? कैसे पुरुष देवताओं की पूजा करने वाले आर्य भारत में बस कर शक्ति, लक्षमी और ज्ञान की देवियों को मानने लगे?
इन प्रश्नों के उत्तर कहाँ से मिलेंगे, अगर आप किसी बढ़िया किताब के बारे में जानते हों तो मुझे अवश्य बताईयेगा. आप को मिले तो राजेश कोच्चड़ की इस किताब को अवश्य पढ़ियेगा. और अगर आप इस किताब को पढ़ चुके हैं तो यह भी बतलाईयेगा कि उनके तर्क आप को कैसे लगे?
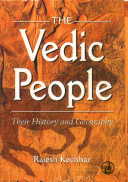
वेदों को लिखने वाले कौन लोग थे, वह कहाँ से आये थे, उनका क्या इतिहास था, इस सबके बारे में लिखने के लिए राजेश जी भाषा विज्ञान, साहित्य, प्राकृतिक इतिहास, पुरात्तवशास्त्र, नक्षत्रशास्त्र आदि विभिन्न दृष्टिकोणों से इस विषय की छानबीन करते हैं. उनके शौध के निष्कर्श चौंका देते हैं लेकिन उनके तर्क को नकारना कठिन है. जिस वैज्ञानिक तरीके से विभिन्न दृष्टिकोणों से उपलब्ध जानकारी को वह प्रस्तुत करते हैं, उससे यह लगता है कि किसी अन्य निष्कर्श पर पहुँचना संभव भी नहीं. इस पुस्तक को पढ़ कर, भारत की प्रचीन संस्कृति और धर्म के बारे में जो धारणाएँ थी, उनको नये सिरे से सोचने का अँकुश सा चुभता है.
पुस्तक का प्रमुख निष्कर्श है कि इंडोयूरोपी मूल के लोग एशिया के मध्य भाग में बसे थे, जहाँ इन्होंने घोड़े को पालतु बनाया, पहिये, रथों तथा घोड़ेगाड़ियों का आविष्कार किया. इन्हीं का एक गुट, पश्चिम की ओर निकला जिससे यूरोप के विभिन्न लोग बने. इन लोगों का फिनलैंड और हँगरी के मूल लोगों से सम्पर्क था जिससे दोनों की भाषाओं में आपसी प्रभाव पड़ा, जिसकी वजह से फिनिश तथा हँगेरियन इंडोयूरोपी भाषाएँ न होते हुए भी, इन भाषाओं के कुछ शब्द मिलते हैं. इन लोगों के दल विभिन्न समय पर जहाँ आज अफगानिस्तान है उस तरफ़ से हो कर ईरान भी गये और भारत की ओर भी बढ़े, जहाँ वह लोग हड़प्पा के जनगुटों से मिलजुल गये. इसी वजह से प्राचीन ईरानी धर्म जोरस्थत्रा के धर्मग्रंथ अवेस्ता में कुछ वही देवता मिलते हैं जो कि ऋगवेद में मिलते हैं जैसे कि इंद्र, मित्र, वरुण आदि. अग्नि पूजा का मूल भी दोनों लोगों को मिला.
राजेश जी के अनुसार ईसा से 1400 वर्ष पहले वहीं दक्षिण अफगानिस्तान में इसी भारतीय ईरानी मूल के कुछ लोगों ने ऋगवेद के श्लोक लिखना प्रारम्भ किया. यह श्लोक लिखने का कार्य करीब पाँच सौ वर्ष तक चला इसलिए ऋगवेद का मूल प्राचीन भाग ईसा से 900 वर्ष पहले के आसपास पूर्ण हुआ, तब तक यह लोग भारत के पश्चिमी भाग में पहुँच चुके थे. उनका कहना है कि जिस सरस्वती नदी जिसे "नदियों की माँ" कहा गया, वह दक्षिण अफगानिस्तान में बहने वाली नदी थी. उनके अनुसार रामायण की घटनाओं का समय भी ईसा से 1480 वर्ष पूर्व का है, वह सब दक्षिण अफगानिस्तान में ही घटित हुआ. महाभारत का युद्ध जो ईसा से करीब 900 वर्ष पहले हुआ, उसकी कर्मभूमि भी पश्चिम का वह हिस्सा है जहाँ आज पाकिस्तान है.
उनका कहना है पूर्व को बढ़ते यह मानव गुट, हड़प्पा के लोगों से मिल कर यायावर जीवन छोड़ कर कृषि में लगे. यह लोग अपने साथ साथ नदियों तथा जगहों के पुराने नाम भी ले कर आये और नये देश में कुछ जगहों तथा नदियों को यह पुराने नाम दिये, कुछ वैसे ही जैसे इटली, फ्राँस, ईग्लैंड से अमरीका जाने वाले प्रवासी अपने साथ अपने शहरों के नाम ले गये और नये अमरीकी शहरों को न्यू योर्क, न्यू ओरलियोन, रोम, वेनिस जैसे नाम दिये. यानि कुरुक्षेत्र, अयोध्या आदि मूल जगह दक्षिण अफगानिस्तान में थीं जिनके नामों को भारत में लाया गया. इसी वजह से ऋगवेद में गँगा नदी का नाम नहीं मिलता.
इन सब बातों के बारे में वह साहित्य, भाषाविज्ञान, पुरात्तव, गणिकी, नक्षत्रज्ञान आदि विभिन्न सूत्रों से जानकारी देते हैं, और उनके तर्कों के सामने अचरज सा होता है और लगता है कि हाँ यह हो सकता है.
किताब को पढ़ने के बाद सोच रहा था कि अगर अफगानिस्तान में पुरात्तव की खुदाई हो सके और राजेश जी कि विचारों को पक्का करने के लिए अन्य सबूत मिलने लगें तो इसका क्या असर पड़ेगा? शायद इस तरह की बातें भारत विभाजन के समय अगर मालूम होतीं तो क्या असर पड़ता?
मन में यह बात भी उठी कि पश्चिम से आने वाले यह लोग, अपने पहले आ कर बस जाने वाले लोगों से किस तरह मिले, किस तरह उनके धर्मों का समन्वय हुआ? जैसे कि हिंदू धर्म के तीन सबसे अधिक पूजे जाने वाले भगवान, राम, कृष्ण तथा शिव, तीनों ही श्याम वर्ण के कैसे हुए जबकि ऋगवेद को लिखने वाले तो गोरे रंग के थे? कैसे भारत के एक हिस्से में महोबा का पूजा होती है, दूसरे हिस्से में उसे महिषासुर कह कर मारा जाता है? कैसे पुरुष देवताओं की पूजा करने वाले आर्य भारत में बस कर शक्ति, लक्षमी और ज्ञान की देवियों को मानने लगे?
इन प्रश्नों के उत्तर कहाँ से मिलेंगे, अगर आप किसी बढ़िया किताब के बारे में जानते हों तो मुझे अवश्य बताईयेगा. आप को मिले तो राजेश कोच्चड़ की इस किताब को अवश्य पढ़ियेगा. और अगर आप इस किताब को पढ़ चुके हैं तो यह भी बतलाईयेगा कि उनके तर्क आप को कैसे लगे?
रविवार, मार्च 21, 2010
स्मृति शेष
18 फरवरी 2010 को सुबह सात बज कर दस मिनट पर माँ ने अंतिम साँस ली. कुछ दिन पहले ही मालूम हो गया था कि उनके जाने का समय आ रहा था. एक तरफ़ मन चाहता था कि वह हमेशा हमारे साथ रहें, दूसरी ओर सारे जीवन की उनकी शिक्षा थी कि तड़प तड़प कर जीना, कोई जीना नहीं और यह भी जानते थे अगर वह स्वयं निर्णय ले पाती तो शायद इससे बहुत पहले ही चली गयीं होतीं.
 पिछले दस सालों से धीरे धीरे उनकी यादाश्त जा रही थी. पिछले वर्ष जून में दिल्ली में उनके पास रहा था अपनी छोटी बहन के घर जहाँ वह पिछले कई सालों से रह रही थीं. उन्हें घर के कम्पाऊँड में घूमाने ले गया था. अचानक वह मेरी ओर मुड़ कर बोली थीं, "भाई साहब, आप मेरे इतना साथ साथ क्यों चल रहे हैं?" यानि बीच बीच मुझे भी नहीं पहचान पाती थीं. पिछले चार पांच महीनों से उनका बोलना अधिकतर समझ में नहीं आता है, शब्द, वा्कय, अर्थ सब गुड़मुड़ हो गये थे.
पिछले दस सालों से धीरे धीरे उनकी यादाश्त जा रही थी. पिछले वर्ष जून में दिल्ली में उनके पास रहा था अपनी छोटी बहन के घर जहाँ वह पिछले कई सालों से रह रही थीं. उन्हें घर के कम्पाऊँड में घूमाने ले गया था. अचानक वह मेरी ओर मुड़ कर बोली थीं, "भाई साहब, आप मेरे इतना साथ साथ क्यों चल रहे हैं?" यानि बीच बीच मुझे भी नहीं पहचान पाती थीं. पिछले चार पांच महीनों से उनका बोलना अधिकतर समझ में नहीं आता है, शब्द, वा्कय, अर्थ सब गुड़मुड़ हो गये थे.
उन दिनों रात को उनके साथ ही बिस्तर पर सोता था, उनका हाथ पकड़ कर सहलाता रहता या छोटे बच्चे की तरह उनसे लिपट जाता. सारी उम्र कठिनाईयों से लड़ने वाली माँ चमड़ी में लिपटी हड्डियों का ढाँचा रह गयी थी, लगता कि ज़ोर से दबाओ तो चटख जायेंगी.
रात को वह कई बार उठती और मुझे भी जगा देतीं. एक रात को उन्होंने चार पाँच बार जगाया. समझा बुझा कर हर बार उन्हें दोबारा सुला देता. सुबह चार बजे के करीब जब उन्होंने फ़िर जगाया तो मैंने नींद में ही उनसे कुछ गुस्से से कहा कि माँ बहुत नींद आ रही है, मुझे सोने दो, तो रोने लगीं. अचानक उनकी समझ कुछ देर के लिए लौट आयी थी, कातर हो कर बोलीं कि इस तरह का जीना मरने से बदतर है. फ़िर कहा, "तू तो डाक्टर है, मुझे कुछ दवा दे कर सुला नहीं सकता कि इस नर्क से छुटकारा मिले?" उनके साथ साथ मैं भी रो पड़ा था. कुछ देर में ही वह सब कुछ भूल कर फ़िर से सो गयीं थीं.
8 फरवरी को चीन में था, जब रात को माँ के बारे में बुरा सपना देखा. दिल घबराया तो रात को उठ कर छोटी बहन को ईमेल लिखी और माँ का हाल पूछा. बहन का उत्तर थोड़ी देर में ही आ गया, माँ होश में नहीं थीं और उन्हें अस्पताल में इनटेंसिव केयर में रखा गया था. अगले दिन ही भारत आने की उड़ान खोजी. दिल्ली पहुँचा तो अस्पताल में डाक्टर बोले कि कुछ और नहीं हो सकता था तो सोचा कि अगर कुछ नहीं हो सकता तो माँ को घर ले जा कर स्वयं ही उनके आखिरी दिनों की देखभाल करूँ. कम से कम घर के सब लोग साथ तो रह सकेंगे, अस्पताल में तो किसी को पास नहीं जाने देते.
करीब तीस साल पहले कुछ समय इनटेंसिव केयर में काम किया था, सोचा जितनी देखभाल करनी चाहिये, वह करनी तो मुझे आती है. घर ला कर सब इंतज़ाम किया. नाक से पेट में ट्यूब जिससे खाना दिया जाये, इंट्रावीनस ड्रिप दवाई देने के लिए, पिशाब के लिए केथेटर. माँ की पीठ पर घाव बन गया था, बाँहें और टाँगें दर्द से जुड़ी अकड़ गयी थीं जिन पर खून के गट्ठे बन गये थे, बेहोशी में भी दिन रात पीड़ा से कराह रही थीं. बार बार माँ के शब्द मन में आते कि मुझे तड़प तड़प कर मत मरने देना, ऐसी दवा देना कि आराम से चली जाऊँ. मेरे अंदर का डाक्टर कैसे क्या दवाई दी जाये, कैसे करवट बदलायी जाये, कब क्या खाने को दिया जाये सोचता था. अंदर का बेटा माँ के जाने का सोच कर द्रवित हो उठता. कई बार मन में आता कि इस तरह के इलाज से माँ की तड़प को और भी लम्बा कर रहा था. लगता कि माँ मुझसे चिरनिंद्रा की दवा माँग रही हों, दर्द से मुक्ति मांग रही हो, पर मुझमें इतनी ताकत नहीं थी कि माँ की यह इच्छा पूरी कर पाता.
माँ के जाने के बाद उनकी डायरियाँ पढ़ रहा हूँ. डायरी वाली माँ, मेरी यादों वाली माँ से अलग लगती है. बाहर से बहादुर, निडर दिखने वाली माँ, अपने डरों को सिर्फ़ डायरी को ही कह पाती थी. डायरी में अतीत के बहुत से लोगों की कहानियाँ और बातें हैं, लोहिया की समाजवादी पार्टी की बातें, भारत के पहले प्रधान मंत्री नेहरू की बातें, भारत पाकिस्तान विभाजन की बातें, पिता के मित्रों लेखकों कवियों की बातें, अपने अकेलेपन की बातें -
कितनी बातें जीवन की, कुछ भी नहीं रहता. बस यही लिखे कागज़ बचे हैं और यादें.

उन दिनों रात को उनके साथ ही बिस्तर पर सोता था, उनका हाथ पकड़ कर सहलाता रहता या छोटे बच्चे की तरह उनसे लिपट जाता. सारी उम्र कठिनाईयों से लड़ने वाली माँ चमड़ी में लिपटी हड्डियों का ढाँचा रह गयी थी, लगता कि ज़ोर से दबाओ तो चटख जायेंगी.
रात को वह कई बार उठती और मुझे भी जगा देतीं. एक रात को उन्होंने चार पाँच बार जगाया. समझा बुझा कर हर बार उन्हें दोबारा सुला देता. सुबह चार बजे के करीब जब उन्होंने फ़िर जगाया तो मैंने नींद में ही उनसे कुछ गुस्से से कहा कि माँ बहुत नींद आ रही है, मुझे सोने दो, तो रोने लगीं. अचानक उनकी समझ कुछ देर के लिए लौट आयी थी, कातर हो कर बोलीं कि इस तरह का जीना मरने से बदतर है. फ़िर कहा, "तू तो डाक्टर है, मुझे कुछ दवा दे कर सुला नहीं सकता कि इस नर्क से छुटकारा मिले?" उनके साथ साथ मैं भी रो पड़ा था. कुछ देर में ही वह सब कुछ भूल कर फ़िर से सो गयीं थीं.
8 फरवरी को चीन में था, जब रात को माँ के बारे में बुरा सपना देखा. दिल घबराया तो रात को उठ कर छोटी बहन को ईमेल लिखी और माँ का हाल पूछा. बहन का उत्तर थोड़ी देर में ही आ गया, माँ होश में नहीं थीं और उन्हें अस्पताल में इनटेंसिव केयर में रखा गया था. अगले दिन ही भारत आने की उड़ान खोजी. दिल्ली पहुँचा तो अस्पताल में डाक्टर बोले कि कुछ और नहीं हो सकता था तो सोचा कि अगर कुछ नहीं हो सकता तो माँ को घर ले जा कर स्वयं ही उनके आखिरी दिनों की देखभाल करूँ. कम से कम घर के सब लोग साथ तो रह सकेंगे, अस्पताल में तो किसी को पास नहीं जाने देते.
करीब तीस साल पहले कुछ समय इनटेंसिव केयर में काम किया था, सोचा जितनी देखभाल करनी चाहिये, वह करनी तो मुझे आती है. घर ला कर सब इंतज़ाम किया. नाक से पेट में ट्यूब जिससे खाना दिया जाये, इंट्रावीनस ड्रिप दवाई देने के लिए, पिशाब के लिए केथेटर. माँ की पीठ पर घाव बन गया था, बाँहें और टाँगें दर्द से जुड़ी अकड़ गयी थीं जिन पर खून के गट्ठे बन गये थे, बेहोशी में भी दिन रात पीड़ा से कराह रही थीं. बार बार माँ के शब्द मन में आते कि मुझे तड़प तड़प कर मत मरने देना, ऐसी दवा देना कि आराम से चली जाऊँ. मेरे अंदर का डाक्टर कैसे क्या दवाई दी जाये, कैसे करवट बदलायी जाये, कब क्या खाने को दिया जाये सोचता था. अंदर का बेटा माँ के जाने का सोच कर द्रवित हो उठता. कई बार मन में आता कि इस तरह के इलाज से माँ की तड़प को और भी लम्बा कर रहा था. लगता कि माँ मुझसे चिरनिंद्रा की दवा माँग रही हों, दर्द से मुक्ति मांग रही हो, पर मुझमें इतनी ताकत नहीं थी कि माँ की यह इच्छा पूरी कर पाता.
माँ के जाने के बाद उनकी डायरियाँ पढ़ रहा हूँ. डायरी वाली माँ, मेरी यादों वाली माँ से अलग लगती है. बाहर से बहादुर, निडर दिखने वाली माँ, अपने डरों को सिर्फ़ डायरी को ही कह पाती थी. डायरी में अतीत के बहुत से लोगों की कहानियाँ और बातें हैं, लोहिया की समाजवादी पार्टी की बातें, भारत के पहले प्रधान मंत्री नेहरू की बातें, भारत पाकिस्तान विभाजन की बातें, पिता के मित्रों लेखकों कवियों की बातें, अपने अकेलेपन की बातें -
... पाकिस्तान से आये तो दिल्ली में माडलबस्ती शीदीपुरा में एक मुसलमान के खाली घर में हमें शरण मिली, घर आधा जला हुआ था. मैं मृदुला साराभाई के शान्ती दल में काम करने लगी, घूम घूम कर मुसलमान लड़कियों को खोजते और उन्हें बचा कर उनके परिवारों में भेजते. तब अरुणा आसिफ़ अली, सुभद्रा जोशी आदि से भी भेंट हुई. कमला देवी चट्टोपाध्याय से रिफ्यूज़ी सेंटर में मिली. शाम को गाँधी जी की प्रार्थना सभा में जाते.
पहले मुझे तीन महीने सोशलिस्ट पार्टी के केंद्रीय दफ्तर में बाड़ा हिंदुराव में हिंदी टाईपिंग का काम मिला, वहाँ जे. स्वामीनाथन, सूरजप्रकाश, कश्यप भार्गव और दीपक जी से मिली. चमनलाल भी मित्र थे जिन्होंने फैज़रोड पर एक मुसलमान के खाली घर में स्कूल खोला तो मैं, कश्पी, दीपक और विमला जो बाद में चमन की पत्नी बनी, वहाँ स्कूल में काम करते और मेरे तीन भाई और एक बहन वहाँ पढ़ने लगे. मुझे 40 रुपये तन्ख्वाह मिलती जिसमें से 20 रुपये अपने भाई बहन की फ़ीस में दे देती. छः मास वहाँ काम किया...
.. 1949 में जब लोहिया नेपाल आंदोलन के संदर्भ में जेल से छूटे तो औखला में एक पार्टी दी गयी. मैं भी वहाँ थी. और मेरे साथ एक युगोस्लाविया की लड़की मलाडा कलाबावा भी थी जो लोहिया के यहां ही रह रही थी, बारहखम्बा रोड में पदमसिंह के यहां. आयु उसकी उस समय 23-24 की होगी. लड़की बहुत ही अच्छी थी. लोहिया की दोस्त थी. हम दोनो नहर के किनारे बैठे बात कर रहे थे. वह हिंदी जानती थी.
तभी एक टोकरी में पांच छः आम लिए लोहिया हमारे पास आ कर बैठ गये कि अरे तुम लोग यहां बैठी हो और सब आम खत्म हो गये हैं. इतने स्नेह से वह दे रहे थे कि मेरी आँखों में पानी भर आया. तो बोले, पीठ थपथपा कर, जल्दी से खालो. मुझे आम अधिक अच्छा नहीं लगता था फ़िर भी मैंने हाथ में लिया. तभी कश्पी, सूरज और दीपक तीनो आ गये, बोले कि यह तो बहुत ज्यादती है कि तुम दोनो सब आम खाओगी और हम देखते रहेंगे. मैंने मलाडा से कहा कि तुम ले लो और बाकी उन्हें दे दो और अपने हाथ वाला आम भी उन्हें दे दिया. मलाडा ने मेरी शिकायत लोहिया से की तो वह बहुत नाराज़ हुए कि मैंने तुम्हें बाँटने को नहीं दिये थे. मैंने माफ़ी माँग ली तो खिलखिला कर हँस पड़े. साथ ही कहा कि बहादुर तो तुम हो लेकिन समझदार नहीं हो...
..जब नेहरू की सरकार बनी तो लेजेस्लेटिव असेम्बली में संसद भवन में काम करना शुरु किया. तब सिद्धवा, दादा धर्माधिकारी, शाहनवाज़, पूर्णिमा बैनर्जी, मदनमोहन चतुर्वेदी आदि से पहचान हुई. मौलाना आज़ाद तब शिक्षा मंत्री थे, मसूद उनका पी.ए. था, मुझे उनके साथ काम मिलता. काम बहुत था और देर तक रुकना पड़ता था. मैं साईकल से आती जाती थी, रात को लौटती तो बिल्कुल सुनसान होता, रात के ग्यारह बारह भी बज जाते थे. वहाँ एक दक्षिण भारतीय अफसर था जिसने मुझे तंग करना शुरु कर दिया, उल्टी सीधी अटपट बातें करने लगा. तो मैं पंडित नेहरु के पास गयी जो मुझे मृदुला बहन के समय से जानते थे और मुझे बहादुर बेटी के नाम से पुकारते थे क्योंकि मैंने एक बार शान्ति दल में एक मुसलमान लड़की को भीड़ से बचाया था. तब मैं कभी भी तीन मूर्ती भवन के अंदर आ जा सकती थी.
मैंने पंडित जी को कहा कि मुझे असेम्बली से घर जाने में बहुत देर हो जाती है और अकेले घर जाने में डर लगता है. तो वह बोले तुम बहादुर लड़की हो, डर कैसा. मैंने कहा कि मुझे दरियागंज में नयी खुली टीचर्स इंस्टिट्यूट में भेज दीजिये, अभी तो ट्रेनिंग शुरु हुए दो महीने ही हुए हैं, मैं वह पूरा कर लूँगी. मौलाना आज़ाद के पी.ए. मसूद साहब मुझे फार्म दे गये, बस मैं संसद का काम छोड़ कर बेसिक टीचर्स ट्रैंनिग में चली गयी, जहाँ तीस रुपये महीने का वज़ीफ़ा मिलता था. एक साल बाद ट्रेनिंग पूरी हुई, मुझे दिल्ली के नवादा गाँव के स्कूल में नौकरी मिल गयी...
कितनी बातें जीवन की, कुछ भी नहीं रहता. बस यही लिखे कागज़ बचे हैं और यादें.
गुरुवार, जनवरी 21, 2010
मनप्रिय लेखक
क्रोएशिया की लेखिका मिलाना रुँजिच का एक लेख पढ़ रहा था. उन्हें किसी पाठक ने लिखा था कि उसे मिलाना का लेखन पढ़ कर उससे प्यार होने लगा था. मिलाना ने उत्तर में लिखा, "मेरे विचार में मुझे ऐसे पुरुष से प्यार होने में कोई दिक्कत नहीं होगी जो मेरे लिखे हुए को पढ़ कर मुझसे प्रेम करने लगा हो. सचमुच कहूँ तो मुझे लगता है कि तुम्हारा पत्र पढ़ कर मुझे भी तुमसे कुछ कुछ प्रेम सा हो ही गया है. मुझे हमेशा ही वह पुरुष अच्छे लगे हैं जो मेरी किताबों को पढ़ते हों. अगर उन्हें मेरा लिखा अच्छा लगता है तो इसका मतलब है कि उन्हें मैं भी अच्छी लगती हूँ क्योंकि मेरे लेखन में भी तो मैं ही होती हूँ. अगर कोई पुरुष कहे कि उसे मेरी कविताएँ अच्छी लगीं तो उसका मुझ पर और भी अधिक असर होता है. और अगर किसी को मेरे लेख भी अच्छे लगते हैं तो मैं उससे तुरंत विवाह करने को तैयार हूँ."
यानि लेखक भी सभी मानवों की तरह, अपने को चाहने वाले और पसंद करने वालों की तलाश में रहता है. पर किताब पढ़ कर लेखक की एक छवि मन में बना लेना और उसके प्रेम के सपने देखना या फ़िल्म देख कर अभिनेता या अभिनेत्री के सपने देखना, शायद यह कम उम्र में ही संभव होता है. सचमुच के जीवन में कितनी बार पाया कि जो लेखक या अभिनेता, किताब में या पर्दे पर इतना भाता है, सामान्य जीवन में सामान्य ही होता है, किसी बात में अच्छा लगता है और किसी बात में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता.
कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि किताबों कहानियों में बहुत अच्छा लगने वाले लेखक से जब मिलने का मौका मिला तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा. तब दुख भी होता है कि क्यों ऐसे व्यक्ति से मिला और बाद में उसकी लिखी किताब या कहानियाँ भी पढ़ने का मन नहीं करता.
अधिक प्रसिद्ध होने वाले व्यक्तियों से यह खतरा कुछ अधिक है, क्योंकि प्रसिद्ध के साथ साथ उनके सामान्य आचरण में निरंकुषता सी आ सकती है.
***
हिंदी की पत्रिका हँस को नियमित पढ़ते जाने कितने साल हो गये. पत्रिका का मेरा सबसे प्रिय हिस्सा है "मेरी तेरी उसकी बात", नयी पत्रिका आये तो सबसे पहले उसी को पढ़ता हूँ, कई बार दोबारा भी पढ़ता हूँ.
"मेरी तेरी उसकी बात" हँस के संपादक श्री राजेंद्र यादव लिखते हैं. जनवरी 2010 का हँस का नया अंक आया तो भी सबसे पहले इसी को पढ़ा. इस बार यादव जी ने "धर्मयुग" के संपादक श्री धर्मवीर भारती की पत्नी श्रीमति पुष्पा भारती से होने वाले झगड़े की बात की है. पुष्पा जी ने यादव जी की पत्नी मन्नू भँडारी से कहा कि वह अपनी पुस्तक में भारती जी बारे में लिखी किसी बात को हटा दें, क्योंकि वह गलत है. यादव जी अपने संपादकीय में अपनी पत्नी और पुष्पा जी बीच होने वाले इसी झगड़े की बात का विस्तार से सारा इतिहास बताते हैं. आरोप है भारती जी के सत्ता में होने वाले लोगों की चापलूसी का, इमरजैंसी के दौरान चुप्पी का और पहले इंदिरा-संजय वंदना का, फ़िर सत्ता पलटने पर अटल बिहारी वाजपेयी वंदना का.
आलेख को बहुत मज़े ले कर पढ़ा. किसी की बुराई हो रही हो तो चटकारे ले कर पढ़ना, मसालेदार चाट खाने से कम नहीं. आलेख में यादव जी और मन्नू भँडारी जी हैं कहानी के नायक, साथ में कुछ अन्य लोग हैं जैसे कि पंकज विष्ट. यह नायक लोग अपने आदर्शों पर बने रहे, सत्ताधारियों के आगे नहीं झुके, उनके पैसे और पुरस्कार ठुकरा दिये. दूसरी ओर सत्ता के सामने झुकने वाले, समझौता करने वालों कमज़ोर लोग हैं जिनके सरताज थे धर्मवीर भारती. इस झुकने समझौता करने वालों की लिस्ट में और भी बहुत से नाम हैं. साथ में अपने आदर्शों पर डटने के कुछ गवाहों के नाम भी हैं.
अधिक मसालेदार चाट खायी हो तो बाद में पेट में दर्द भी उठ सकता है, कुछ ऐसा ही लगा आलेख पढ़ कर.
यादव जी की लिस्ट में रघुवीर सहाय और अनीता औलक के भी नाम हैं. अनीता जी का ज़िक्र तो कुछ दिन पहले ही किया था जब मोहन राकेश जी के बारे में लिखा था. सोचा कि मोहन राकेश की मृत्यु तो 1972 में हुई थी फ़िर अनीता जी को क्यों इमरजेंसी के चक्कर में खींचा गया जिससे उन्हें सत्ता से समझौता करना पड़ा?
रघुवीर सहाय जी को बहुत सालों तक पिता के मित्र के रुप में जाना था, उनका नाम देख कर मन में अन्य बातें उठीं, अगर 1978 में इमरजैंसी के दौरान मेरे पिता जीवत होते तो क्या वह भी सत्ता से समझौता कर लेते? समझौता क्या होता है और क्यों करते हैं? आदर्शों को बना कर रखना इतना कठिन क्यों होता है? कौन करते हैं समझौता?
आलेख में धर्मवीर भारती की तो इतनी धूँआदार धुलाई की गयी है कि उनकी आत्मा छुपने की जगह खोज रही होगी. बची खुची कसर निकाली है तीस साल पहले "माया" पत्रिका में छपे आलेखों से, जिनमें भारती जी के बारे में अन्य विवरण हैं. इन सब पुराने आलेखों को हँस में दोबारा से छापा गया है. ऐसा सबूत सहित जूता मारा है कि दोबारा सिर उठाने की कोशिश ही न करें.
कहते हैं तिब्बत में कोई मरता है तो उसके शरीर को काट कर चील गिद्धों को खिलाते हैं, भारती जी का वही क्रिया कर्म हो गया लगता है. हँस के अगले अंक में यादव जी की बहादुरी की सराहना करने वाले बहुत से पत्रों को पढ़ने का इंतज़ार रहेगा. शायद आलेख की अगली किश्त भी छपे, जिसमें अन्य बातें जानने को मिलेंगी. और चाट खायेंगे, और पेट दुखेगा.
क्या करते बेचारे यादव जी, उनका कुछ दोष नहीं, पुष्पा भारती की धमकी का उत्तर तो देना ही था.
यानि लेखक भी सभी मानवों की तरह, अपने को चाहने वाले और पसंद करने वालों की तलाश में रहता है. पर किताब पढ़ कर लेखक की एक छवि मन में बना लेना और उसके प्रेम के सपने देखना या फ़िल्म देख कर अभिनेता या अभिनेत्री के सपने देखना, शायद यह कम उम्र में ही संभव होता है. सचमुच के जीवन में कितनी बार पाया कि जो लेखक या अभिनेता, किताब में या पर्दे पर इतना भाता है, सामान्य जीवन में सामान्य ही होता है, किसी बात में अच्छा लगता है और किसी बात में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता.
कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि किताबों कहानियों में बहुत अच्छा लगने वाले लेखक से जब मिलने का मौका मिला तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा. तब दुख भी होता है कि क्यों ऐसे व्यक्ति से मिला और बाद में उसकी लिखी किताब या कहानियाँ भी पढ़ने का मन नहीं करता.
अधिक प्रसिद्ध होने वाले व्यक्तियों से यह खतरा कुछ अधिक है, क्योंकि प्रसिद्ध के साथ साथ उनके सामान्य आचरण में निरंकुषता सी आ सकती है.
***
हिंदी की पत्रिका हँस को नियमित पढ़ते जाने कितने साल हो गये. पत्रिका का मेरा सबसे प्रिय हिस्सा है "मेरी तेरी उसकी बात", नयी पत्रिका आये तो सबसे पहले उसी को पढ़ता हूँ, कई बार दोबारा भी पढ़ता हूँ.
"मेरी तेरी उसकी बात" हँस के संपादक श्री राजेंद्र यादव लिखते हैं. जनवरी 2010 का हँस का नया अंक आया तो भी सबसे पहले इसी को पढ़ा. इस बार यादव जी ने "धर्मयुग" के संपादक श्री धर्मवीर भारती की पत्नी श्रीमति पुष्पा भारती से होने वाले झगड़े की बात की है. पुष्पा जी ने यादव जी की पत्नी मन्नू भँडारी से कहा कि वह अपनी पुस्तक में भारती जी बारे में लिखी किसी बात को हटा दें, क्योंकि वह गलत है. यादव जी अपने संपादकीय में अपनी पत्नी और पुष्पा जी बीच होने वाले इसी झगड़े की बात का विस्तार से सारा इतिहास बताते हैं. आरोप है भारती जी के सत्ता में होने वाले लोगों की चापलूसी का, इमरजैंसी के दौरान चुप्पी का और पहले इंदिरा-संजय वंदना का, फ़िर सत्ता पलटने पर अटल बिहारी वाजपेयी वंदना का.
आलेख को बहुत मज़े ले कर पढ़ा. किसी की बुराई हो रही हो तो चटकारे ले कर पढ़ना, मसालेदार चाट खाने से कम नहीं. आलेख में यादव जी और मन्नू भँडारी जी हैं कहानी के नायक, साथ में कुछ अन्य लोग हैं जैसे कि पंकज विष्ट. यह नायक लोग अपने आदर्शों पर बने रहे, सत्ताधारियों के आगे नहीं झुके, उनके पैसे और पुरस्कार ठुकरा दिये. दूसरी ओर सत्ता के सामने झुकने वाले, समझौता करने वालों कमज़ोर लोग हैं जिनके सरताज थे धर्मवीर भारती. इस झुकने समझौता करने वालों की लिस्ट में और भी बहुत से नाम हैं. साथ में अपने आदर्शों पर डटने के कुछ गवाहों के नाम भी हैं.
अधिक मसालेदार चाट खायी हो तो बाद में पेट में दर्द भी उठ सकता है, कुछ ऐसा ही लगा आलेख पढ़ कर.
यादव जी की लिस्ट में रघुवीर सहाय और अनीता औलक के भी नाम हैं. अनीता जी का ज़िक्र तो कुछ दिन पहले ही किया था जब मोहन राकेश जी के बारे में लिखा था. सोचा कि मोहन राकेश की मृत्यु तो 1972 में हुई थी फ़िर अनीता जी को क्यों इमरजेंसी के चक्कर में खींचा गया जिससे उन्हें सत्ता से समझौता करना पड़ा?
रघुवीर सहाय जी को बहुत सालों तक पिता के मित्र के रुप में जाना था, उनका नाम देख कर मन में अन्य बातें उठीं, अगर 1978 में इमरजैंसी के दौरान मेरे पिता जीवत होते तो क्या वह भी सत्ता से समझौता कर लेते? समझौता क्या होता है और क्यों करते हैं? आदर्शों को बना कर रखना इतना कठिन क्यों होता है? कौन करते हैं समझौता?
आलेख में धर्मवीर भारती की तो इतनी धूँआदार धुलाई की गयी है कि उनकी आत्मा छुपने की जगह खोज रही होगी. बची खुची कसर निकाली है तीस साल पहले "माया" पत्रिका में छपे आलेखों से, जिनमें भारती जी के बारे में अन्य विवरण हैं. इन सब पुराने आलेखों को हँस में दोबारा से छापा गया है. ऐसा सबूत सहित जूता मारा है कि दोबारा सिर उठाने की कोशिश ही न करें.
कहते हैं तिब्बत में कोई मरता है तो उसके शरीर को काट कर चील गिद्धों को खिलाते हैं, भारती जी का वही क्रिया कर्म हो गया लगता है. हँस के अगले अंक में यादव जी की बहादुरी की सराहना करने वाले बहुत से पत्रों को पढ़ने का इंतज़ार रहेगा. शायद आलेख की अगली किश्त भी छपे, जिसमें अन्य बातें जानने को मिलेंगी. और चाट खायेंगे, और पेट दुखेगा.
क्या करते बेचारे यादव जी, उनका कुछ दोष नहीं, पुष्पा भारती की धमकी का उत्तर तो देना ही था.
रविवार, जनवरी 10, 2010
मोहन राकेश
अंग्रेज़ी की अखबार हिंदुस्तान टाईमस में मोहन राकेश जी के बारे में छोटा से लेख देखा तो उन दिनों की याद आ गयी जब वह दिल्ली के राजेंद्र नगर के आर ब्लाक में रहते थे. तालकटोरा बाग से शंकर रोड की तरफ़ आईये तो जहाँ राजंद्र नगर प्रारम्भ होता है वहाँ बायें कोने पर पम्पोश की दुकान थी जिसकी वजह से उस सारी जगह को पम्पोश ही कहते थे. पम्पोश से आने वाली सड़क जहां आर ब्लाक के बड़े बाग से मिलती, वहीं बायें कोने वाले तीन मज़िला घर में बरसाती पर रहते थे.
उनके घर से थोड़ी दूर पर ही जंगल के सामने वाली सड़क पर मेरी बुआ का घर था. 1966-67 के आस पास ही बुआ के यहाँ छुट्टियों में गया था जब दीदी के साथ मोहन जी के घर जाने का एक दो बार मौका मिला था. तब तक उनकी कुछ कहानियाँ नाटक पढ़े थे, लेकिन इतनी समझ नहीं थी कि वह कितने बड़े लेखक हैं. मैं तब बारह या तेरह साल का था पर जब उन्हें पहली बार देखा था उसके बारे में सोचूँ तो सबसे पहली बात जो मन में आती है वह उनका कद छोटा होने की है. उनकी पत्नी अनीता, जो उम्र में उनसे बहुत छोटी लगती थीं, उनसे थोड़ी ऊँची थी. दूसरी बात याद आती है उनकी गूँजती आवाज़ में पँजाबी भाषा का पुट. तीसरी बात याद है उनका छोटा और मोटा सा सिगार पीना.
तब उनकी बेटी पुरुवा का मुँडन हुआ था और उसके बारे में सोचूं तो उसके गँजे सिर पर हाथ फ़ैरना याद आता है. दीदी, अनीता जी और मोहन जी में क्या बातें हुईं, यह सब कुछ याद नहीं क्योंकि तब अपना ध्यान खेलने की ओर अधिक होता था. हां उनके कमरे के बीच में रखी गोल नीची मेज़ याद है जिसके आसपास ज़मीन पर बैठ कर कुछ खाया था.
जब उनकी मृत्यु का सुना था तो मुझे अनीता जी और उनकी बेटी पुरुवा का ही ध्यान आया था. अनीता जी से पहले वह अन्य विवाह कर चुके थे और शायद अनीता जी उनकी धरौहर की कानूनी मालिक नहीं थीं. बच्चे छोटे हों और अचानक पिता न रहे का क्या अर्थ होता है, इसका अपना अनुभव मुझे कुछ वर्ष बाद हुआ था जब मेरे पिता भी कम उम्र में अचानक गुज़र गये थे.
पर समय सब कुछ भुला देता है. अनीता जी कहाँ गयीं, उनकी बेटी का क्या हुआ, यह कुछ भी मुझे मालूम नहीं शायद दीदी को मालूम हो.
उनके घर से थोड़ी दूर पर ही जंगल के सामने वाली सड़क पर मेरी बुआ का घर था. 1966-67 के आस पास ही बुआ के यहाँ छुट्टियों में गया था जब दीदी के साथ मोहन जी के घर जाने का एक दो बार मौका मिला था. तब तक उनकी कुछ कहानियाँ नाटक पढ़े थे, लेकिन इतनी समझ नहीं थी कि वह कितने बड़े लेखक हैं. मैं तब बारह या तेरह साल का था पर जब उन्हें पहली बार देखा था उसके बारे में सोचूँ तो सबसे पहली बात जो मन में आती है वह उनका कद छोटा होने की है. उनकी पत्नी अनीता, जो उम्र में उनसे बहुत छोटी लगती थीं, उनसे थोड़ी ऊँची थी. दूसरी बात याद आती है उनकी गूँजती आवाज़ में पँजाबी भाषा का पुट. तीसरी बात याद है उनका छोटा और मोटा सा सिगार पीना.
तब उनकी बेटी पुरुवा का मुँडन हुआ था और उसके बारे में सोचूं तो उसके गँजे सिर पर हाथ फ़ैरना याद आता है. दीदी, अनीता जी और मोहन जी में क्या बातें हुईं, यह सब कुछ याद नहीं क्योंकि तब अपना ध्यान खेलने की ओर अधिक होता था. हां उनके कमरे के बीच में रखी गोल नीची मेज़ याद है जिसके आसपास ज़मीन पर बैठ कर कुछ खाया था.
जब उनकी मृत्यु का सुना था तो मुझे अनीता जी और उनकी बेटी पुरुवा का ही ध्यान आया था. अनीता जी से पहले वह अन्य विवाह कर चुके थे और शायद अनीता जी उनकी धरौहर की कानूनी मालिक नहीं थीं. बच्चे छोटे हों और अचानक पिता न रहे का क्या अर्थ होता है, इसका अपना अनुभव मुझे कुछ वर्ष बाद हुआ था जब मेरे पिता भी कम उम्र में अचानक गुज़र गये थे.
पर समय सब कुछ भुला देता है. अनीता जी कहाँ गयीं, उनकी बेटी का क्या हुआ, यह कुछ भी मुझे मालूम नहीं शायद दीदी को मालूम हो.
शनिवार, जनवरी 02, 2010
टाँग कहाँ, हाथ कहाँ?
जब से फोटोशोप जैसे प्रोग्राम बने है, मानव शरीर को तोड़ने या जोड़ने के नये अवसर मिलने लगे हैं, जिनसे डा. फ्रेंकेस्टाईन की कहानियों की याद आ जाती है. फोटोशोप डिज़ास्टर के चिट्ठे पर उन तस्वीरों को जगह मिलती है जिनमें शरीर के अंगों को तोड़ने जोड़ने का काम कुछ विषेश सफ़ाई से किया जाता है. इस चिट्ठे से कुछ ऐसी तस्वीरों के नमूने प्रस्तुत हैं जिनमें शरीर के अंगो को तोड़ने जोड़ने में प्लास्टिक सर्जरी बहुत बढ़िया की गयी है.
इस पहली तस्वीर में देखिये और सोचिये कि इस बालिका की बायीं टांग कहाँ गयी? शायद उसे बिल्ली ले गयी?
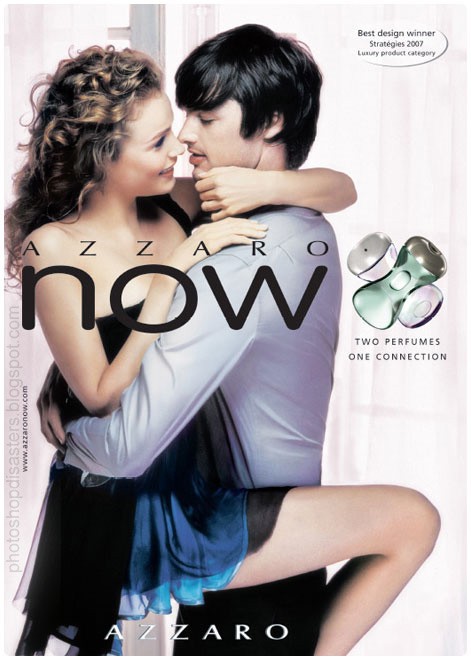
इस दूसरी तस्वीर वाली कन्या के शरीर के ऊपरी हिस्से के वस्त्र चुरा लिये गये हैं लेकिन शायद वस्त्र उतारते समय शरीर के कुछ भाग भी साथ ही चोरी हो गये थे या शायद, यह कन्या असल में कन्या का पति है?

इस तीसरी कन्या के बायें हाथ में गलती से शायद उसका पैर लगा दिया गया था?

कितनी ज़ालिम है यह माँ जिसने अपनी बड़ी बेटी को टब और दीवार के बीच में दबा कर उसकी टाँगें ही काट दीं.

इन अगले साहब की तस्वीर वैसे तो बहुत बढ़िया है लेकिन कार के दरवाज़े का हैंडल अगर किसी अन्य जगह होता तो शायद बेहतर नहीं होता?

आप सब को नववर्ष की शुभकामनाएँ.
इस पहली तस्वीर में देखिये और सोचिये कि इस बालिका की बायीं टांग कहाँ गयी? शायद उसे बिल्ली ले गयी?
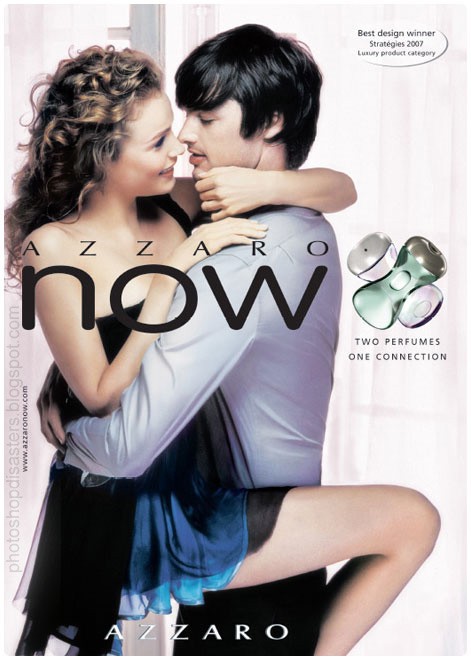
इस दूसरी तस्वीर वाली कन्या के शरीर के ऊपरी हिस्से के वस्त्र चुरा लिये गये हैं लेकिन शायद वस्त्र उतारते समय शरीर के कुछ भाग भी साथ ही चोरी हो गये थे या शायद, यह कन्या असल में कन्या का पति है?

इस तीसरी कन्या के बायें हाथ में गलती से शायद उसका पैर लगा दिया गया था?

कितनी ज़ालिम है यह माँ जिसने अपनी बड़ी बेटी को टब और दीवार के बीच में दबा कर उसकी टाँगें ही काट दीं.

इन अगले साहब की तस्वीर वैसे तो बहुत बढ़िया है लेकिन कार के दरवाज़े का हैंडल अगर किसी अन्य जगह होता तो शायद बेहतर नहीं होता?

आप सब को नववर्ष की शुभकामनाएँ.
सदस्यता लें
संदेश (Atom)
इस वर्ष के लोकप्रिय आलेख
-
हिन्दू जगत के देवी देवता दुनिया की हर बात की खबर रखते हैं, दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं जो उनकी दृष्टि से छुप सके। मुझे तलाश है उस देवी या द...
-
अगर लोकगीतों की बात करें तो अक्सर लोग सोचते हैं कि हम मनोरंजन तथा संस्कृति की बात कर रहे हैं। लेकिन भारतीय समाज में लोकगीतों का ऐतिहासिक दृष...
-
अँग्रेज़ी की पत्रिका आऊटलुक में बँगलादेशी मूल की लेखिका सुश्री तस्लीमा नसरीन का नया लेख निकला है जिसमें तस्लीमा कुरान में दिये गये स्त्री के...
-
पत्नी कल कुछ दिनों के लिए बेटे के पास गई थी और मैं घर पर अकेला था, तभी इस लघु-कथा का प्लॉट दिमाग में आया। ***** सुबह नींद खुली तो बाहर अभी ...
-
सुबह साइकल पर जा रहा था. कुछ देर पहले ही बारिश रुकी थी. आसपास के पत्ते, घास सबकी धुली हुई हरयाली अधिक हरी लग रही थी. अचानक मन में गाना आया &...
-
पिछले तीन-चार सौ वर्षों को " लिखाई की दुनिया " कहा जा सकता है, क्योंकि इस समय में मानव इतिहास में पहली बार लिखने पढ़ने की क्षमता ...
-
२५ मार्च १९७५ को भी होली का दिन था। उस दिन सुबह पापा (ओमप्रकाश दीपक) को ढाका जाना था, लेकिन रात में उन्हें हार्ट अटैक हुआ था। उन दिनों वह एं...
-
ईसा से करीब आठ सौ वर्ष पहले, इटली के मध्य भाग में, रोम के उत्तर-पश्चिम में, बाहर कहीं से आ कर एक भिन्न सभ्यता के लोग वहाँ बस गये जिन्हें एत्...
-
कुछ सप्ताह पहले आयी फ़िल्म "आदिपुरुष" का जन्म शायद किसी अशुभ महूर्त में हुआ था। जैसे ही उसका ट्रेलर निकला, उसके विरुद्ध हंगामे होने...
-
भारत की शायद सबसे प्रसिद्ध महिला चित्रकार अमृता शेरगिल, भारत से बाहर कला विशेषज्ञों में उतनी पसिद्ध नहीं हैं, पर भारतीय कला क्षेत्र में उनका...







