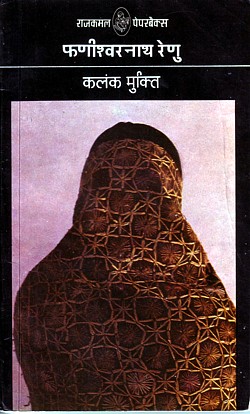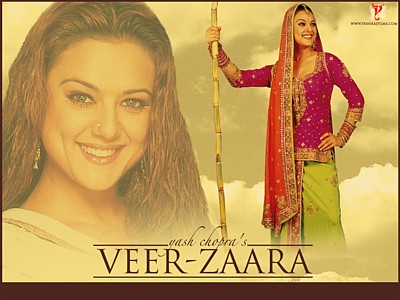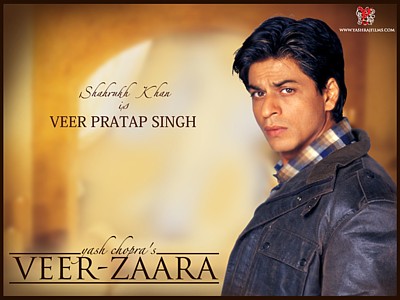अपनी मर्जी से, बिना विषेश निमंत्रण के किसी सभा आदि में किसी को सुनने जाऊँ यह बहुत कम होता है. पर जब सुना कि हमारे शहर से करीब सौ किलोमीटर दूर, फैरारा शहर में देश विदेश के पत्रकार और लेखक जमा हो रहे हैं तो वहाँ जाने की मन में उत्सुक्ता हुई और काम से छुट्टी ले कर तीन दिन वहाँ बिताये.
शहर में कई जगहों पर फोटोपत्रकारों के चित्रों की प्रदर्शनियाँ लगीं थीं जिनमें से मुझे इतालवी फोटोग्राफर फ्राँचेस्को जुजोला के युद्ध और मृत्यू के क्षणों की तस्वीरें बहुत प्रभावशाली लगीं. शब्दों से युद्ध के कारण या हाल के बारे में लिखने वाले पत्रकार स्थूल तथ्यों की जानकारी दे सकते हैं पर युद्ध का मानव जीवन पर क्या असर हो सकता है, इसके लिए जो बात एक अच्छी तस्वीर कह सकती है वह हजार शब्द भी नहीं कह पाते, यह मेरा विचार है.

ब्राजील के सुप्रसिद्ध पत्रकार मीनो कार्ता, वेनेजुएला की पत्रकार क्रिस्तीना मरकानो और मेक्सिको के पत्रकार उगो पिपीतोने की दक्षिण अमरीका में आज के बड़े वामपंथी नेताओं के बारे में बहस बहुत दिलचस्प लगी. बहस के मुख्य विषय थे ब्राजील के राष्ट्रपति लूला और वेनेजुएला के उगो शावेज. लूला जनप्रिय हैं, कुछ अच्छा काम भी कर रहे हैं, पर वह वामपंथी नेता नहीं हालाँकि राजनीति में आने से पहले कामगारी यूनियन के नेता थे, बल्कि वह बड़े बिसनेस के फायदे के लिए ही अधिक काम कर रहे हैं, यह निष्कर्श था मीनो कार्ता का. शावेज जी तानाशाह हैं, मिलेट्री से आये हैं, वह प्रेस की स्वतंत्रता का मुख बाँध रहे हैं पर साथ ही उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य सम्बंधी नीतियों से गरीब लोगों को सहायता मिली है, यह निष्कर्श था क्रिस्तीना का.
ब्लोग और अंतर्जाल के पत्रकारिता में बढ़ते महत्व पर बहस में मुझे फ्राँस के पियर्र हस्की और चीन के विद्यार्थी नेता काई छोंगवो, जो अब चीन छोड़ कर विदेश में रहने को बाध्य हैं, की बातें अच्छी लगी. बात हो रही थी कि अगर तियानामेन स्कावयर की बात आज होती तो क्या चीन की सरकार उसे इतनी आसानी से दबा पाती? उनका कहना था कि बाजार तथा उपभोक्तावादी संस्कृति से प्रभावित उदारवादी नीति अपनाने से चीन में इंटरनेट का तेजी से विकास हुआ है पर साथ ही चीन की सरकार ने इस माध्यम को किस तरह से काबू में रखा जाये, कैसे लोगों को इंटरनेट के भीतर एक सीमा में बाँध कर रखा जाये इस दिशा में बहुत तकनीकी विकास किया है जितना अन्य किसी देश में नहीं हुआ. इसके बावजूद चीनी ब्लागर और अतंर्जाल प्रयोग करने वाले नये नये तरीके निकलते रहते हें ताकि वह बँधनों से बाहर निकल सके.

बर्मा में मिल्ट्री तानाशाहों द्वारा देश में होने वाली बातों को बाहर जाने से रोकने की कोशिश करने के बारे में उनका विचार था कि दमन की प्रशासन कुछ दिनों में ही दमन की तीव्रता कम करने को बध्य होगा और धीरे धीरे समाचार फ़िर से आने लगेगें.
डाकूमेंट्री फ़िल्मों में मुझे अमरीकी फिल्म निर्देशक जेसन दा सिल्वा की फ़िल्म "हम भूल न जायें" (Lest we forget, 2003) अच्छी लगी. द्वितीय महायुद्ध के दौरान अमरीका में रहने वाले जापानियों का दमन और सितंबर 2001 में न्यू योर्क में हुए बम विस्फोटों के बाद अरब देशों और पाकिस्तान से आये नागरिकों के विरुद्ध हुए व्यवहार के बारे में थी यह फिल्म.
उपन्यास लिखने वाले लेखकों से उपन्यास और पत्रकारिता के दायरों के बारे में बातचीत भी बहुत दिलचस्प लगी. इसमें भाग लेने वालों में से मुझे मोरोक्को की लैला लालामी, तुर्की की एलिफ शफाक और भारत की अरुँधति राय की बातें मुझे अच्छी लगीं. लैला का कहना था कि क्योंकि वह मुसलमान हैं और मध्यपूर्व के देश से हैं, इसलिए बड़ी किताब छापने वाले पब्लिशिंग कम्पनियाँ उनसे केवल मुसलमान स्त्रियों का कितना बुरा हाल है इस विषय पर लिखना माँगती हैं और उनकी किताबों पर केवल बुर्का पहनने वाली औरतों या रेगिस्तानों और ऊँटों की तस्वीरें ही लगती हैं. एलिफ ने बात की अपने विभिन्न देशों में यहाँ से वहाँ बिताये अपने बचपन की जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि उनकी जड़ें धरती में नहीं गड़ी बल्कि वह उल्टा पेड़ हैं जिसकी जड़े हवा में हैं. उन्होंने कहा कि लेखन तो लेखक की कल्पना पर निर्भर करता है, कि अगर वह तुर्की की नारी हो कर भी नोर्वे में रहने वाले समलैंगिक व्यापरी को ले कर कहानी लिखना चाहें या अमरीकी अश्वेत पुरुष के जीवन के बारे में लिखना चाहें, उन्हें इसका पूरा अधिकार है और वह कोई भी बँधन मानने को तैयार नहीं कि उन्हें किस विषय पर लिखना चाहिये और किस तरह!
अरुँधति राय जी का बोलने का तरीका बहुत प्रभावशाली है और उनके बोलने के दौरान खचाखच भरा हाल बार बार तालियों से गूँज उठा. अपने अँग्रेजी में लिखने के बारे में उन्होने लंदन में बीबीसी टेलिविजन के बारे में हुए एक साक्षात्कार के बारे में बताया. बुक्कर पुरस्कार मिलने के बाद हो रहे इस साक्षात्कार में उनके साथ एक अंग्रेजी प्रोफेसर भी थे जिनकी सारी बात ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बने देशों को क्या फायदा हुआ और किस तरह अंग्रेजी सभ्यता ने इन पिछड़े देशों की सभ्यताओं को सही दिशा दी, फ़िर अरुँधती की ओर बोले कि उन्हें बुक्कर पुरस्कार मिलना ब्रिटिश साम्राज्य की छोड़ी धरोहर का ही नतीजा है. अरुँधती बोली कि इस तरह की बात करना कुछ वही बात हई कि बलात्कार की बाद पैदा हुई संतान को दिखा कर बलात्कार हुई औरत से कहा जाये कि देखो उस पुरुष ने कुछ ठीक ही किया था. उनकी कही बहुत सी बातों से मन में बहुत से प्रश्न उठे, पर उनके बारे में तो अलग से फ़िर कभी लिखना पड़ेगा.