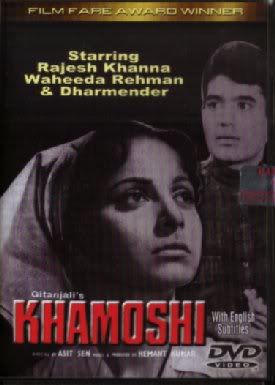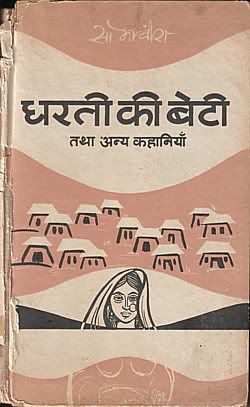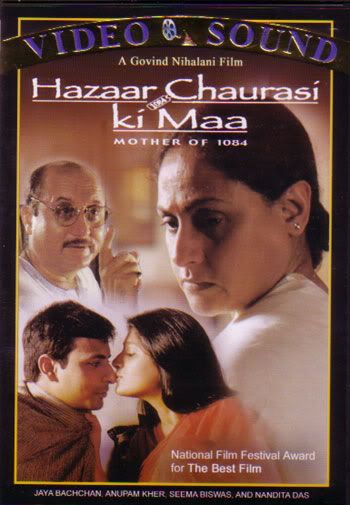रोम के भारतीय दूतावास पर प्रवासी भारतीय नागरिकता के कार्ड के लिए अपने और पुत्र के कागज़ जमा करवाने थे, सुबह सुबह बोलोनिया से गाड़ी में हम लोग निकले, मैं, पुत्र और पुत्रवधु. तीन महीने हो गये पुत्रवधु को इटली आये, सोचा कि काम समाप्त होने के बाद रोम की सैर भी जाये तो चार घँटे की जाने की और चार घँटे की वापस आने की यात्रा का कुछ लाभ होगा.
भारतीय दूतावास पहुँचते पहुँचते ग्यारह बजने लगे थे. छोटे से तँग गलियारे से घुसने का रास्ता, अँदर वीसा लेने वाले विदेशियों और पासपोर्ट नये बनवाने वाले भारतीयों की भीड़, उमस भरी गर्मी में छत पर टँगा धीरे धीरे घूमता पँखा, और ऊपर दफ्तर में फाईलों के पहाड़ों के पीछे छुपे बाबू लोग, यानि अगर भारत जाने के लिए पैसे न हों और मातृभूमि की बहुत याद आ रही हो तो दूतावास में घुसते ही लगता है कि दिल्ली के किसी सरकारी दफ़्तर में ही पहुँच गये हों. पर एक महत्वपूर्ण अंतर था, प्रवासी भारतीय नागरिकता के जिम्मेदार व्यक्ति का हमसे इज्जत से बात करना और सब कुछ ठीक से समझाना. हालाँकि भीड़ बहुत थी पर इंतज़ार भी बहुत अधिक नहीं करना पड़ा सब काम पूरा करने में.
काम पूरा करके सारी दोपहर और शाम रोम घूमने में निकल गयी. पहले कोलोसियम, फ़िर रोम के प्राचीन सम्राट के महलों के खँडहर, फ़िर मार्को आउरेलियो का भव्य भवन काम्पी दोलियो जहाँ आजकल नगरपालिका का दफ़्तर है और कला सँग्रहालय भी है, फ़िर युद्ध में मरे सैनिकों की याद में बने विटोरियानो, फ़िर नाव के आकार में बना नवोना चौबारा और त्रेवी का फुव्वारा, फ़िर वेटीकेन में सेंट पीटर. पाँच छहः घँटों में रोम के एक कोने से दूसरे कोने तक पर्यटकों के लिए सभी महत्व वाले स्थानों को बाहर बाहर से देख चुके थे. बस अब और कुछ नहीं होगा, वापस बोलोनिया की ओर चलना चाहिए सोच कर उस कार पार्क की तरफ़ लौटे जहाँ गाड़ी रखी थी.
चलते चलते तो मालूम नहीं हुआ था पर गाड़ी में बैठते ही दर्द की आह को नहीं रोक पाया. हल्का सा थैला था कँधे पर जिसमें दूतावास के कागज़ और कैमरा थे, वह दर्द से जकड़ गया था, दोनों घुटनों का बाजे अलग बज रहे थे. पुत्र और पुत्रवधु थके अवश्य थे पर मेरी तरह दर्द से नहीं कराह रहे थे. घर पहुँचते रात के ग्यारह बज रहे थे और शरीर का कोई अंग ऐसा नहीं था जहाँ दर्द न हो रहा हो, सी सी करते सीढ़ियाँ चढ़ीं. रात को पत्नी ने बाम लगा कर कँधे, कमर और टाँगों की मालिश की और बोली, "अब बचपना छोड़ो और अपनी उम्र को याद रखो. अब बच्चे नहीं हो कि कुछ भी भागा दौड़ी कर लो, हड्डियाँ माँस पेशियाँ अपनी उम्र दिखाने लगी हैं, उनका नहीं सोचेगो तो रहे सहे से भी जाते रहोगे."
*****
शायद यह जोड़ों में हो रहे दर्द का असर था, या फ़िर बिना वजह कभी कभी अचानक मन में आ जाने वाली उदासी का असर था.
ओम थानवी जी का
निर्मल वर्मा की मृत्यू पर लिखे आलेख को पढ़ कर मन बार बार मृत्यु और गुजरते समय के बारे में सोच रहा था. भारत में रहते हुए मृत्यु को भुलाना आसान नहीं है, जीवन और मृत्यु दोनो ही अपनी पूरी शक्ति के साथ जीवन के हर पहलू में घुले मिले हैं. किसी के दाह संस्कार पर जाईये तो अग्नि में भस्म होते शरीर को देख कर समझ आता है कि मृत्यू जीवन का ही दूसरा पहलू है, उसका अभिन्न अंग.
पर किसी के दाह संस्कार में गये बरसों बीत गये हैं. हर बार भारत जाओ तो मालूम है ये नहीं रहे या वे नहीं रहे. नाना नानी, बुआ फूफा, मौसी, मित्र. पर सबके समाचार मिले जब भारत से दूर था. और इटली में पत्नी के परिवार में या फ़िर जान पहचान के लोगों में जब भी किसी की मृत्यु हुई तो मैं कहीं विदेश यात्रा में था. हालाँकि इसाई कब्र में रखते शरीर की छवि में मुझे वह दाह संस्कार वाली "यही अंत है, धूल में मिल गया सब फ़िर से" जैसी बात कम लगती है पर यहाँ भी मुझे किसी प्रियजन की मृत्यु पर साथ रहने का मौका नहीं मिला.
ओम जी ने अपने आलेख में लिखा है, "हम चिता की बगल में एक पत्थर की बैंच पर बैठे हुए थे. चिता की राख और आँच रह रह कर इसी तरफ़ आती थी. हर झोंका आग की लपटों के साथ यादों के अनगिनत थपेड़े साथ लाता था. मेरी सूनी नज़र चिता पर टिकी थी, बल्कि उनके कपोल पर..." . पढ़ कर झुरझुरी सी आ गयी.
यहाँ जीवन में लगता है कि मौत जैसे है ही नहीं, जैसे हम सब शास्वत अंतहीन जीवन का वरदान पाये हुए हैं, यह करो, वह बनाओ, इसको कैसे काटो, उसको कैसे नीचा दिखाओ, जवान लगो, पतले लगो, स्वस्थ रहो, यह खाओ, यह न खाओ, अंतहीन चक्कर जिसमें मृत्यु कहीं भूलभुल्लियाँ में छुपी हुई है, उसकी कोई बात न करो, लगना चाहिए कि वह है ही नहीं और शायद वह सचमुच खो ही जायेगी!
यमराज का नचिकेता को उत्तर, "सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिवाजायते पुनः" मानो हमारे ऊपर नहीं लागू होता, वह तो केवल अन्य लोगों के लिए बना है. पर जब शरीर आने वाली वृद्धावस्था के संकेत महसूस करने लगता है, तो शायद हमें उस आने वाले अंतिम पल के बारे में भी सोचना चाहिए, उसकी तैयारी करनी चाहिए?
जब तक कमर, कँधे और टाँगों का दर्द कम हुआ तो बिस्तर पर लेटे लेटे यही सब विचार मन में आ रहे थे.
*****
पुस्तकालय जा रहा था तो बस स्टाप वह दिखा. करीब आ कर उसने धीरे से पूछा, "आप पाकिस्तान से हैं क्या?"
"नहीं मैं भारत से हूँ, क्या आप पाकिस्तान से हैं?" मैंने पूछा. यहाँ बोलोनिया में भारतीय बहुत कम हैं और पाकिस्तानी बहुत अधिक इसलिए अपने जैसा चेहरा दिखे तो पहला विचार यही मन में आता है कि "पाकिस्तानी होगा". वह मुस्कुरा कर बोला, "नहीं मैं भी इंडिया से हूँ, होशियार पुर से".
साथ में बस में सफ़र करते करते उसने अपनी कहानी सुनाई. दसवीं पास है वह और मेटल का काम जानता है. 29 साल का है पर देखने में बहुत छोटा लगता है. सोलह महीने की यात्रा की है उसने यहाँ पहुँचने के लिए. पंजाब में बरोड़ नाम के किसी एँजेंट को पाँच लाख रुपये दिये और रूस में मोस्को पहुँचा, जहाँ पाँच महीने जेल में रहा. फ़िर एँजेंट के किसी आदमी ने जेल से निकलवाया. फ़िर यूक्रेन पहुँचा, वहाँ अन्य पाँच महीनो के लिए जेल. फ़िर किसी ने जेल से निकलवाया. यात्रा उसे अन्य कई देश ले गयी जिनके बारे में वह कुछ अधिक नहीं बता पाता. अंत में समुद्र में लहरों से लड़कर छोटी सी नाव में पहुँचा इटली की सीमा रक्षा करने वालों के हाथ यहाँ की एक जेल में. किसी मानव अधिकारों की बात करने वाले ने बाहर निकलने में सहायता की और शरणार्थी के फोर्म भरने की सहायता की. अब उसे कोई भारत वापस नहीं भेज सकता, क्योंकि वह किसी को नहीं बताता कि उसका पासपोर्ट और कागज़ कहाँ हैं और बिना कागजों के न तो भारत उसे स्वीकारेगा न पाकिस्तान. आजकल श्रीलँका के एक व्यक्ति के साथ रहता है और काम खोज रहा है. तब तक भूखा न मरने के लिए घर से पाँच सौ यूरो मँगवाये हैं.
उसकी आँखों में आशावान जीवन चमकता है, "एक बार काम मिल जायेगा तो घर की दरिद्री दूर हुई समझो, सब ठीक हो जायेगा. सब काम करने को तैयार हूँ, कुछ भी थोड़ा सा दे दो. कोई काम हो तो बताईयेगा."
साथ आने वाले कितने मरे और कितनों ने यह यात्रा पूरी की, पूछने का साहस नहीं हुआ. हर रोज़ टीवी पर समुद्र में गैरकानूनी आने वालों के मरने के समाचार बताते हैं, वह किसमत वाला है, मरा नहीं, जीवित पहुँच गया. जीवन जीवित रहने के लिए हिम्मत नहीं हारता, एक मुठ्ठी भर जगह चाहिए उसे, बस खड़ा होने भर की, जिंदा रहने के लिए पत्थर में भी जड़े खोद कर पानी खोज लेगा.
*****
रोम यात्रा से कुछ तस्वीरें प्रस्तुत हैं.