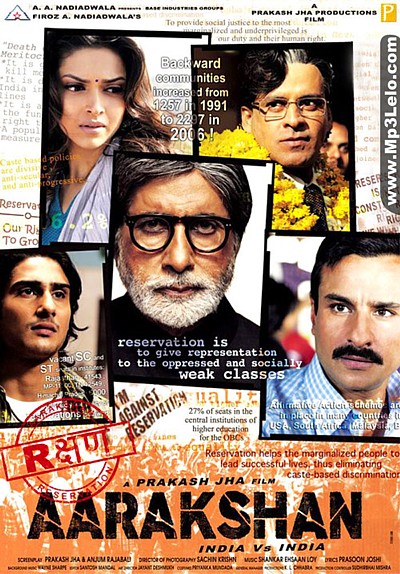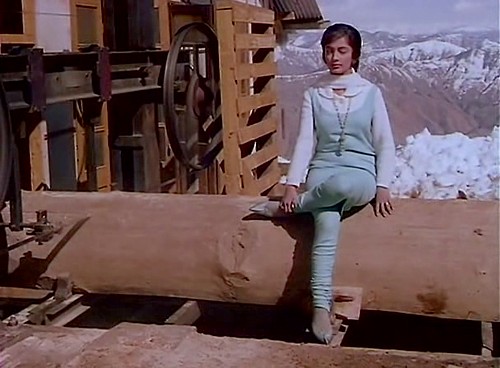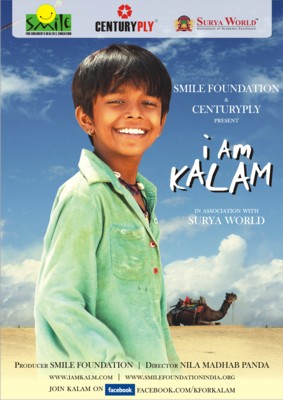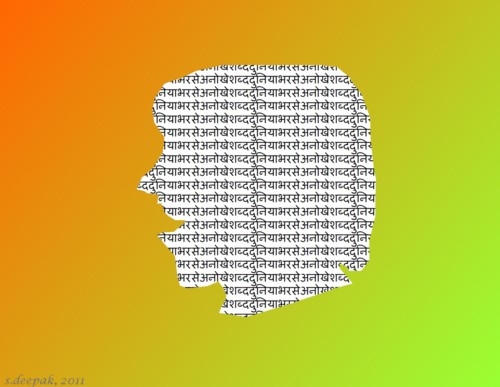"संग्रहालय के मूल्य को केवल खर्चे और फायदे में मापना गलत है, उसकी कीमत को मापने के लिए उसके उद्देश्य को मापिये. उसका उद्देश्य है जनता को नागरिक बनाना." यह बात कह रहे थे रोम के
वेटीकेन संग्रहालय के निर्देशक श्री
अन्तोनियो पाउलूच्ची (Antonio Paolucci).
श्री पाउलूच्ची इन दो शब्दों, जनता और नागरिक, को विषेश अर्थ देते हैं. "जनता" यानि एक जगह पर रहने वाले लोग और "नागरिक" यानि वह लोग जो अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझते हैं, जिनके लिए जीवन में सभ्य होने का महत्व हो, जिनमें अपनी कला, संगीत, लेखन, शिल्प को जानने की समझ हो. लेकिन आज के भूमण्डलिकृत जगत में जहाँ पूँजीवाद के आदर्शों से स्वास्थ्य, शिक्षा, आदि जनकल्याण सेवाओं को मापते हैं, सभ्यता के मापदँड भी अधिकतर खर्चे और फायदे में गिने जाते हैं. उसे नागरिक अधिकार मानना कोई कोई विरला शहर ही कर पाता है, जैसे कि लंदन जहाँ सभी संग्रहालय मुफ्त हैं, अपनी कला और सभ्यता को जानने के लिए आप को कोई टिकट नहीं खरीदना पड़ता.
मैं श्री पाउलूच्ची की बात से सहमत हूँ कि अपनी कला, संस्कृति को बाज़ार के मापदँड से नहीं, सभ्यता के मादँड से तौलना चाहिये. पर यही काफ़ी नहीं. साथ ही, मुझे यह भी लगता है कि कला और सभ्यता की बातों को विषेशज्ञों के बनाये पिँजरों से बाहर निकाल कर जनसामान्य के लिए समझने लायक बनाया जाये. वह कहते हैं कि कला सँग्रहालयों को मैनेजरों की नहीं, कला को समझने वाले निर्देशकों की आवश्यकता है, जो नफ़े नुक्सान की बातों से ऊपर उठ सकें.
बदलते परिवेश में पर्यटक बदल गये हैं जिसके बारे में पाउलूच्ची कहते हैं, "आज कल चार्टर उड़ानों से अलग अलग देशों के बहुत से पर्यटकों के गुट आते हैं. उनके पास रोम घूमने के लिए एक ही दिन होता है, जिसमें से वह लोग एक डेढ़ घँटा वेटीकेन संग्रहालय को देखने के लिए रखते हैं. उनके पास संग्रहालय के अमूल्य चित्रों या शिल्पों की कोई कीमत नहीं, क्योंकि उनके पास कुछ देखने का समय नहीं है. उन्हें देखना होता है केवल सिस्टीन चेपल में माईकल एँजेलो की कलाकृति को. वह लोग संग्रहालय में भागते हुए घुसते हैं, सिस्टीन चेपल देख कर, सेंट पीटर के गिरजाघर की ओर भागते है. फ़िर कोलोसियम देखो, त्रेवी का फुव्वारा देखो, स्पेनी सीढ़ियाँ देखो, बस रोम हो गया. अब बारी है अगले शहर जाने की."
यह सच है कि विदेश घूमते हुए थोड़े दिनों की छुट्टियाँ होती हैं, रहने घूमने के खर्चे भी भारी होते हैं. तो बस यही चिन्ता रहती है कि कैसे जानी मानी प्रसिद्ध चीज़ें देखीं जायें. बाकी सबको देखना समझना मुमकिन नहीं होता. मेरे विचार में असली प्रश्न है कि जिन शहरों में हम रहते हैं क्या वहाँ के इतिहास को जानते समझते हैं, वहाँ के कला संग्रहालयों को देखने का समय होता है हमारे पास?
जब बात संग्रहालयों की हो रही हो तो कला और शिल्प को कैसे जाना और समझा जाये, इसकी बात करना उतना ही आवश्यक है. और मेरे विचार में इस बात को खर्चे और फायदे की बात करने वाले मैनेजरों ने भी समझा है, चाहे वह अपने स्वार्थवश ही समझा हो. यानि पैसे बनाने के लिए, कला और सभ्यता का भला करने के लिए नहीं.
बचपन में स्कूल के साथ कभी दिल्ली के कुछ संग्रहालयों को देखने का मौका मिला था, लेकिन सामने गुज़रने भर से क्या समझ में आता? कोई बताने समझाने वाला नहीं था. कुछ साल पहले एक बार इंडियागेट के पास पुरात्तव संग्रहालय में गया था लेकिन तब भी वहाँ संग्रहालय की विभिन्न कलाकृतियों को समझने के लिए कोई गाइड या किताब आदि नहीं थे. वहाँ जो कुछ देखा उसका हमारे समाज और संस्कृति के लिए क्या अर्थ था? हमारी संस्कृति में क्या स्थान था उस पुरात्तव इतिहास का, यह सब समझने की कोई जगह नहीं थी.
जब विभिन्न देशों में घूमने का मौका मिला तो भी शुरु शुरु में समझ नहीं थी कि कला, इतिहास या पुरात्तव को उसकी सन्दरता देखने के अतिरिक्त, और गहराई से जानना और समझना भी दिलचस्प हो सकता था. वाशिंगटन का आधुनिक कला का संग्रहालय, अमस्टरडाम का वान गोग संग्रहालय, लंदन की टेट गेलरी, जैसे जगहें देखीं पर तब बात वहीं तक जा कर रुक जाती थी कि कौन सी कलाकृति देखने में अच्छी लगती है.
फ़िर एक बार मेरे मन में कुछ आया और मैंने "खुले विश्वविद्यालय" के "कला को कैसे समझा जाये" के कोर्स में अपना नाम लिखवा लिया. इस कोर्स की कक्षाएँ रात को होती थी. दिन भर काम के बाद रात को कक्षा जाने में नींद बहुत आती थी. कई बार मैं कक्षा में ही सो गया. फिर भी, उस कोर्स का कुछ फ़ायदा हुआ. यह समझ आने लगी कि कला को समझने के लिए उसके कलाकार को और जिस परिवेश में उस कलाकार ने जिया और वह कृति बनायी, उसे समझना उतना ही आवश्यक है. समझ आने लगा कि संग्राहलय में जो देखो, उसकी सुन्दरता के साथ साथ, उसके बारे में भी जानो और समझो, तो संग्रहालयों से किताबे खरीदना प्रारम्भ किया.
पिछले दस वर्षों में इंटरनेट के माध्यम से संग्रहालय, कला और शिल्प को समझने के अन्य बहुत से रास्ते खुल गये हैं. जब भी किसी नये संग्रहालय में जाने का मौका मिलता है तो पहले उसके बारे में, वहाँ की प्रसिद्ध कलाकृतियों के बारे में पढ़ने की कोशिश करता हूँ. वहाँ जा कर जो कुछ अच्छा लगता है उसकी बहुत सी तस्वीरें खींचता हूँ. घर वापस आ कर, उन तस्वीरों के माध्यम से कलाकृतियों और कलाकारों के बारे में जानने की कोशिश करता हूँ. कई बार इस तरह से उन कलाकृतियों के बारे में मन में और जानने समझने की इच्छा जागती है तो वापस संग्रहालय जा कर उन्हें दोबारा देखने जाता हूँ.
शायद यही वजह है कि आजकल दुनिया के बहुत से आधुनिक संग्रहालयों में तस्वीर खींचने से कोई मना नहीं करता, बस फ्लैश का उपयोग निषेध होता है. पहले लोग सोचते थे कि संग्रहालय की हर वस्तु को गुप्त रखना चाहिये, तभी लोग आयेंगे. संग्रहालय चलाने वाले लोग सोचते थे कि अगर लोग तस्वीर खींच लेंगे तो उनके मित्र तस्वीरें देख कर ही खुश हो जायेंगे, संग्रहालय नहीं आयेंगे. इसलिए वहाँ फोटो खींचने की मनाई होती थी. तस्वीरें, कार्ड आदि कुछ भी हो, उसे आप केवल संग्रहालय की दुकान से मँहगा खरीद सकते थे.
आज के संग्रहालयों को समझ आ गया है कि जो लोग वहाँ घूमते हुए तस्वीरें खींचते हैं, वही लोग बाद में उन्हें फेसबुक, फिल्क्र, चिट्ठों आदि के द्वारा अपने मित्रों व अन्य लोगों में उस संग्रहालय का मुफ्त में विज्ञापन करते हैं. जितनी तस्वीरें अधिक खींची जाती हैं, उतना विज्ञापन अधिक होता है, और अधिक लोग वहाँ जाने लगते हैं.
पैसा कमाने के लिए संग्रहालयों को नये तरीके समझ में आये हैं, जैसे कि विभिन्न कलाकारों की कला को समझने के लिए उसके बारे में किताबें, पोस्टर, प्रिंट आदि और संग्रहालय में बने काफ़ी हाउस, बियर घर और रेस्टोरेंट.
यह सच है कि ग्रुप यात्रा में निकले लोगों के पास समय कम होता है, बस कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को ही देख सकते हैं. लेकिन मेरे विचार में ग्रुप यात्रा के बढ़ने के साथ साथ, दुनिया में कला को अधिक गहराई से समझने वाले भी बढ़ रहे हैं, जो अब इंटरनेट के माध्यम से कला और इतिहास को इस तरह समझ सकते हैं जैसे पहले मानव इतिहास में कभी संभव नहीं था.
इसका एक उदाहरण है दिल्ली के पुरात्तव संग्रहालय में मोहनजोदारो और हड़प्पा से मिली प्राचीन मुद्राएँ. जब उन्हें देखा था तो वह मुद्राएँ केवल छोटे मिट्टी के टुकड़े जैसी दिखी थीं, उनमें कुछ दिलचस्प भी हो सकता है, यह समझ नहीं आया था. आज टेड वीडियो पर
प्रोफेसर राजेश राव का यह वीडियो देखिये. उन मुद्राओं को देख कर उन्हें समझने की उत्सुकता अपने आप बन जाती है.
कलाकार और उसके परिवेश को जानने से, उसकी कला को समझने की नयी दृष्टि मिलती है, इसका एक उदाहरण है
श्री ओम थानवी द्वारा लिखा वान गोग की एक कलाकृति "तारों भरी रात" का विवरण. किसी संग्रहालय में वान गोग के चित्र देखने का मौका मिल रहा हो, तो पहले इसे पढ़ कर देखिये, कला को समझने की नयी दृष्टि मिल जायेगी.
पर इस तरह कला को देखने, समझने का जिस तरह का मौका आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बन गया है वैसा पहले कभी नहीं था, जिसका एक उदाहरण है
गूगल द्वारा संग्रहालयों की प्रसिद्ध कलाकृतियों को देख पाना.
भारत में कला के बारे में, संग्रहालयों के बारे में कैसे जानकारी मिलेगी, यह अभी आसान नहीं हुआ है. भारत के कौन से प्रसिद्ध चित्रकार हैं, किसी अच्छे भले, पढ़े लिखे व्यक्ति से पूछिये तो भी आप को अमृता शेरगिल, मकबूल फिदा हुसैन आदि दो तीन नामों से अधिक नहीं बता पायेगा. हेब्बार, राम कुमार, बी प्रभा जैसे नाम कितनों को मालूम हैं? काँगड़ा और राजस्थानी मिनिएचर चित्रकला शैलियों की क्या विषेशताएँ हैं, शायद लाखों में एक व्यक्ति भी नहीं बता सकेगा.
भारत के प्रसिद्ध शिल्पकार कौन हैं तो शायद कुछ लोग अनिश कपूर का नाम ले सकते हैं क्योंकि वे लंदन में प्रसिद्ध हैं. कैसे कला में पैसा लगाना आज फायदेमंद है, इस पर फायनेन्शियल टाईमस या बिजनेस टुडे पर लेख मिल जायें, पर आम टीवी कार्यक्रमों में भारतीय कलाकारों की कला को कैसे समझा जाये, इसका कोई कार्यक्रम क्या आप ने कभी देखा है? जब तक किसी कलाकार की बिक्री लाखों करोड़ों में न हो, या उसे विदेश में कुछ सम्मान न मिले, लगता है कि भारत में उसका कुछ मान नहीं.
भारतीय पुरात्तव विभाग की वेबसाईट तो हिन्दी में भी है लेकिन वहाँ पर आप को केवल प्रकाशनों की लिस्ट मिलेगी. इंटरनेट पर पढ़ने वाली किताबों पत्रिकाओं की लिंक अंग्रेज़ी वाले हिस्से में हैं. तस्वीरों की गैलरी है, लेकिन उनमें जगह के नाम के सिवा, उसे जानने समझने के लिए कुछ नहीं. वैसे तो भारत दुनिया भर के क्मप्यूटरों की क्राँती का काम कर रहा है तो आशा है कि भारतीय पुरात्तव विभाग की वेबसाईट को भी अच्छा होने का मौका मिलेगा.
दिल्ली के
राष्ट्रीय संग्रहालय की वेबसाईट केवल अंग्रेज़ी में है और उसपर उपलब्ध जानकारी बहुत सतही है. तस्वीरें छोड़ कर किसी तरह की समझ बढ़ाने वाली जानकारी नहीं मिलती. वेबसाईट पुराने तरीके की है, उसे देख कर नहीं लगता कि यह भारत के सबसे प्रमुख संग्रहालय का परिचय दे सकती है.
दिल्ली के राष्ट्रीय कला संग्रहालय की
वेबसाईट देखने में बहुत सुन्दर है, और हिन्दी में भी है. वेबसाईट पर संग्रहालय के विभिन्न संग्रहों की कुछ सतही जानकारी भी है, लेकिन सभी प्रकाशन केवल खरीदने के लिए ही हैं, इंटरनेट से कलाकारों और कला के बारे में जानकारी सीमित है.
अगर हमारी संस्कृति, सभ्यता को जनसामान्य तक पहुँचाना आवश्यक है तो भारतीय संग्रहालय और पुरात्तव विभागों को इंटरनेट के माध्यम से नये कदम उठाने चाहिये, ताकि जनता में अपने इतिहास और कला को जानने समझने की इच्छा जागे.
***
नीचे की मेरी खींची तस्वीरें दुनिया के विभिन्न देशों में संग्रहालयों से हैं.