अमरीका में जाह्न होपकिनस में एक कोर्स करने गया था, सन 1989 में. वह पहला मौका था कि एडस के रोगियों को करीब से देखने का मौका मिला था. तब तक पश्चिमी संसार में एडस के बारे में बहुत शोर हो रहा था. तब इस रोग का संक्रमण अधिकतर समलैंगिक यौन सम्बंधों के साथ जुड़ा था. उस समय यह तो समझता था कि समलैंगिक सम्बंध क्या होते हैं पर "समलैंगिक सभ्यता" क्या होती है यह पहली बार करीब से देखने का मौका मिला.
कोर्स के दौरान कुछ समलैंगिक युगलों से मिल कर बात करने का मौका मिला जिनमें से एक को एडस का रोग था. इन मुलाकातों ने मन में बने समलैंगिक रिश्तों के बारे में बैठे विश्वासों को हिला दिया था. सोचता था कि समलैंगिक सम्बंध रखने वाले युवक किसी के साथ प्रेम नहीं, बल्कि जितने अधिक शारीरिक सम्बंध हो सकते हैं सिर्फ वही खोजते हैं.
उस समय इस रोग के फ़ैलने के बारे में जानकारी बहुत अधिक नहीं थी, और बाहर से छुपाने की कोशिश करने के बावजूद, मन में किसी रोगी के करीब जाने या छूने में बहुत डर लगता था. रोगियों के प्रति कैसे अमानवीय व्यवहार हो रहे हैं, इसकी बात उठती तो मन में अपने डर के प्रति क्षोभ उठता पर फ़िर भी डर पर पूरा काबू नहीं कर पाता. ऐसे में जो रोगी नहीं थे उनका अपने रोगी साथियों के प्रति प्रेम देख कर विश्वास नहीं होता था कि उन्हें इस तरह रोगी के साथ रहने में डर नहीं लगता?
तब से विभिन्न देशों में एडस के रोगियों को करीब से देखने का मौका मिला है. आज एडस के बारे में सोचूँ तो मन में समलैंगिक शब्द नहीं आता, बल्कि अफ्रीका के गाँव आते हैं जहाँ नवजवान पीढ़ी की फसल को इस रोग ने काट दिया है और पूरे गाँव में केवल बूढ़े और बच्चे दिखते हैं जिनमें खेतों में काम करने की शक्ति नहीं है. कितने ही मित्र जो अफ्रीका में डाक्टर और नर्स थे, पिछले सालों इस रोग की वजह से खो चुके हैं. कुछ को आज यह बीमारी है और सबको एआरवी दवाईयाँ नहीं मिल पाती.
पर आज इस बीमारी का विश्व प्रतिमान भारत को मिल गया है, जहाँ दुनिया के सबसे अधिक रोगी हैं. निरंतर के माध्यम से मुझे इस स्थिति पर लिखने का मौका मिला है. नया निरंतर कल 7 अगस्त से अंतरजाल पर एक साल के अंतराल के बाद नया रुप ले कर फ़िर से आया है, उसे पढ़ना न भूलियेगा.
*****
आषीश, तुम्हारी टिप्पणी के लिए धन्यवाद. तुमने ठीक ही कहा है कि शब्द तो हैं, बात कहने का साहस चाहिए. पर मैंने सोचा कि जब यौन विषयों पर ऐसी बात लिखूँ जो केवल व्यस्कों के लिए हो, तो उसे चिट्ठे में लिखना ठीक नहीं होगा. इसलिए ब्राज़ील के यौन व्यवहार के सर्वेक्षण के बारे में जो लिखा है, उसे आप कल्पना पर पढ़ सकते हैं, वह "जो न कह सके" में नहीं कहा जायेगा.
मंगलवार, अगस्त 08, 2006
सोमवार, अगस्त 07, 2006
हिंदी फिल्मों में मानसिक रोग (2)
अब बात करें 15 पार्क एवेन्यू की.
"15 पार्क एवेन्यू" देखने की बहुत दिनों से इच्छा थी. अपर्णा सेन ने "परोमा" और "36 चौरँगी लेन" जैसी फ़िल्में बनायी हैं इसलिए उनकी फिल्मों से भावपूर्ण कथानक और सुरुचि की आशा स्वस्त ही बन जाती है. फ़िर अगर फ़िल्म में वहीदा रहमान, शबाना आज़मी, कोंकणा सेन शर्मा, शेफाली शाह, सोमित्र चैटर्जी, ध्रृतिमान चैटर्जी, राहुल बोस जैसे सुप्रसिद्ध अभिनेता हों तो न भूल पाने वाली फ़िल्म देखने की आशा और भी बढ़ जाती है.
पर जब आशाएँ इतनी ऊँचीं उठी हों तो उनका पूरा होना भी उतना ही कठिन हो जाता है, और शायद इसीलिए फिल्म देख कर अच्छा तो लगा पर यह नहीं लगा कि "वाह क्या बढ़िया फिल्म थी".

कथा साराँशः 15 पार्क एवेन्यू कहानी है श्रीमति गुप्ता (वहीदा रहमान) की और उनकी दो बेटियों, अँजली (शबाना आज़मी) और मिताली यानि मिट्ठू (कोंकणा सेन) की. मिट्ठू मानसिक रोगी हैं, उन्हें स्कित्जोफ्रेनिया है और वह अपनी कल्पना के घर को खोजना चाहती हैं जो 15 पार्क एवेन्यू पर है जहाँ उनके अनुसार उनके पति और बच्चे उनकी राह देख रहे हैं. अँजली तलाकशुदा हैं और विश्वविद्यालय में पढ़ाती हैं और उनके सम्बंध अपने साथ पढ़ाने वाले एक अन्य शिक्षक (कँवलजीत) से हैं. अँजली के मन में एक तरफ घर में प्रतिदिन का मानसिक रोगी के साथ रहने का तनाव है, दूसरी तरफ अपनी छोटी बहन के लिए प्यार भी है, और किसी की देखभाल में अपना जीवन पूरा न पाने का क्रोध भी है.
इस रोजमर्रा के एक तरह चलते जीवन में नयी घटना घटती है जब एक दिन अँजली के कालेज जाने के बाद घर में एक झाड़फूँक करने वाले बाबा जी को बुलाया जाता है. बाबा जी मिट्ठू में घुसी "चुड़ेल" को भगाने के लिए उसे झाड़ू से खूब मारते हैं और कहते हैं अब वह ठीक हो जायेगी. शाम को जब अँजली घर वापस लौटती है तो मिट्ठू अन्य बातों के साथ उसे बताना चाहती है कि दिन में उसे खूब मारा गया पर अँजली अपने जीवन की बातों और काम में व्यस्त है और मिट्ठू की बातें सुन कर भी नहीं सुनती, उसे लगता है कि हर बार की तरह मिट्ठू बिना सिर पैर की काल्पनिक बाते कर रही है.
उसी दिन रात को मिट्ठू कलाई काट लेती है. अँजली अपराध बोध से घिर जाती है, उसने अपनी बातों में खो कर, अपनी छोटी बहन की सही बात को झूठ माना. कुछ ठीक होने पर मनोचिकित्सक (ध्रृतिमान चैटर्जी) की सलाह पर अँजली माँ और मिट्ठू के साथ कुछ दिन आराम करने भूटान चली जाती है.
भूटान में एक नदी के किनारे घूमती मिट्ठू को जयदीप (राहुल बोस) देख लेता है जो अपनी पत्नी (शेफाली शाह) और बच्चों के साथ वहाँ छुट्टियों में आया है. दस साल पहले जयदीप और मिट्ठू का विवाह होने वाला था, जब बलात्कार के बाद मिट्ठू अपना मानसिक संतुलन खो बैठी थी और जयदीप मँगनी तोड़ कर चला गया था. जयदीप के मन में भी मिट्ठू को ले कर अपराध बोध है और वह उससे मिलने की कोशिश करता है.
पहले तो अँजली गुस्सा होती है, उसे डर है कि मिट्ठू की तबियत फ़िर से न बिगड़ जाये पर फ़िर देखती है कि मिट्ठू ने जयदीप को नहीं पहचाना और उससे एक अजनबी की तरह बात करती है. दूसरी तरफ, जयदीप की पत्नी परेशान है, उसे विश्वास है कि जयदीप अपनी पुरानी प्रेमिका के चक्कर में पड़ गया है, तब जयदीप उसे बताता है कि मिट्ठू मानसिक रोगी है और वह सिर्फ अपने पिछले बरताव के अपराध बोध से मुक्त होने की कोशिश कर रहा है.
टिप्पणीः फ़िल्म के सभी अभिनेता बहुत बढ़ियाँ हैं. कोंकणा सेन की तरीफ़ सबसे अधिक करनी चाहिये क्योंकि मानसिक रोग जो चेहरे से झलक कर चेहरे को बदल देता है, इसको वे बहुत प्रभावशाली ढ़ँग से दिखातीं हैं. फ्लैशबेक में दिखाये कुछ भागों को छोड़ कर बाकी सारी फिल्म में कोंकणा का नीचे झुकते होंठ और आँखों में झलकता खोयापन उनके रोग को विश्वासनीय बना देता हैं हाँलाकि उसकी वजह से वे "हीरोइन" नहीं लगतीं. उनका मिर्गी का दौरा पड़ने का दृश्य बिल्कुल विश्वासनीय है.

बाकी सभी अभिनेता भी बढ़ियाँ हैं. छोटे से भाग में मिट्ठू के पिता के भाग में सोमित्र चैटर्जी को देख कर बहुत अच्छा लगा. ध्रृतिमान चैटर्जी जिन्हें देखे पँद्रह बीस साल हो गये थे और जो "गोपी गायन बाघे बायन" के दिनों से मुझे बहुत अच्छे लगते थे, उन्हें देख कर भी बहुत अच्छा लगा.
इन सब अच्छे अभिनेताओं के होते हुए भी, फ़िल्म में क्या कमियाँ थीं जिनकी वजह से मेरे विचार में यह फ़िल्म उतनी प्रभावशाली नहीं बनी?
मेरे विचार में फ़िल्म का कथानक ही इसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है. कथानक में वह नाटकीय घटनाएँ, मिट्ठू का जयदीप से प्यार, उसका बलात्कार, जयदीप का रिश्ता तोड़ कर उसे छोड़ कर चले जाना, यह सब बातें जो फिल्म में उतार चढ़ाव और दिलचस्पी ला सकती थीं, सभी छोटे छोटे फ्लैशबैक में ही सीमित रह जाती हैं. फिल्म का मुख्य केंद्र है दस साल बाद जयदीप का मिट्ठू से मिलना पर इसमें कोई अंतर्निहित नाटकीयता या तनाव नहीं बनता क्योकि मिट्ठू उसे पहचान भी नहीं पाती.
इस सारे हिस्से में तनाव बनाया गया है जयदीप की पत्नी के शक का और समझ नहीं आता कि जयदीप पत्नी को ठीक से सब कुछ क्यों नहीं बताता? इसकी वजह से फिल्म का कथानक कुछ नकली सा हो जाता है.
फ़िल्म अँग्रेज़ी में है. फ़िल्म के सभी मुख्य कलाकार आपस में अँग्रेजी में ही बात करते हैं पर कभी सड़क पर या काम करने वाली से हिंदी और बँगाली में भी बात कर सकते हैं. यह सच है कि आज का पढ़ा लिखा भारतीय उच्च मध्यम वर्ग अँग्रेजी में ही अपनी बात आसानी से कह पाता है और उसके सोच तथा व्यवहार में पश्चिमी उदारवादी विचार उसकी भारतीयता के साथ घुलमिल गये हैं. श्रीमति गुप्ता का पति के छोड़ जाने के बाद दूसरा विवाह करना या अँजलि का अपने मित्र के साथ अमरीका न चलने पर उसका पूछना "क्या तुम बिना विवाह के शारीरक सम्बंधों की नैतिकता की बात तो नहीं सोच रही हो?", जैसी बातें इसी बदलाव को दर्शाती हैं.
मानसिक रोग के साथ जीने में फ़िल्म के पात्रों के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला, जैसे पहले जीवन चल रहा था, वैसा ही चलता रहेगा, कोई चमत्कार नहीं होने वाला, यही फ़िल्म का अंतिम संदेश है. ऐसे आशाहीन जीवन में अचानक निर्देशक अपर्णा सेन अंत में नया प्रश्न उठा देती हैं, "सोचो कि अगर मिट्ठू की बातों को कल्पना कहने और सोचने वाले अगर गलत हों? अगर सचमुच कोई ऐसा जीवन स्तर हो जहाँ मिट्ठू के कल्पना का जीवन सच हो पर हम उस जीवन स्तर को नहीं देख सकते तो कैसा होगा?" फिल्म का अंत इसी फँतासी वाले प्रश्न से होता है जब मिट्ठू किसी अन्य स्तर पर बने अपने 15 पार्क एवेन्यू वाले अपने घर को खोज लेती हैं जहाँ उनका मिलन अपने पति और पाँच बच्चों से होता है.
कुछ यही अंत था ख्वाजा अहमद अब्बास की 1963 की फिल्म "शहर और सपना" का जिसमें सड़क पर पुरानी पाईप में जीवन बिताने को मजबूर युगल अंत में उसी पाईप में छुपा अपने सपने का घर पाता है. शायद यही एक रास्ता है आशाहीन जीवनों को परदे पर निराशा से बचाने का!
"15 पार्क एवेन्यू" देखने की बहुत दिनों से इच्छा थी. अपर्णा सेन ने "परोमा" और "36 चौरँगी लेन" जैसी फ़िल्में बनायी हैं इसलिए उनकी फिल्मों से भावपूर्ण कथानक और सुरुचि की आशा स्वस्त ही बन जाती है. फ़िर अगर फ़िल्म में वहीदा रहमान, शबाना आज़मी, कोंकणा सेन शर्मा, शेफाली शाह, सोमित्र चैटर्जी, ध्रृतिमान चैटर्जी, राहुल बोस जैसे सुप्रसिद्ध अभिनेता हों तो न भूल पाने वाली फ़िल्म देखने की आशा और भी बढ़ जाती है.
पर जब आशाएँ इतनी ऊँचीं उठी हों तो उनका पूरा होना भी उतना ही कठिन हो जाता है, और शायद इसीलिए फिल्म देख कर अच्छा तो लगा पर यह नहीं लगा कि "वाह क्या बढ़िया फिल्म थी".

कथा साराँशः 15 पार्क एवेन्यू कहानी है श्रीमति गुप्ता (वहीदा रहमान) की और उनकी दो बेटियों, अँजली (शबाना आज़मी) और मिताली यानि मिट्ठू (कोंकणा सेन) की. मिट्ठू मानसिक रोगी हैं, उन्हें स्कित्जोफ्रेनिया है और वह अपनी कल्पना के घर को खोजना चाहती हैं जो 15 पार्क एवेन्यू पर है जहाँ उनके अनुसार उनके पति और बच्चे उनकी राह देख रहे हैं. अँजली तलाकशुदा हैं और विश्वविद्यालय में पढ़ाती हैं और उनके सम्बंध अपने साथ पढ़ाने वाले एक अन्य शिक्षक (कँवलजीत) से हैं. अँजली के मन में एक तरफ घर में प्रतिदिन का मानसिक रोगी के साथ रहने का तनाव है, दूसरी तरफ अपनी छोटी बहन के लिए प्यार भी है, और किसी की देखभाल में अपना जीवन पूरा न पाने का क्रोध भी है.
इस रोजमर्रा के एक तरह चलते जीवन में नयी घटना घटती है जब एक दिन अँजली के कालेज जाने के बाद घर में एक झाड़फूँक करने वाले बाबा जी को बुलाया जाता है. बाबा जी मिट्ठू में घुसी "चुड़ेल" को भगाने के लिए उसे झाड़ू से खूब मारते हैं और कहते हैं अब वह ठीक हो जायेगी. शाम को जब अँजली घर वापस लौटती है तो मिट्ठू अन्य बातों के साथ उसे बताना चाहती है कि दिन में उसे खूब मारा गया पर अँजली अपने जीवन की बातों और काम में व्यस्त है और मिट्ठू की बातें सुन कर भी नहीं सुनती, उसे लगता है कि हर बार की तरह मिट्ठू बिना सिर पैर की काल्पनिक बाते कर रही है.
उसी दिन रात को मिट्ठू कलाई काट लेती है. अँजली अपराध बोध से घिर जाती है, उसने अपनी बातों में खो कर, अपनी छोटी बहन की सही बात को झूठ माना. कुछ ठीक होने पर मनोचिकित्सक (ध्रृतिमान चैटर्जी) की सलाह पर अँजली माँ और मिट्ठू के साथ कुछ दिन आराम करने भूटान चली जाती है.
भूटान में एक नदी के किनारे घूमती मिट्ठू को जयदीप (राहुल बोस) देख लेता है जो अपनी पत्नी (शेफाली शाह) और बच्चों के साथ वहाँ छुट्टियों में आया है. दस साल पहले जयदीप और मिट्ठू का विवाह होने वाला था, जब बलात्कार के बाद मिट्ठू अपना मानसिक संतुलन खो बैठी थी और जयदीप मँगनी तोड़ कर चला गया था. जयदीप के मन में भी मिट्ठू को ले कर अपराध बोध है और वह उससे मिलने की कोशिश करता है.
पहले तो अँजली गुस्सा होती है, उसे डर है कि मिट्ठू की तबियत फ़िर से न बिगड़ जाये पर फ़िर देखती है कि मिट्ठू ने जयदीप को नहीं पहचाना और उससे एक अजनबी की तरह बात करती है. दूसरी तरफ, जयदीप की पत्नी परेशान है, उसे विश्वास है कि जयदीप अपनी पुरानी प्रेमिका के चक्कर में पड़ गया है, तब जयदीप उसे बताता है कि मिट्ठू मानसिक रोगी है और वह सिर्फ अपने पिछले बरताव के अपराध बोध से मुक्त होने की कोशिश कर रहा है.
टिप्पणीः फ़िल्म के सभी अभिनेता बहुत बढ़ियाँ हैं. कोंकणा सेन की तरीफ़ सबसे अधिक करनी चाहिये क्योंकि मानसिक रोग जो चेहरे से झलक कर चेहरे को बदल देता है, इसको वे बहुत प्रभावशाली ढ़ँग से दिखातीं हैं. फ्लैशबेक में दिखाये कुछ भागों को छोड़ कर बाकी सारी फिल्म में कोंकणा का नीचे झुकते होंठ और आँखों में झलकता खोयापन उनके रोग को विश्वासनीय बना देता हैं हाँलाकि उसकी वजह से वे "हीरोइन" नहीं लगतीं. उनका मिर्गी का दौरा पड़ने का दृश्य बिल्कुल विश्वासनीय है.

बाकी सभी अभिनेता भी बढ़ियाँ हैं. छोटे से भाग में मिट्ठू के पिता के भाग में सोमित्र चैटर्जी को देख कर बहुत अच्छा लगा. ध्रृतिमान चैटर्जी जिन्हें देखे पँद्रह बीस साल हो गये थे और जो "गोपी गायन बाघे बायन" के दिनों से मुझे बहुत अच्छे लगते थे, उन्हें देख कर भी बहुत अच्छा लगा.
इन सब अच्छे अभिनेताओं के होते हुए भी, फ़िल्म में क्या कमियाँ थीं जिनकी वजह से मेरे विचार में यह फ़िल्म उतनी प्रभावशाली नहीं बनी?
मेरे विचार में फ़िल्म का कथानक ही इसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है. कथानक में वह नाटकीय घटनाएँ, मिट्ठू का जयदीप से प्यार, उसका बलात्कार, जयदीप का रिश्ता तोड़ कर उसे छोड़ कर चले जाना, यह सब बातें जो फिल्म में उतार चढ़ाव और दिलचस्पी ला सकती थीं, सभी छोटे छोटे फ्लैशबैक में ही सीमित रह जाती हैं. फिल्म का मुख्य केंद्र है दस साल बाद जयदीप का मिट्ठू से मिलना पर इसमें कोई अंतर्निहित नाटकीयता या तनाव नहीं बनता क्योकि मिट्ठू उसे पहचान भी नहीं पाती.
इस सारे हिस्से में तनाव बनाया गया है जयदीप की पत्नी के शक का और समझ नहीं आता कि जयदीप पत्नी को ठीक से सब कुछ क्यों नहीं बताता? इसकी वजह से फिल्म का कथानक कुछ नकली सा हो जाता है.
फ़िल्म अँग्रेज़ी में है. फ़िल्म के सभी मुख्य कलाकार आपस में अँग्रेजी में ही बात करते हैं पर कभी सड़क पर या काम करने वाली से हिंदी और बँगाली में भी बात कर सकते हैं. यह सच है कि आज का पढ़ा लिखा भारतीय उच्च मध्यम वर्ग अँग्रेजी में ही अपनी बात आसानी से कह पाता है और उसके सोच तथा व्यवहार में पश्चिमी उदारवादी विचार उसकी भारतीयता के साथ घुलमिल गये हैं. श्रीमति गुप्ता का पति के छोड़ जाने के बाद दूसरा विवाह करना या अँजलि का अपने मित्र के साथ अमरीका न चलने पर उसका पूछना "क्या तुम बिना विवाह के शारीरक सम्बंधों की नैतिकता की बात तो नहीं सोच रही हो?", जैसी बातें इसी बदलाव को दर्शाती हैं.
मानसिक रोग के साथ जीने में फ़िल्म के पात्रों के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला, जैसे पहले जीवन चल रहा था, वैसा ही चलता रहेगा, कोई चमत्कार नहीं होने वाला, यही फ़िल्म का अंतिम संदेश है. ऐसे आशाहीन जीवन में अचानक निर्देशक अपर्णा सेन अंत में नया प्रश्न उठा देती हैं, "सोचो कि अगर मिट्ठू की बातों को कल्पना कहने और सोचने वाले अगर गलत हों? अगर सचमुच कोई ऐसा जीवन स्तर हो जहाँ मिट्ठू के कल्पना का जीवन सच हो पर हम उस जीवन स्तर को नहीं देख सकते तो कैसा होगा?" फिल्म का अंत इसी फँतासी वाले प्रश्न से होता है जब मिट्ठू किसी अन्य स्तर पर बने अपने 15 पार्क एवेन्यू वाले अपने घर को खोज लेती हैं जहाँ उनका मिलन अपने पति और पाँच बच्चों से होता है.
कुछ यही अंत था ख्वाजा अहमद अब्बास की 1963 की फिल्म "शहर और सपना" का जिसमें सड़क पर पुरानी पाईप में जीवन बिताने को मजबूर युगल अंत में उसी पाईप में छुपा अपने सपने का घर पाता है. शायद यही एक रास्ता है आशाहीन जीवनों को परदे पर निराशा से बचाने का!
रविवार, अगस्त 06, 2006
हिंदी फिल्मों में मानसिक रोग (1)
कुछ दिन पहले अपर्णा सेन द्वारा निर्देशित फिल्म "१५ पार्क एवेन्यू" देखी, जिसका विषय है स्कित्जोफ्रेनिया, वह मानसिक रोग जिसमे रोगी सच और कल्पना का अंतर खो बैठता है. फिल्म देख कर हिंदी फिल्मों में मानसिक रोग के विषय को किन विभिन्न तरीकों से लिया गया है इसके बारे में सोच रहा था.
बढ़ते शहरीकरण, टूटते संयक्त परिवार, काम में तरक्की पाने और पैसे कमाने की होड़, इन सब बदलावों से जीवन स्तर अच्छे हुए हैं पर साथ ही साथ अकेलापन, उदासी और तनाव जैसे मानसिक रोग बहुत तेज़ी से बढ़े हैं. मानसिक रोगों को दो श्रेणियों में बाँटा जा सकता है. पहली श्रेणी में वह मानसिक रोग आते हैं जैसे गहरी उदासी, जिसमें व्यक्ति यथार्थ और कल्पना का अंतर समझता है. दूसरी श्रेणी में आते हैं स्कित्जोफ्रेनिया जैसे रोग, जिसमें व्यक्ति यथार्थ के जीवन और कल्पना के जीवन की सीमारेखा नहीं पहचान पाता. विश्व स्वास्थ्य संसथान का कहना है कि अगले दशकों में मानसिक रोग बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे.
मानसिक रोग फ़िल्म को नाटकीय तनाव देने का काम अच्छा कर सकते हैं हालाँकि मानसिक रोग का प्रतिदिन का यथार्थ इतना निराशात्मक और बोझिल हो सकता है जिससे फिल्म देखने वालों को हताशा और तकलीफ़ हो जाये. शायद इसीलिए हिंदी फिल्मों ने मानसिक रोग के विषय को अक्सर असफल प्रेम का नतीजे के रुप में प्रस्तुत किया है और उसे कथा के दुखांत से जोड़ कर ट्रेजेडी फिल्म बनाई हैं. इस रुप में मानसिक रोग फिल्म का मुख्य विषय नहीं होता बल्कि प्रेम कथा को नया मोड़ देने का माध्यम बन कर रह जाता है.
स्कित्जोफ्रेनिया को कई बार व्यक्तित्व के दो हिस्सों में बँट जाने, यानि एक शरीर में दो विपरीत व्यक्तित्वों का रहना, स्टीवनसन के सुप्रसिद्ध उपन्यास डा जैकिल और मिस्टर हाईड से प्रभावित हुआ कथानक भी कुछ भारतीय फिल्मों ने चुना है जिनमें से उन्लेखनीय हैं "रात और दिन" (1967, निर्देशक सत्येन बोस) जो नरगिस की सशक्त अभिनय की वजह से प्रभावशाली बन गयी थी. इसी से कुछ मिलते जुलते कथानक वाली एक अन्य फ़िल्म जो कुछ समय पहले आई थी, "मदहोश" (2004) जिसमें बिपाशा बसु ने स्कित्जोफ्रेनिया के रोग को सतही और अप्रभावशाली तरीके से दिखाया था. इस तरह की फ़िल्में इस रोग की सही तस्वीर नहीं दिखातीं बल्कि उसे केवल कहानी में अप्रत्याशित मोड़ लाने का बहाना बना कर रह जाती हैं.

असफल प्रेम और मानसिक रोग के विषय पर केंद्रित फ़िल्मों के बारे में सोचा जाये तो सबसे पहले असित सेन की "खामोशी" (1967) को भूल पाना कठिन है. "खामोशी" में थी वहीदा रहमान, प्रेम में ठुकराए आहित प्रेमियों को मानसिक पीड़ा से निकालने के प्रेम का नाटक करने वाली नर्स के रुप में, जो हर बार खुद प्रेम करने लगती है और रोगी के जाने के बाद पागल हो जाती है. उनके साथ असफल प्रेमी के रुप में थे राजेश खन्ना और धर्मेंद्र. हालाँकि खामोशी की कहानी मानसिक रोगियों की पीड़ा दिखाने में सक्षम थी पर साथ साथ कुछ नकली भी, उसके पागलपन में किसी उपन्यास की नाटकीयता थी. प्रमुख पात्रों को छोड़ कर, फ़िल्म में दिखाये गये मानसिक रोग अस्पताल में अन्य सभी रोगी, रोगी कम और विदूषक अधिक थे जिनका काम फ़िल्म को कुछ हल्के फुल्के क्षण देना था.
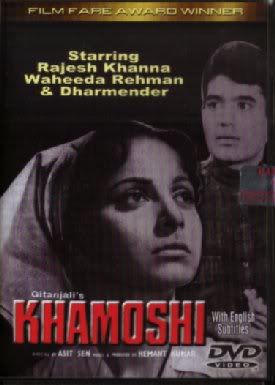
खामोशी जैसी ही कहानी थी कुछ दिन पहले आई प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित फ़िल्म "क्यों कि" (2005) की. "खामोशी" की अतिनाटकीयता, उसके मानसिक रोग के चिकित्सकों के केरिकेचर, उसके विदूषक जैसे मानसिक रोगी, सभी कमियाँ "क्यों कि" में और भी कई गुणा बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत की गयीं थीं. कोशिश कर भी मैं यह फिल्म पूरी नहीं देख पाया, उसकी चीख चिल्लाहट से सिर दुखने लगा था, इसलिए इसके बारे में और कुछ कहना बेकार है.
एक और फ़िल्म थी कुछ साल पहले की, "तेरे नाम" (निर्देशक सतीश कौशिक, 2003) जिसका विषय भी मानिसक रोग ही था. हालाँकि "क्यों कि" की तरह इसमें भी व्यवसायिक फ़िल्म वाली अतिश्योकत्ताएँ थी, पर इसमें मानसिक रोगियों पर अकसर होने वाले अमानवीय व्यवहार, हिंसा और अँधविश्वास का चित्रण था जो वे सब लोग पहचान सकते हैं जिन्हें कभी किसी मानसिक अस्पताल में जाने का मौका मिला है. मानसिक अस्पताल अक्सर अस्पताल नहीं पागलखाने कहलाते हैं और वहाँ मानव अधिकारों को बात तो छोड़िये, मानसिक रोगियों से अमानवीय व्यवहार होता है.
नई फ़िल्मों में मुझे अधिक विश्वासनीय लगी थी "मैंने गाँधी को नहीं मारा" (2005, निर्देशक जाह्नू बरुआ) जिसमें मानसिक रोग का असफल प्रेम से कोई सम्बंध नहीं था, बल्कि जिसका मानसिक रोगी एक बूढ़ा प्रोफेसर था जिसकी अल्सहाईमर जैसे रोग से यादाश्त गुम रही थी. फिल्म में रोगी की बेटी, फिल्म की नायिका का प्रेमी उसे ठुकरा देता है. समाज में मानसिक रोगों के साथ बहुत से अंधविश्वास जुड़े हैं और रोगियों और उनके परिवारों को इसकी वजह से बहुत कठिनाईयाँ उठानी पड़ती हैं.
"सदमा" तथा "कोई मिल गया" जैसी फ़िल्मों ने मानसिक विकास की कमी की बात को लिया है पर यह बात मानसिक रोगों की बात से भिन्न है, हालाँ कि दोनो बातों में कुछ साम्यताएँ भी हैं और लोगों का दोनो ही तरह के रोगियों के प्रति व्यवहार अक्सर घृणा और भर्त्सना भरा होता है.
बढ़ते शहरीकरण, टूटते संयक्त परिवार, काम में तरक्की पाने और पैसे कमाने की होड़, इन सब बदलावों से जीवन स्तर अच्छे हुए हैं पर साथ ही साथ अकेलापन, उदासी और तनाव जैसे मानसिक रोग बहुत तेज़ी से बढ़े हैं. मानसिक रोगों को दो श्रेणियों में बाँटा जा सकता है. पहली श्रेणी में वह मानसिक रोग आते हैं जैसे गहरी उदासी, जिसमें व्यक्ति यथार्थ और कल्पना का अंतर समझता है. दूसरी श्रेणी में आते हैं स्कित्जोफ्रेनिया जैसे रोग, जिसमें व्यक्ति यथार्थ के जीवन और कल्पना के जीवन की सीमारेखा नहीं पहचान पाता. विश्व स्वास्थ्य संसथान का कहना है कि अगले दशकों में मानसिक रोग बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे.
मानसिक रोग फ़िल्म को नाटकीय तनाव देने का काम अच्छा कर सकते हैं हालाँकि मानसिक रोग का प्रतिदिन का यथार्थ इतना निराशात्मक और बोझिल हो सकता है जिससे फिल्म देखने वालों को हताशा और तकलीफ़ हो जाये. शायद इसीलिए हिंदी फिल्मों ने मानसिक रोग के विषय को अक्सर असफल प्रेम का नतीजे के रुप में प्रस्तुत किया है और उसे कथा के दुखांत से जोड़ कर ट्रेजेडी फिल्म बनाई हैं. इस रुप में मानसिक रोग फिल्म का मुख्य विषय नहीं होता बल्कि प्रेम कथा को नया मोड़ देने का माध्यम बन कर रह जाता है.
स्कित्जोफ्रेनिया को कई बार व्यक्तित्व के दो हिस्सों में बँट जाने, यानि एक शरीर में दो विपरीत व्यक्तित्वों का रहना, स्टीवनसन के सुप्रसिद्ध उपन्यास डा जैकिल और मिस्टर हाईड से प्रभावित हुआ कथानक भी कुछ भारतीय फिल्मों ने चुना है जिनमें से उन्लेखनीय हैं "रात और दिन" (1967, निर्देशक सत्येन बोस) जो नरगिस की सशक्त अभिनय की वजह से प्रभावशाली बन गयी थी. इसी से कुछ मिलते जुलते कथानक वाली एक अन्य फ़िल्म जो कुछ समय पहले आई थी, "मदहोश" (2004) जिसमें बिपाशा बसु ने स्कित्जोफ्रेनिया के रोग को सतही और अप्रभावशाली तरीके से दिखाया था. इस तरह की फ़िल्में इस रोग की सही तस्वीर नहीं दिखातीं बल्कि उसे केवल कहानी में अप्रत्याशित मोड़ लाने का बहाना बना कर रह जाती हैं.

असफल प्रेम और मानसिक रोग के विषय पर केंद्रित फ़िल्मों के बारे में सोचा जाये तो सबसे पहले असित सेन की "खामोशी" (1967) को भूल पाना कठिन है. "खामोशी" में थी वहीदा रहमान, प्रेम में ठुकराए आहित प्रेमियों को मानसिक पीड़ा से निकालने के प्रेम का नाटक करने वाली नर्स के रुप में, जो हर बार खुद प्रेम करने लगती है और रोगी के जाने के बाद पागल हो जाती है. उनके साथ असफल प्रेमी के रुप में थे राजेश खन्ना और धर्मेंद्र. हालाँकि खामोशी की कहानी मानसिक रोगियों की पीड़ा दिखाने में सक्षम थी पर साथ साथ कुछ नकली भी, उसके पागलपन में किसी उपन्यास की नाटकीयता थी. प्रमुख पात्रों को छोड़ कर, फ़िल्म में दिखाये गये मानसिक रोग अस्पताल में अन्य सभी रोगी, रोगी कम और विदूषक अधिक थे जिनका काम फ़िल्म को कुछ हल्के फुल्के क्षण देना था.
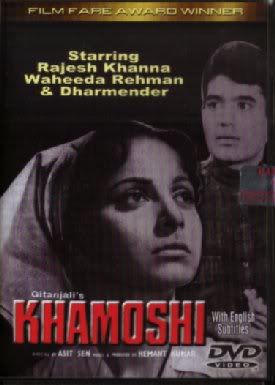
खामोशी जैसी ही कहानी थी कुछ दिन पहले आई प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित फ़िल्म "क्यों कि" (2005) की. "खामोशी" की अतिनाटकीयता, उसके मानसिक रोग के चिकित्सकों के केरिकेचर, उसके विदूषक जैसे मानसिक रोगी, सभी कमियाँ "क्यों कि" में और भी कई गुणा बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत की गयीं थीं. कोशिश कर भी मैं यह फिल्म पूरी नहीं देख पाया, उसकी चीख चिल्लाहट से सिर दुखने लगा था, इसलिए इसके बारे में और कुछ कहना बेकार है.
एक और फ़िल्म थी कुछ साल पहले की, "तेरे नाम" (निर्देशक सतीश कौशिक, 2003) जिसका विषय भी मानिसक रोग ही था. हालाँकि "क्यों कि" की तरह इसमें भी व्यवसायिक फ़िल्म वाली अतिश्योकत्ताएँ थी, पर इसमें मानसिक रोगियों पर अकसर होने वाले अमानवीय व्यवहार, हिंसा और अँधविश्वास का चित्रण था जो वे सब लोग पहचान सकते हैं जिन्हें कभी किसी मानसिक अस्पताल में जाने का मौका मिला है. मानसिक अस्पताल अक्सर अस्पताल नहीं पागलखाने कहलाते हैं और वहाँ मानव अधिकारों को बात तो छोड़िये, मानसिक रोगियों से अमानवीय व्यवहार होता है.
नई फ़िल्मों में मुझे अधिक विश्वासनीय लगी थी "मैंने गाँधी को नहीं मारा" (2005, निर्देशक जाह्नू बरुआ) जिसमें मानसिक रोग का असफल प्रेम से कोई सम्बंध नहीं था, बल्कि जिसका मानसिक रोगी एक बूढ़ा प्रोफेसर था जिसकी अल्सहाईमर जैसे रोग से यादाश्त गुम रही थी. फिल्म में रोगी की बेटी, फिल्म की नायिका का प्रेमी उसे ठुकरा देता है. समाज में मानसिक रोगों के साथ बहुत से अंधविश्वास जुड़े हैं और रोगियों और उनके परिवारों को इसकी वजह से बहुत कठिनाईयाँ उठानी पड़ती हैं.
"सदमा" तथा "कोई मिल गया" जैसी फ़िल्मों ने मानसिक विकास की कमी की बात को लिया है पर यह बात मानसिक रोगों की बात से भिन्न है, हालाँ कि दोनो बातों में कुछ साम्यताएँ भी हैं और लोगों का दोनो ही तरह के रोगियों के प्रति व्यवहार अक्सर घृणा और भर्त्सना भरा होता है.
गुरुवार, अगस्त 03, 2006
सँकरा नर दिमाग
आज बात का विषय नर के सँकरे दिमाग का है. बात मानव जाति के पुरुष पर उतनी लागू नहीं होती, बल्कि अधिकतर यह बात कुत्ता जाति के नरों की है. मेरे बहुत से उच्च विचारों की तरह, यह उच्च विचार भी उस समय मन में आया जब अपने कुत्ते, श्री ब्राँदो को ले कर कल शाम को बाग में सैर को निकला.
अगर आप ने कभी नर कुत्ते को करीब से कुछ समय के लिए जाना पहचाना हो तो आप जानते ही होंगे कि सैर को बाहर निकलते समय, आप को अन्य नर कुत्तों से बच कर चलना पड़ता है. पिल्ले, बहुत बूढ़े कुत्ते और वह कुत्ते जिनका आपरेश्न से गोली हरण हो चका हो, उनको छोड़ कर बाकि के सभी नर कुत्ते हमारे ब्राँदो जी के जानी दुश्मन हैं. उन्हें यह दूर से ही पहचान लेता है, शायद उनकी नर सूँघ से, और देखते ही उनकी तरफ़ ऐसे झपटता है कह रहा हो, "छोड़ो मुझे, रोको मत, इसका खून पी जाऊँगा." और दोनो जोर शोर से एक दूसरे की ओर भौंकते हैं.
फ़िर जैसे ही हो सके उसे वहीं मूतना होता है जहाँ दूसरे कुत्ते ने मूता हो. यह उनके "क्षेत्र" पर झँडे गाड़ने वाली बात है. वह बात और है कि कई क्षत्रों पर इतनी तरह के झँडे गड़े होते हैं कि स्वयं वे खुद भी नहीं पहचान सकते कि उनका झँडा वहाँ गड़ा भी या नहीं.
कितने सालों से हर दिन वही कुत्ते एक दूसरे को देख कर ऐसे ही भौंकते रहते हैं, हालाँकि कई बार लगता है कि यह भौंकना केवल आदत की वजह से है और बेमन से किया जा रहा है.
पर किसी भी मादा कुत्ते को देखते ही पूँछ हिलनी शुरु हो जाती है. अगर आप थोड़ी सी ढील दें तो उसके आसपास जा कर सूँघाई शुरु हो जाती है. थोड़ी सी और ढील दें तो टाँगे उठा कर उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश शुरु हो जाती है. आप कहते रह जाईये, "अरे यार, थोड़ा शाँत हो, तुम्हें हर समय क्या एक ही बात सूझती है? क्या नर और मादा में केवल यही रिश्ता होता है? किसी को केवल मित्र बना कर देखो, और भी तो रिश्ते हो सकते हैं पुरुष और नारी के बीच!", वह कुछ नहीं सुनता.
मानव किशोरावस्था भी शायद कुछ कुछ एसी ही होती है, जब अचानक जवान हुए शरीर में नर होरमोन टेस्टोस्टिरोन तूफ़ान मचा देता है. सड़कों पर रोमियो बन कर सीटियाँ बजाने वाले या बस में झीड़ में लड़कियों के शरीरों को छूने की कोशिश करने वाले शायद हमारे ब्राँदो जी जैसे ही होते हैं, जिनका जीवन होरमोन से संचालित होता है. उनके लिए रुक कर सोचना कि क्या कर रहा हूँ और क्यों, बहुत कठिन होता है.
आज की तस्वीरें हमारे ब्राँदो जी की हैं.




अगर आप ने कभी नर कुत्ते को करीब से कुछ समय के लिए जाना पहचाना हो तो आप जानते ही होंगे कि सैर को बाहर निकलते समय, आप को अन्य नर कुत्तों से बच कर चलना पड़ता है. पिल्ले, बहुत बूढ़े कुत्ते और वह कुत्ते जिनका आपरेश्न से गोली हरण हो चका हो, उनको छोड़ कर बाकि के सभी नर कुत्ते हमारे ब्राँदो जी के जानी दुश्मन हैं. उन्हें यह दूर से ही पहचान लेता है, शायद उनकी नर सूँघ से, और देखते ही उनकी तरफ़ ऐसे झपटता है कह रहा हो, "छोड़ो मुझे, रोको मत, इसका खून पी जाऊँगा." और दोनो जोर शोर से एक दूसरे की ओर भौंकते हैं.
फ़िर जैसे ही हो सके उसे वहीं मूतना होता है जहाँ दूसरे कुत्ते ने मूता हो. यह उनके "क्षेत्र" पर झँडे गाड़ने वाली बात है. वह बात और है कि कई क्षत्रों पर इतनी तरह के झँडे गड़े होते हैं कि स्वयं वे खुद भी नहीं पहचान सकते कि उनका झँडा वहाँ गड़ा भी या नहीं.
कितने सालों से हर दिन वही कुत्ते एक दूसरे को देख कर ऐसे ही भौंकते रहते हैं, हालाँकि कई बार लगता है कि यह भौंकना केवल आदत की वजह से है और बेमन से किया जा रहा है.
पर किसी भी मादा कुत्ते को देखते ही पूँछ हिलनी शुरु हो जाती है. अगर आप थोड़ी सी ढील दें तो उसके आसपास जा कर सूँघाई शुरु हो जाती है. थोड़ी सी और ढील दें तो टाँगे उठा कर उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश शुरु हो जाती है. आप कहते रह जाईये, "अरे यार, थोड़ा शाँत हो, तुम्हें हर समय क्या एक ही बात सूझती है? क्या नर और मादा में केवल यही रिश्ता होता है? किसी को केवल मित्र बना कर देखो, और भी तो रिश्ते हो सकते हैं पुरुष और नारी के बीच!", वह कुछ नहीं सुनता.
मानव किशोरावस्था भी शायद कुछ कुछ एसी ही होती है, जब अचानक जवान हुए शरीर में नर होरमोन टेस्टोस्टिरोन तूफ़ान मचा देता है. सड़कों पर रोमियो बन कर सीटियाँ बजाने वाले या बस में झीड़ में लड़कियों के शरीरों को छूने की कोशिश करने वाले शायद हमारे ब्राँदो जी जैसे ही होते हैं, जिनका जीवन होरमोन से संचालित होता है. उनके लिए रुक कर सोचना कि क्या कर रहा हूँ और क्यों, बहुत कठिन होता है.
आज की तस्वीरें हमारे ब्राँदो जी की हैं.




मंगलवार, अगस्त 01, 2006
भारतीय पत्रकारिता समाज
कल शाम को जनसत्ता के सम्पादक श्री ओम थानवी का नया आलेख "अपने पराए" पढ़ा तो बहुत देर तक मन क्षुब्ध रहा. आलेख का प्रारम्भ में है इफ्तिखार गीलानी की नई पुस्तक के लोकार्पण के अवसर पर, गीलानी जी के जेल में डाले जाने और उस स्थिति में भारतीय पत्रकारिता के आचरण के बारे में थानवी जी के विचार.
इफ्तिख़ार बड़े अफ़सोस भरे स्वर में कहते हैं कि जेल में उन्होंने जो अत्याचार झेला, वह "मीडिया ट्रायल" का नतीजा था. "पत्रकार के शब्द लोग इतना भरोसा करते हैं, इसका अहसास मुझे पहले न था. और न इसका कि हम अपने फर्ज को कितने हलके ढंग से लेते हैं.आलेख के अंतिम भाग में थानवी जी ने भारतीय पत्रकारिता समाज के बढ़ते बेहाल की चर्चा की है.
कुछ अखबारों का सारा सम्पादकीय विवेक तो जैसे इस फिक्र में सिमट कर रह गया है कि दुनिया के किस कोने में शराब की कैसी महक पाई जाती है या किस सात तारा होटल का खानसामा झींगामछली किस हुनर से पकाता है... अँग्रेजी मानसिकता में, साहित्य हो चाहे पत्रकारिता, हिंदी वालों को किस तिरस्कार से देखा जाता है, हम सब जानते हैं....शायद आप कहेंगे कि इसमें नया क्या है? विश्वीकरण के साथ जुड़े उपभोक्तावाद की संस्कृति की वजह से समाचार पत्रों का और नामनीय सम्पादकों का सभ्यता छोड़ कर पन्ने बेच कर विज्ञापन बनाने और उत्पादन बढ़ाने का लालच आसानी से समझा जा सकता है. हिंदी बोलने वाले उपभोक्ताओं से पैसे तो कमाये जा सकते हैं पर उच्च स्तर की फर्राटेदार अँग्रेजी न बोल पाने वालों को तो नीचा समझा ही जाता है. जात पात और वर्ग भेद की आकुण्ठाओं से जकड़े भारतीय समाज को इस सब की आदत है. हिंदी बोलने वालों के मन में अक्सर विश्वास है कि वे हीन हैं तो इसका फायदा अँग्रेज़ी का "सभ्य" समाज उठाये तो उसमे अचरज क्यों?
सोमवार, जुलाई 31, 2006
शब्दों की शक्ति
जेनेवा में अखबार में एक लेख पढ़ा जिसमे हँगरी के सुप्रसिद्ध लेखक पेटर ऐस्तरहाज़ी (Péter Esterhàzy) ने अपने लेखन के बारे में एक साक्षात्कार में कहा, "अचानक मुझे समझ में आया कि मेरे मन में सच और कल्पना के बीच की सीमा रेखा स्पष्ट नहीं थी, शब्दों में कहा गया या सचमुच कुछ बात हुई मेरे लिए एक बराबर ही था. यानि मेरे लिए शब्दों की महत्वता उतनी ही थी जितनी जीवन में होने वाली बातों की... अपनी कल्पना से लिखी वह पहली कहानी मुझे अभी भी याद है, वह अनूठी शक्ति का अनुभव कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, चाहूँ तो किसी को मोटा या पतला, गंदा या पसीने से लथपथ, उसका वक्ष छोटा हो या बड़ा, सब कुछ मेरी इच्छा पर निर्भर है. पहली बार सृजन का आनंद मिला, भगवान को भी कुछ कुछ ऐसा ही लगता होगा."
पेटर की बात कि वह कल्पना में सोची बात और जीवन में होने वाली बातों के बीच की सीमारेखा में अंतर नहीं समझ पाते, मुझ पर भी कुछ कुछ लागू होती है. शाम को बाग में घूमते समय, या रात को सोने से पहले किसी बात को सोचते हुए या सपने में हुई बात, कई बार मुझे लगता है कि वह सचमुच हुई थी. अक्सर पुरानी बातों के बारे में मैं यह नहीं बता पाता कि वह सचमुच हुआ था या फ़िर केवल मैंने सोचा था.
कई बार मन ही मन में किसी मित्र को पत्र लिखता हूँ, सोचता हूँ कि उसे यह बताऊँगा, वह समझाऊँगा, आदि. बाद में लगता है कि मैंने सचमुच वह बात मित्र को लिखी थी और कभी कभी गुस्सा हो जाता हूँ कि मित्र ने उसका जवाब क्यों नहीं दिया!
काम पर भी ऐसा कभी कभी होता है. फेलिचिता, मेरी सचिव अब मेरी इस प्रवृति को समझने लगी है. कभी कभी कुछ काम के बारे में पूछूँ तो कहती है, ठीक से सोचो कि तुमने मुझे सचमुच वह काम दिया था या फ़िर सिर्फ शाम को सोचा था कि मुझे वह काम करना चाहिए?
शायद इसका अर्थ यह हुआ कि मैं भी पेटर की तरह उच्च दर्जे का लेखक बन सकता हूँ?
*****
जेनेवा से वापस आते समय हवाई जहाज में इंटनेशनल हेराल्ड ट्रीब्यून (International Herald Tribune) अखबार में हर तरफ भारत को पाया. एक समाचार था किसी सरीन के बारे में जो कि यूरोप के सबसे बड़ी टेलोफ़ोन कम्पनी वोदाफ़ोन के डायरेक्टर हैं. दूसरा समाचार था रतन टाटा के बारे में जिन्होंने फियट कार वालों के साथ कोई समझोता किया है.
तीसरा समाचार एक लेख था श्रीमति अनुपमा चोपड़ा का मुम्बई के सिनेमा संसार में आते बदलाव के बारे में. अनुपमा जी बात प्रारम्भ करती हैं करण जौहर की नयी फ़िल्म "कभी अल्विदा न कहना से" जिसमें पति परमेश्वर मानने वाली स्त्री पात्र के बदले में एक विवाहित पुरुष के एक विवाहित स्त्री से प्रेम की कहानी है.
कल्पना जी लिखती हैं, "जौहर जैसे फ़िल्म निर्माता इसलिए उन प्रश्नों से जूझ रहे हैं जैसे आत्मीयता (intimacy) के बारे में (क्या दर्शक स्वीकार करेंगे कि इनके प्रिय सितारे साथ सोते हैं), नैतिकता के बारे में (जौहर जी बोले मैं अपनी फ़िल्म में विवाह के रिश्ते से विश्वासघात करने को स्वीकृति नहीं दे सकता), भाषा के बारे में (सेक्स के विषय में हिंदी में बात करना कठिन है क्योंकि इससे जुड़े शब्द यह तो पुराने और कठिन हैं या फ़िर भद्दे). इस आखिरी परेशानी का हल जौहर जी ने यह खोजा कि इस सब बातों के बारे में बातें अँग्रेज़ी में हों."
****
जेनेवा में ग्रेगोर वोलब्रिंग से मुलाकात हुई. ग्रगोर केनेडावासी हैं और जन्म से विकलाँग. ग्रगोर ने सभा में कृत्रिम प्राणीविज्ञान (synthetic biology), और अतिसूक्षम तकनीकी (nanotechnology) इत्यादि विधाओं के मिलन से हो रहे नये प्रयासों के बारे में बोला जिससे अगले 20 या 30 वर्षों में विकलाँगता के बारे में हमारे सोचने का तरीका बदल सकता है. ग्रेगोर का कहना है कि इन तकनीकों से मानव शरीर और मस्तिष्क का ऐसा विकास हो सकता है जो मानव को नयी दिशाओं में ले जा सकता है, ऐसे समाज में विकलाँग वह लोग होंगे जिनके पास इन तकनीकों को खरीदने के लिए साधन नहीं होंगे. ग्रेगोर के बारे में पढ़ना चाहें तो उनके वेबपृष्ठ पर पढ़ सकते हैं.
आज की सभी तस्वीरें जेनेवा से हैं और पहली तस्वीर में मेरे साथ हैं ग्रेगोर वोलब्रिंग.




पेटर की बात कि वह कल्पना में सोची बात और जीवन में होने वाली बातों के बीच की सीमारेखा में अंतर नहीं समझ पाते, मुझ पर भी कुछ कुछ लागू होती है. शाम को बाग में घूमते समय, या रात को सोने से पहले किसी बात को सोचते हुए या सपने में हुई बात, कई बार मुझे लगता है कि वह सचमुच हुई थी. अक्सर पुरानी बातों के बारे में मैं यह नहीं बता पाता कि वह सचमुच हुआ था या फ़िर केवल मैंने सोचा था.
कई बार मन ही मन में किसी मित्र को पत्र लिखता हूँ, सोचता हूँ कि उसे यह बताऊँगा, वह समझाऊँगा, आदि. बाद में लगता है कि मैंने सचमुच वह बात मित्र को लिखी थी और कभी कभी गुस्सा हो जाता हूँ कि मित्र ने उसका जवाब क्यों नहीं दिया!
काम पर भी ऐसा कभी कभी होता है. फेलिचिता, मेरी सचिव अब मेरी इस प्रवृति को समझने लगी है. कभी कभी कुछ काम के बारे में पूछूँ तो कहती है, ठीक से सोचो कि तुमने मुझे सचमुच वह काम दिया था या फ़िर सिर्फ शाम को सोचा था कि मुझे वह काम करना चाहिए?
शायद इसका अर्थ यह हुआ कि मैं भी पेटर की तरह उच्च दर्जे का लेखक बन सकता हूँ?
*****
जेनेवा से वापस आते समय हवाई जहाज में इंटनेशनल हेराल्ड ट्रीब्यून (International Herald Tribune) अखबार में हर तरफ भारत को पाया. एक समाचार था किसी सरीन के बारे में जो कि यूरोप के सबसे बड़ी टेलोफ़ोन कम्पनी वोदाफ़ोन के डायरेक्टर हैं. दूसरा समाचार था रतन टाटा के बारे में जिन्होंने फियट कार वालों के साथ कोई समझोता किया है.
तीसरा समाचार एक लेख था श्रीमति अनुपमा चोपड़ा का मुम्बई के सिनेमा संसार में आते बदलाव के बारे में. अनुपमा जी बात प्रारम्भ करती हैं करण जौहर की नयी फ़िल्म "कभी अल्विदा न कहना से" जिसमें पति परमेश्वर मानने वाली स्त्री पात्र के बदले में एक विवाहित पुरुष के एक विवाहित स्त्री से प्रेम की कहानी है.
कल्पना जी लिखती हैं, "जौहर जैसे फ़िल्म निर्माता इसलिए उन प्रश्नों से जूझ रहे हैं जैसे आत्मीयता (intimacy) के बारे में (क्या दर्शक स्वीकार करेंगे कि इनके प्रिय सितारे साथ सोते हैं), नैतिकता के बारे में (जौहर जी बोले मैं अपनी फ़िल्म में विवाह के रिश्ते से विश्वासघात करने को स्वीकृति नहीं दे सकता), भाषा के बारे में (सेक्स के विषय में हिंदी में बात करना कठिन है क्योंकि इससे जुड़े शब्द यह तो पुराने और कठिन हैं या फ़िर भद्दे). इस आखिरी परेशानी का हल जौहर जी ने यह खोजा कि इस सब बातों के बारे में बातें अँग्रेज़ी में हों."
****
जेनेवा में ग्रेगोर वोलब्रिंग से मुलाकात हुई. ग्रगोर केनेडावासी हैं और जन्म से विकलाँग. ग्रगोर ने सभा में कृत्रिम प्राणीविज्ञान (synthetic biology), और अतिसूक्षम तकनीकी (nanotechnology) इत्यादि विधाओं के मिलन से हो रहे नये प्रयासों के बारे में बोला जिससे अगले 20 या 30 वर्षों में विकलाँगता के बारे में हमारे सोचने का तरीका बदल सकता है. ग्रेगोर का कहना है कि इन तकनीकों से मानव शरीर और मस्तिष्क का ऐसा विकास हो सकता है जो मानव को नयी दिशाओं में ले जा सकता है, ऐसे समाज में विकलाँग वह लोग होंगे जिनके पास इन तकनीकों को खरीदने के लिए साधन नहीं होंगे. ग्रेगोर के बारे में पढ़ना चाहें तो उनके वेबपृष्ठ पर पढ़ सकते हैं.
आज की सभी तस्वीरें जेनेवा से हैं और पहली तस्वीर में मेरे साथ हैं ग्रेगोर वोलब्रिंग.




रविवार, जुलाई 30, 2006
जेनेवा की गर्मी
एक अंतर्राष्ट्रीय सभा के लिए स्विटज़रलैंड में जेनेवा आया हूँ. घर से चला था तो बोलोनिया में इतनी गरमी थी कि बुरा हाल था. पहले, जून तक, इस लिए रो रहे थे सब कि इस साल गरमियाँ ही नहीं आ रहीं थीं, अब इस लिए रो रहे हैं, बहुत गरमी पड़ रही है. खैर स्विटज़लैंड में पहली बार अपने कमरे में छोटा सा मेज़ वाला पँखा देखा. कमरे में गरमी और उमस से बुरा हाल था और उस छोटे से पँखे से कुछ विषेश राहत नहीं मिल रही थी पर दिल को थोड़ी तसल्ली अवश्य होती थी.
चाहे बुश जी माने या न माने और क्योटो के समझोते पर हस्ताक्षर करें या नहीं, यहाँ रह कर कहना कि पर्यावरण में तेज़ी से परिवर्तन नहीं आ रहा, असम्भव है. हमने यहाँ अपने घर में पहला पँखा करीब 1992 या 1993 के आसपास खरीदा था. फ़िर कई पँखे खरीदे, हर कमरे के लिए एक. इस साल घर को वातानाकूलित बनाना ही पड़ा. केवल दस पंद्रह सालों में इतना बदलाव आ गया है. इस साल पहली बार स्विटज़रलैंड में भी पँखे दिख रहे हैं, यानि गरमी और बढ़ती जा रही है.
एक जगह पढ़ा था कि अगले कुछ सालों में वातावरण परिवर्तन से पूरे यूरोप में बरफ़ छा जायेगी और उत्तरी देशों से लोग दक्षिणी देशों के ओर प्रवास करेंगे. यानि भारत, अफ्रीका, मेक्सिको आदि से यूरोप, अमरीका, कनाडा जाने के बदले, लोग भारत, अफ्रीका और मेक्सिको की ओर जायेंगे. वह बर्फ़ीली सर्दी कब आयेगी यह तो मालूम नहीं, अभी तो गरमी भुगतने का मौका है.
अब जब गरमी की लहर की वजह से रोम, लंदन इत्यादि में बिजली उड़ने के समाचार आते हैं तो मन ही मन खुशी होती है. ऐसी ही खुशी तब होती है जब मूसलाधार बारिश के बाद यहाँ के शहरों का जीवन अस्त वयस्त हो जाता है और नालियाँ पानी से भर कर, पानी सड़कों पर आ जाता है. पहले यहाँ के लोग भारत या अफ्रीका की ओर जाते तो नखरे दिखाते थे कि वहाँ बिजली चली जाती है, विकास अच्छी तरह से नहीं हुआ और बेचारे गरीब देश हैं! ये तो मौसम की कृपा थी, न कभी तेज़ गरमी न कभी तेज़ बारिश, जिसकी वजह से सब कुछ अच्छा चलता था और अब मौसम बदलने से यहाँ भी वही हाल होने वाला है ?
जेनेवा झील के किनारे, गरमियों का आनंद लेते हुए


दूसरी प्रदर्शनी में विभिन्न देशों में आते पर्यवरण परिवर्तन जिसमें चीन में पीली नदी पर बन रहे दुनिया के सबसे बड़े बाँध के बनने से आये परिवर्तनों की तस्वीर

चाहे बुश जी माने या न माने और क्योटो के समझोते पर हस्ताक्षर करें या नहीं, यहाँ रह कर कहना कि पर्यावरण में तेज़ी से परिवर्तन नहीं आ रहा, असम्भव है. हमने यहाँ अपने घर में पहला पँखा करीब 1992 या 1993 के आसपास खरीदा था. फ़िर कई पँखे खरीदे, हर कमरे के लिए एक. इस साल घर को वातानाकूलित बनाना ही पड़ा. केवल दस पंद्रह सालों में इतना बदलाव आ गया है. इस साल पहली बार स्विटज़रलैंड में भी पँखे दिख रहे हैं, यानि गरमी और बढ़ती जा रही है.
एक जगह पढ़ा था कि अगले कुछ सालों में वातावरण परिवर्तन से पूरे यूरोप में बरफ़ छा जायेगी और उत्तरी देशों से लोग दक्षिणी देशों के ओर प्रवास करेंगे. यानि भारत, अफ्रीका, मेक्सिको आदि से यूरोप, अमरीका, कनाडा जाने के बदले, लोग भारत, अफ्रीका और मेक्सिको की ओर जायेंगे. वह बर्फ़ीली सर्दी कब आयेगी यह तो मालूम नहीं, अभी तो गरमी भुगतने का मौका है.
अब जब गरमी की लहर की वजह से रोम, लंदन इत्यादि में बिजली उड़ने के समाचार आते हैं तो मन ही मन खुशी होती है. ऐसी ही खुशी तब होती है जब मूसलाधार बारिश के बाद यहाँ के शहरों का जीवन अस्त वयस्त हो जाता है और नालियाँ पानी से भर कर, पानी सड़कों पर आ जाता है. पहले यहाँ के लोग भारत या अफ्रीका की ओर जाते तो नखरे दिखाते थे कि वहाँ बिजली चली जाती है, विकास अच्छी तरह से नहीं हुआ और बेचारे गरीब देश हैं! ये तो मौसम की कृपा थी, न कभी तेज़ गरमी न कभी तेज़ बारिश, जिसकी वजह से सब कुछ अच्छा चलता था और अब मौसम बदलने से यहाँ भी वही हाल होने वाला है ?
जेनेवा झील के किनारे, गरमियों का आनंद लेते हुए



जेनेवा में पर्यावरण पर लगी दो प्रशनियाँ - पहली प्रदर्शनी में दुनियाँ के बच्चों ने अपने देश के बदलते जीवन के चित्र बनाये हैं, उसी में से अफगानिस्तान के बच्चे द्वारा बनाये गये बोनियान के बुद्ध की मूर्ती जो कट्टरवादी तालीबानों ने धवंस कर दी थी.

दूसरी प्रदर्शनी में विभिन्न देशों में आते पर्यवरण परिवर्तन जिसमें चीन में पीली नदी पर बन रहे दुनिया के सबसे बड़े बाँध के बनने से आये परिवर्तनों की तस्वीर

सदस्यता लें
टिप्पणियाँ (Atom)
इस वर्ष के लोकप्रिय आलेख
-
पिछले कुछ दिनों में फेसबुक पर साहित्यकारों से जुड़ी यौन दुराचरण की एक बहस चल रही है। मैं फेसबुक पर कम ही जाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि नकारात...
-
हिन्दू जगत के देवी देवता दुनिया की हर बात की खबर रखते हैं, दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं जो उनकी दृष्टि से छुप सके। मुझे तलाश है उस देवी या द...
-
कुछ दिन पहले भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने टीवी के प्रोग्राम वाले श्री समय रैना और अन्य विदूषकों को आदेश दिया कि वे अपने कार्यक्रम में विकलां...
-
केवल एक सप्ताह के लिए मनीला आया था और सारे दिन कोन्फ्रैंस की भाग-दौड़ में ही गुज़र गये थे. उस पर से यूरोप से सात घँटे के समय के अंतर की वज...
-
भारत की शायद सबसे प्रसिद्ध महिला चित्रकार अमृता शेरगिल, भारत से बाहर कला विशेषज्ञों में उतनी पसिद्ध नहीं हैं, पर भारतीय कला क्षेत्र में उनका...
-
पाराम्परिक भारतीय सोच के अनुसार अक्सर बच्चों को क्या पढ़ना चाहिये और क्या काम करना चाहिये से ले कर किससे शादी करनी चाहिये, सब बातों के लिए मा...
-
एक दो दिन पहले टीवी के सीरियल तथा फ़िल्में बाने वाली एकता कपूर का एक साक्षात्कार पढ़ा जिसमें उनसे पूछा गया कि क्या आप को अपने बीते दिनों ...
-
आज सुबह चाय बना रहा था तो अचानक मन में बचपन की एक याद कौंधी। यह बात १९६३-६४ की है। मैं और मेरी छोटी बहन, हम दोनों अपनी छोटी बुआ के पास मेरठ...
-
कुछ दिन पहले "जूलियट की चिठ्ठियाँ" (Letters to Juliet, 2010) नाम की फ़िल्म देखी जिसमें एक वृद्ध अंग्रेज़ी महिला (वेनेसा रेडग्रेव...
-
पिछली सदी में दुनिया में स्वास्थ्य सम्बंधी तकनीकों के विकास के साथ, बीमारियों के बारे में हमारी समझ बढ़ी है जितनी मानव इतिहास में पहले कभी नह...




.JPG)