अखबार में पढ़ा कि इंफोसिस कम्पनी ने अपने व्यापार को विभिन्न दिशाओं में विकसित करने का फैसला किया है, इसलिए कम्पनी अब प्राईवेट बैंक के अतिरिक्त चिकित्सा क्षेत्र में भी काम खोलेगी. चिकित्सा क्षेत्र को नया "सूर्योदय उद्योग" यानि Sunrise industry कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत कमाई है, जो धीरे धीरे उगते सूरज की तरह बढ़ेगी.
सोचा कि दुनिया कितनी बदल गयी है. पहले बड़े उद्योगपति बहुत पैसा कमाने के बाद खैराती अस्पताल और डिस्पैंसरियाँ खोल देते थे ताकि थोड़ा पुण्य कमा सकें, अब के उद्योगपति सोचते हैं कि लोगों की बीमारी और दुख को क्यों न निचोड़ा जाये ताकि और पैसा बने.
पिछले वर्ष फरवरी में चीन में काम से गया था जब छोटी बहन ने खबर दी थी कि माँ बेहोश हो गयी है और वह उसे अस्पताल में ले जा रही है. माँ का यह समय भी आना ही था यह तो कई महीनो से मालूम हो चुका था. पिछले दस सालों में एल्सहाईमर की यादाश्त खोने की बीमारी धीरे धीरे उनके दिमाग के कोषों को खा रही थी, जिसकी वजह से कई महीनों से उनका उठना, बैठना, चलना,सब कुछ बहुत कठिन हो गया था. मन में बस एक ही बात थी कि माँ के अंतिम दिन शान्ती से निकलें. मैं खबर मिलने के दूसरे ही दिन दिल्ली पहुँच गया. अस्पताल पहुँचा तो माँ के कागजों में उन पर हुए टेस्ट देख कर दिमाग भन्ना गया. जाने कितने खून के टेस्ट, केट स्कैन आदि किये जा चुके थे, पर मुझे दुख हुआ जब देखा कि माँ की रीढ़ की हड्डी से जाँच के लिए पानी निकाला गया था.
करीब सत्ततर वर्ष की होने वाली थी माँ. इतने सालों से लाइलाज बिमारी का कुछ कुछ इलाज उसी अस्पताल के डाक्टर कर रहे थे. यही इन्सान की कोशिश होती है कि मालूम भी हो कि कुछ विषेश लाभ नहीं हो रहा तब भी लगता है कि बिना कुछ किये कैसे छोड़ दें. मरीज़ कुछ गोली खाता रहे, तो मन को लगेगा कि हम बिल्कुल लाचार नहीं हैं, कुछ कोशिश कर रहे हैं.
कोमा में पड़ी माँ के अंतिम दिन थे, यह सब जानते थे. किसी टेस्ट से उन्हें कुछ होने वाला नहीं था. उस हाल में खून के टेस्ट, ईसीजी, ईईजी, केट स्कैन आदि सब बेकार थे, पर उन्हें स्वीकारा जा सकता था, यह सोच कर कि इतना बड़ा प्राईवेट अस्पताल चलाना है तो वह लोग कुछ न कुछ कमाने की सोचेंगे ही. पर रीढ़ की हड्डी से पानी निकालना? यानि उनकी इस हालत में जब हाथ, पैर घुटने अकड़े और जुड़े हुए थे, उन्हें खींच तान कर, इस तरह से तकलीफ़ देना, यह तो अपराध हुआ.
मुझे बहुत गुस्सा आया. छोटी बहन को बोला कि तुमने उन्हें यह रीढ़ की हड्दी से पानी निकालने का टेस्ट करने क्यों दिया? वह बोली मैं उन्हें क्या कहती, वह डाक्टर हैं वही ठीक समझते हैं कि क्या करना चाहिये, क्या नहीं करना चाहिये! डाक्टर आये तो मन में आया कि पूछूँ कि रीढ़ की हड्दी से पानी वाले टेस्ट में क्या देखना चाहते थे, लेकिन कुछ कहा नहीं. मैंने उन्हें यही कहा कि मैं माँ को घर ले जाना चाहूँगा. तो बोले कि हाँ ले जाईये, यही बेहतर है, इनकी हालत ऐसी है कि यहाँ हम तो कुछ कर नहीं सकते.
मैं माँ को घर ला सका था क्योंकि मेरे मन में था कि मैं स्वयं माँ का अंतिम दिनो में उपचार करूँगा. कुछ समय तक मैंने आई.सी.यू. में काम किया था, मालूम था कि उनकी देखभाल जिस तरह मैं कर सकता हूँ, उस तरह अन्य लोग नहीं कर सकते. क्योंकि मेरे उपचार में अपना लाभ नहीं छुपा था, केवल माँ के अंतिम दिनों में उनको शान्ति मिले इसका विचार था. लेकिन जिनके अपनों में कोई डाक्टर न हो जो उनका ध्यान कर सके, क्या उसके अच्छा इलाज का अर्थ यही है कि पैसे कमाने वाले "सूर्योदय उद्योग" से उसे निचोड़ सकें?

भारत के डाक्टर, नर्स, फिज़योथेरापिस्ट आदि अपने काम के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं. मेरे विचार में अगर कोई चिकित्सा क्षेत्र में काम करने की सोचता है तो उसे धँधा समझ कर यह सोचे, ऐसे लोग कम ही होंगे. इस क्षेत्र में काम करने वाले अधिकतर लोग अपने मन में स्वयं को भले आदमी के रूप में ही देखते सोचते हैं कि वह लोगों की भलाई का काम कर रहे हैं. लेकिन जब अपने काम से अपनी रोटी चलनी हो और मासिक पागार नहीं बल्कि कौन मरीज़ कितना देगा की भावना हो तो धीरे धीरे लालच मन में आ ही जाता है. बिना जरूरत के आपरेशन से बच्चा करना, बिना बात के ओपरेशन करना या दवाईयाँ खिलाना, नयी बिमारियाँ बनाना, बेवजह के टेस्ट और एक्सरे कराना, जैसी बातें इसी लालच का नतीजा हैं.
हर क्षेत्र की तरह इस क्षेत्र में भी अच्छे और बुरे दोनो तरह के लोग होते हैं. भारत में चिकित्सा क्षेत्र में काम करने वाले ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो आदर्शवादी हैं और इसे सेवा के रूप में देखते हैं. भारत के चिकित्सा से जुड़े कुछ उद्योगों ने भी दुनिया में अपनी धाक आदर्शों के बल पर ही बनायी है, जैसे कि जेनेरिक दवा बनाने वाले तथा सिपला जैसी दवा बनाने की कम्पनियाँ जिन्होंने एडस, मलेरिया, टीबी जैसी बीमारियों की सस्ती दवाईयाँ बना कर विकासशील देशों में रहने वाले गरीब लोगों को इलाज कराने का मौका दिया है.
पर बड़े शहरों में पैसे वालों के लिए सरकारी अस्पतालों की तुलना में पाँच सितारा अस्पतालों में या नर्सिंग होम में लोगों को सही इलाज मिल सकेगा, इसके बारे में मेरे मन में कुछ दुविधा उठती है. वहाँ सरकारी अस्पताल सी भीड़ और गन्दगी शायद न हो, लेकिन क्या चिकित्सा की दृष्टि से वह इलाज मिलेगा जिसकी आप को सच में आवश्यकता है?
अहमदाबाद की संस्था "सेवा" के एक शौध में निकला था कि भारत में गरीब परिवारों में ऋण लेने का सबसे पहला कारण बीमारी का इलाज है. प्राईवेट चिकित्सा संस्थाओं को बीमारी कैसी कम की जाये, इसमें दिलचस्पी नहीं, बल्कि पैसा कैसे बनाया जाये, इसकी चिन्ता उससे अधिक होती है. वहाँ काम करने वाले लोग कितने भी आदर्शवादी क्यों न हों, क्या वह निष्पक्ष रूप से अपने निर्णय ले पाते हैं और वह सलाह देते हैं जिसमें मरीज़ का भला पहला ध्येय हो, न कि पैसा कमाना?
इसीलिए जब सुनता हूँ कि भारत में अब अमरीका जैसे बड़े स्पेशालिटी अस्पताल खुले हैं जहाँ पाँच सितारा होटल के सब सुख है, जहाँ सब नयी तकनीकें उपलब्ध हैं, विदेशों से भी लोग इलाज करवाने आते हैं, तो मुझे लगता है कि अगर मुझे कुछ तकलीफ़ हो तो वहाँ नहीं जाना चाहूँगा, कोई सीधा साधा डाक्टर ही खोजूँगा.
***


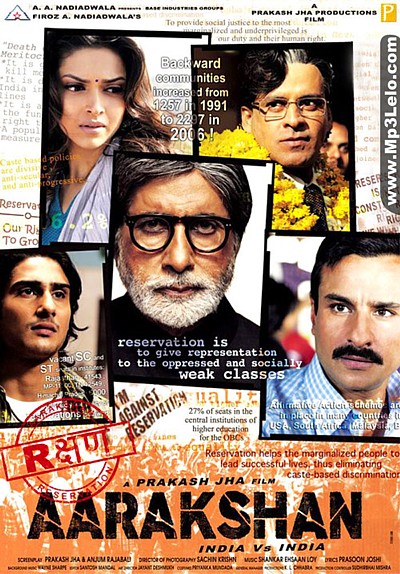




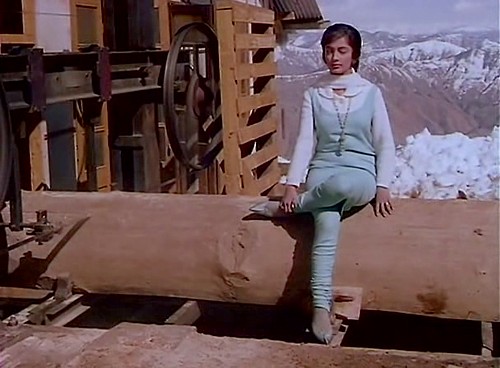
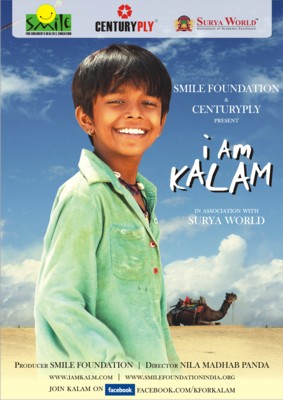












.JPG)