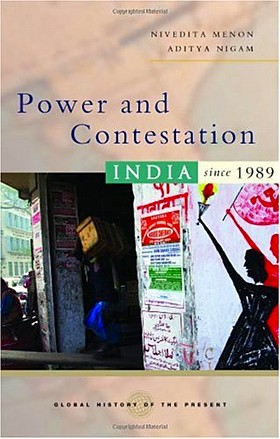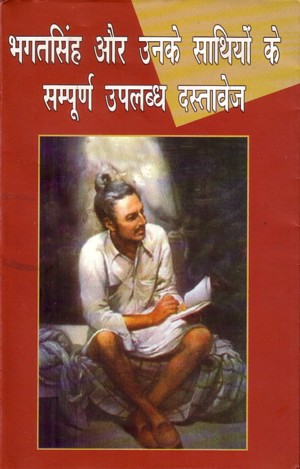"एक बहुत सुन्दर बाग है यहाँ, देखने चलेंगे?", मित्र ने मुझसे पूछा तो समझ में नहीं आया कि कैसे उत्तर दिया जाये, जिससे कहीं जाना भी न पड़े और उसे बुरा भी नहीं लगे. सुबह सुबह निकले थे प्रोजेक्ट देखने, दिन भर भरी धूप में घूमे थे, अब वजाय कमरे में जा कर सुस्ताने के, उसका सुझाव था कि किसी बाग को देखने जाया जाये.
"क्या है बाग में?", जब और कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने बेवकूफ़ी वाला प्रश्न पूछा.
लेकिन मेरा प्रश्न मेरे मित्र को बेवकूफ़ी वाला नहीं लगा, उत्साहित हो कर बोला, "बहुत सुन्दर गुलाब के फ़ूल हैं. कुछ जानवर भी हैं, ऊँठ और घोड़े आदि. बहुत बढ़िया जगह है, तुम्हें अवश्य अच्छी लगेगी."
इतने उत्साह से मुझे वह बाग दिखाना चाहता था कि आखिरकार हाँ कहनी ही पड़ी. मैं बैलरी जिले में हेगड़ी बोम्मन्नाहल्ली तालुक में कुष्ठ रोग और विकलाँग पुनर्स्थान सम्बन्धी प्रोजेक्ट के सिलसिले में आया था. वह बाग वहाँ से करीब तीस मिनट की कार यात्रा पर, होसपेट जाने वाले रास्ते पर था.
जब गाड़ी एक फैक्टरी जैसे गेट से घुसी और बड़े से इन्डस्ट्रियल शैड के सामने रुकी तो थोड़ा अचरज हुआ कि यह कैसा बाग है.
दरअसल वह गुलाब के फ़ूलों का निर्यात करने वाली फैक्टरी थी. अन्दर बीसयों लोग काम में लगे थे. कोई ट्राली में रँग बिरँगे गुलाबों को इधर से उधर ले रहा था, कहीं गुलाब की टहनियाँ काट कर उन्हें गुलदस्तों में सजा कर पैक किया जा रहा था. अन्दर दो वातानुकूलित कक्ष भी बने थे जिनमें ठँडक में हज़ारों गुलाब की कलियाँ कतारों में सजी थीं. पँद्रह बीस भिन्न रँगों के गुलाब थे वहाँ.


यह वीएसएल कृषि-तकनीकी प्रजेक्ट का हिस्सा था जिसके मालिक है राज्य सभा के सदस्य अनिल लाड, जिनकी लोहे की खानें और अन्य कई व्यवसाय भी हैं.
शैड से बाहर निकले तो पीछे बड़े बड़े ग्रीनहाउस थे, जिनमें नियंत्रित वातावरण में गुलाब उगाये जाते हैं. हर एक ग्रीन हाउस में करीब 35 हज़ार गुलाब के पौधे हैं और सारा काम आधुनिक तकनीकों के सहारे से किया जाता है. यानि, कहने का बाग था, पर असल में विषेश प्रकार की फैक्टरी है.


ग्रीन हाउस वाले हिस्से से बाहर निकले तो गाय और बैलों के हिस्से में पहुँचे. फैक्टरी के इस हिस्से में अलग अलग शैड के नीचे दसियों तरह की सुन्दर गाय और बैल बँधे थे. मुझे कर्णाटकी गायों और बैलों के सीधे नुकीले सींग बहुत अच्छे लगे. हाँलाकि मुझे विभिन्न गायों और बैलों की नस्लों का पता नहीं, पर फ़िर भी अलग अलग नस्लें देखना अच्छा लगा.



गायों के शैड के पीछे ऊँठों और घोड़ों के शैड बने थे, और सबके पीछे एक कृत्रम झील में पानी चमक रहा था, यह झील भी फैक्टरी वालों ने बनवायी है जिससे पूरी फैक्टरी को पानी मिलता है.

सब जगह घूम कर अंत में हम लोग "जननी गौशाला" पहुँचे, जो एक अलग तरह की फैक्टरी है. यहाँ एक रयासन विषेशज्ञ काम कर रहे थे. उन्होंने बताया कि इस गौशाला में गौ मूत्र से एक रामबाण दवा बनायी जाती है. एक सिलिन्डर में गौ मूत्र रखा जाता है, जिसे भाप बना कर उसके स्वच्छ पानी को अलग जगह बोतलों में भरा जाता है. गौ मूत्र से बने इस पानी की रसायनिक जाँच भी की गयी है और इसमें कई तरह के रसायन पाये जाते हैं. उन सज्जन के अनुसार इस पानी में शरीर की बहुत सी बीमारियाँ, जैसे कि ब्लड प्रैशर, डायबेटीज, अस्थमा, एक्ज़ीमा आदि ठीक करने की शक्ति है, और यह एक आयुर्वेदिक दवा मानी जाती है.

उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं उस पानी का स्वाद चखना चाहूँगा, तो मैंने सिर हिला दिया कि नहीं. मूत्र से बनी कोई चीज़ पीने का विचार अच्छा नहीं लगा. हालाँकि मन ही मन सोच रहा था कि यह तो स्वच्छ किया हुआ पानी है, इसमें मूत्र का स्वाद नहीं होना चाहिये. अब इस बात को सोचूँ तो थोड़ा दुख होता है कि क्यों नहीं चखा, क्या जाने फ़िर कभी इसका मौका मिले भी कि न मिले. उस तरह का स्वच्छ किया हुआ मूत्र खोज पाना आसान नहीं होगा.
आखिर में जब हम उस "बाग" से निकले तो हमारे मित्र ने कहा कि रास्ते में रुक कर अँगूर खरीदे जायें. कर्णाटक का यह हिस्सा बहुत उपजाऊ है, और आज कल यहाँ जगह जगह अँगूर, अनार जैसे फ़लों की खेती की जा रही है. जब अंगूर के खेतों के बीच पहुँचे तो हरे भरे दूर दूर तक फ़ैले खेत और अंगूर से लदी लताएँ देख कर सुखद आश्चर्य हुआ. तब तक शाम घिर आयी थी और वहाँ काम करने वाले लोग, टेम्पू या आटो में हर तरफ़ से चढ़ कर अपने गाँवों की ओर वापस जा रहे थे.


घूमने के बाद अँगर खाते हुए वापस हेगड़ी बोम्मन्नाहल्ली की ओर जा रहे थे तो सोच रहा था कि मित्र ने ठीक ही कहा था, यह आम बाग में घूमने वाली बात नहीं बल्कि विषेश मौका था जिसका फ़ायदा उठा कर नयी जगह देखने का मौका मिल गया था. इस घूमने फ़िरने में सारे दिन के काम की थकान और तनाव भी गुम हो गये थे.

***
"क्या है बाग में?", जब और कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने बेवकूफ़ी वाला प्रश्न पूछा.
लेकिन मेरा प्रश्न मेरे मित्र को बेवकूफ़ी वाला नहीं लगा, उत्साहित हो कर बोला, "बहुत सुन्दर गुलाब के फ़ूल हैं. कुछ जानवर भी हैं, ऊँठ और घोड़े आदि. बहुत बढ़िया जगह है, तुम्हें अवश्य अच्छी लगेगी."
इतने उत्साह से मुझे वह बाग दिखाना चाहता था कि आखिरकार हाँ कहनी ही पड़ी. मैं बैलरी जिले में हेगड़ी बोम्मन्नाहल्ली तालुक में कुष्ठ रोग और विकलाँग पुनर्स्थान सम्बन्धी प्रोजेक्ट के सिलसिले में आया था. वह बाग वहाँ से करीब तीस मिनट की कार यात्रा पर, होसपेट जाने वाले रास्ते पर था.
जब गाड़ी एक फैक्टरी जैसे गेट से घुसी और बड़े से इन्डस्ट्रियल शैड के सामने रुकी तो थोड़ा अचरज हुआ कि यह कैसा बाग है.
दरअसल वह गुलाब के फ़ूलों का निर्यात करने वाली फैक्टरी थी. अन्दर बीसयों लोग काम में लगे थे. कोई ट्राली में रँग बिरँगे गुलाबों को इधर से उधर ले रहा था, कहीं गुलाब की टहनियाँ काट कर उन्हें गुलदस्तों में सजा कर पैक किया जा रहा था. अन्दर दो वातानुकूलित कक्ष भी बने थे जिनमें ठँडक में हज़ारों गुलाब की कलियाँ कतारों में सजी थीं. पँद्रह बीस भिन्न रँगों के गुलाब थे वहाँ.


यह वीएसएल कृषि-तकनीकी प्रजेक्ट का हिस्सा था जिसके मालिक है राज्य सभा के सदस्य अनिल लाड, जिनकी लोहे की खानें और अन्य कई व्यवसाय भी हैं.
शैड से बाहर निकले तो पीछे बड़े बड़े ग्रीनहाउस थे, जिनमें नियंत्रित वातावरण में गुलाब उगाये जाते हैं. हर एक ग्रीन हाउस में करीब 35 हज़ार गुलाब के पौधे हैं और सारा काम आधुनिक तकनीकों के सहारे से किया जाता है. यानि, कहने का बाग था, पर असल में विषेश प्रकार की फैक्टरी है.


ग्रीन हाउस वाले हिस्से से बाहर निकले तो गाय और बैलों के हिस्से में पहुँचे. फैक्टरी के इस हिस्से में अलग अलग शैड के नीचे दसियों तरह की सुन्दर गाय और बैल बँधे थे. मुझे कर्णाटकी गायों और बैलों के सीधे नुकीले सींग बहुत अच्छे लगे. हाँलाकि मुझे विभिन्न गायों और बैलों की नस्लों का पता नहीं, पर फ़िर भी अलग अलग नस्लें देखना अच्छा लगा.



गायों के शैड के पीछे ऊँठों और घोड़ों के शैड बने थे, और सबके पीछे एक कृत्रम झील में पानी चमक रहा था, यह झील भी फैक्टरी वालों ने बनवायी है जिससे पूरी फैक्टरी को पानी मिलता है.

सब जगह घूम कर अंत में हम लोग "जननी गौशाला" पहुँचे, जो एक अलग तरह की फैक्टरी है. यहाँ एक रयासन विषेशज्ञ काम कर रहे थे. उन्होंने बताया कि इस गौशाला में गौ मूत्र से एक रामबाण दवा बनायी जाती है. एक सिलिन्डर में गौ मूत्र रखा जाता है, जिसे भाप बना कर उसके स्वच्छ पानी को अलग जगह बोतलों में भरा जाता है. गौ मूत्र से बने इस पानी की रसायनिक जाँच भी की गयी है और इसमें कई तरह के रसायन पाये जाते हैं. उन सज्जन के अनुसार इस पानी में शरीर की बहुत सी बीमारियाँ, जैसे कि ब्लड प्रैशर, डायबेटीज, अस्थमा, एक्ज़ीमा आदि ठीक करने की शक्ति है, और यह एक आयुर्वेदिक दवा मानी जाती है.

उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं उस पानी का स्वाद चखना चाहूँगा, तो मैंने सिर हिला दिया कि नहीं. मूत्र से बनी कोई चीज़ पीने का विचार अच्छा नहीं लगा. हालाँकि मन ही मन सोच रहा था कि यह तो स्वच्छ किया हुआ पानी है, इसमें मूत्र का स्वाद नहीं होना चाहिये. अब इस बात को सोचूँ तो थोड़ा दुख होता है कि क्यों नहीं चखा, क्या जाने फ़िर कभी इसका मौका मिले भी कि न मिले. उस तरह का स्वच्छ किया हुआ मूत्र खोज पाना आसान नहीं होगा.
आखिर में जब हम उस "बाग" से निकले तो हमारे मित्र ने कहा कि रास्ते में रुक कर अँगूर खरीदे जायें. कर्णाटक का यह हिस्सा बहुत उपजाऊ है, और आज कल यहाँ जगह जगह अँगूर, अनार जैसे फ़लों की खेती की जा रही है. जब अंगूर के खेतों के बीच पहुँचे तो हरे भरे दूर दूर तक फ़ैले खेत और अंगूर से लदी लताएँ देख कर सुखद आश्चर्य हुआ. तब तक शाम घिर आयी थी और वहाँ काम करने वाले लोग, टेम्पू या आटो में हर तरफ़ से चढ़ कर अपने गाँवों की ओर वापस जा रहे थे.


घूमने के बाद अँगर खाते हुए वापस हेगड़ी बोम्मन्नाहल्ली की ओर जा रहे थे तो सोच रहा था कि मित्र ने ठीक ही कहा था, यह आम बाग में घूमने वाली बात नहीं बल्कि विषेश मौका था जिसका फ़ायदा उठा कर नयी जगह देखने का मौका मिल गया था. इस घूमने फ़िरने में सारे दिन के काम की थकान और तनाव भी गुम हो गये थे.

***