प्रारम्भ में तो कियारा को एक कृत्रिम बाजू मिली, जिसे लगाने से, अगर गौर से न देखें तो पता नहीं चलता था कि कियारा का दाँया हाथ नहीं है, पर उस कृत्रिम हाथ से कियारा कुछ काम नहीं कर पाती थी. लेकिन फ़िर भी वह वापस कोंगो लौट गयी, जहाँ वह नर्सों और स्वास्थ्य कर्मचारियों को पढ़ाने के काम में लग गयी.
हर एक दो सालों में जब भी कियारा वापस इटली आती है, बुद्रियो के ओर्थोपेडिक केंद्र में अपने कृत्रिम हाथ की जाँच कराने जाती है. समय के साथ उसका कृत्रिम हाथ भी बदल गया है, और अब वह अपनी बाजु की बची माँस पेशियों से अपने हाथ से कुछ काम कर सकती है.
कियारा की वजह से शरीर के कृत्रिम अंगों के विषय में मेरी दिलचस्पी बनी और इस क्षेत्र में कोई नयी खोज तो मैं उसके बारे में पढ़ने जानने की कोशिश करता हूँ. इसीलिए जब मैंने टच बायोनिक्स नाम की कम्पनी द्वारा प्रोडिजिट उँगलियों के बनाये जाने के बारे में सुना तो उसके बारे में अधिक जानने की कोशिश की.

अगर किसी की हथेली या उँगलियाँ कट गयी हों तो प्रोडिजिट उँगलियों से वह अपने हाथ का पूरा उपयोग कर सकते हैं. कृत्रिम उँगलियों को बनाने में अब तक सबसे कठिन बात थी उनके हिलने, पकड़ने आदि कामों ऐसा नियंत्रण लाना जिससे बारीक काम जैसे कि उँगली और अँगूठे के बीच में बारीक चीज़ को पकड़ना.
अभी तक कृत्रिम हाथ इस तरह का बारीक काम नहीं कर सकते थे, लेकिन अब प्रोडिजिट से यह भी संभव हो गया है.

यह तकनीकी प्रगति किसके लिए?
एक तरफ़ विज्ञान इतनी तेज़ी से प्रगति कर रहा है, जो बात कल तक असंभव लगती थी, वह आज संभव हो रही है, पर मेरे विचार में एक प्रश्न हम शायद अक्सर भूल जाते हैं, कि यह प्रगति किसके लिए है? हम सोचते हें कि कोई भी नया आविष्कार होगा तो समय के साथ उसकी कीमत कम हो जायेगी और वह आविष्कार सब जन साधारण तक पहुँचेगा. शायद यह बात उन सब तकनीकी प्रगतियों के लिए सच हो जिनका बाज़ार है, जिनको उपयोग करने वाले लाखों करोड़ों लोग हैं, तो बेचने के लिए वह वस्तु देर सवेर सस्ती हो सकती है, जैसे कि मोबाइल टेलीफोन.
लेकिन कृत्रिम अंग जिनका उपयोग कुछ ही लोगों को करना होगा, क्या कभी वह गरीब लोगों या फ़िर मध्यम वर्ग के बस की बात होंगे?
कियारा तो इटली आ कर नया हाथ बनवा सकती है लेकिन जिन गरीब लोगों के लिए काम करती है, उनमें से कितने अफ्रीका के लोग इस तरह का हाथ खरीद सकते हैं? प्रोडिजिट की उँगलियाँ कितनों के काम आयेंगी?
और भारत जैसा देश, जहाँ अमीरी गरीबी की विषमताएँ शायद दुनिया में सबसे अधिक हैं, वहाँ तकनीकी प्रगति किसके काम आयेगी? एक तरफ़ भारत के चिकित्सक और अपोलो जैसे अस्पताल दुनिया में प्रसिद्ध हैं, विदेशों से लोग अपना इलाज करवाने भारत आते हैं, दूसरी ओर दुनिया में दस्त या न्योमोनिया जैसे सामान्य एवं आसानी से इलाज हो सकने वाली बीमारियों से मरने वाले पाँच साल से कम आयु के बच्चों में से 25 प्रतिशत भारत में मरते हैं. तेज़ी से तरक्की करता विकासरत भारत, भुखमरी और अनपढ़ता में भी दुनिया में सबसे पहले स्थान पर है, और विषमताएँ घटने की बजाय बढ़ रही हैं. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) के अनुसार ब्राज़ील में पिछले दशक में आर्थिक विकास के साथ साथ विषमताएँ भी कम हुई हैं जबकि भारत में विषमताएँ बढ़ी हैं.
मेरे एक केनेडा के मित्र ग्रेगोर वोलब्रिंग का कार्यक्षेत्र नेनोटेकनोलोजी जैसी नयी तकनीकें है. ग्रेगोर कहते हैं कि तकनीकी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, नये नये आविष्कार हो रहे हैं, लेकिन उनके लिए जिनके पास इसकी कीमत चुकाने की क्षमता है. अगर पिछले दो सौ सालों दुनिया में उद्यौगिक विषमताएँ बनी, फ़िर डिजिटल विषमताओं का दौर आया, तो अब नयी तकनीकों की विषमताओं का दौर आ रहा है. पहले विषमताएँ दुनिया के उत्तर में अमरीका, यूरोप आदि देश और दक्षिण में विकासशील देशों के बीच में थी, यह नयी विषमताएँ देशों के बीच में नहीं, अमीरों और गरीबों के बीच होंगी. जिनके पास सामर्थ्य है, वह जीन थैरेपी से तंदरुस्त पैदा होंगे, लम्बा जीवन जीयेंगे, शरीर का कोई अंग कष्ट देगा तो उसे बदल पायेंगे, वे नये सुपर मानव होंगे. जिनके पास सामर्थ्य नहीं, वह दस्तों, बुखारों से वैसे ही मरते रहेंगे जैसे आज मरते हैं.
इस बार कर्नाटक के गाँवों में घूम रहा था तो लोग सरकारी साक्षरता, रोजगार, विकलाँगता आदि विषयों से सम्बधित कार्यक्रमों के बारे में बताते थे, पर साथ ही कहते कि घूसखोरी से कुछ भी करवा लो उसे बदलना कठिन है, जातपात का दबाव कम नहीं होता, कागज़ पर कुछ लिखते हैं पर सच्चाई कुछ और होती है.
कुछ बदलाव आया है पर जितना आना चाहिये था, उतना नहीं. क्या उपाय होगा इसका?



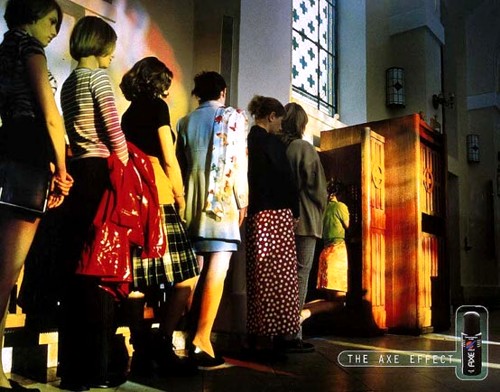

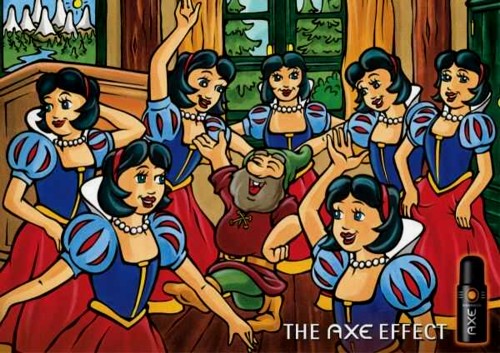









.JPG)