रमा जी का यह आलेख उसमें ४२ से ५० तक पृष्ठों में छपा था. रमा जी और डा. लोहिया ने विवाह नहीं किया था, वे जीवनसाथी थे, करीब बीस वर्ष तक साथ रहे. जब १९६७ में डा. लोहिया की मृत्यु हुई उस समय रमा जी समाजवादी दल की अंग्रेज़ी पत्रिका "मैनकाइन्ड" की सम्पादक थीं और दिल्ली विश्वविद्यालय के मिराण्डा कॉलेज में इतिहास की प्रोफेसर भी थीं.
१९७५ में मेरे पिता की मृत्यु के बाद, कई वर्षों तक रमा जी का हमारे घर आना मुझे याद है. उनके इस आलेख में डा. लोहिया के व्यक्तित्व का व्यक्तिगत रूप दिखता है.
***
रमा मित्र
चौथे आम चुनाव से पहले कुछ दिन वह पूरे निखार पर थे। उन्होंने गैर कांग्रेसवाद के सिद्धांत का निरूपण कर दिया था। उनका नारा था - कांग्रेस हटाओ, देश बचाओ। पर इसकी कल्पना चुनाव के मौके पर ही उन्होने नहीं की थी. काफ़ी पहले तीसरे आम चुनाव के वक्त जनवरी १९६२ में उन्होंने बताया था कि समाजवादी, राष्ट्रीयतावाद और भाषा जैसे प्रश्नों पर जनसंघ के और सम्पत्ति तथा समता जैसे प्रश्नों पर साम्यवादियों के किस तरह निकट हैं? राष्ट्रीयतावाद और भाषा के मामलों में वे जनसंघ के ज़्यादा निकट थे और सम्पत्ति और भाषा के मामलों के बारे में साम्यवादियों के, ज़्यादा। पर ऐसा कोई भी सवाल नहीं था और न ही हो सकता था कि जिस पर समाजवादी कांग्रेस के निकट हो सकते।
"कांग्रेस हटाओ" का नारा बुलंद करते हुए वह देश का अनवरत दौरा करते रहे। उनका ख्याल था कांग्रेस के हटने से हालांकि विभिन्न राज्यों में तरह तरह के मेल की खट्मिट्ठी गंगाजमुनी सरकारें बनेंगी पर बदलाव की प्रक्रिया चल पड़ेगी। वह बदलाव चाहते थे। बदलाव के लिए वह इतना व्यग्र थे कि उन्हें धीरज न था - ऐसा बदलाव जो स्थिरता के नाम पर देश में चलने वाली जड़ता को खत्म करे। आंकड़ों तथा तथ्यों से वह लैस थे। देहाती जलसों में आंकड़ों तथा अर्थशास्त्र की पेचीदगियों को एक दम आसान, सहज और बोधगम्य ढंग से रखने की उनकी प्रतिभा पर हैरत होती थी। देहाती लोग अत्याधुनिक शहरी बुद्धजीवियों के अपेक्षा उनकी बातें ज़्यादा आसानी और स्पष्टता से समझ पाते थे। कार्यक्रम को तफसील से बताते - कृषि, उद्योग, खरच, भाषा, जाति, विदेशी नीति जैसे मामलों पर। हर प्रश्न पर कांग्रेस ने देश और जनता का कैसे बंटाधार किया है, साबित करते।
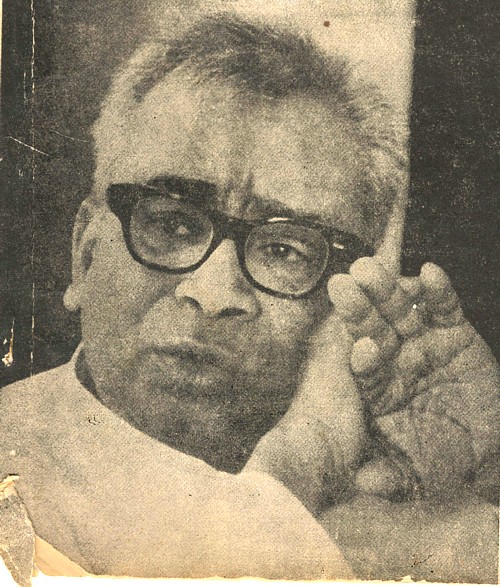
चुनावों से उन पर जबरदस्त बोझ पड़ रहा था - शारीरिक और मानसिक दोनों। बिना किसी केन्द्रीय कोष के चुनाव लड़ना अतिमानवीय कार्य था. पार्टी ने एक साल पहले केन्द्रीय कोष के लिए पैसा जमा करना का शानदार कार्यक्रम बनाया था - ऐसा कोष जिसमें विभिन्न राज्यों तथा दलित उम्मीदवारों - महिलाओं, पिछड़ा वर्ग, मुसलमान तथा अन्य अल्पसंख्यक, आदिवासियों, हरिजनों, आदि - को चुनाव लड़ने का पैसा दिया जा सके। पर हुआ कुछ नहीं। फैसला करने और उस पर अमल न करने से उन्हें सबसे ज़्यादा दुख होता था। वही एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने केन्द्रीय कोष के लिए पैसा इक्ट्ठा किया। वह मुझे संदेशे भेजते रहे कि उनके कोष से फलां फलां उम्मीदवार को पैसे भेजूँ। उन उम्मीदवारों में से अधिकतर पिछड़े वर्गों को होते। कुछ ऊँची जातियों के भी होते पर ऐसे जो बिना किसी कोष, गाड़ी व जीप और इश्तहार व साहित्य के चुनाव लड़ रहे थे। अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में उनका कड़ा निर्देश था कि जब तक वह स्पष्ट आदेश न दें तब तक कोई पैसा न भेजा जाये। एक बार उन्होंने मुझे तार दिया कि कहीं से एक टेपरिकार्डर खरीदो और मेरे निर्वाचन क्षेत्र को भेजो ताकि मेरे भाषण उन इलाकों में सुनाये जा सकें, जहाँ मैं नहीं पहुँच पाया। चुनाव दौरों में वह थक जाते थे पर हमेशा उत्सुकता और आशा बनी रहती थी। उनकी गाड़ी बिगड़ जाती, माइक्रोफोन खराब हो जाता, वह साइकल या बैलगाड़ियों पर चल पड़ते। पर रिक्शा पर कभी नहीं, उसका सवाल ही नहीं उठता था, क्योंकि नीम जवानी के दिनों में उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि वह कभी रिक्शा पर नहीं चढ़ेंगे, किसी दूसरे आदमी पर सवार नहीं होंगे। रिक्शे का खयाल ही उनमें जुगुप्सा भर देता था। उन्होंने रिक्शा चलाने वाले को आधा इन्सान आधा जानवर कहा था, भारत के पतन का प्रतीक।
अपने निर्वाचन क्षेत्र में मतदान से चार दिन पहले वह दिल्ली आये। अपने निर्वाचन क्षेत्र से निकलने की वजह थी कि वह किसी न किसी तरह सुदूर उड़ीसा जाना चाहते थे कि अन्तिम घड़ी के प्रयत्नों से कुछ हजार मतों को किशन पटनायक के पक्ष में मोड़ सकें। दीवार पर टँगे नक्शे, हवाई यात्रा और रेलवे की पंजिकाओं को उन्होंने देखा, किराए पर विषेश विमान लेने के सिवाय समय पर उड़ीसा पहुँचने का कोई और रास्ता नहीं था। किशन उनके बहुत नज़दीक थे। वह संसद में बहुत तेज़ी से उभर रहे थे और वे चाहते थे कि किशन जरूर जीतें।
जब चुनाव के नतीजे आने लगे तो उन्हें काफ़ी आशा थी। दिल्ली आने पर उन्होंने मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराया और १९ फरवरी को रविवार था, ऐसा ही मुझे याद है, वह पहली मरतबा अपना मत देने गये. किसने उस समय सोचा था कि यह उनका अंतिम मतदान भी होगा। उनके कुछ दोस्त भी साथ थे। अपना मत देने के बाद मैं भी आ गयी। काफी हँसी मजाक और छींटाकसी चल रही थी। उनके कुछ दोस्त एक उम्मीदवार के पक्ष में मत देने को उनकी मनौवल कर रहे थे। वह उम्मीदवार कांग्रेसी नहीं था। मतदान के बाद हमने पूछा कि किसको मत दिया, पर वह बताने वाले नहीं थे। हंसी में उन्होंने हमें मत की गोपनीयता की याद दिलायी और हम भी हंसी में शामिल हो गये। चुनाव नतीजे तेजी से आने लगे तो आनन्दित और निराश होने का क्रम बंध गया - सारे वक्त रेडियो चलता रहता। फ़िर नतीजा सुन पड़ता, एक बड़ा कांग्रसी नेता धराशायी हो गया है या उनका कोई ऐसा साथी जिसके जीतने की पूरी उम्मीद थी, हार गया है। मुझे उनकी वह खिलखिलाहट अभी भी याद है, आधी रात बीत गयी थी कि उनके एक जवान दोस्त ने, जो अखबार में काम करता था, मुझे टेलीफोन किया। "इतनी रात बीते टेलीफोन कर आपको परेशान करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, पर एक मज़ेदार चीज़ हुई है - कामराज हार गये हैं।" मैं उनके कमरे में गयी - वह अभी भी पढ़ रहे थे, खबर सुनायी। उनका सारा चेहरा हंसी से भर गया, बोले "बढ़िया, बहुत बढ़िया।"
उनके खुद के चुनाव का नतीजा नहीं आ रहा था। अखबारों में कोई खबर नहीं थी, आगे हैं या पीछे। चुनाव क्षेत्र से एकदम चुप्पी थी। फ़िर उस शाम को जब हम लोग सब खाने के कमरे में बैठे चुनाव नतीजे की खबरें सुन रहे थे, उन दिनों हमारा चलन यही था, केन्द्रीय दफ्तर से फोन आया कि वह विधुना में कुछ हज़ार वोटों से आगे हैं. विधुना का विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र उनके निर्वाचन क्षेत्र में हाल में ही जोड़ा गया था। यह भी खबर आयी कि दो और जगहों में उनके मतों की गणना हो रही है। इस टेलीफोन के आधे घँटे बाद एक और टेलीफोन आया कि वह पीछे हो गये हैं। अपनी स्वाभाविक परिपूर्णता के साथ उन्होंने कागज़ और पेंसिल ली और अपने निर्वाचन क्षेत्र के सभी संसदीय उम्मीदवारों के मतों का जोड़ करने लगे। नतीजा एकदम निराशाजनक था। एक एक करके सब लोग अपने अपने घर चले गये थे और मैं ही उनके साथ अलेके रह गयी थी। मैंने कहा कि वह थोड़ी देर आराम कर लें तब तक मैं उनके लिए खाना परस दूँ। खाते हुए उन्होंने मेरी ओर देखा, "मेरे हारने से तुम्हें बहुत दुख होगा। होगा न?" उस वक्त भी जब हार जीत के बीच लगभग फर्क नहीं रहा था वह अपने बारे में नहीं दूसरों की बाबत सोच रहे थे। यह उनका स्वभाव था, उनकी बात थी। बीस साल के सान्निध्य में मैंने कभी उन्हें अपने बारे में सोचते नहीं पाया। मैंने कहा, "कोई आसमान नहीं फट रहा है यह सोचो कि आप हार गये हो। अब जा कर सो जाओ।" मैंने उन्हें दवा की गोलियाँ दीं और खुद लगभग सारी रात टेलीफोन के पास बैठी रही। आखिरकार अगले दिन दोपहर को हमारे पास खबर आयी कि वह बहुत कम वोटों से जीत गये हैं। "तुम इसे जीतना कहती हो।" मैं क्या कहती।
उनकी भविष्यवाणी कि कांग्रस कुछ राज्यों में हार जायेगी सही साबित हुई, पर कुल नतीजे से वह प्रसन्न नही हुए. नतीजों का उन्होंने विश्लेषण शुरु किया - उत्तरप्रदेश में उनके खुद के इलाके में नतीजा अच्छा रहा नहीं कहा जा सकता। बिहार काफ़ी अच्छा रहा। जैसा कि उन्होंने कहा था द्रमुक को छोड़ कर कोई भी दल उन जगहों पर जहाँ कांग्रेस हार गयी अकेला खड़ा नहीं हुआ। इस बात से वह परेशान हुए कि कुछ राज्यों में जहां जनता ने कांग्रेस को विधान सभा में अल्पसंख्यक बना दिया था, वहां उसने केन्द्र में कांग्रेस को विजयी बनाया। यह रोग का मुख्य लक्षण था। चुनावों के बाद वह हिन्दुस्तानी राजनीति के रोग - राज्यीय गैरकांग्रेसवाद और केन्द्रीय कांग्रेसवाद - के बारे में मुखर हुए। रूपक उपस्थिक करने में वह माहिर थे। उन्होंने हिन्दुस्तान की राजनीति को उच्च रक्तचाप का मरीज बताया - डायस्टोल और सायसटोल का तुलनात्मक फरक जिससे अंततः रोगी के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है और वह खत्म हो जाता है। केन्द्र को उन्होंने कलक्टर और गैरकांग्रेसी राज्य को पटवारी की भी उपमाएँ प्रदान कीं। इसलिए चुनावों के बाद इस रोग को दूर करने के लिए उनकी मुख्य चाल यह थी कि केन्द्र में गैरकांग्रेसी सरकार हो। इस चाल का पहला दाँव राष्ट्रपति का चुनाव था।
उस वक्त वह कुछ दिनों राज्यों में गैर कांग्रेसी मिली जुली सरकारों का कार्यक्रम बनाने में व्यस्त रहे। राष्ट्रीय समिति की भोपाल में बैठक हो रही थी। उन्होंने कार्यक्रम का मस्विदा बनाया जिसमें खास तौर पर यह बताया कि सत्तारूढ़ होने के पहले ६ महीनों के भीतर यह सरकारें क्या करें और ऐसा न कर पाने पर उनकी पार्टी बेहिचक सरकार से बाहर आ जाये। लोग कांग्रेसी और गैर कांग्रेसी सरकार के बीच फरक आँक सकें। इस तरह के कार्यक्रम में एक सर्वोपरि बात थी ६॥ एकड़ भूमि पर से लगाना हटाना।
भोपाल से हम उन्हें कुछ दिनों के वास्ते कन्याकुमारी ले गये। कन्याकुमारी उनका प्रिय रमणीक स्थान था। एक बार वहां से उन्होंने मुझे लिखा था कि उन्हें यह बात रह रह कर कोंचती है कि कन्याकुमारी पर जहाँ भूमि समाप्त होती है वहाँ चट्टान पर जब विवेकानन्द ने समाधी लगायी थी तो उनका मुख भारत की ओर था या समुद्र की ओर। इस बारे में उन्होंने विवेकानन्द सोसाइटी के लोगों से पूछताछ की लेकिन कोई उन्हें उत्तर नहीं दे सका। इस प्रस्न का उन्होंने खुद अपना उत्तर प्राप्त किया। विवेकानन्द जेसे थे उसे देखते हुए वह निश्चित ही भारत की ओर उन्मुख रहे होंगे। कन्याकुमारी में ही उन्हें खबर मिली कि हमारे एक सदस्य विंध्येश्वरी मण्डल जो लोकसभा के लिए चुन लिये गये थे, बिहार सरकार में मंत्री बन गये हैं। उनका गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया, अपनी पार्टी के लोगों से इतनी जल्दी पदलोलुपता की उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। दिल्ली पहुँचने पर प्रेस बयान दे कर इस घोर सिद्धांतहीनता पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की।
उन दिनों वह बहुत अनुत्साहित थे, स्वास्थ्य अच्छा नहीं था। रक्तचाप की अक्सर शिकायत रहती। आँखें काफ़ी दिनों से परेशान कर रही थीं. यह भी सुझाया गया कि ग्लोकोमा के वास्ते उनकी आँखों का आपरेशन किया जाये पर यह सुझाव टाल दिया गया और आँखों में रोज दवा डालते रहने से हालत और बिगड़ी नहीं। लगातार थकान और उनींदेपन की शिकायत करते रहे। अक्सर मुझे कहा करते कि उन्हें भी वही शिकायत है जो अश्वनी को थी। अश्वनी उनके बहुत अज़ीज़ दोस्त थे जिनकी डेढ़ साल पहले मृत्यू हो गयी थी। मैं उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश करती कि यह केवल थकान की वजह से है, उन्हें गुर्दे की कोई शिकायत नहीं जैसी कि उनके दोस्त को थी। उनके सारे बदन में दर्द होता रहता। पर शारीरिक पीड़ा से अधिक मानसिक चिन्ता व परेशानी थी।
वह कहते "क्या तुम सोचती हो कि इस देश में कभी कुछ होगा। क्या मेरी सारी कोशिशे बेकार जायेंगी?" थोड़ी देर में उनकी आशा लौट आती, "क्या पता कुछ आश्चर्यजनक हो जाये।" इसके बाद थोड़ा रुक कर अपने तईं बोलने लगते, "जनता उठेगी, इसमें मुझे कोई शक नहीं पर वह क्या हिंसा का रास्ता अख्तियार करेगी?" यह द्वन्द, यह शँका और भय कि जनता हिंसा का रास्ता अख्तियार करेगी उन्हें लगातार चिंतित करता रहता। एक पल के लिए घोर निराशा में वह अहिंसा को मानने से इंकार करते पर अन्तिम दिन तक अहिंसा में उनकी आस्था बनी रही। राष्ट्रपति चुनाव पर उनका पूरा जोर था और इसमें वह पूरी तरह जुटे हुए थे। भारतीय राजनीति की अलगाव व विघटनकारी बुराई व रोग को दूर करना ही होगा। इस कार्य का पहला कदम था कांग्रेस के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को हराना। यह ध्यान देने की बात है कि उनका प्रचार अभियान ही एकमात्र ऐसा प्रचार था जो परदे के पौछे नहीं वरन् खुल्लमखुल्ला जनता के बीच चला। सार्वजनिक प्रश्नों पर सार्वजनीन बहस-मुबाहिसा होना चाहिए - राजनीतिक अन्दोलन के लिए यही उनका नुस्खा था। चुनाव अभियान में उन्होंने सभाएँ की, अखबारों को भेंट दी और अंत में मतदाताओं से अपील की, कुछ भी उठा न रखा। यही नहीं वही एकमात्र नेता थे जिसने विरोधपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के लिए भी प्रचार किया। विरोधी पक्ष उम्मीदवार चुनने के बाद मौन साध गया। विरोध पक्ष हारा और बड़ी संख्या से हारा। इस हार से चौकन्ने हो कर कारणों का विश्लेषण करने बैठे। सूक्ष्म विश्लेषण की अपनी स्वाभाविक प्रतिभा से उन्होंने नतीजे के कारणों का रेशा रेशा उघाड़ लिया। गैर कांग्रेसवाद को केन्द्र में लाने का उनका पहला निशाना खाली गया - सभी विरोधी सदस्यों ने साथ जो नहीं दिया।
अप्रैल में हमने उन्हें विलिंगडन अस्पताल डाक्टरी जाँच के लिए भेजा। नवम्बर में भी जाँच के लिए वहाँ गये थे। अब डाक्टरों ने पौरुष ग्रंथि के आपरेशन की बात कही. आपरेशन की बात उन्हें नहीं भायी। वह खिन्न हो गये। मैंने उनसे कहा कि हम इसके बारे में दुबारा राय मालूम करेंगे और शल्य क्रिया के प्राध्यापक द्वारा जाँच कराने के लिए अखिल भारतीय चिकित्सा संस्थान ले गयी जिसकी राय थी कि आपरेशन की तात्कालिक ज़रूरत नहीं थी और इन्जेक्शनों वह दुरुस्त होने लगेंगे। वह काफी खुश हो गये और मैंने राहत महसूस की। जब वह विलिंगडन अस्पताल में थे तब भी राजनीति में एकदम बँधे हुए थे। इस बीच दिल्ली में पुलिस आन्दोलन भड़क उठा था। वह लगातार सलाह मशविरा और परामर्श देते रहते थे, अपने साथियों को भेजते और क्या कदम उठाये जायें सोचते। प्रेस वक्तव्य देते और अस्पताल के मैदान में उन्होंने एक सभा की जिसकी खबर एक दैनिक में भी छपी जिससे अस्पताल अधिकारी काफ़ी परेशान दीखे। अस्पताल से जा कर दिल्ली के मजदूर संघों की एक सभा में वह भाषण भी दे आये। दिल्ली के अधिकाँश मजदूरसंघों पर दक्षिणपंथी साम्यवादियों का नियंत्रण है। सभा में उन्होंने हड़ताली पुलिस सिपाहियों की सहानुभूति में आम हड़ताल की अपील की। उनको लगा कि यह एक ऐसा स्वर्णिम अवसर है जबकि जनता और पुलिस के बीच एका बैठाया जा सकता है। इस एक्य से दिल्ली में स्वयंमेव एक क्रांतिकारी स्थिति पैदा हो जायेगी जिसका असर देश भर पर पड़ेगा।
पर १८ नवम्बर १९६६ की छात्र कूच की तरह इस बार भी साम्यवादी यूनियन आगे नहीं बढ़े। उनके आगे बढ़ने से स्थिति बदल जाती। डा. साहब का तरीका यह नहीं था कि क्राति की बात को बहुत ज्यादा की जायेपर कोई आन्दोलन या उस पर अमल नहीं किया जाये। उनके लिए कार्य का असफल होना या उसका एकदम ही निष्प्रभाव होना कार्य न होने से बेहतर था। उन्होंने दिल्ली भर में कई सभाओं में भाषण दिये और जनता को आम पुलिस सिपाही के हाल के बारे में बताया - अफसरों और सिपाहियों के बीच की गहरी खाई और किस तरह सिपाहियों को मानवीय गुणों से च्युत कर पशु बनाया जा रहा है, बताया। साथ ही उन्होंने इन सभाओं में पुलिस जनता दोस्ती की कसम दिलवायी। वही एकमात्र नेता थे जिसने स्थिति की विस्भोटक संभावना को आंका था - केन्द्र पर प्रहार करने का एक बेहतरीन और अद्भुत मौका था. इस मौके के जाने से वह दुखी और निराश हुए थे।
मई की शुरुआत में मेरे एक आत्मीय की मृत्यू हो गयी। वह कितने कोमल और संवेदनशील थे। सार्वजनिक सभाओं में वह अक्सर भारतीय नारी की दुर्गति की चर्चा करते, भारतीय नारी जो हजारों साल से दबायी गयी। वह सभा में उपस्थित पुरुषों से कहते आप स्त्रियों की अधोगति जानने के लिए अर्धनारीश्वर बनो (उसी तरह जिस तरह वह आधा हिन्दू आधा मुसलमान होने की बात कहते), वह खुद इसी तरह थे। मैंने बार बार उनमें यह बात पायी है, ऐसी कोमलता पायी जो केवल माँ में ही मिलती है। जब भी मैं बीमार पड़ी हूँ या दुखी हुई हूँ, माँ की तरह उन्होंने मेरा जतन किया।
मई में पार्टी शिविर में वह त्रवेन्द्रम गये। वहाँ उन्होंने विभिन्न विषयों पर, जिनमें विदेश नीति भी थी, भाषण किये। व्यवहारिकता, प्रचार और दक्षिण भारतीय श्रोताओं के शोर मचा कर बैठा दिये जाने के भय जैसे कारणों ने उन्हें कभी अपनी मातृभाषा के बजाय दूसरी भाषा में बोलने को विचलित नहीं किया। दूसरी भाषा में बोलने के बजाय उन्हें मौन मंजूर था। जून के मध्य में मैं वाराणसी उनके साथ हो ली। रात वह गंगा में नाव पर बिताना चाहते थे। हम सभी नाव में थे। नौका ने मणिकर्णिका घाट के सामने सीध पर लंगर डाला. मणिकर्णिका घाट पर हमेशा कोई न कोई चिता जलती रहती है. मैंने पहली बार शमशान देखा। वह सोचमग्न हो गये, "मृत देह को ले कर इतना झमेला क्यों किया जाता है? प्राणों के बिना देह क्या है। मृत देह को नष्ट करने के वास्ते इतना ज्यादा खरच क्यों? मृतक के धनी होने पर कितना खरच होता होगा, यह सोचो। मृतदेह को जल्दी, आसान, स्वस्थ ढंग और कम खरच में नष्ट करना चाहिये।" मुझे याद आता है एक बार जब हम दिल्ली में रिंग रोड से गुजर रहे थे तो मैंने उनसे कहा था जब मैं मर जाऊँ आप मुझे बिजली के शमशान में ले जाइयेगा। इस पर वह हँसे, "देखो कौन किसको लाता है। मैं तुमसे बड़ा हूँ।"
वाराणसी से पार्टी विधायकों और कार्यकर्ताओं की सभा में भाषण देने लखनउ गये। अब वह गैर कांग्रेस सरकारों, कम से कम उत्तर प्रदेश की सरकार से उम्मीद हारने लगे थे। मार्च में जब उन्होंने चरणसिंह के संयुक्त विधायक दल में सामिल होने की बात सुनी तो उनके उत्साह और खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और अपने स्वाभाविक अतिरेक में उन्होंने चरणसिंह की तारीफ के पुल बाँध दिये। उन्होंने उम्मीद की थी कि चरणसिंह जैसा पिछड़े वर्ग का आदमी जमीन पर लगाना हटाने, हिन्दी में कामकाज शुरु करने आदि जैसे कार्यक्रमों से राज्य में तुरंत बदलाव की ताकतों को बढ़ावा देगा। पर उन्हें अपनी पार्टी के विधायकों से कम निराशा नहीं थी। मेरे ख्याल में उनसे वह ज्यादा ही निराश थे। उस सभा में उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि वह अपनी पार्टी के विधायकों से क्या उम्मीद करते हैं, क्या कदम पार्टी के विधायक उठायें। उन्होंने कहा था कि आगे देखूँ कानून के मामले में वे कांग्रेस के साथ भी मत देने तक जा सकते हैं। अगर उदाहरण के लिए कांग्रेस लगान का खात्मा करने के लिए संशोधन रखे तो उसका सर्मथन करने में कोई हिचक या क्लेश नहीं होना चाहिये।
एक बार उन्होंने कहा था कि वह अच्छे काम के लिए शैतान के साथ भी मत देंगे। हालाँकि शैतान का इरादा उसके स्वाभाव के कारण शैतानियत का ही होगा। वह काम और नतीजे को महत्व देते थे। वह कभी इरादे ढूँढ़ निकालने की कोशिश न करते। काम और काम ही उनकी राजनीति की आधारशिला था।
हम दिल्ली लौट आये, अब काफी गरमी पड़ने लगी थी। वह बहुत मेहनत कर रहे थे और उनकी तबियत भी अच्छी नहीं रहती थी, पर भाषण देना, लिखना और असंख्य मुलाकातियों से मिलना और बातचीत करना जारी था। मेरे जानते वही अकेले नेता थे जो एक साथ ही जीवन का आन्नद भी लेते रहते थे - हँसते हुए, चिढ़ाते हुए, तरह तरह के काम करते हुए, ऐसे काम जो राजनीति के दायरे में नहीं आते।
गरमियों के उन दिनों में मैंने बहुत हिचकिचाते हुए कहा कि मैं एक रूम कूलर लेना चाहती हूँ। "माफ करो, मेरे कमरे के लिए नहीं। यह सुख सुविधाएँ मेरे लिए नहीं हैं हालाँकि इससे मुझे काम करने में ज्यादा मदद मिलेगी। नहीं, कतई नहीं।"
इससे काफी पहले जब वह पहली बार संसद के सदस्य चुने गये तो उनके कुछ दोस्तों ने उन्हें मोटर खरीद देने की बात रही। मोटर का आर्डर भी दे दिया गया। मैं मोटर देख कर आई और उन्हें बताया। उस बार वह नाराज नहीं हुए थे। उन्होंने मुझे बिठाया और मोटर के खर्च का अन्दाज लगाने लगे औेर फ़िर विजयोल्लास में कहा "टेक्सी सस्ती रहेगी"। उन्होंने इस संभावना की भी गवेषणा की कि ऐसे ६-७ दोस्त हो सकते हैं जो उन्हें एक महीने में चार बार मोटर देंगे, इस तरह २८ दिन मोटर वाले हो जायेंगे। पर वह एक दोस्त ही जुटा पाये और उसकी मोटर भी नियमित नहीं आ पायी। पैसों की बरबादी के बारे में वह बहुत ज्यादा आगाह रहते थे। जनता के बीच जो कहते उसी को हमेशा सबसे पहले अपने उपर लागू करते।
जुलाई के आरम्भ में इंजेक्शनों का कोर्स खत्म करने के बाद अखिल भारतीय चिकित्सा संस्थान में सर्जन ने उनकी फ़िर जाँच की। इस बार सर्जन की राय थी कि आपरेशन के सिवाय कोई चारा नहीं। यही नहीं, जितना जल्दी किया जाये उतना अच्छा। नहीं तो जिस तरह की ज़िन्दगी वह जीते हैं, जिसने देहातों में जाना होता है, उसमें नाना प्रकार की पेचदगियाँ पैदा हो सकती हैं, और काफ़ी पीड़ा और असुविधा हो सकती है। आपरेशन का ख्याल उन्हें खराब लगता था, वह सिद्धांततः इसके खिलाफ़ थे। आपरेशन के खयाल से ही उन्हें अरुचि थी। मैंने उनसे पूछा क्या वह छुरे से डरते हैं? यह सवाल मैंने ऐसे आदमी से किया था जिसे ज़िन्दगी में किसी तरह के डर का अहसास नहीं था. उन्होंने कहा कि "ऐसा नहीं है"।
वह चुप हो गये तो मैंने कहा क्या इसका हिंसा अहिँसा से तालुक है। उनका मुख स्नेह की अपूर्व मुस्कान में खिल गया। "तुमने बात ठीक पकड़ी। यह चीरने फाड़ने की बात मुझे पसन्द नहीं आती। मुझे समझ में नहीं आता तुम लोग किस तरह मुर्गी, मछली और जीवित जानवर खाते हो और फ़िर चटखारे भी भरते हो।" उन्हें पेड़ों की शाखाएँ काटना भी कभी नहीं भाया। बहुत दफ़े उन्होंने मुझसे शिकायत की कि माली डालें काट देता है। मैं उनसे कहा करती कि यह पेड़ों के भले के वास्ते है, काँट छाँट से वे बढ़ते हैं। "अगर तुम्हारे हाथ पाँव काट दिये जायें तो तुम्हें कैसा लगे।" आप की यह तुलना सही नहीं है, मैं कहती। जीवित प्राणी के प्रति किसी भी तरह की निर्ममता उनके स्वाभाव के प्रतिकूल थी। वही अकेले आदमी थे, जिन्होंने हिँसा को ले कर जान और माल के बीच फरक किया। माल इस देश में ज़्याद रक्षणीय रहा है, वह व्यंग में कहते, मनुष्य तो मक्खियों की तरह है सो उसके मरने की किसी को क्यों परवाह हो।
एक रात शायद अगस्त का महीना था, उन्होंने अपना हाथ मेरे आगे फैला दिया और कहा हाथ देखो। मैंने हाथ देखते हुए कहा, "आप प्रधान मंत्री नहीं बनोगे"। "तुम क्या सोचती हो मैं प्रधानमंत्रित्व की कामना करता हूँ, बस यह बताओ कि मैं क्या देश का भला, सही मायने में भला कर सकता हूँ। क्या लोग मेरी बात सुनेंगे और काम करेंगे?" इसके बाद फ़िर, "क्या जो होगा वह हिँसक होगा?", मैंने कहा, "कुछ न कुछ हो कर रहेगा। आप का आयुष्य दीर्घ है और सत्तर बरस तक जीयेंगे।" "केवल सत्तर, कुछ और बरस तो दो।"
विरोधी दलों और अपनी पार्टी पर से विश्वास उठने पर भी जनता में उनका विश्वास कभी नहीं डिगा। किस तरह जनता को, जो दो हज़ार साल से भी अधिक पशुओं जैसा जीवन जीती आ रही है, उठाया जाये, जगाया जाये। किस तरह जाति व्यवस्था का घृण्य प्रभाव दूर किया जाये. "तुम इतिहास की कैसी विद्यार्थी हो। क्या तुम्हें हमारे इतिहास की इस सचाई की पड़ताल करने की इच्छा नहीं होती। क्या हमारे प्रसिद्ध इतिहासकारों में एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो हमारे इतिहास के बारे में वास्तविक अनुसंधान करे। एक नहीं तो इतिहासकारों की टीम ही सही। क्यों विदेशी शासन के आगे हमने बार बार आत्मसमर्पण किया। विश्व के इतिहास में इस तरह की कोई मिसाल नहीं।"
उन दिनों वह पूर्व जर्मनी के हाले स्थित मारटिन लूथर विश्वविद्यालय से मारटिन लूथर की ४५०वीं बरसी पर पूर्व जर्मनी आने का निमंत्रण पा कर उत्साहित थे। उनका उत्साह बढ़ रहा था। निमंत्रण पत्र अगस्त में उस दिन आया जिस दिन वह दिल्ली से कहीं दौरे पर जा रहे थे। "तुम क्या समझती हो, मुझे क्यों निमत्रित किया गया है। क्यों हमेशा निमंत्रण पूर्व जर्मनी से आता है, पश्चिमी जर्मनी से नहीं। तुम्हें पता है छात्रावस्था में मैंने एक बार हाले की एक सभा में भाषण दिया था. पौन घँटे के भाषण में २० बार तालियाँ बजी थीं। यूरोप के लोग तालियाँ बजाना जानते हैं। हम एशियाइयों की तरह मरी मरी ताली नहीं बजाते। अरे हमें तो ताली बजाना भी नहीं आता।" निमंत्रण से उनकी तबियत रंग पकड़ रही थी। "पूर्वी जर्मन साम्यवादियों से प्रोटेस्टैंट वाद पर बात करने में गजब का मजा आयेगा। आखिर मुझसे बड़ा प्रोटेस्टैंट है कौन। यहाँ पर मैं उस दिन कृष्ण पर बोला, वहाँ मैं लूथर पर बोलूँगा।"
दौरे से लौटने पर उन्होंने सबसे पहले पूछा कोई और उत्तर आया? "शायद वह नहीं चाहते कि मैं बोलूँ। मैं निमंत्रित अतिथि की हैसियत से वहाँ नहीं जाना चाहता। मैं बहस में भाग लेने ही जाउँगा।"
पटना, दंगाग्रस्त रांची और अन्य स्थानों का दौरा करने के बाद वह लौटे थे। वह जयप्रकाश से भी मिले थे। मैंने पूछा जे.पी. से क्या बातचीत हुई? "इस तरह की बातचीतों से कुछ होता है, हमारे देश में कुछ भी होता है क्या?" पर आखिर आप उनके साथ कई घँटे थे, आप दोनो ने एक दूसरे के चेहरे को ही तो नहीं देखा होगा और केवल मौसम के बारे में ही बातचीत नहीं की होगी। "हाँ हमने बातचीत की। जयप्रकाश ने एक लम्बा कार्यक्रम बनाया है जिसे बिहार सरकार को अमल में लाना चाहिये।" मैंने उनसे कहा बिखरे कार्यक्रम के बजाय सरकार को एक एक मामला, जैसे लगान का, लेना चाहिये और उस पर पूरी दृढ़ता से काम करना चाहिये। इसके बाद उन्होंने आन्दोलन की बात तिरस्कार व अवहेलनात्मक ढंग से कही, मुझे इस पर गुस्सा आया और मैंने उन्हें कहा, "देखो जयप्रकाश, मुझे भी आन्दोलन की खातिर आन्दोलन करना पसन्द नहीं और न ही जेल जाना पर ऐसी मजबूरियाँ होती हैं कि आन्दोलन जरूरी हो जाता है। उनके सिवाय कोई दूसरा चारा नहीं रहता। तुम कभी जेल नहीं गये हो", इस पर उन्होंने मेरी ओर आँखें चढ़ा कर देखा तो मैंने जोड़ा, "आजादी के बाद"! जयप्रकाश से यही मेरी बातचीत हुई। इस निकम्मे देश में कुछ भी नहीं होता।"
उन दिनों उनसे मिलने तरह तरह के बहुत से व्यक्ति, कांग्रेसी, साम्यवादी, स्वतंत्र, सब आया करते थे। एक बार वह लोकसभा के अध्यक्ष श्री संजीव रेड्डी के यहाँ रात दावत पर गये थे. दावत में वही अकेले मेहमान थे. मैंने दावत के बारे में और क्या बातचीत हुई, पूछा तो अनूत्साहित स्वर में उन्होंने कहा।
"एक गैर कांग्रेसी केन्द्र हो सकता था। दोनो किस्म के साम्यवादियों, जनसंघी और स्वतंत्र दल जैसे हैं, उन्हें देखते हुए मैं संजीव रेड्डी को क्या आश्वासन दे सकता था था कि मैं एक गैर कांग्रसी मिली जुली सरकार बना सकूँगा।"
अब उन्हें आपरेशन की जल्दी पड़ी थी क्योंकि डाक्टरों की यही सलाह थी। एक बार किसी बात को मान लेने पर उन्हें देर बरदाश्त नहीं होती थी। वह मुझे बार बार आपरेशन की तारीख तय करने को कहते। उनकी तबियत ठीक नहीं थी और वह जल्द चंगा होना चाहते थे, उन्हें बहुत कुछ करना था, विदेश जाना था और न जाने क्या क्या करना था। इस बात पर काफी बहस होती रही कि आपरेशन कहाँ हो और उसे कौन करे। जब वह कलकत्ता जा रहे थे तब मैंने कहा कि आप वहाँ किसी सरजन से जाँच कराना। "तुम जानती हो यह डाक्टर और सरजन कैसे एक दूसरे की बात को काटते हैं, और अपनी काटवाली बातों से आदमी को घपले में डाल देते हैं।" उनकी राय थी कि आपरेशन दिल्ली में हो या लखनऊ में। लखनऊ पर उनका मन ज्यादा था, क्योंकि उनका ख्याल था कि वहाँ आराम ज्यादा होगा। आखिर में उन्होंने विलिंगडन अस्पताल चुना। क्रूर नियति ही की बात है कि उन्हें विलिन्घडन अस्पताल के सुपरिन्टेडेंट ब्रिगेडियर लाल पर जबरदस्त भरोसा था। इससे पहले उन्होंने ब्रिगेडियर लाल को चाय पर बुलाया था और मुझे चेतावनी दी थी मैं उनसे उनके स्वास्थ्य की बात न करूँ। वह लाल को बहुत बड़ा डाक्टर मानते थे क्योंकि लाल ने एक बार हमारे एक कार्यकर्ता की जान बचायी थी। डा. साहब का स्वभाव अत्यंत उदार था और तारीफ़ व निन्दा दोनो में ही वह कंजूस न थे।
२८ सितम्बर को वह अस्पताल में दाखिल हुए, ३० को आपरेशन हुआ और ११ अक्टूबर को मध्य रात्री के थोड़ी देर बाद मृत्यू। वह हमेशा सफाई, सुथराई के कायल थे। अस्पताल आने पर उन्होंने बिस्तर की चादर देखी कि वह साफ़ है या नहीं। उन्होंने कहा कि मैं घर से तौलिये ले आऊँ पर हमें लगा कि घर के तौलिये स्वच्छता की दृष्टि से निर्दोष और निरापद नहीं रहेंगे, शायद उनसे छूत लगे। पर हुआ यह कि उनकी मृत्यू एक ऐसे घातक दोष से हुई जो ओज़ारों को निर्दोष करने की कमी के कारण छूत से पैदा हुआ। आपरेशन के मौके पर उन्होंने आपरेशन के बारे में फ़िर से पूछताछ की कि वह किस तरह होगा और कैसे होगा। जीवन में हर बात में उनका आग्रह तह तक जाने का था। इसके बाद उन्होंने कहा, "हंसी की बात है कि इस उमर में भी मुझे पता नहीं मेरा खून किस वर्ग का है।" जब मैंने कहा कि यह जानना कोई जरूरी नहीं, तो उन्होंने झिड़कते हुए कहा, "तुम्हारा पक्का एशियाई दिमाग है। हर यूरोप अमरीका वाला अपने रक्त का वर्ग जानता है।" मुझे इस पर एक घटना याद हो आयी। एक बार हमारे रसोईये ने माली को यह कह कर रसोई में नहीं घुसने दिया कि वह छोटी जात का है। जब उन्होंने यह बात सुनी तो रसोईये को बुलाया और इनसाइक्लोपीडिया की जिल्द निकाली और चित्रों के माध्यम से बड़े धीरज से रक्त रहस्य बताया - रक्त जाति से निर्धारित नहीं होता वरन उसके अंतर्निहित तत्वों से. इसके बाद रसोई बनाने वाले इस लड़के ने फिर कभी जाति की बात नहीं उठायी।
अपनी सक्षिप्त बीमारी के दौरान जब वह मौत से जूझ रहे थे मैंने देखा कि उनके दिमाग पर दो बोझ थे। इनमें अव्वल देश की हालत थी। बार बार भयानक पीड़ा और कराह में वह लगान के खात्मे, हिन्दु मुसलिम एकता, गरीब किसानों की दुर्दशा, भाषा तथा अन्य मामलों के बारे में बोलने लगते। मेरे खयाल में वह कभी भी पूरी तरह बड़बड़ाने या संज्ञाशून्य होने की स्थिति में नहीं थे। अपने आसपास के प्रति वह जागरूक दीखते थे। हममें से कुछ को उन्होंने हमेशा पहचाना - स्पर्श से या आवाज़ सुन कर या आँखें खोल कर। एक बार उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, "बताओ, तुम मुझसे कभी झूठ नहीं बोलोगी - क्या हमारे देश में कोई बड़ी चीज़ हो रही है?" "यह पहला रिहर्सल है" - इसके बाद वह भारत पाक महासंघ की बात कहने लगे। हालांकि जब वे अस्पताल में दाखिल हुए तब उनको आसन्न मृत्यु का कोई आभास नहीं था पर शायद जब उनकी हालत खतरनाक हो गयी तो उन्हें लगा कि समय बीता जा रहा है। लिहाजा देश के भवितव्य को ले कर उनकी चिंता व क्लेश मुखर हो उठा। दूसरी बात यह दीख पड़ी कि उन्हें ऐसा लगा कि उनके शरीर में कहीं कोई भारी गड़बड़ हो गयी है। इतने ज्यादा डाक्टरों का जमा होना उन्हें जताता रहा कि वह कितने ज्यादा बीमार हैं। बार बार वह इतने ज्यादा डाक्टरों की मौजूदगी की चर्चा करते रहे, "इतने डाक्टरों का होना अच्छा नहीं"।
वह इतनी पीड़ा पा रहे थे और जबरदस्त बेचैनी थी, पर इसके बावजूद कभी पीड़ा में चिल्लाते हुए मैंने उन्हें नहीं देखा। बीमारी के दौरान मैं लगभग सारे समय उनके साथ थी। हमें इस बात का कभी पता नहीं लगेगा कि वह किस तरह और क्यों मरे? केवल मृत्यु के वक्त उनके चेहरे पर शांति विराज रही थी हालांकि भौंहें तनी थीं. उनके प्रिय चेहरे की यह परीचित भृकुटि थी।
क्या यह महज संयोग है कि जब वह बीमार पड़े थे और मृत्यु से संघर्ष कर रहे थे तभी गैरकांग्रेसवाद पर जबरदस्त प्रहार शुरु हुआ? कौन जानता है? गैरकांग्रेसवाद के जनक की मृत्यु के बाद एक एक कर गैरकांग्रेसी राज्य ढहने लगे। दिल्ली में मार्च अप्रैल के दौरान जब गैरकांग्रेसी सरकारें बन रहीं थीं एक चुटकला चालू था. इस चुटकले पर वह बाग बाग हो उठते - अमृतसर से हावड़ा तक गैरकांग्रेस राज्यों का बोलबाला है, बीच में कहीं कांग्रेसी इलाका नहीं आता। अब यह बात नहीं रही।
इस साल जाड़ा बड़ा सख्त था और बेहद लम्बा चला। दिल्ली की सरदी उन्हें बरदाश्त नहीं होती थी। अक्सर मुझे कहा करते "जाड़े में मुझे दिल्ली मत रहने दिया करो।" आग के आगे बैठने में उन्हें आनन्द आता। बिजली का हीटर भी रहता था, पर अपनी वैज्ञानिक भंगिमा में वह बतलाते कि किस प्रकार जलता हुआ काठ सारे घर को गरमा देता है। उन्हें उष्णता प्यारी थी, शायद भारतीय राजनीति में उन जितना कोई स्नेही नहीं था। अब डाक्टर साहब नहीं रह गये, अपने साथ वह सारा स्नेह और ममत्व ले गये हैं, और मेरी दुनिया निस्तेज, उदास और खोखली रह गयी है।
***
टिप्पणी: मुझे रमा मित्र की कोई तस्वीर नहीं मिली. नीचे वाली तस्वीर १९४९-५० की है, इसमें नीचे मेरी माँ जो उस समय कमला दीवान होती थीं, वह बैठी हैं. उनके पीछे शायद रमा जी हैं, पर पक्का नहीं कह सकता. बीच में खड़े डा. लोहिया भी हैं.






























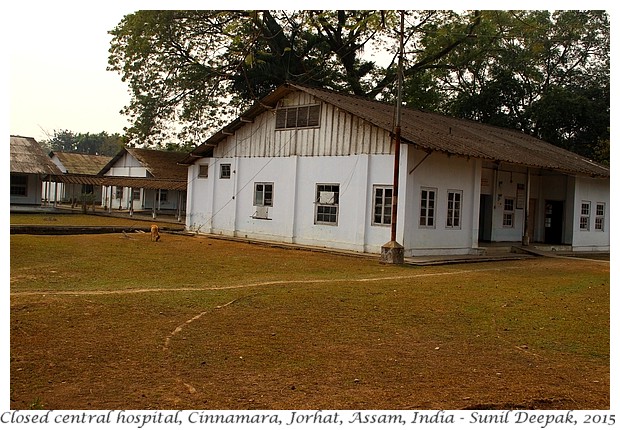






.JPG)